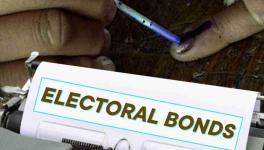हिंदू राष्ट्रवाद बनाम बांग्ला राष्ट्रवादः किसका खेला देखेगी विधानसभा

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दीदी ममता बनर्जी की रोचक आक्रामक और लच्छेदार भाषा में युगलबंदी चल रही है। न ही वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां विधानसभा में जीत के बाद भाजपा के पास एक और राज्य आ जाएगा और उसकी राज्यसभा में सीटें बढ़ जाएंगी। वह एक हद तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तय होगा कि देश में एक पार्टी का लोकतंत्र रहेगा या बहुदलीय लोकतंत्र। इससे भी ज्यादा वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक दक्षता, क्रांतिकारिता, राजनीतिक पराभव और आर्थिक विपन्नता में जीने वाला पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र से निकले हिंदू राष्ट्रवाद के उस वर्चस्व को स्वीकार करेगा जो उसे पराजित करने में उन्नीसवीं सदी से लगा हुआ है। यह लड़ाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उस क्षेत्रीय उप-राष्ट्रीयता के बीच है जो भारत के विचार की लड़ाई है और जिसे पश्चिम बंगाल से संबल मिलता रहा है।
एक ओर ममता बनर्जी कह रही हैं कि माथे पर तिलक लगाकर और मुंह में पान दबाकर लोग आ रहे हैं बंगाल पर कब्जा करने। बहिरागत यानी बाहरी लोग हैं वे। उन्हें हम यहां काबिज नहीं होने देंगे। बंगाल के लोगों को बहिरागत नहीं चाहिए अपनी बेटी यानी निजेर मे चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी का प्रचार गीत भी बनाया है----बैरे थेके बारगी आशे/ नियम कोरे प्रति मासे/ अमिया आछी तुमिया रोबे/ बंधु एबार खेला होबे/ खेला खेला खेला होबे। यानी बाहर के गुंडे हर महीने नियम से आते हैं। हमको तुमको तो यहीं रहना है। भाइयों इस बार का चुनाव का खेल मजेदार है।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने पहले अयोध्या आंदोलन से निकले जय श्रीराम के नारे के बहाने हिंदी इलाके की तर्ज पर हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया और जब उससे पूरी बात नहीं बनी तो दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा की निर्बाध छूट का एजेंडा ले आए हैं। लेकिन जीत के लिए इतनी धार्मिक और राष्ट्रवादी भावना काफी नहीं दिख रही है इसलिए एक ओर मतुआ बिरादरी को पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साधने की कोशिश चल रही है तो दूसरी ओर वंदे मातरम और जन गण मन के माध्यम से बंगाल की समावेशिता और अखिल भारतीयता का उदाहरण दिया जा रहा है। ध्यान देने की बात है कि बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका के दो दिवसीय दौरे में तीस्ता जल विवाद समेत कोई दोतरफा मामला एजंडे पर नहीं है। मोदी वहां सतखिरा के जोगेश्वरी काली मंदिर जाएंगे और ओरकंडी में स्थित मतुआ समुदाय के मंदिर जाएंगे। उनके साथ मतुआ आंदोलन के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर के वंशज व भाजपा के सांसद शांतनु ठाकुर और उनके परिवार के अन्य लोग भी जा रहे हैं। इससे वे एक ओर पश्चिम बंगाल की हिंदू भावनाओं को साध रहे हैं तो दूसरी ओर 30 से 40 चुनाव क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाली मतुआ बिरादरी के वोटों को भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक राज्य के चुनाव को ध्यान में रखकर किसी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाने वाला संभवतः यह विचित्र विदेश दौरा होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल का भद्रलोक यानी मध्यवर्ग बंगाली श्रेष्ठता के एक कल्पना लोक में जीता है। वह भले अपने चरित्र आचरण में व्यावहारिक स्थितियों के कारण पतित भी हो जाए लेकिन आदर्श नायकों की महान परंपरा को अपने सीने से लगाए रखता है। उन्नीसवीं सदी का नवजागरण और बीसवीं सदी का क्रांतिकारी आंदोलन उसे भुलाए नहीं भूलता। राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, रवींद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दिरोजियो, लार्ड हेयर, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु जैसे महापुरुषों के विचार और जीवन के हर तरह के संकट में उसको संबल देते रहते हैं। वह रवींद्र संगीत सुनता है, सत्यजित राय, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक की फिल्में देखता है और चारू मजुमदार, कानू सन्याल के संघर्ष और महाश्वेता देवी के साहित्य के बहाने नक्सलवाद की स्मृतियों को भी अपने जेहन में लिए रहता है। इसीलिए विदिया शंकर नायपाल जैसे दक्षिणपंथी लेखक ने भी कहा था कि वह आजाद भारत की सबसे श्रेष्ठ युवा पीढ़ी थी जो नक्सल आंदोलन में मार दी गई। बंगाल के भीतर वामपंथी दलों के शासन की 34 सालों की स्मृतियां हैं जिसके कारण शहर भले बहुत नहीं चमके लेकिन गांवों में एक प्रकार की समता और समृद्धि आई और राज्य को एक राजनीतिक स्थिरता मिली। भले ही औद्योगिक विकास की गति संतोषजनक नहीं रही लेकिन राज्य की अपनी प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी रही। वह तमाम विपन्नताओं और दुखों को दुर्गापूजा के उत्सव और पहले फुटबाल फिर क्रिकेट के खेल महोत्सव में भुला देता है। लेकिन उदारीकरण की चुनौती ने उसे हिला दिया।
पश्चिम बंगाल अपने कल्पना और भावना लोक में किस कदर डूबा रहता है इसकी झलक दुर्गापूजा पंडालों की सजावट से ही नहीं मिलती बल्कि नवरात्रि के मौके पर आने वाले शारदीय विशेषांकों से भी मिलती है। बांग्ला और हिंदी के विशेषज्ञ प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे के अनुसार इस समय करीब तीन सौ उपन्यास हर साल प्रकाशित होते हैं। भारत के किसी सांस्कृतिक और जातीय समाज में ऐसा रचनात्मक विस्फोट शायद ही होता हो। बंगाल की इसी रचनात्मक, भावुक और दुस्साहसी व आलसी समाज में एक तरह का श्रेष्ठता भाव है, उस श्रेष्ठता के कारण छल कपट दांव पेच भी है। लेकिन जब भी अमर्त्य सेन या अभिजीत बनर्जी को नोबेल मिलता है तो फिर एक बार वह समाज खुशी और बौद्धिक श्रेष्ठता के भाव से झूम उठता है। एक बात गौर करने की है कि बंगाल के इस सांस्कृतिक श्रेष्ठता भाव से पूर्वोत्तर के सभी जातीय समाज बेचैन भी रहते हैं। असम आंदोलन के पीछे एक कारण उन पर बांग्ला संस्कृति का बढ़ता प्रभाव भी था। त्रिपुरा के उग्रवादी संगठनों के भीतर एक भावना यह भी है कि बंगाली अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता से उन्हें दबाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन समाजों में बंगला के सांस्कृतिक और बौद्धिक नायकों के जवाब में अपने नायक गढ़ने की होड़ भी मची रहती है।
यूरोप के संपर्क में आने और अंग्रेजी ज्ञान जल्दी पाने के कारण बंगाल की सोचने समझने और व्याख्या करने की क्षमता जल्दी विकसित हुई और उसने देश का नेतृत्व संभालने का प्रयास भी सबसे पहले किया। यह टकराव हम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ आरंभिक दिनों में देख सकते हैं। चूंकि कांग्रेस का गठन बंगाल में हुआ था और उसकी बैठकें भी वहीं होती थीं इसलिए बंगाली और महाराष्ट्रीय लोगों के बीच एक होड़ भी रहती थी। कई बार टकराव भी होता था। मराठों के भीतर एक भावना थी कि अंग्रेजों के काबिज होने से पहले भारत के बड़े हिस्से पर उनका राज था तो बंगालियों के भीतर भारत की राजधानी कलकत्ता में होने का घमंड था।
यहां एक बात ध्यान देने की है कि बंगाल के आरंभिक क्रांतिकारियों में धार्मिक भावना काफी प्रबल थी। 1902 में कलकत्ता में गठित अनुशीलन समिति का वर्णन करते हुए तारिणी शंकर चटर्जी लिखते हैं, `` क्रांतिकारी कार्य के लिए जो इस समिति में आते थे उन्हें दो वर्गो में बांटा जाता था। धर्म में जिनकी आस्था थी उनको एक वर्ग और धर्म विशेष में जिनकी आस्था नहीं थी परंतु क्रांतिकारी कार्यों में जिनकी आस्था थी उनको दूसरे वर्ग में रखा जाता था। .....धर्म के प्रति जिनकी आस्था थी वे मानिक तल्ला बागान में रहते थे, वे ही लड़के प्रथम कोटि के क्रांतिकारी समझे जाते थे। उन दिनों बंगाल के क्रांतिकारियों का बहुमत बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित था। अनुशीलन समिति के सदस्यों को हिंदू ग्रंथों खासकर गीता को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता था।’’ यह बातें भगत सिंह के साथी और क्रांतिकारी शिव वर्मा ने अपने लेख `क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक इतिहास’ में दर्ज की हैं। उनका कहना है कि बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन अपने पहले चरण यानी 1897 से 1913 तक हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान था और उससे प्रेरणा लेता था। उसकी तुलना में पंजाब का गदर पार्टी का आंदोलन धर्म से ज्यादा दूर था और तर्क व अंतरराष्ट्रीय समाजवाद के विचारों से प्रभावित था। भगत सिंह के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पर गदर पार्टी के विचारों का प्रभाव था। लेकिन इस बात को तिलक भी स्वीकार करते हैं कि बंगाल की क्रांतिकारिता महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा व्यापक सरोकारों वाली थी। ऐसा वे चापेकर बंधुओं की कार्रवाई और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की कार्रवाई का विश्लेषण करते हुए कहते हैं।
दरअसल बंगाल से निकले राष्ट्रवाद और क्रांतिकारिता में बंगाल की जातीयता कभी अनुपस्थित नहीं रही। वे दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक ही रहे। यह अलग बात है कि बंगाल से निकले राष्ट्रवाद का आख्यान पूरे देश पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि पहले उसे महाराष्ट्र से निकले तिलक के राष्ट्रवादी आख्यान से प्रतिस्पर्धा करनी होती थी और फिर पंजाब के आख्यान से होड़ थी। उसके बाद मध्य भारत से महात्मा गांधी ने अहिंसा और हिंदुओं और मुसलमानों की साझी विरासत पर आधारित राष्ट्रवाद का जो आख्यान रचा वह पूरे देश पर छा गया। लेकिन हिंदू केंद्रित राष्ट्रवाद का एक विचार अगर बंकिमचंद्र ने आनंदमठ (1882) के माध्यम से प्रस्तुत किया तो लार्ड कर्जन द्वारा लिए गए बंग भंग (1905) के निर्णय ने पहले बंगाल फिर पूरे देश को झकझोर दिया। उस घटना ने बंगाल की जातीयता जिसे उपराष्ट्रीयता भी कह सकते हैं को एक पूरा आकार दिया और इसी के साथ वह भारतीय राष्ट्रवाद से भी जुड़ा।
बंगाल की जातीयता के विकास को रेखाकित करते हुए अरविंद घोष लिखते हैं, `` बंकिम और मधुसूदन दत्त ने तीन आदर्श चीजें दीं। पहली चीज उन्होंने हमें बांग्ला साहित्य दिया जिसकी तुलना यूरोप के क्लासिक साहित्य से की जा सकती है दूसरी चीज उन्होंने वह बांग्ला भाषा दी जो अब बोली नहीं रह गई बल्कि देववाणी बन गई। और तीसरी उन्होंने बांग्ला जाति यानी बंगाली नेशन दिया।’’ ध्यान देने की बात है कि अरविंद घोष ने यह टिप्पणी 1894 में इंदु प्रकाश नामक पत्र में की थी। बंगाल के महत्व और श्रेष्ठता के बारे में वे 1909 में कर्मयोगिन में लिखते हैं, `` भारत में उच्चतर चिंतन के जगत में अब तक बंगाली सर्वदा नेतृत्व करता आया है और आज भी कर रहा है। क्योंकि नए राष्ट्र के उत्थान के लिए जिन गुणों की अपरिहार्य आवश्यकता है, वे स्पष्ट रूप से उनमें है। उनके पास है भावावेग और कल्पना का ऐश्वर्य।’’
यह सही है कि भारत माता का विचार बंकिम चंद्र ने आनंद मठ के माध्यम से पेश किया तो बंगाली नेशन के सवाल को बंग भंग ने सबसे ज्यादा जागृत करने का प्रयास किया। अरविंद घोष के अखबार वंदे मातरम और उनके भाई बारीन घोष के अखबार युगांतर में यह भावना बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन बंग भंग और उसके साथ जुड़ी स्वदेशी और स्वराज की अवधारणा को जगाने में जिस किताब का बड़ा योगदान है वह है देसेर कथा। संयोग से बांग्ला में लिखी गई इस किताब के लेखक बंगाली न होकर मराठी हैं और वे तिलक के विचारों से प्रभावित हैं। उनका नाम था सखाराम गणेश देउस्कर। वे शिक्षक, इतिहासकार और फिर कलकत्ता के हितवादी अखबार के संपादक थे। जाहिर सी बात है बंगाली राष्ट्रीयता, हिंदू राष्ट्रीयता और भारतीय राष्ट्रीयता में बहुत कुछ समान है और बहुत कुछ अलग अलग भी है।
सोवियत क्रांति के बाद बंगाल के क्रांतिकारियों और अनुशीलन समिति के लोगों पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ने लगा और उनके विचारों में भावना से ज्यादा तर्क और विश्लेषण का समावेश होने लगता है। उसी के साथ वे हिंदूवाद के प्रभाव से भी मुक्त होने लगे। यह गजब का संयोग है कि 1917 में जिस साल सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति होती है उसी साल रवींद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध लेख `नेशनलिज्म इन इंडिया’ आता है। यह लेख जितना उस समय प्रासंगिक था उससे कहीं ज्यादा आज प्रासंगिक है। वह दौर मुस्लिम लीग (1906), हिंदू महासभा (1915) और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना (1925) के बीच का दौर है। रवींद्र नाथ टैगोर का वह आलेख यूरोप से आए राष्ट्रवाद के संकीर्ण और भयानक विचार की न सिर्फ पड़ताल करता है बल्कि यह भी बताता है कि भारत का राष्ट्रवाद राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। उसे राजनीतिक और आर्थिक संगठनों की दैत्याकार मशीनें बनाने की बजाय इंसानियत को जीवित रखना चाहिए। इन्हीं विचारों को वे गोरा नामक उपन्यास में विस्तार देते हैं जो एक तरह से बंकिम के आनंदमठ का प्रति आख्यान बन जाता है।
अपने राष्ट्रवाद नामक प्रसिद्ध लेख में रवींद्र नाथ टैगोर कहते हैं, `` राष्ट्र का विचार, मानव द्वारा आविष्कृत, बेहोशी की सबसे शक्तिशाली दवा है। इसके धुएं के असर से पूरा देश नैतिक विकृति के प्रति बिना सचेत हुए स्वार्थ सिद्धि के सांघातिक कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से लागू कर सकता है। वस्तुतः वह खतरनाक ढंग से बदला लेने के बारे में भी सोच सकता है...। राष्ट्रों का यूरोपीय युद्ध प्रतिशोध का युद्ध है। ..............अब समय आ गया है कि अतिक्रमित विश्व की खातिर यूरोप निजी तौर पर राष्ट्र नामक बेतुकी चीज को पूरी तरह समझे।................राष्ट्र विकलांग मानवता पर लंबे समय से फलता फूलता रहा है। ईश्वर की श्रेष्ठ कृति मानव, युद्ध व पैसा बनाने वाली कठपुतलियों की तरह इसी राष्ट्रीय कारखाने से बड़ी तादाद में निकलता रहा है।’’
पश्चिम बंगाल में 34 साल के वामपंथी शासन का सबसे बड़ा योगदान यही रहा है कि उसने विभाजन की भयानक त्रासदी और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से निकले और तमाम तरह की अस्मिताओं में विभाजित बंगाली समाज को बिना किसी श्रेष्ठता का भाव दिलाए स्थिरता और सक्रियता प्रदान की। उसने हिंदी प्रदेशों की तरह न तो सुरक्षा गार्डों और चमचों से घिरे भ्रष्ट नेताओं की फौज पैदा की और न ही निर्लज्ज जातिवाद का माहौल दिया। उसने बंगाली राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद के बीच एक संतुलन कायम कर रखा था और किसी का वह नग्न रूप नहीं प्रदर्शित होने दिया जो आज हो रहा है। यह सही है कि उस शासन के समय समाज की अपनी पीड़ाएं थीं, अभाव था और विपन्नताएं थीं लेकिन दैन्य और अभद्रता नहीं थी। वामपंथी शासन ने भारतीय लोकतंत्र को नया आयाम दिया। उसे बौद्धिकता दी और विमर्श की नई ऊंचाई दी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और घरेलू अंतर्विरोधों के कारण उसका पतन होना ही था। पर अब वह पतन भारतीय लोकतंत्र पर बहुत भारी पड़ रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अगर अस्मिता के बहाने बंगाल की संकीर्णता और क्षेत्रीयता को उभार रही है तो नरेंद्र मोदी की भाजपा नागपुर से निकले ‘हिंदी, हिंदू हिंदुस्थान’ वाले मुस्लिम विरोध पर आधारित राष्ट्रवाद से उसे ध्वस्त करके विजय पाने की कोशिश कर रही है। खेला होबे, पीसी जाओ और पोरिवर्तन होबे की इस खींचतान में बंगाल की श्रेष्ठ परंपरा घायल हो रही है। देखना है कि बंगाल की जनता किसी साहसिक निर्णय से अपने को बचा पाती है या चुनावी अम्फान में फंस कर बर्बाद होती है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।