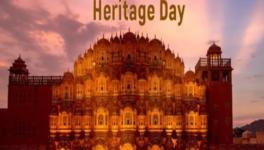पंजाब में राजनीतिक दलदल में जाने से पहले किसानों को सावधानी बरतनी चाहिए

मैं पिछले कुछ वक़्त से फेसबुक पर बहुत सक्रिय नहीं हूं। सिर्फ कुछ अच्छे लेख/खबरों या कुछ पुरानी यादों को साझ कर रहा हूं या कुछ दोस्तों को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहा हूं। इसकी वजह एक पांडुलिपि है, जिसे पूरा करने की अंतिम तारीख़ काफी पहले निकल चुकी है। इसलिए मैं अनुशासन में रहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वक़्त की तमाम कमी के बावजूद अपने दोस्तों और अपने जैसा सोचने वालों के साथ एक मुद्दे पर विचार साझा करता रहता हूं, जो इस दौर में बेहद जरूरी है। यह मुद्दा पंजाब के आने वाले चुनावों में किसानों की भागीदारी का है। यह दूसरे राज्यों में भी ज्वलंत है, लेकिन पंजाब में यह प्राथमिकता पर है। यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, जिसके ऊपर कई लोग चिंतित हैं। यह लोग किसानों के उनके अधिकारों के संघर्ष में उनके साथ हैं। इन विचारों पर खुला विमर्श हो सकता है, इनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन गाली-गलौज या गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए यहां जगह नहीं है।
मुद्दा यह है कि क्या किसानों को इन विधानसभा चुनावों में सीधा हिस्सा लेना चाहिए? सम्युक्त किसान मोर्चा के 34 संगठनों में से 22 ने सम्युक्त समाज मोर्चा (एसएसएम) नाम से एक नया मंच बनाया है, जिसने पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसे भी वोट देने का अधिकार है, वह चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यह अधिकार सिर्फ़ सैद्धांतिक है और कागजों पर है। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव या अंग्रेजों के दौर में हुए चुनावों के बाद भारत में जैसी संसदीय व्यवस्था विकसित हुई है, उसका तार्किक परीक्षण जरूरी है, समझा जा सके कि इस तंत्र में किसानों, कामग़ारों, कम आय वाले लोगों या वंचित तबके से आने वाले लोगों के सफल होने की कितनी जगह है।
सिर्फ़ आजाद भारत में ही नहीं, संसदीय चुनावों का कुछ हिस्सा औपनिवेशिक ताकतों द्वारा छोड़ी गई विरासत है। अंग्रेजों के दौर में केंद्रीय परिषद या राज्य परिषद जैसी संस्थाएं थीं। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आने के बाद, खासतौर पर 1937 में पूरे भारत में चुनाव करवाए गए। इसके पहले भी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्राथमिक संसदीय तंत्र की नींव रखी गई थी। दिलचस्प यह रहा कि अंग्रेजों के संस्थानों की आलोचना करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी, दूसरी छोटी पार्टियां और सरकार समर्थक पार्टियों या व्यक्तियों ने इन संस्थानों के चुनावों में हिस्सा लिया। यहां तक कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने भी इन चुनावों में प्रत्याशियों को समर्थन दिया। 1926 में जब लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू अलग-अलग पार्टियों में चले गए और एक-दूसरे के खिलाफ़ चुनाव लड़े, तो भगत सिंह और उनके साथियों ने लाल लाजपत राय के प्रत्याशी के खिलाफ मोतीलाल नेहरू को समर्थन दिया। क्योंकि लाला लाजपत राय सांप्रदायिक मानसिकता के हो चुके थे। बाद में मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय में सुलह हो गई औऱ दोनों ही केंद्रीय परिषद का हिस्सा रहे।
लेकिन 1937 में तत्कालीन 11 राज्यों में हुए चुनाव बड़ा कदम था। भगत सिंह के पिता किसन सिंह 1938 के उपचुनाव में पंजाब प्रांत परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। वहां वे 1947 तक सदस्य रहे। आजादी के पहले होने वाले चुनावों में लोगों के छोटे वर्ग को ही मताधिकार प्राप्त था, आजादी के बाद इस वर्ग को बड़ा करने की कोशिश हुई। डॉ आंबेडकर ज़्यादातर नामित सदस्य रहे। यहां तक कि वे आजादी के पहले भी मंत्री रहे। 1937 के बड़े चुनावों में 8 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई, मुस्लिम लीग 2 में जीती, वहीं पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई, जो बड़े ज़मीदारों की पार्टी थी। छोटू राम यूनियनिस्ट पार्टी से चुनाव जीते और मंत्री बने। उन्होंने कुछ किसान समर्थित कानून पास करवाए। कॉमरेड सोहन सिंह जोश भी यूनियनिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते और प्रताप सिंह कैरों अकाली दल से चुनाव जीते। गोपी चंद भार्गव कांग्रेस नेता थे। दीवान चमन लाल (जिनका एक बार भगत सिंह ने समर्थन किया था) ट्रेड यूनियन फोरम और मनोहर लाल विश्वविद्यालय विधानसभा क्षेत्रों से जीतकर विभाजन के पहले की 175 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रहे।
तो चुनावों में हिस्सा लेने की बात सोची जा सकती थी, लेकिन निष्पक्ष स्थितियों की विवेचना करना जरूरी है।
आज़ाद भारत में 1952 में पहले लोकसभा चुनाव हुए, जहां कांग्रेस को 489 में से 364 सीटों पर जीत मिली। संयुक्त कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे भी सिर्फ़ 16 सीटें मिलीं। जबकि सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटों पर जीत दर्ज हुई। कुछ छोटी पार्टियों को मिलाकर वामपंथियों ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की। यह वह दौर था जब किसानों ने तेलंगाना के संघर्ष में जीत दर्ज की और सीपीआई के प्रत्याशी रवि रेड्डी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बने। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू से भी बड़ी जीत दर्ज की थी। शायद वह जीत भी जेल से मिली थी। लेकिन आने वाले चुनावों में वामपंथी कभी संसद में दूसरा पायदान हासिल नहीं कर सके। उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें 2004 के लोकसभा चुनाव में जीतीं।
लेकिन 1952 से 2019 के बीच संसदीय व्यवस्था ने दक्षिणपंथी नीतियों की तरफ झुकाव बना लिया था। ऐसा आपातकाल के बाद खासतौर पर हुआ। पिछले 7 सालों में यह सिर्फ़ पैसे और ताकत का खेल बनकर रह गई है, जहां फर्जी सोशल मीडिया, खरीदा गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो 24 घंटे इंसानी दिमाग को बुद्धिरहित रोबोट में बदल रहा है। यह इंसानी दिमाग गहन विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं, बल्कि उन्हें बुद्धिहीन मीडिया ने अमानवीय प्रोपगेंडा का एजेंट बनाकर रख दिया है। इस तरह की व्यवस्था में अपनी जगह खोजना मुश्किल है। वह दिन चले गए जब ए के रॉय जैसे मज़दूर नेता चुनाव जीत सकते थे, जब कॉमरेड या गांधीवादी/समाजवादी साइकिलों या अकेली जीप में प्रचार कर सकते थे, जो कुछ अमीर दोस्तों से उधार ली गई होती थीं। वह दिन चले गए जब प्रत्याशी सामने वाले प्रत्याशी पर निजी हमले नहीं करता था या उसके खिलाफ़ हज़ार झूठ नहीं बोलता था। 2014 आते-आते यह दिन पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे, जहां डॉ धर्मवीर गांधी जैसा कड़क लोकतांत्रिक प्रत्याशी भी एक पार्टी के मंच से चुनाव जीत जाता था। तब तक बीजेपी का फासीवाद शुरू नहीं हुआ था और नई-नई बनी आम आदमी पार्टी में आदर्शवाद दिखाई देता था। बिल्कुल वैसा ही जैसा आज एसएसएम में दिखाई दे रहा है। अब साफ़-सुथरे प्रत्याशियों पर कीचल उछाला जाएगा और कम से कम चुनावी अभियान के दौर में इसे साफ़ नहीं किया जाएगा। किसी को भी किसानों की मांगों, एकता और उनके कार्यक्रम पर चुनाव लड़ने के पहले यह सब बातें ध्यान में रखनी होगी। तथ्य यह है कि मौजूदा चुनावी व्यवस्था, संघर्ष के दौरान बड़ी मेहनत से हासिल हुई उनकी मजबूती को सोख लेगी, यह काफ़ी कठिन काम होगा, किसानों की एकता के चलते हारने वाले कॉरपोरेट सत्ताधारियों को एक बार फिर हंसने का मौका मिल जाएगा और किसान उनके ही बनाए हुए कॉरपोरेटवादी चुनावी तंत्र में फंस जाएंगे!
मैं पूरी सजगता से सलाह देता हूं कि सम्युक्त समाज मोर्चा को पंजाब चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन बहुमत हासिल कर सत्ता में आने के लिए नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक तौ र पर अपनी आंशिक जीत को मजबूत करने के लिए ऐसा करना चाहिए। वैसे भी उनका सत्ता में आना मुश्किल है। सभी 117 सीटों पर लड़ने के बजाए उन्हें 5 से 7 सीटों का चुनाव करना चाहिए और वहां अपने सबसे अच्छे प्रतिनिधि उतारने चाहिए, फिर पूरी ताकत से उन्हें जीतने के लिए दम लगानी चाहिए। यह बेहतर होता कि वे ऐसी सीटों का चुनाव करते जहां बीजेपी या किसानों को धोखा देने वाले बीजेपी के साथी अमरिंदर सिंह और उनके समर्थक मजबूत हैं। इस तरह उन्हें किसानों और दूसरे कामग़ार वर्ग को दबाने के लिए सबक सिखाना था। यह लोग किसी भी गैर बीजेपी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी को भी समर्थन दे सकते हैं, जो पूरी मंशा से किसानों के संघर्ष में साथ रहता। हालांकि ऐसे प्रत्याशी मिलना थोड़ा कठिन है।
लेकिन उन्हें पिछले पंजाब चुनावों से सीख लेने की जरूरत है। एक वक़्त पर किसानों का प्रतिनिधित्व कम्यूनिस्ट पार्टी या छोटे वामपंथी समूहों द्वारा किया जाता था। 1948 में पेप्सू राज्य में मुजारा आंदोलन की सफलता के बाद की बड़े किसान नेताओं ने पेप्सू विधानसभा का चुनाव जीता था। धर्मसिंह फक्कड़, जागिर सिंह जोगा जैसे कई नेता तो जेल से चुनाव जीते थे। पेप्सू के पंजाब में मिल जाने के बाद, 1962 तक सीपीआई अपने दम पर, कांग्रेस या अकाली जैसी बड़ी पार्टियों से गठबंधन किए बिना ही अच्छी संख्या में सीटें जीतती रही। 1967 में तक सीपीआई और सीपीएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन 1967 के बाद, संयुक्त मोर्चा सरकारों में सीपीआई और सीपीएम ने कांग्रेस और अकाली जैसी सत्ताधारी पार्टियों से गठबंधन करना शुरू कर दिया। 1990 के बाद सभी वामपंथी पार्टियां आपस में मिलकर भी पंजाब चुनावों में अपनी उपस्थिति महसूस नहीं करवा सकीं। इन पार्टियों में सीपीएम, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम (पासला, अब आरएमपीआई) शामिल थीं। यह लोग 6-70 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करते, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर 500 से 1000 वोट हासिल कर रहे जाते और राजनीतिक माखौल के पात्र बनते।
राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा हुआ। सीपीएम अपने पैरों पर पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों में खड़ी हो पाई और एक विश्वासपात्र जनाधार बना पाई। लेकिन यह भी सिर्फ़ संसदीय तंत्र में सत्ता में रहने के लिए। पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा या केरल में मौजूदा संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लंबे समय तक सत्ता में रहने के चलते इनकी जन संघर्ष करने की क्षमता कमज़ोर होती गई। विडंबना यह रही कि सीपीआई, फिर बाद में सीपीआई और सीपीएम का उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर और दूसरे राज्यों में जनाधार पूरी तरह खत्म हो गया। और बड़ी विडंबना यह रही कि सीपीएम ने सिर्फ़ पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा में ही चुनाव नहीं हारा, वे चुनावी खेल में तीसरे और चौथे पायदान तक खिसक गए। विधानसभाओं में उनकी मौजूदगी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। कई दूसरी वामपंथी पार्टियों की स्थिति तो और भी बुरी है, वे भारत की राजनीतिक तस्वीर से पूरी तरह खत्म हो गईं। इनमें महाराष्ट्र में लाल निशान पार्टी, बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक (मार्क्सिस्ट) जैसी कई पार्टियां शामिल हैं। ध्यान रहे कि इन सभी वामपंथी पार्टियों का जनाधार कामग़ारों और किसानों के बड़े संगठनों में था।
सीपीआई, सीपीएम, एटक, सीटू या एआईकेएस जैसे मज़दूर संगठन इन पार्टियों के सबसे बड़े संगठनकर्ता थे। लेकिन मौजूदा संसदीय तंत्र में ज़्यादा लंबे वक़्त तक रहने के चलते यह लोग अपने मूल आधार, जैसे एआईकेएस और सीटू-एटक का जनाधार गंवा बैठे। यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि मौजूदा किसान संघर्ष में जहां पूरे भारत से 400 से ज़्यादा अखिल भारतीय संगठन और सम्युक्त किसान मोर्चा के 32 संगठन शामिल हैं, उनमें सीपीआई और सीपीएम की किसान सभाएं कोई बड़ा किसान संगठन नहीं हैं। सीपीआई किसान सभा की बहुत थोड़ी ही उपस्थिति है। सीपीएम ने महाराष्ट्र और राजस्थान में स्वतंत्र संघर्ष आंदोलन कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की और एसकेएम में भी उनकी सम्मानीय उपस्थिति है। लेकिन वे बड़े किसान संगठनों में शामिल नहीं हैं। पिछले एक दशक में बने किसान संगठनों ने ही अपनी ताकत में लगातार किसानों के मुद्दे पर, चाहे स्थानीय या वृहद स्तर पर, संघर्ष कर अपनी ताकत बढ़ाई है। लेकिन सीपीआई और सीपीएम से जुड़े किसानों संगठनों को इसके लिए आभार देना होगा कि वे सम्युक्त किसान मोर्चा के साथ मजबूती से डटे रहे।
किसान आंदोलन और लंबे वक़्त तक शांतिपूर्ण ढंग से चले उनके संघर्ष और उसकी सफलता, बड़े त्याग और दुख के बाद आई है। 700 किसानों की जिंदगियां चली गईं। इन किसान आंदोलनों ने दरअसल मौजूदा कॉरपोरेट समर्थक वैश्विक पूंजीवाद में एक नया ढांचा खड़ा किया है। चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसे कई लैटिन अमेरिकी देशों में जन आंदोलनों और प्रतिरोध के नए प्रयोग हुए हैं, जिनसे उनके समाज में बेहतर कल्याणकारी राज्य संबंधी कई बदलाव आए हैं और उन्हें अमेरिकी प्रभाव से मुक्ति मिली है। दक्षिण भारत में भारतीय किसान आंदोलनों ने अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट के नियंत्रण में रहने वाली नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रतिरोध कर उदाहरण पेश किया है। उन्हें शोषणकारी तंत्र को बदलना होगा, जो उनका मिशन भी रहा है, ना कि शासकों को बदलना होगा। इन मामलों में वे भगत सिंह के विचारों का पालन कर रहे हैं, जो शोषणकारी व्यवस्था पर कहते हैं कि अगर लॉर्ड इरविन की जगह सर तेज बहादुर सप्रू या लॉर्ड री़डिंग की जगह पुरुषोत्तम दास ठक्कर को भारत का वायसराय बना दिया जाए, तो लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, अगर शोषणकारी व्यवस्था जारी रहती है, तो लोगों का शोषण जारी रहेगा। (भगत सिंह के राजनीतिक जीवन में 1921-26 के बीच लॉर्ड रीडिंग और 1926-31 के बीच लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे।) किसानों ने संघर्ष के दौरान अपनी स्थिति बिल्कुल साफ़ रखी है और अगर उन्हें लगता है कि वे सत्ताधारियों को बदलकर, यहां तक कि एसएसएम को सत्ता में लाकर, बिना शोषणकारी तंत्र बदले किसानों की जिंदगी बदल सकते हैं, तो यह सिर्फ़ भ्रम साबित होगा। दुनिया जिस तरह कॉरपोरेट पूंजीवाद के खिलाफ़ लैटिन अमेरिकी देशों में हुए प्रयोगों को उम्मीद के तौर पर देख रही है, उसी तरह उन्हें भारतीय किसानों के संघर्ष से भी उम्मीद है और उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है। अमेरिका से निकलने वाले मंथली रिव्यू जैसे जर्नल, नोआम चॉमस्की जैसे बुद्धिजीवियों को भारतीय किसानों के संघर्ष और सफलताओं में उम्मीद दिखती है। किसी भी फ़ैसले को लेने से पहले किसान संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे ना केवल भारतीय गैर-कृषिगत लोगों की बातों पर ध्यान दें, जो उनके साथ खड़े रहे, बल्कि दुनिया के लोकतांत्रिक लोगों की तरफ भी देखें, क्योंकि खुद किसान भी जानते हैं कि उनका संघर्ष सिर्फ़ एक देश तक सीमित नहीं है। यह लोग दुनिया के कॉरपोरेट निर्मित तंत्र के खिलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं और यह लोग वैश्विक प्रतिरोध आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। किसानों को दूसरे दमित भारतीय लोगों के साथ मिलकर एक वैक्लपिक शोषणरहित लोकतांत्रिक तंत्र का निर्माण करना होगा, जैसा लैटिन अमेरिकी देश कर रहे हैं।
लेकिन किसानों को अपनी आवाज़ पतित होते संसदीय संस्थानों, जैसे विधान परिषद में भी पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन उन्हें व्यवस्था को अंदर से बदलने के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए! यह लोग फासीवादियों और लोगों को दबाने वाली बीजेपी और उसके समर्थकों को अपना मुख्य विरोधी बता सकते हैं, यहां तक कि चुनावी राजनीति में भी ऐसा कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि बुरी से बुरी स्थिति में भी वे ज़मीन पर जीत सकते हैं, चुनावी लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ़ प्रतीकात्मक और सीमित प्रतिस्पर्धा से ही हो सकता है। फिर व्यवहारिक ढंग से भी देखें, तो यह लोग 5 से 7 विधानसभा सीटों पर अपनी पूरी सांगठनिक ताकत लगा सकते हैं और सभी को जिता सकते हैं। यह लोग दूसरी पार्टियों से कह सकते हैं कि वे उनके किसान प्रत्याशियों को समर्थन दे सकते हैं और उनके समर्थन में अपने प्रत्याशी हटा सकते हैं और इसे बीजेपी/समर्थक बनाम् किसानों का संघर्ष बनाकर छोड़ सकते हैं। बीजेपी का पंजाब में कोई चेहरा नहीं है। किसानों को धोखा देने वाला और सामंती अमरिंदर सिंह उनका असली चेहरा है, जिसे करारी हार देनी चाहिए।
अगर डॉक्टर दर्शन पाल या जगमोहन उप्पल या पटियाला के संघर्षरत किसान यह चुनौती स्वीकार करते हैं, तो ठीक है, नहीं तो उन्हें डॉ धर्मवीर गांधी जैसे लोकतांत्रिक व्यक्ति से ऐसा करने की अपील करनी चाहिए, जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमरिंदर की पत्नी प्रणीत कौर को हराया था। उन्हें अमरिंदर के खिलाफ़ चुनाव लड़ने के लिए राजी करना चाहिए और किसानों के समर्थन के साथ, उन्हें बीजेपी के किसान विरोधी प्रतीक के तौर पर करारी हार देनी चाहिए। उस स्थिति में बचे हुए किसान संगठन भी प्रतीकात्मक प्रत्याशियों को मदद के लिए आगे आ सकते हैं और सभी सीटों पर वे बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं और यह सत्ता हासिल करने में लगी पार्टियों से खुद को अलग दिखा सकते हैं। विधानसभा के भीतर यह लोग किसानों के सच्चे प्रतिनिधि होने का दावा कर सकते हैं। इस तरह की नैतिकता पर सभी किसान संगठन एकमत हो सकते हैं। यह लोग चुनावी अभियान में भी उदाहरण पेश कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने दिल्ली की सीमा पर अपने प्रदर्शन में अपने व्यवहार से किया। उन्हें सिर्फ़ साइकिलों और ट्रैक्टरों या पैदल चलकर ही प्रदर्शन करना चाहिए। ना कि सत्ता हासिल करने में लगी पार्टियों द्वारा कारों के बेहूदा इस्तेमाल से प्रचार करना चाहिए। अगर यह लोग ऐसा उदाहरण पेश करने में कामयाब होते हैं, तो उनके चुनावी संघर्ष पर दुनिया का ध्यान जाएगा और दुनिया के सभी लोकतांत्रिक लोग उनका समर्थन करेंगे, जैसे आंदोलन में उनके संघर्ष का किया था। तभ दुनिया में एक नई व्यवस्था की उम्मीद बनाई जा सकती है, जो कॉरपोरेट के इशारों पर चलने वाले चुनावी खेलों में नहीं खो सकेगी।
मैं अपने किसान भाईयों और बहनों और भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के रक्षकों से इन सुझावों पर ध्यान देने की अपील करता हूं। कम से कम वे इन सुझावों पर बहस तो कर ही सकते हैं!
इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
Farmers Entering Political Fray in Punjab Must Remain Cautious
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।