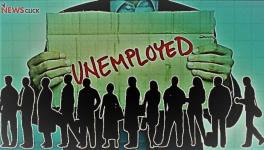विश्लेषण: अंतरिम बजट या तर्क का शीर्षासन

भाजपा सरकार मानती है कि मोदी जी जो कहें, वही सत्य है। अगर साक्ष्य दूसरी ओर इशारा करें, तो साक्ष्य ही गलत होंगे और ऐसे साक्ष्यों को दफ्न ही कर देना अच्छा। मोदी जी कहते हैं कि उनकी सरकार के पिछले दस साल जितना खुशहाल, यह देश कभी नहीं था। लेकिन, खुद सरकारी आंकड़े चूंकि उनकी इस बात को काटते हैं, तो ये आंकड़े ही गलत होने चाहिए और पूरी की पूरी सांख्यिकी की व्यवस्था को ही बदल दिया जाना चाहिए।
सच्चाई को ही नकारने का खेल
विकासशील दुनिया की बेहतरीन सांख्यिकीय प्रणालियों में से एक को, जिसे बड़ी मेहनत से तथा सावधानी से खड़ा किया गया था, नष्ट किया जा रहा है। पीसी महलनबीस ने जिस राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को स्थापित किया था, उसे उपभोक्ता खर्च का डाटा एकत्र करने के मामले में त्याग ही दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि 2017-18 का सर्वे यह दिखा रहा था कि 2011-12 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में सभी मामलों व सेवाओं के, प्रतिव्यक्ति उपभोग में, वास्तविक मूल्य के पैमाने से सत्यानाशी गिरावट आयी थी (खाद्य वस्तुओं पर वास्तविक प्रतिव्यक्ति उपभोग तो और भी पहले से गिरावट दिखा रहा था।) इसी प्रकार, जो जनगणना दशकों से, आजादी से भी पहले से चली आ रही थी, उसे भी त्याग दिया गया है कि कहीं उससे मोदी के दावों का खोखलापन उजागर नहीं हो जाए। इसी प्रकार, बेरोजगारी के वर्तमान संकट को धुंध के पीछे छुपाने की बेशर्म कोशिश में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की इस बुनियादी परिभाषा को ही त्याग दिया गया है कि बिना भुगतान के काम को, रोजगार के तौर पर नहीं गिना जाना चाहिए।
वास्तव में, बिना भुगतान के काम को ही नहीं, सारे भुगतान के कामों को भी रोजगार में नहीं गिना जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर 1930 के दशक की महामंदी के दौरान, ब्रिटेन में बहुत सारे बेरोजगारों ने सडक़ों के किनारे बैठकर बूट पालिश करना शुरू कर दिया था। जाहिर है कि ये लोग कोई मुफ्त में ग्राहकों के जूतों पर पालिश नहीं कर रहे थे। लेकिन, अगर उन्हें रोजगारशुदा लोगों में गिन लिया जाता, तो उस अभूतपूर्व संकट के दौरान भी बेरोजगारी काफी कम नजर आने लगती। इसी तरह की स्थितियों के लिए छद्म बेरोजगारी या डिसगाइस्ड अनएंप्लायमेंट की संज्ञा ईजाद की गयी थी। लेकिन, यह किस्सा तो एक ऐसे समाज का था, जो अपने संकट को गंभीरता से लेता था। दुर्भाग्य से आज के भारत में ऐसा नहीं है।
अगर मोदी की आत्मश्लाघात्मक घोषणाओं को ही सत्य मान लिया गया है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बजट, पहले से जो चल रहा था, उसी को दोहराने की कसरत भर बनकर रह गया है। और सरकार द्वारा तथा मीडिया में उसके ढिंढोरचियों द्वारा इस तथ्य को पहचाना तक नहीं जाएगा कि इससे वास्तव में बेरोजगारी तथा मेहनतकश जनता की बदहाली ही बढ़ेगी और देश में मौजूद भोंडी असमानता और बढ़ जाएगी। वे इन तथ्यों को नहीं पहचानेंगे क्योंकि ‘‘सुप्रीम लीडर’’ ने इन समस्याओं के अस्तित्व को ही नकार दिया है। वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट की पूरी की पूरी कसरत ही, इसी बात की पुष्टि करती है।
ख़ुशहाली के एलान, बदहाली की हक़ीक़त
वित्त मंत्री के भाषण को ही ले लीजिए। उन्होंने यह बेढब एलान कर मारा कि देश की औसत वास्तविक आय, 50 फीसद बढ़ गयी है। हम मान सकते हैं कि यह दावा पिछले एक दशक के दौरान यह बढ़ोतरी होने का ही है। लेकिन, यह आंकड़ा तो महज प्रतिव्यक्ति आय का है, न कि आबादी के अधिकांश हिस्से की आय का। और अकेले इसी आंकड़े को देश की आर्थिक खुशहाली के साक्ष्य के रूप में उद्धत करना, बेईमानी को ही दिखाता है।
इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच देश में और खासतौर पर ग्रामीण भारत में, पोषणगत गरीबी में बढ़ोतरी ही दर्ज हुई थी। 2200 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आहार तक पहुंच, जिसे पहले योजना आयोग द्वारा गरीबी को परिभाषित करने का पैमाना माना जाता है, से वंचित ग्रामीण आबादी का अनुपात उस दौरान 68 से बढक़र 80 फीसद पर पहुंच गया था! इसलिए, यह तो किसी भी तरह से कहा ही नहीं जा सकता है कि देश की जनता का अधिकांश हिस्सा, उक्त अवधि में पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया था। लेकिन, सवाल यह है कि उसके बाद से क्या हुआ है?
जैसा कि हम पीछे जिक्र कर आए हैं, अब हमारे पास उपभोक्ता खर्च पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का पांच साला आंकड़ा रह ही नहीं गया है। फिर भी, कुछ और आंकड़े हैं, जिनका सहारा लिया जा सकता है। और दो अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जिनका उपयोग बहुत से लोग करते रहे हैं। इनमें एक तो यही है कि पिछले पांच साल में ग्रामीण वास्तविक मजदूरी में, जिसमें कृषि कार्यों में मजदूरी तथा गैर-कृषि कार्यों में मजदूरी, दोनों ही शामिल हैं, बढ़ोतरी नकारात्मक रही है यानी गिरावट ही हुई है। और संकेत इसके हैं कि शहरी वास्तविक मजदूरी के बारे में भी यही सच है।
वास्तव में ताजातरीन पीरिओडिक लेबर फोर्स सर्वे दिखाता है कि समग्रता में पूरे देश को लें तो औसत नियमित मासिक मजदूरी में, जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाके, दोनों शामिल हैं, 2017-18 और 2022-23 के बीच, पूरे 20 फीसद गिरावट हुई है! इसलिए, 2017-18 से वास्तविक मजदूरी में गिरावट होने पर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए।
चौतरफ़ा बदहाली
दूसरा साक्ष्य यह है कि आज बेरोजगारी का संकट, आजादी के बाद अपने सबसे विकराल रूप में मौजूद है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी के आंकड़े दिखाते हैं कि कुल रोजगारों की संख्या में पिछले पांच साल में शायद ही कोई बढ़ोतरी हुई है। अब जबकि वास्तविक मजदूरी में गिरावट हो रही है और रोजगार में वृद्धि में गतिरोध बना हुआ है, मजदूरी का काम करने वाली आबादी की प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय तो वास्तव में गिरावट पर ही होगी।
और किसानों और मजदूरों की वास्तविक प्रतिव्यक्ति आमदनियां, विरोधी दिशाओं में जा रही हों यह तो हो ही नहीं सकता है। इसकी वजह यह है कि अगर किसानों की आय बढ़ रही होगी, तो इससे मजदूरी की मांग भी बढ़ जाएगी और इसका नतीजा यह होगा कि मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे होंगे और मजदूरों की वास्तविक मजदूरी भी बढ़ रही होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, समूची मेहनत-मजदूरी करने वाली आबादी की, जिसमें खेतिहर तथा गैर-खेतिहर मजदूर और किसान तथा लघु उत्पादक, सभी शामिल हैं, प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय में गिरावट दर्ज हुई है। और चूंकि देश की आबादी में प्रचंड बहुमत इन मेहनतकशों का ही है, इससे एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि पिछले पांच साल में देश की आबादी के बहुमत की जीवन-दशा बद से बदतर ही हुई है।
इसके साथ, उस तथ्य को और जोड़ लें, जिसे हम पीछे दर्ज कर आए हैं, कि राष्ट्रीय नमूना सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 और 2017-18 के बीच, आबादी के बहुमत के वास्तविक व्यय में गिरावट दर्ज हुई थी। तब हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुल मिलाकर मोदी के राज के दौरान, देश की आबादी के बहुमत की जीवन-दशा बदतर ही हुई है।
निजी निवेश क्यों नहीं बढ़ रहे?
इसी तथ्य में इस सवाल का भी जवाब छुपा है कि क्या वजह है कि भाजपा की बड़े पूंजीपतियों और खासतौर पर चुनिंदा दरबारी पूंजीपतियों की सरपरस्ती के बावजूद, मोदी राज में निजी निवेश में गतिरोध ही बना रहा है। वास्तव में सिर्फ निजी गैर-कारपोरेट निवेश में ही गतिरोध या गिरावट की स्थिति नहीं बनी रही है। उसके निवेश में गतिरोध में किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र को नोटबंदी, जीएसटी और महामारी की पृष्ठभूमि में थोपे गए दमनकारी लॉकडाउन के रूप में बहुत भारी प्रहार झेलने पड़े हैं। पर मोदी राज में तो कारपोरेट निवेशों में भी गतिरोध बना रहा है, जबकि इस दौर में कारपोरेटों के करोपरांत मुनाफे तेजी से ऊपर चढ़ते गए हैं। यह इसी सच्चाई को दिखाता है कि कारपोरेट निवेश, बाजार की वृद्धि को देखकर चलते हैं न कि उन्हें हासिल हुए मुनाफों को देखकर।
बेशक, सरकार की ओर से यह दलील दी जाएगी और वास्तव में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यही दलील दी भी है कि वह बजट-दर-बजट पूंजी खर्च बढ़ाती गयी हैं और इस तथ्य से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी पूंजीपतियों के लिए बाजारों में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इसलिए, उनकी ओर से निवेश में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन, दिक्कत यह है कि इस तरह के पूंजी खर्च से पैदा होने वाली मांग का खासा बड़ा हिस्सा, ‘रिसकर’ विदेश चला जाता है। इसलिए, घरेलू बाजार का विस्तार करने में इस तरह के खर्च का योगदान सीमित ही बना रहता है। और यही बात, सरकार की ‘आर्थिक रणनीति’ के दूसरे बाजू के बारे में भी कही जा सकती है। यह दूसरा बाजू, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से निजी पूंजीपतियों को, जिनमें दरबारी पूंजीपति भी शामिल हैं, ‘‘ढांचागत’’ क्षेत्र में निवेश करने के लिए, बड़े-बड़े ऋण दिलवाने का काम करता है। लेकिन, ऐसा कर के बैंकों पर डुबाऊ कर्जों का बोझ लादकर, निवेश का जोखिम निजी पूंजीपतियों से हटाकर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ही लाद दिया जाता है। लेकिन, अर्थव्यस्था में प्राण फूंकने के इस तरीके के साथ भी वही समस्या लगी हुई है। इसके जरिए अर्थव्यवस्था में जान नहीं डाली जा सकती है क्योंकि इससे पैदा होने वाली मांग का भी बड़ा हिस्सा तो ‘रिसकर’ देश से बाहर ही निकल जाता है।
बजट की उल्टी चाल
अगर इस बजट के हाथ मोदी द्वारा प्रवर्तित ‘‘सत्य’’ ने बांध नहीं रखे होते और यह जनता की वास्तविक दशा के लेकर रत्तीभर भी चिंता का प्रदर्शन करता, तो इसमें जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की रणनीति अपनायी गयी होती। और जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के काम के दो तरीके हो सकते थे--जनता के हक में हस्तांतरण बढ़ाना या कानून बनाकर अर्थव्यवस्था में (न्यूनतम) मजदूरी का स्तर ऊपर उठाना। इस तरह की रणनीति ने एक पंथ अनेक काज कर दिए होते। एक तो इससे सीधे-सीधे जनता को लाभ मिलता, जो अपने आप में वांछनीय है। इसके अलावा, इसने घरेलू बाजार के विस्तार के जरिए, निजी निवेश को ऊपर उठाया होता और इस तरह अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरण दिया होता।
बहरहाल, इस तरह की रणनीति से तो परहेज ही किया गया है। खाद्य, उर्वरकों तथा ईंधन पर सब्सीडी, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 4.13 लाख करोड़ रुपये थी, उसे घटाकर 2024-25 में 3.81 लाख रुपये कर दिया गया है। मनरेगा पर खर्चा 86,000 करोड़ रुपये ही बनाए रखा गया है यानी मोटे तौर पर 2023-24 के संशोधित अनुमान के ही स्तर पर। हैरानी की बात नहीं है कि इस कंजूसी की वफादार मीडिया ने यह कहकर तारीफें की हैं कि यह ‘लोकप्रियतावाद’ के मुकाबले ‘राजकोषीय समझदारी’ के चुने जाने को दिखाता है। और खुद सरकार का आख्यान यह है कि इस तरह की ‘राजकोषीय समझदारी’ से भारत, बहुत सारा विदेशी निवेश आकर्षित करने में समर्थ होगा और यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ा देगा। लेकिन, विडंबना यह है कि ‘राजकोषीय समझदारी’ के प्रति इस तरह की वचनबद्धता के बावजूद, भारत की अंतरराष्ट्रीय ‘ऋण रेटिंग’ रसातल में ही बनी हुई है। यह रेटिंग इंडोनेशिया से एक पायदान नीचे है और थाइलैंड से दो पायदान नीचे और ‘‘जंक बांड’’ या कचरा बांड स्तर से सिर्फ एक पायदान ऊपर! संक्षेप में यह कि इस तरह की ‘राजकोषीय समझदारी’ से भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी बहुत ज्यादा प्रभावित होती नजर नहीं आती है।
(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।