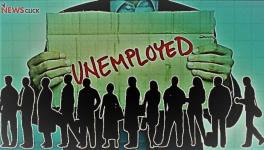पूंजीवाद, समाजवाद और अति-उत्पादन के संकट
इस लेख का उद्देश्य पूर्व में लिखे एक लेख के एक बिंदु को स्पष्ट करने (समाजवादी व्यवस्था के दौरान अति-उत्पादन संकट क्यों नहीं होता, न्यूज़क्लिक, 30 जून, 2018) का है, जिसमें पूर्ववर्ती समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में अति-उत्पादन का संकट नहीं था, जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलता रहता है।
“अति-उत्पादन संकट” का होना पूँजीवाद की प्रकृति में ही है, अर्थात माँग की तुलना में "अति-उत्पादन" से उत्पन्न होने वाला संकट। "अति-उत्पादन" का मतलब यह नहीं है कि मांग की तुलना में लगातार ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता रहे, ताकि अनबिके माल का अंबार जमा हो जाए। ऐसा सिर्फ शुरुआती दौर में थोड़े से समय के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे ही वस्तुओं का ढेर जमा होने लगता है, उत्पादन में कटौती की जानी शुरू हो जाती, और परिणामस्वरूप मंदी और बेरोज़गारी में वृद्धि होती जाती है।
संक्षेप में “अति-उत्पादन” अपने पूर्व अर्थ में है, जैसे कि यदि उत्पादन को अपनी सारी क्षमता के साथ इस्तेमाल में लाया जा रहा हो (या कहें कि इच्छित क्षमता के स्तर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा हो) तो जिस मात्रा में उत्पादन हो रहा था, माँग की कमी के चलते वह बिक नहीं पा रहा था। लेकिन वास्तविक तौर पर यह खुद को मंदी और बढ़ती बेरोज़गारी के संदर्भ में ही दर्शाता है।
यदि कोई इस प्रकार के संकट की प्रकृति को मात्र चक्रीय संकट समझता है तो ऐसा समझना उसकी भूल होगी, जैसा कि इसको लेकर आम धारणा बनी हुई है कि एक निश्चित अवधि के बाद यह चक्र खुदबखुद उलट जाते हैं। जबकि वास्तविकता में देखें तो इसके ठीक उलट 1930 के दशक में आई महामंदी के दौरान, जो अपनेआप में अति-उत्पादन के संकट का क्लासिकल नमूना था, जिसे समाप्त होने में करीब एक दशक का समय लग गया। और अंततः युद्ध के चलते इससे उबरने में मदद मिल सकी थी, और इसे यदि सटीक तौर पर कहें तो दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी में होने वाले सैन्य ख़र्चों के चलते इस संकट से निजात मिल पाई थी।
2008 के बाद से एक बार फिर अति-उत्पादन का संकट देखने में आ रहा है, जो अभी तक अपनी अलग-अलग तीव्रता के साथ कायम है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था में अति-उत्पादन का संकट खुदबखुद गायब हो जाता है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की तत्कालीन समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चौंकाने वाली वास्तविकता यह रही है कि अति-उत्पादन के संकटों से वे मुक्त थे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो सका?
पूंजीवादी व्यवस्था में अति-उत्पादन का संकट दो मुख्य कारणों से उत्पन्न होता है। इसकी पहली वजह है पूँजीवाद में निवेश को लेकर लिए जाने वाले फ़ैसले, जिसे अनुमानित माँग में वृद्धि को देखते हुए लिया जाता है, और इसके लिए वर्तमान में माँग की वृद्धि को एक सूचक के रूप में लिया जाता है। और उसी प्रकार यदि माँग में कमी आने लगती है तो निवेश को भी नियंत्रित किया जाने लगता है। और दूसरा कारण, जब कभी भी निवेश से हाथ खींच लिया जाता है, तो माल के खपत में भी कमी होने लगती है और इस प्रकार से सकल आय में भी कमी का कारक बन जाता है (इसे निवेश का "गुणात्मक" प्रभाव कहा जाता है)।
समाजवादी व्यवस्था ने इन दोनों कारकों को खत्म कर दिया गया था। यहाँ पर निवेश को एक योजनाबद्ध ढंग से लाया गया था, ना कि इस लालच के वशीभूत होकर कि इससे कितना लाभ होने जा रहा है। इसी वजह से जब माँग में वृद्दि दर धीमी होने लगती थी तो उस स्थिति में भी निवेश में कमी का कोई सवाल नहीं उठता था। कहने का मतलब ये नहीं है कि निवेश की मात्रा में किसी प्रकार के उतार-चढ़ाव देखने को ही नहीं मिलते थे। हालाँकि जो उतार-चढ़ाव होते थे, वे लाभ की उम्मीदों की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं, बल्कि पूरी तरह से वाह्य कारणों के चलते पैदा होते थे, जिनमें से दो कारक ख़ासतौर पर महत्वपूर्ण थे।
इसमें एक था कृषि उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव। कुछ ऐसे वर्ष भी होते थे, जिनमें मौसम-सम्बन्धी कारणों से कृषि उत्पादन नीचे चला जाता था, या कुछ और कारणों के चलते निवेश में कटौती की गई, ताकि खाद्य कीमतों पर जरूरत से अधिक दबाव को रोका जा सके, और वे बढती न चली जाएँ। इसी तरह जब कृषि उत्पादन पुनर्जीवित होने लगता था, तो उसी अनुपात में निवेश भी देखने को मिलने लगता था। हालाँकि, निवेश में इस उतार-चढ़ाव के पीछे की वजह यह नहीं थी कि निवेश से कितना लाभ-हानि होने जा रहा है, ये अवश्यम्भावी कारण थे जिसे किसी नियोजित अर्थव्यवस्था में भी रोक पाना मुश्किल था।
दूसरा कारण था संचालन के दौरान उसकी “गूंज से पड़ने वाले प्रभाव" का था। उदाहरण के लिए, मान लेते हैं कि योजनावधि की शुरुआत में ही निश्चित तिथि में एक गुच्छे के रूप में एक साथ कई नए निवेशों को स्थापित किया गया। इन निवेशों का अपना एक जीवन-चक्र होता है, और उस निश्चित अवधि के बाद ये सभी कल-कारखाने और औज़ार समान रूप से एक गुच्छे के रूप में अपनी मीयाद ख़त्म कर रहे होते हैं, और इस प्रकार एक बार फिर से इन क्षेत्रों में निवेश किया जाना तय होता है। इसलिये समय-समय पर सकल निवेश की योजना को बल मिलता है, और इस प्रकार शुद्ध निवेश और पुराने की जगह पर नव निर्माण इन दोनों की ही ज़रूरतों को समायोजित किया जाता है। इस प्रकार यदि निवेश के आंकड़ों पर ग़ौर करेंगे तो पायेंगे कि उसमें कोई लगातार वृद्धि दर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से बताते चलें कि ये उतार-चढ़ाव का सम्बन्ध किसी लाभ के जोड़-घटाव को ध्यान में रखकर नहीं किये जाते, बल्कि इतिहास में पिछले निवेश के चलते इनकी भूमिका उपजती है।
निवेश में होने वाले इस प्रकार के उतार-चढ़ाव के बावजूद समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं ने इस बात को सुनिश्चित कर रखा था कि इसके चलते उपभोग और आय में उतार-चढ़ाव न देखने को मिलें, अर्थात उन अर्थव्यवस्थाओं ने पूँजीवाद की विशिष्टता से उपजने वाले इसके गुणात्मक परिणामों से इसे विभक्त कर रखा था। ऐसा इसलिये हो सका क्योंकि अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी इकाईयों को उनकी क्षमता के अनुसार उत्पादन करने के निर्देश दिए गए थे, और यदि निवेश की कमी के कारण यदि माँग में कमी भी हो जाए, तो उन ईकाइयों को अपनी कीमतों में कटौती करने के निर्देश दिए जाते थे, जब तक कि सारे उत्पाद बिक न जाएँ जिन्हें उत्पादित किया गया था।
इन सस्ते दरों वस्तुओं की बिक्री के कारण कुछ इकाइयाँ ऐसी भी होती थीं, जो घाटे में चली जाती थीं, जबकि कुछ अन्य कम्पनी इस दौरान भी लाभ की स्थिति में बनी रहती थीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कोई भी इकाई चाहे वह नुकसान में हो या लाभ की स्थिति में रही हो, दोनों ही का सीधा सम्बन्ध राज्य से था, जो लाभ कमाने वाली फर्म के मुनाफे से नुकसान उठाने वाली कंपनियों को सहायता प्रदान करके सभी को स्थिर बनाए रखता था। और जब तक निवेश सकारात्मक बना रहे,तब तक इन दोनों प्रकार के समूहों को साथ में लेकर हमेशा ही सकारात्मक शुद्ध लाभ देखने को मिलता रहने वाला था (भले ही किसी अन्य प्रकार से यह कम ही क्यों न हो)।
पूंजीवादी व्यवस्था में जो होता चला आया है, उससे यह अपने तरह का उल्लेखनीय अपवाद सिद्ध हुआ। और इस बात का सूचक है कि जब-जब संकट की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उत्पादन और रोज़गार में गिरावट क्यों होने लगती है। पूँजीवादी व्यवस्था में जब कोई फर्म अपनी लागत नहीं निकाल पाती तो उत्पादन को बंद करने से लेकर कम कर देने के उपाय लिए जाते हैं। लेकिन माँग में कमी आने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें कुछ बेहद धनाड्य घरानों के बीच की आपसी मिलीभगत के ज़रिये "प्रशासित" किया जाता है। उत्पादन को कम कर दिया जाता है और नतीजे में रोज़गार के अवसरों में कमी आने लगती है, जिससे कि माँग और आपूर्ति में संतुलन को फिर से पटरी पर लाया जा सके, और इस बीच जो थोड़ा बहुत अनबिका माल जमा हो रखा है उसे खपाया जा सके।
अब इस मामले को कुछ अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। यदि समान रूप से मज़दूरी और रोज़गार मुहैया कराए गए हों, और इस स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में गिरावट हो रही हो, तो जैसा कि समाजवादी व्यवस्था में हुआ था, तो इसका मतलब होता है कि कुल उत्पादन में मज़दूरी की हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए श्रमिकों के पक्ष में आय के वितरण में वृद्धि हो गई। अब चूंकि श्रमिक कमोबेश अपनी समस्त मज़दूरी का उपभोग कर लेते हैं, इसलिये यदि आय के इस वितरण व्यवस्था में श्रमिकों को अधिक हिस्सा मिल भी जाता है, तो इस तरह के परिवर्तनों से सकल उत्पादन में खपत का हिस्सा भी बढ़ जाता है।
और यही कारण है कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को कभी भी अति-उत्पादन के संकटों को नहीं झेलना पड़ा था, क्योंकि किसी भी वजह से यदि निवेश में कमी भी आ गई, तो उस स्थिति में भी उत्पादन की मात्रा को अपरिवर्तित रखा गया। निवेश में होने वाली गिरावट की भरपाई को खपत में हिस्सेदारी को बढ़ाकर कर लिया गया (उत्पादन में श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि के ज़रिये)।
लेकिन पूँजीवादी व्यवस्था में ऐसा कर पाना असंभव है, क्योंकि पूंजीपति कभी इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि वे स्वेच्छा से उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी को कम कर लें, और उसी अनुपात में श्रमिकों की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी के लिए राज़ी हो जाएँ, चाहे सकल माँग में अच्छी-ख़ास कमी ही क्यों न हो रही हो। यही कारण है कि पूंजीवाद अति-उत्पादन के संकट से गुज़रने के लिए अभिशप्त है: क्योंकि लाभ के वितरण का मामला यहाँ तीखे वर्ग-संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जहाँ पूंजीपतियों के लिए अति-उत्पादन से निपटने के लिए अपने हिस्से के लाभ में कमी करने और उस हिस्से को श्रमिकों में सौंप देने के सवाल पर सहमत होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
यह “गुणात्मक” प्रभाव जिससे पूँजीवाद को गुजरना पड़ता है, जिसमें निवेश में कमी के चलते खपत कम होने लगती है, और फलस्वरूप कुल उत्पादन में कमी होने लगती है। इसके मूल में वजह यह है कि आय के वितरण में यहाँ पर संयोजन की कोई गुंजाईश नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो “गुणात्मक” असर पूँजीपतियों और श्रमिकों के बीच के सापेक्षिक हिस्सेदारी पर आधारित है।
वास्तव में देखें तो पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अपर्याप्त मांग की समस्या से निपटने की कोशिशों में श्रमिकों के हिस्से को बढ़ाने की बात तो रही दूर की बात, कुल मिलाकर इस प्रकार की प्रवृत्ति इस संकट की घड़ी में देखने को मिलती है कि किस प्रकार से मज़दूरी में कटौती की जाए और कम उत्पादन के इस दौर में भी लाभ को बढ़ाया जाए। और जिस वजह से संकट की शुरुआत होती है, उसमें निवेश में और कमी लाकर वास्तव में इसे और गहराते देने की भूमिका निभाई जाती है। ऐसी स्थिति में निवेश में की जाने वाली 10% की गिरावट से उत्पादन में भी मात्र 10% की गिरावट ही नहीं होती, जैसा कि "गुणक" विश्लेषण इसकी ओर इशारा करता है, बल्कि कह सकते हैं कि उत्पादन में 10% से कहीं अधिक 15% तक की गिरावट हो सकती है, क्योंकि श्रमिकों की हिस्सेदारी में कमी को (मज़दूरी में कटौती के ज़रिये) निवेश में कमी के ऊपर मढ़ दिया जाता है।
इस बारे में यह तथ्य कि अति-उत्पादन की बढ़ती प्रवृत्ति को दूर करने के लिए उसी अनुपात में श्रमिकों की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी की इजाज़त को न देना पूंजीवाद की एक बुनियादी विशेषता में रहा है, एक व्यवस्था के रूप में यह, इसकी सर्वोच्च तर्कहीनता को भी दर्शाता है। यह दर्शाता है कि व्यवस्था भले ही बर्बाद हो रही उत्पादकता को बर्दाश्त कर लेगा, और साथ ही बेरोज़गारी को भी। जिसका अर्थ है माँग की कमी के चलते उत्पादक संसाधनों की सरासर बर्बादी को जारी रखना, इसके बजाय कि जितना पहले उत्पादित किया जा रहा था उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए उसे मज़दूरों में दे दिया जाए।
इसके दृष्टिकोण में श्रमिकों के उपभोग के लिए इस्तेमाल में लगाने से अच्छा है कि इन संसाधनों को बर्बाद होने दिया जाए। हालाँकि यह भी सच है कि किसी नियोजित व्यवस्था के न होने के कारण यह काम कोई सचेतन प्रयासों का नतीजा नहीं है, अपितु इसकी आसन्न प्रवृत्तियां इसे ऐसा होने देने के लिए प्रेरित करती हैं। संकट के दौर में समाजवाद इस प्रकार की किसी भी बर्बादी या लापरवाही के बजाय उचित मात्रा में श्रमिकों की खपत में बढ़ोत्तरी लाकर ऐसे संकटों को टाल देता है।
सोवियत संघ के पतन के बाद जैसे-जैसे इसकी कहानी इतिहास से ओझल होती जा रही है, वैसे-वैसे बड़ी तेजी से लोग इस बात को भूलते जा रहे हैं कि इस प्रकार की भी एक व्यवस्था हुआ करती थी, जो अपनी तमाम सीमाओं और कमियों के बावजूद बेरोज़गारी की समस्या, अति-उत्पदान के संकट और पूँजीवाद की अतार्किकता से पूरी तरह से मुक्त हुआ करता था।
अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।