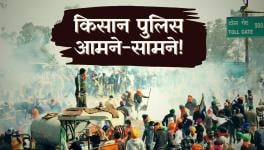किसान जीतें सच की बाज़ी!

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हज़ारों किसान और खेत-मज़दूर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उनका मक़सद है अपने संघर्ष को सरकार के दरवाज़े तक लेकर जाना। पिछले दो महीनों से ये किसान और खेत-मज़दूर अपने श्रम को कॉर्पोरेट घरानों के हाथ सौंपने वाली सरकारी नीतियों के ख़िलाफ़ धरने पर बैठे हैं। महामारी के दौरान जिन कॉर्पोरेट घरानों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कड़कड़ाती ठंड और महामारी के ख़तरे के बावजूद, इन किसानों और खेत-मज़दूरों का हौसला बुलंद है। उन्होंने लंगर और सामूहिक लॉन्ड्री, आवश्यक वस्तुओं के मुफ़्त वितरण केन्द्रों, लोक कला से ओतप्रोत गतिविधियों, लाइब्रेरी संचालन और विचार-विमर्श व चर्चा की जगहें बनाकर अपने डेरों में समाजवादी संस्कृति स्थापित की है। वे अपनी माँगों को लेकर बिलकुल स्पष्ट हैं कि वे किसान, खेत-मज़दूर और जनता विरोधी तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं और अपनी फ़सल में ज़्यादा हिस्सेदारी का अधिकार सुनिश्चित करवाना चाहते हैं।
किसानों का मानना है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जिन तीन क़ानूनों को पास किया है, वो क़ानून राष्ट्रीय और वैश्विक वस्तु (खाद्य) शृंखला में किसानों की मोल-भाव करने की ताक़त को ख़त्म कर देंगे। मूल्य समर्थन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे सरकारी संरक्षण के बिना किसानों और खेत-मज़दूरों को बड़े कॉर्पोरेट घरानों द्वारा तय की गई क़ीमतों पर अपनी फ़सल को बेचना और खाद्य वस्तुओं को ख़रीदना पड़ेगा। सरकार द्वारा पारित क़ानूनों का मक़सद है कि किसान और खेत-मज़दूर कॉर्पोरेट घरानों की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दें; ये क़ानून किसानों और खेत-मज़दूरों की सुनवायी के सभी अवसर को समाप्त कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक समिति बनाने का आदेश दिया है। लेकिन मुख्य न्यायधीश की टिप्पणी ग़ौर करने लायक़ है; उन्होंने कहा कि किसानों -विशेषकर महिलाओं और बुज़ुर्गों- को विरोध स्थल ख़ाली कर देना चाहिए। धरने पर बैठे किसानों और खेत-मज़दूरों ने मुख्य न्यायाधीश की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की। ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान की शोधार्थी, सतरूपा चक्रवर्ती, ने उनकी टिप्पणी का खंडन करते हुए एक लेख लिखा। महिलाएँ समान रूप से किसान और खेत-मज़दूर भी हैं, और किसान आंदोलन की अगुवाई भी कर रही हैं। 18 जनवरी को मनाए गए महिला किसान दिवस पर आंदोलन के सभी स्थलों पर महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने इस तथ्य को पुरज़ोर तरीक़े से स्थापित कर दिया है। उनके बैनर पर लिखा था ‘महिला किसान बोलेंगी, दिल्ली की सरहद हिलाएँगी।' अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए) की महासचिव मरियम धवले ने कहा, ‘नये कृषि क़ानूनों की सबसे ज़्यादा मार महिलाओं पर पड़ेगी। कृषि से जुड़े सभी कामों में शामिल होने के बावजूद, उनके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। [उदाहरण के लिए] आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव भोजन की कमी पैदा करेगा और महिलाओं को इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ेगा।'
इसके अलावा, अदालतों द्वारा बनाई गई समिति में वे नामचीन लोग हैं, जो सरकार के क़ानूनों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते रहे हैं। इस समिति में किसान और खेत-मज़दूर संगठनों के नेताओं में से किसी एक को भी शामिल नहीं किया गया है। मतलब साफ़ है कि उनके साथ विमर्श करके या उनकी सहमति से बने क़ानून के बजाये -एक बार फिर से- क़ानून और आदेश उन पर थोपे जाने के लिए बनाए जाएँगे।

सोली सीसे (सेनेगल), मानव और जीवन (पाँच), 2018
भारत के किसानों और खेत-मज़दूरों के ख़िलाफ़ हालिया हमला लंबे समय से उनपर हो रहे सिलसिलेवार हमलों की कड़ी का हिस्सा है। 10 जनवरी को पीपुल्स आर्काइव फ़ॉर रूरल इंडिया के संस्थापक और ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान के वरिष्ठ फ़ेलो, पी. साईनाथ, ने चंडीगढ़ में एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इन क़ानूनों के व्यापक संदर्भ के बारे में बात की। साईनाथ ने कहा, 'ये केवल [तीन] क़ानूनों का मसला नहीं है, जिसे उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। न ही यह संघर्ष केवल पंजाब और हरियाणा का है; ये इससे आगे बढ़ चुका है। हम क्या चाहते हैं, सामुदायिक या कॉर्पोरेट-निर्धारित कृषि? किसान सीधे कॉर्पोरेट मॉडल को चुनौती दे रहे हैं। भारत अब एक कॉरपोरेट-निर्धारित राज्य बन चुका है, जहाँ सामाजिक-धार्मिक कट्टरवाद और बाज़ारवाद हमारी ज़िंदगियों का पैमाना तय करते हैं। यह संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष है; हमारे गणतंत्र को फिर से हासिल करने का संघर्ष है।'
किसानों का यह आंदोलन ठीक उस समय हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुपक्षीय एजेंसियाँ भुखमरी और खाद्य उत्पादन की स्थिति के बारे में गम्भीर रूप से चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ़एओ) की मुख्य वैज्ञानिक इस्माहेन इलाफ़ी ने हाल ही में रॉयटर्स को बताया कि किसानों और शहरी ग़रीबों ने इस महामारी का बोझ उठाया है। उन्होंने कहा कि 'बाज़ारों से कट जाने और ग्राहकों की मांग में गिरावट के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जबकि शहरी क्षेत्रों के अनौपचारिक श्रमिक, जो अनिश्चितता का जीवन जीते हैं, लॉकडाउन लगने के साथ ही बेरोज़गार हो गए।' ये बिलकुल हो सकता है कि इलाफ़ी भारत के ही बारे में बोल रहीं हों, जहाँ किसान और शहरी ग़रीब ठीक इसी प्रकार से किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इलाफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली में एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं, जिस पर वैश्विक स्तर पर, और देशों के भीतर भी, गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति द्वारा ली गई प्रत्येक पाँच कैलोरी में से एक कैलोरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से आती है। इस आँकड़े में पिछले चार दशकों के दौरान 50% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार नाटकीय रूप से बढ़ा है। हालाँकि पाँच में से चार कैलोरी आज भी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर से ही मिलती हैं। खाद्य उत्पादन के लिए वैश्विक और घरेलू दोनों स्तर पर उचित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियाँ आवश्यक हैं। लेकिन, पिछले कई दशकों में, इन मुद्दों पर कोई वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय बहस नहीं हुई है, इसका मुख्य कारण है नीति-निर्धारण की प्रक्रिया में बड़े खाद्य निगमों का वर्चस्व।
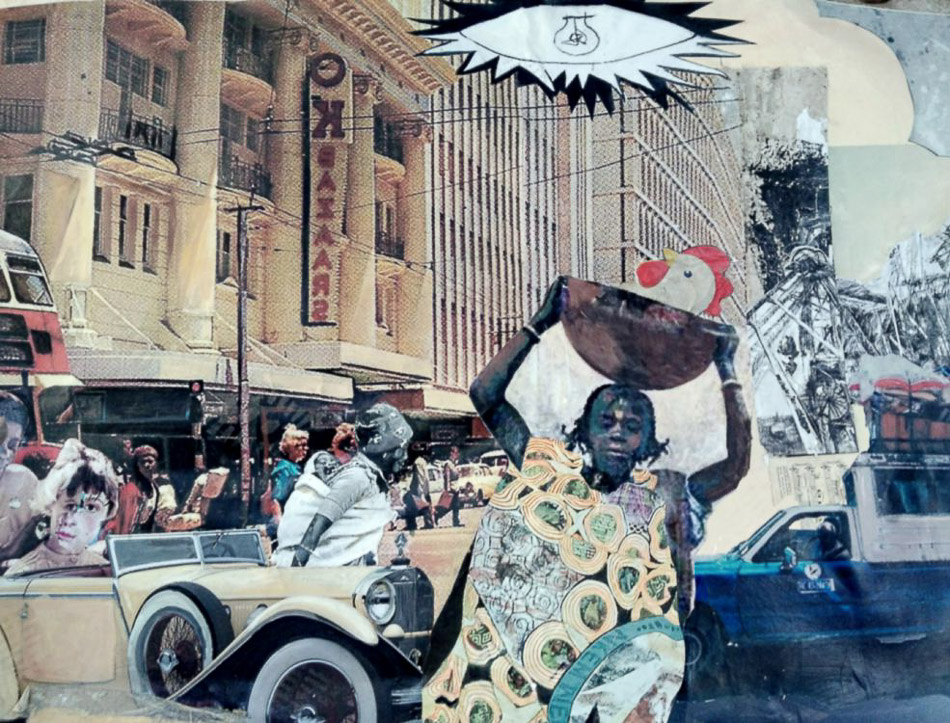
अयंडा मबुलू (दक्षिण अफ्रीका), मारिकाना विधवा, 2011
खाद्य प्रणाली में मुनाफ़े के तर्क से उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है जिनके उत्पादन में कम लागत लगती है और जिन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सकता हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अनाज उत्पादन, जहाँ खाद्य उद्योग पौष्टिक फ़सलों (जैसे अफ़्रीकी बाम्बरा मूंगफली, फोनियो, क्विनोआ) की बजाये 'सस्ती कैलोरी वाले' अनाज (जैसे चावल, मक्का, और गेहूँ) के उत्पादन को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये अनाज बड़े पैमाने पर आसानी से उगाए जा सकते हैं और इनका परिवहन भी आसान हैं। यह प्रक्रिया 'कैलोरी प्रतिस्पर्धा' को बढ़ाती है, जिसके कारण खाद्य उत्पादन में कुछ देशों का वर्चस्व हो जाता है जबकि दुनिया के बाक़ी सभी देश पूर्ण रूप खाद्य आयातक बन जाते हैं।
इसके कई नुक़सान हैं: इन सस्ती कैलोरी वाले अनाजों के उत्पादन में पानी की खपत बहुत अधिक होती है, इनके परिवहन के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है (कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 30% अनाज परिवहन से होता है), जंगल काटे जाने से पारिस्थितिकी प्रणालियाँ नष्ट हो रही हैं। दूसरी ओर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 601 बिलियन डॉलर की राज्य-सब्सिडी दी जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सरकारों को सब्सिडी में कटौती करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह खाद्य उत्पादन प्रणाली किसानों और खेत मज़दूरों के श्रम के ख़िलाफ़ तो है ही, इसके साथ-साथ ये अच्छे स्वास्थ्य और सतत विकास के ख़िलाफ़ भी है, क्योंकि सरल कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

ली फेंगलन (चीन), सुखद काम, 2008
खाद्य उत्पादन में कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन तो होता है। लेकिन जो भोजन उत्पन्न हो रहा है, वह ज़रूरी नहीं है कि स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक पोषण विविधता वाला सबसे अच्छा भोजन हो; और फिर ये भोजन भी उन लोगों को नहीं मिल पता है, जिनके पास इसे ख़रीदने के पैसे नहीं है। महामारी से पहले ही भुखमरी की दर बढ़ रही थी, महामारी के दौरान ये आँकड़े भयावह रूप से बढ़े हैं। भोजन उगाने वाले किसान और खेत-मज़दूर भी भुखमरी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास भोजन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं।
द लांसेट पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित हुए एक अध्ययन के अनुसार युवाओं में भुखमरी के आँकड़े चौंकाने वाले हैं। शोधकर्ताओं ने महामारी से पहले दुनिया भर के 650 लाख बच्चों और किशोरों की लंबाई और वज़न का अध्ययन किया। उन्होंने पोषण की कमी के कारण लंबाई में औसतन 20 सेंटीमीटर का अंतर पाया। विश्व खाद्य कार्यक्रम की मानें तो महामारी के दौरान दुनिया भर के 32 करोड़ बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से स्कूल में मिलने वाले भोजन से महरूम हो गए हैं। यूनिसेफ़ के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप पहले के मुक़ाबले 67 लाख अतिरिक्त पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्वास्थ्य के नज़रिये से तबाह होने की कगार पर हैं। विभिन्न देशों में मिलने वाली मामूली वेतन सहायता भुखमरी के इस ज्वार को रोक नहीं पाएगी। घरों में आने वाले भोजन में कमी का लैंगिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर माँएँ कम खाना खाकर यह सुनिश्चित करती हैं कि परिवार में बाक़ी सभी लोग ठीक से खाएँ।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नवाचार आवश्यक हैं। 1988 में, चीन की सरकार ने 'वेजिटेबल बास्केट प्रोग्राम' (सब्ज़ियों की टोकरी कार्यक्रम) शुरू किया; इस कार्यक्रम के तहत सस्ती, ताज़ी और सुरक्षित ग़ैर-अनाज खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के बारे में प्रत्येक मेयर को हर दो साल का हिसाब देना पड़ता है। शहरों और क़स्बों के भीतरी इलाक़ों को अपने खेत की रक्षा करनी होती थी ताकि ग़ैर-अनाज खाद्य पदार्थ रिहाइश के आस-पास ही उगाए जा सकें। इस कार्यक्रम की सफलता का एक उदाहरण है नानजिंग; 80 लाख की आबादी का ये राज्य साल 2012 तक हरी सब्ज़ियों के उत्पादन में 90% आत्मनिर्भर बन गया था। 'सब्ज़ी की टोकरी कार्यक्रम' के कारण ही महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान भी चीन के शहरों और क़स्बों में ताज़ी सब्ज़ियाँ उपलब्ध होती रहीं। ऐसे कार्यक्रमों को अन्य देशों में विकसित करने की आवश्यकता है, जहाँ सस्ती कैलोरी वाले अनाजों की बिक्री से होने वाले मुनाफ़ों के कारण खाद्य उद्योग उन्हीं के उत्पादन को बढ़ावा देता है; सस्ती कैलोरी का समाज पर बहुत महंगा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
शीर्षक: दिल्ली की सीमाओं पर भारतीय किसानों का प्रतिरोध गान, दिसंबर 2020
भारत के किसान निश्चित रूप से तीन किसान विरोधी क़ानूनों को रद्द करवाने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनकी लड़ाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। यह संघर्ष खेत-मज़दूरों के लिए लड़ा जा रहा है। दुनिया भर के खेत-मज़दूरों में से एक चौथाई प्रवासी हैं, जिनके पास कोई पक्का रोज़गार नहीं होता और जो बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। यह संघर्ष मानवता के लिए लड़ा जा रहा है, एक तर्कसंगत खाद्य नीति के लिए लड़ा जा रहा है जिससे किसान और भूखी जनता दोनों लाभान्वित हों।
दिल्ली की सीमाओं पर उनके डेरे -जहाँ से किसान और खेत-मज़दूर के ट्रैक्टर 26 जनवरी को शहर के अंदर जाएँगे- उल्लास से भरे हैं और नयी संस्कृति रच रहे हैं। यहाँ कई कवि अपनी कविताएँ सुनाने आए हैं। पंजाब के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक सुरजीत पातर ने एक ख़ूबसूरत कविता लिखी है। पातर ने अपना पद्म श्री पुरस्कार सरकार को वापस करने का फ़ैसला किया है। यह कविता दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे संघर्ष के पूरे परिदृश्य और वहाँ के संगीत को बयान करती है:
ये मेला है।
है जहाँ तक नज़र जाती
और जहाँ तक नहीं जाती
इसमें लोक शामिल हैं।
ये मेला है,
इसमें धरती शामिल, पेड़, पानी, पवन शामिल हैं
इसमें हमारी हँसी, हमारे आँसू और हमारे गीत शामिल हैं
और तुझे कुछ पता ही नहीं इसमें कौन शामिल हैं!
कविता में एक युवा लड़की किसानों से बात कर रही है। लड़की कहती है 'तुम जब लौट जाओगे, यहाँ रौनक़ नहीं होगी।' और वो पूछती है 'फिर हम क्या करेंगे?’ जब किसानों की आँखें नम होने लगती हैं तो वो कहती है 'तुम जीतो सच की ये बाज़ी, है ये दुआ मेरी।'
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।