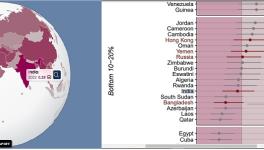अगर मुस्लिमों के भीतर भी जाति है तो इनकी आवाज़ जातिवार जनगणना की मांग में क्यों दब रही है?

जातिगत जनगणना से जुड़ी बहस में केवल हिंदू धर्म के भीतर जाति व्यवस्था का जिक्र हो रहा है। जाति व्यवस्था की प्रकृति से पीड़ित दूसरे धर्म का कोई जिक्र नहीं है।
बिहार की विपक्षी पार्टियों ने जातिवार जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन सौंपा, उसमे लिखा था कि यदि जातिगण जनगणना नहीं कराई जाती है तो पिछड़े/अति पिछड़े हिन्दुओं की आर्थिक व सामाजिक प्रगति का सही आकलन नहीं हो सकेगा और न ही समुचित नीति निर्धारण हो पायेगा। इस पर ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने एतराज जताया। इस संगठन की मांग है कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म की गिनती भी उनके जातिगत श्रेणी के आधार पर की जानी चाहिए। इसे लेकर वह लोगों के बीच जन जागरूकता का काम करेंगे।
यहां पर बहुतों के मन में सवाल उठेगा कि वह हिंदू धर्म में जाति प्रथा के बारे में तो सुनते रहते है लेकिन दूसरे धर्म में भी जाति प्रथा है? है तो किस प्रकार की और कितनी प्रभावी?
समाज और संस्कृति विश्लेषक प्रोफेसर चंदन श्रीवास्तव कहते हैं कि इस्लाम जहां से चला वह ठीक वैसा ही दूसरी जगहों पर नहीं अपनाया गया। यह केवल इस्लाम के साथ नहीं बल्कि हर नए विचार के साथ होता है। हर नया विचार समाज और स्थानीयता को पूरी तरह से खारिज करके नया नहीं बनता। बल्कि अधिकतर हिस्से पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के ही होते हैं। इसलिए अरब से चला इस्लाम ईरान में पहुंचते समय ईरान की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता और भारत में आते समय भारत की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज कर नया नहीं हो सकता। हर समाज कोरे स्लेट की तरह नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नया धर्म आने से पहले से मौजूद रिवाज, ढांचा, परंपरा, मान्यता पूरी तरह से खत्म हो गए और स्लेट पर कुछ नया लिख दिया जाए। भारत पहले से जाति व्यवस्था में रचा हुआ समाज था। इसलिए समानता की बात करने वाला इस्लाम जब भारत पहुंचा तो वह पूरी तरह से ऐसा ढांचा नहीं बन पाया कि पहले से मौजूद भेदभाव खत्म हो जाए। असल में समाज के भीतर जो भी नया होता है उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह पुराने को पूरी तरह से खत्म कर दे। पुराना पूरी तरह से खत्म तभी माना जाता है जब वह लोगों की आदत से पूरी तरह से निकल जाए और जो नया है वह दिमाग की बजाय आदत और बर्ताव का हिस्सा बन जाए। जैसे मौजूदा समय संविधान से संचालित होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले से मौजूद जाति व्यवस्था गहरे तौर पर ढेर सारे लोगों के जीवन की आदत का हिस्सा है। लाख मजबूत तर्क होने के बावजूद भी शादियां अब भी जाति के अंदर ही होती हैं।
इसलिए भारत में जाति व्यवस्था की प्रवृतियां केवल हिंदू धर्म के भीतर नहीं बल्कि भारतीय स्थानीयता के भीतर जितने भी धर्म है सबके साथ मौजूद है। इस्लाम की मान्यता समानता है। लेकिन समानता का पैमाना यह भी है कि यह देखा जाए कि किसी ढांचे के अंदर अलगाव के बर्ताव होते हैं या नहीं। अगर इस आधार पर देखें तो मुस्लिमों के भीतर जो ऊपर मौजूद तबका है, वह खुद को निचले तबके से अलग रखने की कोशिश करता रहता है। भारत में यह केवल इस्लाम के साथ नहीं बल्कि ईसाइयों सहित दूसरे धर्मों के साथ भी है।
विकासशील समाज अध्ययन केंद्र से छपी समाज विज्ञान कोश की किताब में समाजशास्त्री योगेश अटल लिखते हैं कि जाति व्यवस्था ढांचागत दृष्टि से केवल हिंदुओं में सीमित ना होकर कई समाजों में पाई जाती है। भारत में धर्म परिवर्तन के बावजूद जाति व्यवस्था बरकरार रही। ईसाइयत और इस्लाम अपनाने वाले लोग अब भी अपनी जाति के नाम से जाने जाते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं है। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो हिंदू धर्म के कट्टरता के विरोध में चलाए गए उनके भीतर भी जाति व्यवस्था का ढांचा मौजूद है। इस्लाम और ईसाई धर्म के भीतर अंतर विवाही समूह पाए जाते हैं। जो अपने समूह से बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं।
समाजशास्त्री श्याम चरण दुबे का कहना है कि ईसाइयों और मुस्लिमों में जातीय विभाजन बहुत साफ नहीं है लेकिन उनमें भी ऊंची जाति से और नीची जाति से धर्म परिवर्तन करके आए लोगों में भेदभाव किया जाता है। ब्राह्मण और नायर ईसाई या फिर राजपूत और त्यागी मुस्लिम का संबोधन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारतीय चर्च का मानना है कि 60 फीसद से अधिक ईसाई भेदभाव से पीड़ित हैं। इन्हें ओछा ईसाई माना जाता है। दक्षिण में अनुसूचित जातियों से आने वाले ईसाइयों को अलग बस्तियों में रहना पड़ता है। इनका चर्च भी अलग है। शादियां अलग होती हैं। कब्रिस्तान अलग होते हैं। पादरी मृतकों के घर प्रार्थना करने नहीं जाता है। इस तरह के अलगाव के कई लक्षण दिखते हैं।
मुसलमानों में भी मूल और धर्मांतरित मुसलमानों में अलगाव किया जाता है। जो मूल है, यानी अरब के माने जाते हैं उन्हें शरीफ़ और जो धर्मांतरित है उन्हें अजलाफ़ जात का कहते हैं। यह भेद-भाव शादी और आपसी खानपान में भी लागू होता है। अजलाफ़ जात में जुलाहा, भीश्ती, तेली और कलाल जैसी जातियां आती हैं। शरीफ़ जातियों में सैयद, शेख, मुगल और पठान आते हैं। शरीफ़ जात मुस्लिम समाज में ऊंची जातियों की तरह है और अजलाफ़ जात मुस्लिम समाज में निचली जातियों की तरह है। कुछ विद्वान मुस्लिमों के भीतर जाति प्रथा को तीन भागों में बांटते हैं- अशरफ़ ( ऊंचे मुस्लिम), अजलाफ़ ( पिछड़े मुस्लिम), अरजाल ( दलित मुस्लिम)।
पसमांदा आंदोलन से जुड़े प्रोफेसर खालिद अनीस अंसारी अपने एक लेख में लिखते हैं कि बीसवीं सदी के अंत के दौरान पिछड़े और दलित मुस्लिमों ने ऊंचे मुस्लिमों यानी सैयदों से संचालित हो रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ विरोध करना शुरू किया। सवर्ण मुस्लिमों की आबादी मुश्किल से 15 फ़ीसदी के आसपास होगी। साल 1990 में ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज की अगुआई में मुस्लिमों की निचली जातियों के विरोध तेज रुख अख्तियार करने लगे।
इन्हीं विरोधों के चलते पिछड़ी और निचली जातियों के मुस्लिम जैसे कि कुंजरे (रायन), जुलाहे (अंसारी), धुनिया (मंसूरी), कसाई (कुरैशी), फकीर (अल्वी), हज्जाम (सलमानी), मेहतर (हलालखोर), ग्वाला (घोसी), धोबी (हवारी), लोहार-बधाई (सैफी), मनिहार (सिद्दीकी), दारज़ी (इदरीसी) खुद को पसमांदा समूह के तौर पर पेश करते हैं। एकजुट होकर मुस्लिम समुदाय के भीतर मौजूद सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के संघर्ष में लगे रहते हैं।
एक विश्लेषण के अनुसार पहली से चौदहवीं लोकसभा तक चुने गए 7,500 प्रतिनिधियों में से 400 मुस्लिम थे। जिनमें से 340 अशरफ़ (उच्च जाति) समुदाय के थे और अशरफ़ के अलावा दूसरे निचली जातियों की पृष्ठभूमि से केवल 60 मुसलमान थे। 2011 की जनगणना के अनुसार, मुसलमान भारत की आबादी का लगभग 14.2 प्रतिशत हैं। इसका मतलब है कि अशरफ़ों की देश की आबादी में 2.1 फीसदी हिस्सेदारी होगी। लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करीब 4.5 फीसदी था। दूसरी ओर, जनसंख्या में पसमांदा की हिस्सेदारी लगभग 11.4 प्रतिशत थी और फिर भी संसद में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 0.8 प्रतिशत था।
जहां तक नीति निर्माताओं द्वारा मुस्लिम समाज के भीतर जाति प्रथा को स्वीकारने की बात है तो मंडल कमीशन ने गैर मुस्लिम समुदायों के पिछड़ेपन को पिछड़े वर्ग में रखा। जिसके बाद पिछड़े वर्ग और दलित मुस्लिमों को ओबीसी के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों में आरक्षण मिलने लगा। हालांकि पसमांदा आंदोलन की मांग रही है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर कुछ सबसे कमजोर समुदायों को अनुसूचित जाति के वर्गीकरण में शामिल किया जाए।
इन सारी बातों का मतलब यह है कि मुस्लिमों के भीतर जाति प्रथा है। समाज शास्त्रियों ने खूब लिखा है। और भारत सरकार के नीति निर्माता भी इसे स्वीकारते हैं। जाति जनगणना के पक्षधर जिस तरह के तर्क जाति जनगणना के लिए दे रहे हैं, वह सभी तर्क मुस्लिम समुदाय की भीतरी संरचना पर भी लागू होते है। जब मुस्लिम समुदाय की गिनती भी जातिवार होगी तभी पता चलेगा कि कहां पर सरकारी मदद की सबसे अधिक जरूरत है। कौन सा समूह मुस्लिमों के भीतर बहुत पीछे खड़ा है? कौन सा समूह खुद को सरकारी नौकरियों में शामिल करने से बहुत दूर रखता है? यह सारी बातें मुस्लिमों के भीतर जातिवार जनगणना होने पर खुलकर सामने आएंगी।
प्रोफेसर हिलाल अहमद कहते हैं कि जातिवार जनगणना से जुड़ी बहसों में गैर हिंदू धर्म के भीतर जाति की मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। ऐसा लगता है कि भारत के राजनीतिक वर्ग ने भारत में केवल हिंदू धर्म के भीतर स्तरीकरण की संरचना को स्वीकारा कर दूसरे धर्म के भीतर मौजूद जातिगत स्तरीकरण को को खारिज कर दिया हो।
पसमांदा मुस्लिम राजनीति को अक्सर मुस्लिम जातिवाद फैलाने का आरोप लगाकर खारिज किया जाता है। लेकिन उन्होंने मौजूदा समय में जातिवार जनगणना की बहस में बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है।
इन सारी बातों का यह मतलब है कि भारत में सामाजिक न्याय के विचार को जमीन पर उतारने के लिए अगर जातिवार जनगणना की जरूरत है तो गैर हिंदू धर्म खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े भीतरी भेदभाव की संरचना को जाने और अनजाने नजरअंदाज करना बिल्कुल उचित नहीं। एक समुदाय के तौर पर मुस्लिम समुदाय पहले ही भारत में दूसरे समुदायों से पिछड़ा हुआ है। कई तरह के भेदभाव का शिकार होता है। ऐसे में जो समूह मुस्लिमों के भीतर सबसे निचले पायदान पर खड़े होंगे उनकी स्थिति तो बहुत अधिक दयनीय होगी। वरिष्ठ पत्रकार औनिंद्यो चक्रवर्ती न्यूज़क्लिक की अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि सरकार की सारी रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिमों की हिस्सेदारी सरदारी क्षेत्र में बहुत कम है। सरकारी उच्च पदों पर बहुत कम है। सबसे बड़ी बात मुस्लिमों की हिस्सेदारी महीने में सैलरी मिलने वाली नौकरियों और फॉर्मल सेक्टर की नौकरियों में बहुत कम है। मुस्लिमों का अधिकतर हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। वैसे जगहों पर काम करता है जहां का मेहनताना दूसरे नौकरियों के मुकाबले बहुत कम है। आप खुद सोच कर देखिए कि ठेलेवाला, दर्जी, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर, मिस्त्री, फल और सब्जी वाले की मासिक कमाई क्या होगी? इन्हीं सब क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े अधिक लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए डटे हुए हैं।
ऐसे में एक बात साफ होती है कि अगर जातिगत जनगणना का मकसद सामाजिक आर्थिक नीतियों को सामाजिक न्याय के विचार से जोड़कर लागू करने का है तो इसकी जरूरत मुस्लिम समुदाय को भी है।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।