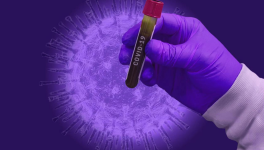पंचायत, चुनाव और शिक्षकों का बलिदान

कोविड-19 की दूसरी घातक लहर के बीच उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव जिस संवेदनहीनता से संपन्न हुए हैं, हाई कोर्ट और राज्य सरकार जिस तरह से उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, उसे देखकर अपनी संस्थाओं के प्रति गहरा अविश्वास उत्पन्न होता है। जो चुनाव इतनी क्रूरता के साथ संपन्न हुए हैं, उनसे निकलने वाली सत्ता कैसी होगी; इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। लगता है कि भारतीय लोकतंत्र अपनी मूल अवधारणा से भटककर महज चुनावी समारोह तक सीमित रह गया है।
तकरीबन 550 से 1000 शिक्षकों की मौत के साथ संपन्न हुआ यह चुनाव अभी और कितने लोगों को संक्रमित करेगा और मौत के मुंह में ठेलेगा कहा नहीं जा सकता। इस दौरान 2,241 पुलिस वाले भी संक्रमित हुए और इनमें से 97 की मौत हुई है।
लगता है लोकतांत्रिक संस्थाओं का उद्देश्य लोगों के जीवन, स्वास्थ्य की सुरक्षा और सांस्कृतिक, नैतिक विकास न रह कर सत्ता हथियाना और धन कमाना रह गया है। ऐसा दावा किया जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायत चुनाव के माध्यम से संपन्न होता है। जबकि चुनाव होने के बाद निरंतर सत्ता के केंद्रीकरण और उसके नैतिक पतन की ढलान खड़ी होती जा रही है। अगर किसी को यह उम्मीद रही है कि पंचायतों में हुए आरक्षण से समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी और समाज की जातिव्यवस्था और पुरुषसत्ता कमजोर होगी तो वह भी इन चुनावों को देखकर टूटती है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव महेंद्र नाथ राय का कहना है कि चुनाव की इस प्रक्रिया में तकरीबन 1000 शिक्षक, शिक्षा मित्र और शैक्षणिक कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। हालांकि सरकारी दावा 135 शिक्षकों की मौत का है। इसके लिए वे इलाहाबाद हाई कोर्ट और राज्य चुनाव आयोग के मनमाने और सख्त निर्देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं। शिक्षकों को सुरक्षा के उपकरण न देने और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था किए बिना चुनावी ड्यूटी पर भेज देने के कारण इतने लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग संक्रमित हुए हैं।
इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को यह कहते हुए नोटिस जारी कर दिया है कि वह बताए कि उसके अधिकारियों पर क्यों न मुकदमा चलाया जाए। हाई कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा है कि कोविड दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। न तो पुलिस ने और न ही चुनाव आयोग ने ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौतें आक्सीजन की कमी से हुई हैं। हाई कोर्ट ने इस स्थिति को शर्मनाक कहा है।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रेस बयान में कहा है कि वह तो चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव कराने पर मजबूर किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में विनोद उपाध्याय की 2020 में एक याचिका पड़ी थी जिसमें पंचायत चुनाव कराने का अनुरोध किया गया था। उसी याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने 4 फरवरी 2021 को आदेश दिया कि सरकार 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव करा डाले। इस तरह हाई कोर्ट और राज्य सरकार अपना नैतिक स्तर ऊंचा रखने के लिए पंचायत चुनावों में हुई संवेदनहीनता की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं।
एक दूसरे पर दोष डालने का यह पाखंड भारतीय लोकतंत्र का नया चरित्र बन चुका है। इस खींचतान में कभी कभी किसी पीड़ित का पक्ष भी सुन लिया जाता है और उसे न्याय भी मिल जाता है लेकिन आखिरकार इसकी गाज जनता पर ही गिर रही है। इस पूरे चक्रव्यूह में उस जनता का भी कम दोष नहीं है जो पंचायत के सारे आदर्श और उद्देश्य को भूलकर सत्ता के नशे में चूर है। इन पंचायत चुनावों के दौरान गांवों के लोगों में जानलेवा उत्साह देखा गया है। खांसी, बुखार, टूटते शरीर के बीच वे भी चुनाव प्रचार में लगे रहे और वोट देने मतदान केंद्रों पर पहुंचे जिन्हें सरकार ने किसी तरह से बाध्य नहीं किया था। कई उम्मीदवार भी ऐसे थे, जिनका टेस्ट होता तो वे कोरोना पाजिटिव निकलते लेकिन वे और उनके समर्थक धड़ल्ले से प्रचार करते रहे और नोटों के साथ गांव गांव कोरोना बांटते रहे। सीतापुर के 152 गावों में 40 लोग पाजिटिव निकले।
उत्तर प्रदेश के पंचायतों की क्या हकीकत है; इसकी एक झलक अप्रैल 2020 में आमेजन प्राइम वीडियो पर आई पंचायत नाम एक कामेडी फिल्म बहुत अच्छे ढंग से करती है। दीपक कुमार मिश्र के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आईआईटी ग्रेजुअट जितेंद्र कुमार ने मुख्य पात्र का अभिनय किया है। फिल्म में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक पंचायत की कथा दिखाई गई है। वहां की प्रधान नीना गुप्ता हैं। लेकिन प्रधानी का सारा काम उनके पति रघुबीर यादव करते हैं। इस व्यवस्था को कहते हैं प्रधान पति। इस बीच इंजीनियर जितेंद्र कुमार ग्राम सचिव की स्थायी सरकारी नौकरी पाकर वहां पहुंच जाता है और तमाम चुनौतियों का सामना करता है। वह गांव में रहकर सिविल सेवा और आईआईएम की तैयारी भी करता है और उसमें विफल रहता है । उसके सामने गांव की जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, दांव पेंच और हिंसा सब कुछ चुनौती बन कर खड़े होते हैं।
वह फिल्म परिवार कल्याण और दूसरी सरकारी योजनाओं के गांव के स्तर पर लागू किए जाने की विडंबना को व्यक्त करती है। लेकिन उसमें चुनाव नहीं दिखाया गया है। पंचायतों के निर्माण की प्रक्रिया को देखना हो तो चुनाव को भी देखना चाहिए क्योंकि महिला सीट पर न तो महिलाएं प्रचार करने जाती हैं और न ही उनका चित्र पोस्टरों पर शायद दिखता है। उसी तरह अनुसूचित जाति के कई उम्मीदवार किसी दबंग के लिए ही काम करते हैं। एक तरह से यह चुनाव पहले से चली आ रही असमानता पर आधारित व्यवस्था के नवीकरण का आयोजन हैं। जहां पिछले के नवीकरण में दिक्कत होती है वहां हिंसा होती है।
निश्चित तौर पर ग्राम पंचायतों ने कुछ राज्यों में अच्छा काम भी किया है लेकिन ऐसा उन्हीं राज्यों में हो सका है जहां जाति व्यवस्था और पुरुष सत्ता व सांप्रदायिकता के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन पहले से मजबूत थे। उनकी रोशनी में स्त्रियों, दलितों और पिछड़े वर्ग के योग्य नेतृत्व भी निकले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों की भूमिकाओं का जिस तरह कांग्रेसी सरकारों फिर सपा और बसपा सरकारों और अब भाजपा की सरकार ने अवमूल्यन किया है उसके परिणामस्वरूप यह सब होना सहज लगता है। गलत साधनों के प्रयोग से अनैतिक पंचायतों का निर्माण हुआ है और वे समाज की रक्षा करने की बजाय आत्महंता प्रवृत्ति रखती हैं।
यही कारण है कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के आदर्शों का मजाक उड़ाते हुए डा भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि गांव असुविधा, अज्ञानता और अन्याय के केंद्र हैं। वहां से किसी आदर्श की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन राजीव गांधी की पहल पर पंचायती व्यवस्था लाने की कोशिशें शुरू हुईं और 1992 में किए गए 73 और 74 वें संविधान संशोधन के साथ तीन स्तरीय व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जा सका।
हालांकि ग्राम सभा और न्याय पंचायत जैसी इसकी कई संस्थाएं अभी भी दिखावटी ही हैं और उनकी शक्तियां न के बराबर हैं। क्योंकि एक बार चुनाव हो जाने के बाद कभी यह लगता ही नहीं कि ग्राम सभा सर्वोच्च संस्था है और बाकी सारी संस्थाओं ने अपनी शक्तियां इसी से प्राप्त की हैं। पंचायती संस्थाओं को नया रूप देने का प्रयास अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त और आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ डा ब्रह्मदेव शर्मा ने भी किया था। उनका `मावा नाटे मावा राज’ का आंदोलन काफी चर्चित है। उनका आदर्श था कि हमारे गांव में हमारा राज। इसी के साथ उन्होंने एक नारा दिया था कि लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा। इन्हीं आदर्शों को लेकर उन्होंने पेसा जैसा कानून पारित करवाया। इस कानून के तहत आदिवासी पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। उसके लागू होने की जो दिक्कतें हैं उसे वर्जीनिया खाखा ने अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज किया है।
ग्राम स्वराज की दिक्कतें शुरू से रही हैं। गांधी जब उसे एक आदर्श संस्था बनाना चाहते थे तब उनके पास बहुत किस्म की शिकायतें आती थीं। उन्होंने 1931 के अप्रैल महीने में `यंग इंडिया’ में एक शिकायत का जिक्र किया है। उस पत्र में गांव में काम करने गए एक युवक ने लिखा है कि हमें गांव में नीचे लिखी बातें देखने को मिलती हैः----
1- दलबंदी और लड़ाई झगड़े
2- ईर्ष्या- द्वेष
3- दुष्टता
4- फूट
5- लापरवाही
6- सभ्यता का अभाव
7- पुरानी रूढ़ियों का आग्रह और
8- निर्दयता
गांधी ने उस युवक को समझाते हुए लिखा है कि सेवाभाव के बगैर जो लोग गांवों में जाते हैं उनके लिए तो उसकी नवीनता नष्ट होते ही ग्राम जीवन नीरस हो जाएगा।
गांधी ने गांवों में सांप्रदायिक झगड़े देखे थे। जातिवाद और छुआछूत देखा था। इसलिए यह कहना उचित है कि वे उस समय के गांवों को आदर्श नहीं मानते थे। बल्कि वे उसे आदर्श बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाते थे। उसी में एक योजना शांति सेना बनाने की थी। ऐसी सेना जो गांवों में जाए। वहां सद्भाव पैदा करे, लोगों को नई तालीम दे और उन्हें सफाई, स्वास्थ्य रक्षा के उपाय बताते हुए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे सिखाए। गांधी गोरक्षा की भी बात करते थे खेती की भी बात करते थे लेकिन वे उसके लिए सामुदायिकता को बहाल करने का सुझाव देते थे। इसलिए अगर पंचायत राज की संस्थाएं सामुदायिकता को बढ़ावा देती हैं और ग्रामीण समाज में पारस्परिक सहयोग बढ़ाती हैं और ग्रामीण संसाधनों को संरक्षित और संवर्धित करती हैं तो उनके होने का औचित्य सिद्ध होता है। लेकिन अगर ग्रामीण संस्थाएं नेताओं के भाई- भतीजों के राजनीतिक करियर बनाने की सीढ़ी हैं और योजनाओं के लिए धन हड़पने का माध्यम हैं तो उनका होना फायदेमंद नहीं है।
सवाल उठता है कि जो पंचायती संस्थाएं शिक्षकों की गरिमा गिराकर, उनकी जान लेकर और समाज को चुनाव की संक्रामक प्रवृत्ति में झोंककर अपना निर्माण करती हैं वे कैसे लोकतंत्र को जीवंत बना सकती हैं। अनुचित साधनों और मनमाने आदेशों से निर्मित होने वाली ऐसी पंचायती संस्थाएं राजनीतिक पार्टियों की पिछलग्गू हो सकती हैं ग्राम स्वराज लाने का साधन नहीं।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।