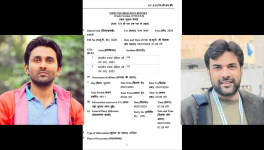ट्रस्ट और राष्ट्र के बीच प्रेस

भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), ट्रस्ट और राष्ट्र के बीच फंस गई है। उसने चीन के सीमा विवाद पर दोनों देशों के राजदूतों का इंटरव्यू क्या लिया कि उस पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एक तरफ केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय ने उस पर 1984 से लीज की जमीन का किराया न देने का आरोप लगाते हुए 84.84 करोड़ रुपये की अदायगी का नोटिस दिया है तो दूसरी ओर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्गिंग जर्नलिस्ट ने उस पर महामारी के दौरान कर्मचारियों की छंटनी का आरोप लगाते हुए मज़दूर आंदोलन का मोर्चा खोल दिया है।
अगर वह प्रेस और सत्य के साथ अपना न्यास धर्म (ट्रस्ट धर्म) निभाए तो उसका राष्ट्रधर्म खंडित होता है और राष्ट्रधर्म निभाए तो पत्रकारिता के धर्म के साथ छल करती है। पीटीआई की मौजूदा स्थिति देखकर आपातकाल और उसके बाद 1980 के दशक के आखिर में इंडियन एक्सप्रेस समूह की स्थितियों की याद ताजा हो गई।
इंडियन एक्सप्रेस आपातकाल में इंदिरा गांधी की सरकार से भिड़ा हुआ था तो सरकार ने एक्सप्रेस बिल्डिंग के अवैध कब्जे का मसला उठा दिया और दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर जगमोहन ने बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित नई एक्सप्रेस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी कर ली। बाद के दिनों में जब एक्सप्रेस समूह ने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो एक्सप्रेस समूह में बोनस का मसला उठा और मजदूरों की हड़ताल हुई और काम पर लौट रहे पत्रकारों पर तेजाब फेंका गया।
उस समय भी यह मसला उठा था कि एक्सप्रेस समूह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करता है और मजदूरों का हक मारता है। इसलिए उसके कार्यालय में होने वाली हड़ताल या सरकारी नोटिसें न तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हैं और न ही प्रेस की आजादी का दमन। वह सरकार की नियमित कार्रवाई है। जबकि रामनाथ गोयनका के नेतृत्व में अरुण शौरी और प्रभाष जोशी जैसे पत्रकारों ने उसे प्रेस का आजादी के दमन का मुद्दा बनाया था। जब इंडियन एक्सप्रेस में तेजाब कांड के बाद अखबार शुरू हुए तो अरुण शौरी ने अंग्रेजी अखबार में पहले पेज पर रोमन में शीर्षक दिया----दम है कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे।
हालांकि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मामला एक्सप्रेस समूह से अलग है लेकिन फिर भी उनकी कई चीजें मिलती हैं। एक्सप्रेस समूह जहां सरकार के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति के साथ जुटा हुआ था और उसकी छवि भी मीडिया के जेहादी योद्धा के रूप में देखी जाती थी। उसके ठीक विपरीत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देश के अखबार मालिकों के एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है जिसमें सरकार का ट्रस्ट ज्यादा ही रहा है। पीटीआई को कभी सरकार के खिलाफ खबर करने वाली एजेंसी के रूप में देखा भी नहीं गया। बल्कि उसे सरकार का भोंपू ही माना जाता था। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि पीटीआई किसी अपुष्ट खबर को चलाती नहीं थी और हर खबर को ठोंक बजाकर ही जारी करती थी। अखबार के दफ्तरों में तमाम संवाददाता और उपसंपादक या समाचार संपादक अक्सर पीटीआई की खबर का इंतजार करते थे और उसके आ जाने के बाद ही समाचार बनाते थे। इसके ठीक विपरीत यूएनआई के बारे में कहा जाता था कि `फास्ट विथ द न्यूज एंड फास्टर विथ दा कांट्राडिक्शन’(यानी जितनी तेजी से खबर उतनी ही तेजी से खंडन)।
जनसत्ता में काम कर चुके एक पत्रकार जब पीटीआई की हिंदी एजेंसी भाषा के संपादक बने तो उन्होंने वहां एक्सप्रेस के तरीके से काम करने की कोशिश की। उन्हें न सिर्फ प्रबंधन ने टोका बल्कि सहयोगियों ने भी कहा कि यहां जनसत्ता और एक्सप्रेस की स्टाइल नहीं चलेगी। दरअसल पीटीआई हमेशा केंद्र में बैठी सरकारों के साथ ही रही। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो या तीसरे मोर्चे की, वह सरकार के विरुद्ध खबर जारी करने में यकीन नहीं करती थी। एक वरिष्ठ पत्रकार तो अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि जब जार्ज फर्नांडीज पर बड़ौदा डायनामाइट कांड के तहत देशद्रोह का आरोप लगा तो एजेंसी ने उनके नाम के आगे श्री लगाना बंद कर दिया।
इसलिए सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि एक सरकार समर्थक और एक कन्जरवेटिव किस्म की समाचार एजेंसी अचानक देशद्रोही हो गई? विडंबना देखिए कि देशद्रोह की श्रेणी वाली खबर करने का आरोप देश में प्रसारण की स्वायत्तता कायम करने के लिए बनी `प्रसार भारती’ जैसी संस्था ने लगाया है जो संस्था अपने गठन के उद्देश्य में पूरी तरह से विफल रही है। प्रसार भारती ने अपनी सात करोड़ रुपये की ग्राहकी बंद करने की धमकी भी दी है। एक खबर तो यह भी है कि प्रसार भारती पीटीआई के बोर्ड में अपना सदस्य बिठाना चाहती थी लेकिन पीटीआई ने मना कर दिया। हालांकि इस बारे में पीटीआई का यही कहना है कि पीटीआई मेमोरेन्डम एंड आर्टीकिल ऑफ एसोसिएशन के तहत ऐसा करना संभव ही नहीं है। उसके बोर्ड में वही लोग आ सकते हैं जो या तो शेयर धारक हैं या फिर जिनका संस्था से कोई वित्तीय संबंध है।
यहां कुछ सवाल उठते हैं जो प्रेस, विश्वास और राष्ट्र के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल यही है कि क्या पीटीआई ने लीज के किराए का भुगतान न करके सही किया या गलत? दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार द्वारा दी गई जमीन और सहायता पर आश्रित मीडिया और सरकारी एजेंसियां अपनी स्वायत्त कार्यप्रणाली विकसित कर सकती हैं? तीसरा सवाल यह है कि क्या दो राष्ट्रों के बीच विवाद या युद्ध होने की स्थिति में समाचार एजेंसी और मीडिया महज प्रोपेगंडा मॉडल अपनाए और विवाद की आग में घी डालें या तटस्थ होकर ऐसा काम करे जिससे विवाद का हल निकले?
क्या पत्रकारिता के मूल्य और आदर्श राष्ट्र के आदर्श से अलग हैं या वे उसके साथ नत्थी हैं?
यहां एक सवाल यह भी मौजूं है कि क्या पीटीआई पर होने वाली इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर पूरी दुनिया में लग रहे ग्रहण और प्रेस की आजादी पर कसे जा रहे शिकंजे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए या इस मसले को महज पीटीआई तक सीमित रखना चाहिए?
किसी भी मीडिया संस्थान की आर्थिक गड़बड़ी को इस आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता कि वह जनता की सेवा करता है तो उसे ऐसा करने का हक है। न ही यह कहा जा सकता है कि सरकार ने यह मांग अब तक क्यों नहीं उठाई। आर्थिक लेन देन में उन संस्थाओं का हिसाब ज्यादा साफ होना चाहिए जो ट्रस्ट यानी न्यास की बात करती हैं और जिनका पूरा कारोबार विश्वसनीयता और साख के आधार पर चलता है। न ही किसी कंपनी या ट्रस्ट की ओर से कर्मचारियों की नियम विरुद्ध छंटनी को सही ठहराया जा सकता है। लेकिन यहां सरकार पर भी सवाल उठता है कि वह इतने लंबे समय से किराये की वसूली को लेकर खामोश क्यों थी? यहां `मीठा मीठा गप्प और कड़वा कड़वा थू’ वाली कहावत चरितार्थ होती है। यानी जब तक पीटीआई आपकी छाया बन कर चल रही थी तब तक उसकी सारी अनियमितता माफ थी। तब तक सरकार को यह भी नहीं दिखाई पड़ रहा था कि उसने इमारत में अवैध निर्माण कराए हैं और कर्मचारियों की छंटनी की है । आज जब उसका एक इंटरव्यू नागवार गुजरा तो सारी गाज गिर गई।
यहीं पर नोम चोमस्की की `मैन्यूफैक्चरिंग कन्सेंट’ की अवधारणा में पांच फिल्टरों की बात याद आती है। जब भी मीडिया सरकार के अनुकूल काम नहीं करता तभी इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उसका स्वामित्व बदल दिया जाता है, उसका विज्ञापन रोक दिया जाता है, उसके पत्रकारों को खबरें नहीं बताई जातीं, उसकी खबरों को झूठा बताकर बदनाम किया जाता है, स्रोत को अविश्वसनीय कहा जाता है और आखिर में किसी संस्थान और पत्रकार को कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अल्पंसख्यक, प्रवासी, देशद्रोही और आतंकवादी बताकर खारिज कर दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है।
जाहिर है देशद्रोह का आरोप तो साफ तौर पर लगाया ही गया है। मैन्यूफैक्चरिंग कन्सेंट को चरितार्थ करने में पीटीआई जैसी शक्तिशाली एजेंसी का बड़ा योगदान हो सकता है। दिक्कत यही हुई कि पीटीआई भले ही सरकार के लिए काम करती हुई दिखती है लेकिन उसने सरकार के हाथों में पूरी तरह समर्पित होने से इनकार कर दिया। पीटीआई के मुख्य संपादक एमके राजदान के रिटायर होने के बाद सरकार चाहती थी उसके किसी चहेते को संपादक बनाया जाए। इस कड़ी में उसके अपने चहेते पत्रकारों की सूची थी जो भाजपा और संघ से गहरे संबंध रखते थे। इस अभियान में अरुण जेटली सक्रिय थे। पीटीआई बोर्ड ने उनमें से किसी नाम को स्वीकार नहीं किया और विजय जोशी जैसे प्रोफेशनल पत्रकार को संपादक बना दिया। इस बात से भी सरकार चिढ़ी हुई थी।
पीटीआई के साथ होने वाली इन घटनाओं को हम दुनिया के स्तर पर लोकतंत्र में आई महामंदी के दौर से अलग करके नहीं देख सकते। एक ओर तो पीटीआई के बरअक्स निजी कारपोरेट की समाचार एजेंसी एएनआई को विकसित किया जा रहा है तो दूसरी ओर पीटीआई को दरकिनार किया जा रहा है। कहते हैं कि आजकल मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के हेलीकाप्टर में एएनआई के कैमरामैन की जगह निश्चित होती है और किसी की हो या न हो। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि पीटीआई ने चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री और भारत में चीन के राजदूत सन वीडांग का इंटरव्यू लेकर कौन सा गलत काम कर दिया? अगर चीनी राजदूत ने गलवान घाटी में झड़पों के लिए भारतीय सैनिकों को समझौते के उल्लंघन का दोषी बताया तो भारतीय राजदूत ने चीन को पीछे हटने के लिए कहा। इससे प्रधानमंत्री की वह बात खंडित हो गई कि कोई किसी की जमीन पर नहीं गया है लेकिन दोनों पक्ष तो आ गए।
असली सवाल यह है कि क्या पत्रकारों की स्वायत्तता छीनने से राष्ट्रों का भला होता है या फिर नुकसान होता है। हमें यह मानना चाहिए कि पत्रकार किसी संस्थान में काम करने वाले महज कर्मचारी नहीं होते। वे दो देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक दूत होते हैं। यहां 1963 में भारतीय संसद में डॉ. लोहिया द्वारा चीन पर की गई बहस को याद करना चाहिए। डॉ. लोहिया ने कहा था कि दुनिया के चर्चित पत्रकार और चीन पर रेड स्टार ओवर चाइना जैसी प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तक लिखने वाले एडगर स्नो चीन की ओर से कोई प्रस्ताव लाने वाले हैं जिससे सीमा विवाद को हल करने में मदद मिलेगी।
इसी संदर्भ में हमें वेब मिलर, लुई फिशर, मार्गरेट बर्कह्वाइट, विलियम शरर, विन्सेंट सीन जैसे पत्रकारों के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को नहीं भूलना चाहिए। वेब मिलर तो एजेंसी के पत्रकार थे और उनकी खबर रुकवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पूरी कोशिश की थी पर उन्होंने नमक सत्याग्रह का ऐसा कवरेज किया कि पूरी दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक धाक जम गई। महात्मा गांधी ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास लुई फिशर के हाथों चिट्ठी भिजवाई थी ताकि वे चर्चिल पर भारत की आजादी के लिए दबाव डाल सकें। भारत पाक विभाजन के समय गांधी कई बार अपनी प्रार्थना सभाओं में या गृह मंत्री सरदार पटेल से वार्ता करते हुए डान जैसे पाकिस्तानी अखबारों का उल्लेख करके बताते थे कि फलां स्थान पर दंगा हुआ है।
जब तक हम पत्रकारिता को प्रोपगेंडा माडल के रूप में देखेंगे तब तक समाजार एजेंसी या अखबार से वही खबर चलवाने की उम्मीद करेंगे जिससे छद्म सहमति का निर्माण हो। ऐसे में साख से बड़ा राष्ट्रहित माना जाएगा। लेकिन अगर हम मीडिया को शासक वर्ग और जनता के बीच संवाद और व्यापक रूप से सच्चाई को बताने वाला माध्यम मानते हैं तो उसकी स्वायत्तता से लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे। अगर सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से होंगे भी।
आखिरी सवाल मीडिया के आर्थिक पक्ष पर है। निश्चित पर मीडिया संस्थानों को न तो सरकार से और न ही कारपोरेट से अनैतिक रूप से लाभ लेना चाहिए। उसे अपना हिसाब किताब भी साफ रखना चाहिए। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या मीडिया का कोई ऐसा मॉडल बन सकता है जो सरकार और कारपोरेट से कोई आर्थिक मदद न ले। शायद नहीं। अगर मीडिया और समाचार एजेंसी इसी समाज की सेवा करने और उसे सूचनाएं देने के लिए हैं तो वह सरकार और समाज से अपना दाय क्यों न ले?
जूलिया केज ने सेविंग मीडिया में तो सरकारों के सहयोग से मीडिया की स्वतंत्रता बचाने का सुझाव दिया है। हालांकि उनका मुख्य तर्क तो क्राउड फंडिंग का है। जाहिर है पीटीआई के विवाद ने फिर एक बार प्रेस की आजादी, लोकतंत्र की महामंदी और मीडिया की वित्तीय अनियमितता का मसला उठा दिया है। ट्रस्ट और राष्ट्र के बीच प्रेस फंसा हुआ है। देखना है वह इस विवाद से निकल कर सत्य के करीब कैसे पहुंचता है?
(अरुण कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।