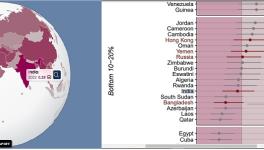सुप्रीम कोर्ट से ब्राह्मणवादी ना होने की अपेक्षा करना बेमानी है
1 अक्टूबर 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने डॉ॰ सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में मार्च 2018 को दिए गए अपने आदेश को वापस ले लिया था, यह वह आदेश था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधानों को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था।
सुभाष काशीनाथ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह चिंता व्यक्त की थी कि "...अत्याचार अधिनियम को ऐसे लागू करने से कहीं जातिवाद स्थिर न हो जाए..." इस चिंता को आधार बनाते हुए अदालत ने संशय के निवारण के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि कोई भी सरकारी मुलाज़िम जिन पर भी अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है उसे तब तक गिरफ़्तार न किया जाए तब तक कि उसके नियुक्ति अफ़सर से अनुमति न ले ली जाए और किसी आम आरोपी की तब तक गिरफ़्तारी न की जाए तब तक कि यह अनुमति इलाक़े के एसएसपी से ने ली जाए।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अत्याचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले संबंधित डीएसपी द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। अग्रिम ज़मानत के संबंध में, जो कि अधिनियम की धारा 18 में स्पष्ट रूप से वर्जित है, अदालत ने माना कि अग्रिम ज़मानत देने के ख़िलाफ़ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है "यदि कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है या जहां न्यायिक जांच में शिकायत पाई जाती है या फिर मामला बुरे इरादे से दायर किया जाता है तो अग्रिम ज़मानत दी जा सकती है।"
सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में अत्याचार अधिनियम के उद्देश्य के मामले में काफ़ी विरोधाभासी था और इसने इसके उन कड़े प्रावधानों को बेअसर करने की कोशिश की थी जो यह सुनिश्चित करता था कि न्याय के रास्ते में शिकायतकर्ताओं और अपराधियों के बीच मौजूद सर्व-शक्तिमान जातिगत समीकरण नहीं आए। इस आदेश की व्यापक रूप से समीक्षा हुई, और 1 अक्टूबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ख़ुद के आदेश की समीक्षा की, उसने पाया कि इस आदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति अविश्वास का भाव दिखाया गया है और सिया के प्रति पूरे देश में सहज और आक्रामक विरोध शुरू हो गया था।
केंद्र सरकार ने भारी राजनीतिक दबाव के चलते तुरंत ही सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया, और सुभाष काशीनाथ केस में आदेश के निंदनीय और घातक प्रभाव को पूर्ववत करने के लिए एट्रोसिटी अधिनियम में धारा 18ए की शुरुआत की गई। धारा 18ए में अन्य बातों के अलावा, धारा 18 की तुलना में कड़े शब्दों को दोहराया गया है कि अत्याचार करने के आरोपी को, "किसी भी अदालत के आदेश के बावजूद" अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती।
पुनर्विचार याचिका और स्मरण:
1 अक्टूबर के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ग़लतियों को दुरुस्त किया और अत्याचार अधिनियम के सुरक्षित प्रावधानों को बहाल कर दिया। इस मामले में उसने 2018 के आदेश की याद दिलाई कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी और अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किए गए किसी भी अत्याचार या घृणा से भरे अपराध के बाद आरोपी व्यक्ति की गिरफ़्तारी से पहले किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, अदालत ने धारा 18 का पालन करने से इंकार कर दिया और नई शुरू की गई धारा 18ए जो कि अग्रिम ज़मानत पर जल्द और निरपेक्ष प्रतिबंध लगाती है को लागू कर दिया।
इस आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति को बहाल करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत वास्तव में उस मामले में दी जा सकती है "जहां कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है", जबकि, दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि इस तरह की बाधाएं अन्य ज़मीनी हक़ीक़तों के साथ क़ानून के प्रभावी कार्यान्वयन को बाधित करती हैं।
एक निरंतर इनकार :
अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम दो स्पेशल लीव पिटीशन को ख़ारिज कर दिया था, जो कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत आरोपित व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ दायर की गई थी। इन मामलों में से एक में बहस के दौरान, अदालत ने सवाल खड़ा किया था कि क्या महिला शिकायतकर्ता को यौन उत्पीड़न और मौत की मिली धमकियों के मामले में वास्तव में कोई जातिगत कोण था। यह एक और ऐसी बात थी जिसे कि अदालत ने दरकिनार कर दिया था और माना कि अभियुक्त शिकायतकर्ता को अपने स्कूटर के हॉर्न से सड़क पर यौन उत्पीड़न नहीं कर सकता था और न ही मौत की धमकी दे सकता था जो मामला तीन साल से चल रहा था, और कोर्ट ने कहा कि इस तरह के ख़तरों की कोई "समाप्ति की तारीख़" होनी चाहिए।
निचली अदालत ने इन मामलों में आरोपी के ख़िलाफ़ एट्रोसिटी एक्ट के तहत लगे आरोप सहित एक प्रथम दृष्टया मामला पाया था। उच्च न्यायालय के सामने, जांच अधिकारी ने अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया था और इस मामले में एक आरोप-पत्र भी दायर किया था। जो यह स्पष्ट करता था कि आरोपियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मुक़दमा चल रहा था। इन सब के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में अग्रिम ज़मानत देने के आदेश के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया।
अत्याचार अधिनियम की धारा 18 और 18ए का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने के अलावा, स्पेशल लीव पेटीशन को खारिज करना और उच्च न्यायालय के आदेशों के साथ रज़ामंदी दिखाकर सुप्रीम कोर्ट जाति के अस्तित्व को लंबे समय से इनकार करता रहा हैं, या किसी भी दर पर अत्याचार और सामाजिक बहिष्कार के विभिन्न रूपों में जाति द्वारा निभाई गई सर्वव्यापी भूमिका से भी इनकार किया है।
गणपत बनाम रिटर्निंग ऑफिसर (1975) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "हिंदू धर्म इतना सहिष्णु और हिंदू धार्मिक परम्पराएँ इतनी विविध और उदार है कि किसी के बारे में भी यह कहना मुश्किल होगा कि कौन हिंदू धर्म को मान रहा और कौन नहीं।" हिंदू/ब्राह्मणवादी प्रथाओं पर यह एक हानिरहित अवलोकन के रूप में प्रतीत होता है, लेकिन इसके बाद हिंदू और भारतीय समाज में जाति और जाति आधारित अत्याचारों से एक तरह का इनकार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “सौभाग्य से चीज़ें बदल रही हैं।
शहरों या बड़े शहरों में [जाति] कहा जा सकता है कि लगभग ग़ायब हो गई है। शायद ही कोई यह बात जानता है कि वह जिस व्यक्ति से मिल रहा है वह अनुसूचित जाति का सदस्य है या नहीं और कोई भी इन दिनों इसके बारे में परेशान नहीं होता है। गाँवों में ऊँची जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों पर ज़ुल्म के बारे में अख़बारों में जो हम कभी-कभी पढ़ते हैं, वह वास्तव में कृषि मज़दूर या ज़मींदार के बीच संघर्ष की अभिव्यक्ति है, क्योंकि अनुसूचित जातियों के सदस्य ज़्यादातर एक तरफ़ होते हैं और ज़मींदार दूसरी तरफ़ होते हैं। इसे उच्च जातियों द्वारा अनुसूचित जाति के उत्पीड़न के रूप में वर्णित करना ग़लत है।”
कोर्ट में: अतीत के अवशेष के रूप में जाति:
पुराने समय या दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों में जाति का ऐसा पुनर्मूल्यांकन और जातिगत हिंसा को पूरी तरह से नकार देना और इसे केवल एक आर्थिक संघर्ष के रूप में ख़ारिज करना हिंदू जाति व्यवस्था की रक्षा के रूप में स्पष्ट तर्क है। कई अन्य देशों में भी नरसंहार से इनकार किया जाता रहा है, या जैसा कि कई यूरोपीय देशों में हुआ है, कि उन्होंने कभी नहीं माना कि उनके देशों में कभी भी नरसंहार हुआ था जो अपने आप में एक आपराधिक अपराध होगा। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था का जाति आधारित भेदभाव और जाति आधारित हिंसा में स्पष्ट रूप से जाति की भूमिका को नकारना समझ से बाहर की बात है। यह उपमहाद्वीप में जाति की हिंसक और सर्वव्यापी भूमिका को इनकार करने का प्रयास है।
अन्य मामलों में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी भारतीयों के जीवन में जाति द्वारा निभाई गई भूमिका को मानने से इनकार किया है। कोर्ट यह जानने में भी अक्सर विफल रहा है कि कैसे प्रमुख जातियों की गोद में अनुचित लाभ जा रहे है, और वह साथ ही जातिगत हिंसा और उससे हुए नुकसान को भी स्वीकार करने से इनकार करता रहा है। यह तब स्पष्ट हो गया था जब 1985 में, सोसई बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि दलित जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म या अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे, ज़रूरी नहीं कि वे उसी नुकसान का सामना कर रहे हों जैसा कि उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर किया था।
जब ईसाई दलितों ने मांग की कि उन्हें भी संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए, जिस पर हर दलित का अधिकार है, तो अदालत ने मांग की कि वे साबित करें कि उनकी स्थिति में धर्म परिवर्तन के बाद भी सुधार नहीं हुआ है। जब ईसाई दलित समूहों ने यह दिखाते हुए सबूत पेश किए कि हिंदू धर्म से दूर जाने पर भी उनकी उत्पीड़ित सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि वे जहां भी जाते हैं उनकी जाति की पहचान उनका अपमान करना जारी रखती है, लेकिन अदालत ने इसे "आधिकारिक" या "निर्णायक" सबूत नहीं माना।
धर्म-तटस्थ अधिकारों का प्रश्न:
यह स्थिति संविधान में हिंदू (ब्राह्मणवादी) पूर्वाग्रह के कारण उत्पन्न हुई। अपनी सभी क्रांतिकारी उपलब्धियों के बावजूद उन वर्षों में जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, स्वतंत्रता/राष्ट्रवादी आंदोलन के अत्यंत मजबूत ब्राह्मणवादी ताक़तों के प्रभाव को वह पूरी तरह से अवरुद्ध या रोक नहीं पाया।
संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची घोषित करने का काम सौंपा था। इस शक्ति का प्रयोग कराते हुए, राष्ट्रपति ने संविधान के तहत (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जारी किया था। इस आदेश में कहा गया है कि केवल उन्हीं अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान और अन्य भेदभाव विरोधी क़ानूनों का संरक्षण दिया जाएगा जो हिंदू धर्म को मानते थे। जबकि ऐसा कर इसने दलितों को हिंदू धर्म छोड़ने और दूसरे धर्म को अपनाने के लिए तुरंत दंडित करने का प्रावधान रखा।
1956 में, केंद्र ने अपने आदेश को उन लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति के लोग सिख धर्म या बुद्ध धर्म को मानते थे, संशोधन किया और 1989 में उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस बात का तो कोई कारण नहीं है कि संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा केवल हिंदू या उस मामले में सिख या बौद्ध दलितों तक सीमित होनी चाहिए। जबकि सिख और बौद्ध धर्म के सदस्यों को खुद संविधान और उसके प्रावधानों ने हिंदू धर्म में एक तरह से अपहरण कर लिया। सभी धर्मों के दलितों के लिए संविधान के रक्षा उपायों और भेदभाव-विरोधी क़ानूनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रमुख जातियों के सदस्य अन्य धर्मों में धर्मांतरण करके हिंदू धर्म की तह के बाहर क़दम रखने के बाद भी उनके ख़िलाफ़ अत्याचार करते हैं, और उनका दमन करना जारी रखते हैं।
एक और हालिया उदाहरण मौजूद है जहां सर्वोच्च न्यायालय जाति के मामले में अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहा था, जब उसने संविधान (एक सौ तीन वां संशोधन) संशोधन अधिनियम, 2019 पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। इस संशोधन के ज़रिये अनुच्छेद 15 और 16 में जोड़े गए नए खंडों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत तक सीटों की पहुंच पर रोक लगाने की मांग की थी। यह पहली नज़र में हाशिए के समुदायों का बहिष्कार था। यह पहले से ही राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली जाति समूहों स्थिति को अधिक मज़बूत करता है, जिनके सदस्य पहले से ही शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सेवाओं और सत्ता के सभी पदों पर आसन हैं।
संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में निहित समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों पर चौतरफ़ा धोखाधड़ी किए जाने के बावजूद, न्यायालय ने उसे उन्हीं लोगों के सर पर डाल दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और प्रमुख जातियों की प्रधानता जो अवसरों के अवरोध के रूप में काम करती है, इसको मानने से इनकार कर दिया और इसे आरक्षण के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के साथ भ्रमित कर दिया, जो आरक्षण के उद्देश्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।
अगस्त 2019 में पहले से रेखांकित की गई एसएलपी में से एक को ख़ारिज करते हुए, पीठ में से एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि सिया के लिए किसी "एक बड़े केस की प्रतीक्षा की जानी चाहिए", ("बड़े" का मतलब यहाँ यौन उत्पीड़न और मौत के ख़तरों से अधिक भीषण अत्याचार है।) कुछ समय के लिए मान लें कि अत्याचारों के भीतर अत्याचार का एक पदानुक्रम है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे "बड़े" केसों में भी कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। अक्टूबर 2013 में, पटना उच्च न्यायालय ने 1997 में बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों के नरसंहार के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए रणवीर सेना से जुड़े सभी लोगों को बरी कर दिया था।
लेकिन बरी किए गए लोगों के खिलाफ विभिन्न अपीलों पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई नहीं करके मामले के प्रति घोर रवैया दिखाया है। इस केस को सुनवाई के लिए बार भी सूचीबद्ध नहीं किया गया था वह भी इस तथ्य के बावजूद की कि 2015 में कई आरोपियों ने वीडियो पर कहा था कि उन्हे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था इसलिए उन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया था। इस प्रकार, जब भी सर्वोच्च न्यायालय को "बड़े" मामलों का सामना करना पड़ा है, तब भी इसकी प्रतिक्रिया में उस पर जरूरी सुनवाई करने या बेहतर रुख रखने की भावना का अभाव रहा है।
मर्दाना, और विशेषाधिकार भी:
सर्वोच्च न्यायालय एक विशेषाधिकार प्राप्त जाति-प्रधान पुरुष प्रधान संस्था है। यह उल्लेखनीय है कि उस समय जब अदालत - अपने अस्तित्व के लगभग तीन दशकों के बाद - अतीत में [गणपत बनाम रिटर्निंग ऑफिसर] के मामले में जाति का आरोप लगाया गया था,तब से दलित या आदिवासी समुदायों से अदालत का एक भी न्यायाधीश नहीं आया है। जाति की हिंसक भूमिका को अस्वीकार करना, न मानना और उस पर लीपापोती करना, और अचेतन रहना और ऊपर से ब्राह्मणवादी रुख की रक्षा करना तथा और यहां तक कि ब्राह्मणवादी तरीक़ों की वकालत करना शिक्षित शहरी उच्च जातियों की विशेषता है। इस प्रकार हम उच्चतम न्यायालय से थोड़ा भिन्न होने की अपेक्षा ग़लत कर रहे हैं। यह स्थिति निश्चित रूप से तब तक जारी रहेगी जब तक कि जाति, लिंग और सामाजिक हाशिए की अन्य सभी पंक्तियों को उसकी जनसांख्यिकी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता।
(सिद्धार्थ सीम मानव अधिकार क़ानून नेटवर्क से संबंधित वकील हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)
अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।