भारत को अपने पहले मुस्लिम न्यायविद को क्यों याद करना चाहिए
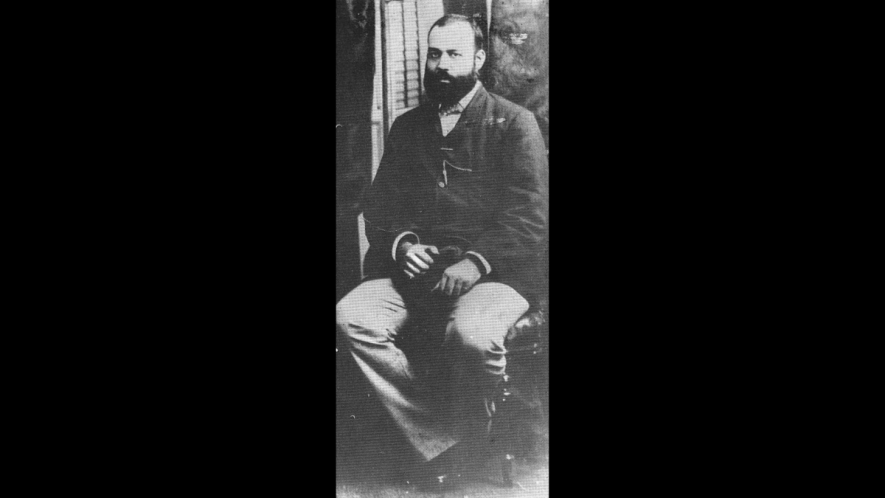
न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर ने पिछले साल दिसम्बर में हैदराबाद में आरएसएस से संबद्ध अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की 16वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था, “महान वकील और न्यायाधीश जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि वे सही तालीम और महान क़ानूनी परंपराओं के जरिए बनाए जाते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत में मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, नारद, पराशर, याज्ञवल्क्य और अन्य क़ानूनी दिग्गज थे।” न्यायमूर्ति नजीर ने “भारतीय विधिक प्रणाली का उपनिवेशीकरण” विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में यह भी कहा था कि “उनके महान ज्ञान की निरंतर उपेक्षा किए जाने और विदेशी औपनिवेशिक विधिक प्रणाली का पालन हमारे संविधान के लक्ष्यों और हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है...”.
शायद जस्टिस नजीर को 19वीं सदी के मशहूर विधिवेत्ता जस्टिस सैयद महमूद (1850-1903) को भी याद करना चाहिए था, जो औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था के खिलाफ मुखर थे और उन्होंने इस बारे में एक तल्ख क़ानूनी टिप्पणी पेश की थी, जो उनके एक दुस्साहसी असंतुष्ट दृष्टिकोण को दर्शाती है। तब एक उर्दू अखबार में लिखते हुए, उनके पिता सर सैयद अहमद खान ने 1893 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से महमूद के इस्तीफे को "ब्रिटिश न्यायाधीशों के नस्लवाद के खिलाफ भारतीयों के आत्मसम्मान की रक्षा" में उठाया गया एक कदम बताया था।
उस समय भी भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणाएं विकसित हो रही थीं। भारतीय न्यायाधीश तब साम्राज्यवादी सत्ता और यूरोपीय न्यायाधीशों के नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष करने का साहस नहीं जुटाते थे। इस खिलाफ माहौल में भी जस्टिस महमूद ने निडर तरीके से ऐसा किया, जो कई मायनों में बड़ा ही दुस्साहिक कदम था। खान ने 1877 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (एमएओ) कॉलेज की स्थापना की और समकालीन राष्ट्रवाद पर बहस में ब्रिटिश के प्रति वफादार और अलगाववादियों के प्रमुखता से आंकड़े दिए, जिस पर विवाद हुआ। महमूद ने अपने पिता की आधुनिक शिक्षा परियोजना का समर्थन किया, लेकिन दुर्भाग्य से, इतिहासकारों और क़ानूनी बिरादरी द्वारा उनके योगदान को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया।
1920 तक, एमएओ कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वह देश में सबसे प्रमुख आवासीय विश्वविद्यालय था। इसका इतिहास विभाग आधी सदी तक उन्नत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 1889 में, मुख्य रूप से सैयद महमूद की पहल पर एवं उनकी तरफ से पुस्तकों, पत्रिकाओं और नकदी के रूप में दिए गए उपहारों के बिना पर, एएमयू ने क़ानून संकाय की स्थापना की थी। हालांकि उसका शोध पक्ष उपेक्षित था। 1973 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शताब्दी के सात साल बाद, अलीगढ़ लॉ जर्नल ने महमूद के योगदान को प्रकाश में लाया और क़ानून के विद्वानों ने एक वकील और न्यायाधीश के रूप में उनकी उच्च दक्षता-क्षमता को प्रतिबिंबित किया।
एक अच्छी खबर यह है कि 2004 में, एलन एम गुएन्थेर ने मैकगिल विश्वविद्यालय, कनाडा में महमूद पर अपनी डॉक्टरेट थीसिस पेश की, जो अब जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। उनका सावधानीपूर्वक और अच्छी तरह से किए गए शोध का विवरण महमूद के सार्वजनिक जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। गुएन्थेर ने 19वीं शताब्दी के भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर महमूद के विचारों पर 2011 में एक विस्तारित निबंध भी प्रकाशित किया था।(1895 में, महमूद ने शैक्षिक सम्मेलन में अपने दिए गए भाषणों की थीम पर एक किताब लिखी थी।)
असफ़ अली असगर फ़ेज़ी (1899-1981) ने 1965 में यह शिकायत की, "भारत में मुस्लिम क़ानून के परिवर्तन में सैयद महमूद के योगदान को इतिहासकारों द्वारा काफी हद तक उपेक्षित कर दिया गया है और उन्हें मुख्य रूप से मुस्लिम क़ानून पर क़ानूनी ग्रंथों में फुटनोट्स के रूप में जीवित रखा गया है।” गुएन्थेर भी कहते हैं, “… अपने शानदार पिता, अहमद खान के जीवन और लेखन से अभिभूत होने के चलते, उनकी विरासत पर उतना गौर नहीं किया गया,जिसके वे हकदार हैं। शिक्षा के सुधार में उनके पिता की एक बड़ी उपलब्धि दरअसल सैयद महमूद की सहायता के बिना संभव नहीं थी। लेकिन जब वे उस उम्र तक पहुंच गए जिस पर उनके पिता ने अपनी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थीं, तो वे [महमूद] चल बसे थे।”
महमूद ने अपनी जिंदगी का खाका बड़ी शिद्दत से बनाया था। एस खालिद राशिद, 1973 में लिखते हुए, रिपोर्ट करते हैं कि महमूद ने तुरंत ही फैसला किया कि वे अपने पूर्वजों की तरह ही अपने जीवन की पहली तिहाई खुद को शिक्षित करने के लिए समर्पित करेंगे। दूसरी तिहाई का समय जिंदगी जीने के लिए और आखिरी तिहाई "सेवानिवृत्त हो कर अध्ययन, लेखन और सार्वजनिक उपयोगिता के मामलों के प्रति समर्पित रखेंगे।" लेकिन गुएन्थर लिखते हैं कि शराब के दुरुपयोग और बीमारी से महमूद की सेहत इस कदर बिगड़ गई थी कि 53 वर्ष की उम्र से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। वे जबरन सेवानिवृत्ति से टूट गए थे, अपने पिता (जिनका इंतकाल महमूद के इंतकाल से पांच साल पहले हो गया था) से अलग हो गए थे, जिस कॉलेज की स्थापना में उन्होंने मदद की थी, वहां की जिम्मेदारियों से उन्हें अलग कर दिया गया था, अपनी पत्नी और बेटे से अलग-थलग हो गए थे और गरीबी में जी रहे थे। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना निजी सामान बेचना पड़ता था। "उनके पिता के बेशुमार लेख और पत्र अभी भी अप्रकाशित हैं, लेकिन मुस्लिम विमर्श के लिए सैयद महमूद का योगदान भारतीय क़ानून रिपोर्ट की बाइंडिंग और सरकार से हुई चिट्ठी-पत्री की नाजुक फाइलों में छिपा हुआ है।"
महमूद की जिंदगी के अंतिम वर्षों के एक पहलू को प्रोफेसर इफ्तिखार आलम खान की उर्दू में लिखी दो पुस्तकों, सर सैयद: दारून-ए-खाना (2006, 2020) में और फिर हाल ही में प्रकाशित रुफ़क़ा-ए-सर सैयद:रफ़ाक़त, रक़ाबात वा इक़तिदार की कशमकश में बखूबी उकेरा गया है। ये विवरण सर सैयद के तीन परवर्ती सहयोगियों-शमीउल्लाह, मोहसिन-उल-मुल्क और विकार-उल-मुल्क-द्वारा सैयद महमूद के खिलाफ निंदा अभियानों का पर्दाफाश करते हैं क्योंकि उन्होंने एमएओ कॉलेज में सचिव पद के लिए वकालत की थी। एमएओ कॉलेज के यूरोपीय सदस्य अक्सर उनके साथ साजिश रचते थे। इन लोगों ने महमूद की कमजोरियों और सनक का फायदा उठाते हुए, उन्होंने कॉलेज से बाहर कर दिया,जिससे उनके जीवन के अंतिम सालों में गहरा आघात लगा।
सर सैयद के शैक्षिक उद्यम में महमूद की भूमिका
1872 में इंग्लैंड से अध्ययन कर भारत लौटने के बाद, महमूद ने अपने पिता के सुधार-कार्यों, विशेष रूप से एमएओ कॉलेज की स्थापना में सहायता करने के लिए अपने नए नए क़ानूनी करियर से समय निकालते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने अनुभवों की तर्ज पर एक विस्तृत योजना तैयार की थी। उनका खास मकसद जैसा कि फरवरी 1872 में समझाया गया था, एक शैक्षिक संस्थान के जरिए भारत के भविष्य के नेताओं को गढ़ना था, जिनकी आवासीय प्रकृति "अध्ययन के पाठ्यक्रम के रूप में अनिवार्य शिक्षा"होगी। इसका मकसद छात्रों और शिक्षकों का एक ऐसा समाज बनाना था, जो बाकी समाज से काफी अलग हो।
महमूद 1873 में अपने पिता के साथ पंजाब के दौरे पर भी गए और वहां की एक रैली में इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए भाषण दिया। 1889 में, सर सैयद ने महमूद को एमएओ कॉलेज के न्यासी बोर्ड के संयुक्त सचिव के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उनके विरोध के बावजूद उनकी सहायता पर प्रकाश डाला गया। विशेष रूप से, वे अपने बेटे के प्रभाव को वह प्राथमिक कारक मानते थे, जिसने यूरोपीय प्रोफेसरों को भारत आने और वहां पढ़ाने के लिए राजी किया था।
यूरोपीय स्टाफ मेम्बरानों ने लगभग छह साल बाद इसकी पुष्टि की जब संयुक्त सचिव के रूप में महमूद को बनाए रखने के मुद्दे पर नए सिरे से विरोध किया गया था। प्रिंसिपल, थियोडोर बेक (1859-1899), ने कहा था, "सैयद अहमद ने सभी मामलों में सलाह के लिए सैयद महमूद पर अपनी निर्भरता को कबूल किया था और स्कूल से संबंधित पत्राचार में इसकी छाप देखी जा सकती है। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास जताया था कि सैयद महमूद एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज के विकास के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया था, और उनके अलावा, कोई भी उस नजरिए से स्कूल का प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं होगा।” हालांकि, समीउल्लाह (1834-1908) के इस ब्योरे पर सर सैयद से असहमत थे। इसके चलते कॉलेज प्रबंधन में सत्ता के लिए खींचतान शुरू हो गई। इस पावर-प्ले ऐसे समझा सकता है कि एएमयू ने महमूद की जीवनी को रोशनी में लाने में बाधा क्यों महसूस की थी और उन पर शोध के अंतर को गुएन्थेर की डॉक्टरेट थीसिस पाटता है। उन्होंने अपने शोध कार्य में लंदन इंडिया ऑफिस (ब्रिटिश) लाइब्रेरी में संरक्षित महमूद के महत्त्वपूर्ण पत्राचारों पर व्यापक रूप से भरोसा किया है।
मुस्लिम क़ानून से सैयद महमूद का साक्षात्कार
महमूद आधुनिक दक्षिण एशिया में मुस्लिम क़ानून के परिवर्तन के एक भूले-बिसरे अग्रदूत हैं।1882 में,केवल 32 वर्ष की उम्र में, वे ब्रिटिश भारत में उच्च न्यायालयों के पहले मुस्लिम न्यायाधीश बने थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने मुस्लिम क़ानून, सामान्य क़ानून और इसके प्रशासन को आकार देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय दिए।
इससे पहले, उन्होंने ब्रिटिश भारत में अपनी न्यायिक भूमिकाओं में अपने युवा समकालीनों में पर्याप्त प्रभाव पैदा किया। वे इंग्लैंड जा कर अध्ययन करने वाले और न्यायशास्त्र की अंग्रेजी प्रणाली में प्रशिक्षित होने वाले पहले भारतीय मुसलमान थे। 1872 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में बैरिस्टर के रूप में नामांकित होने वाले पहले भारतीय थे। 1879 में अवध की पुनर्गठित न्यायिक प्रणाली में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए पहले भारतीय थे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए पहले भारतीय थे। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए भारत में न्याय प्रशासन में शामिल होने का एक मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन उनका योगदान मुस्लिम युवाओं के लिए मलाईदार कैरियर के अवसरों तक ही सीमित नहीं है। उनकी स्थायी विरासत यह है कि आज दक्षिण एशिया में मुस्लिम क़ानून को माना जाता है और प्रशासित किया जाता है।
सुलभ न्याय के चैंपियन
महमूद की एक स्थायी चिंता न्यायिक पाने में आने वाली लागत थी। अदालत की प्रक्रिया लंबी और महंगी थी, और "मॉस ऑफ लॉ" जटिल था। अदालतों से दूरी उनकी एक और चिंता थी, जिसके लिए उन्होंने "ऑन-द-स्पॉट" निर्णय के लिए ग्राम अदालतों का एक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने अवैतनिक न्यायाधिकरणों और मानद मुंसिफों के माध्यम से न्याय को सुलभ बनाने की मांग रखी थी। उन्होंने इसके लिए एक व्यापक मसौदा तैयार किया, जैसा कि गुएन्थेर बताते हैं।
इसके अलावा, उन्होंने [नस्लीय] मानसिकता और अदालत की फीस और क़ानूनी दस्तावेजों पर लगने वाले स्टांप शुल्क पर भी प्रहार किया। उन्होंने अगस्त 1884 और फरवरी 1885 में व्यवस्था दी कि "यदि न्याय पाने का खर्चा अमीरों और गरीबों के लिए एक समान रखा जाता है तो यह इसका मतलब होगा कि अमीर आदमी तो इसे खरीदने में सक्षम होगा, जबकि गरीब आदमी नहीं होगा।” उन्होंने एक से अधिक बार यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश न्यायाधीश धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे थे।
इलाहाबाद बार में अप्रैल 1885 में दिए गए अपने एक भाषण में, महमूद ने न्यायिक व्यवहारों में अपनाई जाने वाली भाषा का मुद्दा उठाया और कहा कि क़ानून जनता को समझ में आने वाली भाषाओं में होना चाहिए। उन्होंने तर्कों, दलीलों और न्याय प्रदान करने और अदालती फैसलों के स्थानीय भाषा में अनुवाद कराए जाने पर जोर दिया ताकि जो लोग अंग्रेजी से अपरिचित हैं, वे भी इस बात को लेकर आश्वस्त रह सकें कि उनके मामले में किया गया निर्णय तर्कपूर्ण है। बेशक, न्यायिक भाषा के मुद्दे पर बहस आज भी जारी है, और इसका श्रेय भी महमूद को जाता है।
ब्रिटिश उपनिवेशवाद की दोपहर में एक भारतीय असंतुष्ट
महमूद अपने बेहतरीन असहमति वाले फ़ैसलों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। रोहिंग्टन एफ.नरीमन अपनी 2021 पुस्तक के खंड 2 में, डिस्कोर्डेंट नोट्स, जस्टिस (रिटायर्ड) में लिखते हैं कि महमूद विस्तृत निर्णय देने के लिए जाने जाते थे, जिनमें से कुछ अपनी संपूर्णता में और निडर भाषा में लिखे गए हैं। महमूद हिंदू क़ानूनों पर फैसला देते समय प्रासंगिक ग्रंथों की व्याख्याओं का उपयोग करने की बजाय संस्कृत के मूल संस्करणों का और मुस्लिम क़ानूनों के लिए अरबी ग्रंथों पर उल्लेख करते थे।
1860 के दशक से 1880 के दशक तक, क़ानूनों के संहिताकरण के दौरान, जस्टिस महमूद ने भारत में लागू किए जाने वाले ब्रिटिश क़ानूनों की तादाद को सीमित करने की मांग की और इस बात को लेकर विरोध किया कि ब्रिटिश क़ानून भारत के स्थानीय संदर्भ की अनदेखी कर रहे हैं। उनकी चिंता न केवल क़ानून को लेकर थी बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के भीतर उनकी प्रभावकारिता और अनुकूलनशीलता के बारे में भी थी।
गुएन्थेर का मानना है कि... “वे अपने पूरे जीवन में, खुद को एक मुसलमान के साथ-साथ एक भारतीय और ब्रिटिश ताज का भी विषय माना। वे भारतीय मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और उनमें सुधार को लेकर सक्रिय रूप से शामिल थे। उसी समय, महमूद ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयास किए, और... धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना सभी भारतीयों की स्थिति में सुधार की पहल का (समर्थन) किया...”
इस प्रसंग में, अल्ताफ हाली की हयात-ए-जावेद (1901) का एक किस्सा, साझा करने के काबिल है, जिसे शम्सुर रहमान फारुकी (2006) ने उद्धृत किया है।"अंग्रेजी औपनिवेशिक हुकूमत के सामने चापलूसी करने और उनकी गोद में जा बैठने की संस्कृति के विपरीत सैयद अहमद खान और उनकी ऊंची शख्सियत वाले प्रतिभाशाली बेटे सैयद महमूद खुद को ऐसे पेश करते रहे जैसे कि वे अंग्रेज के बराबर हैं...सैयद अहमद खान (1867 के आगरा) दरबार से दूर-दूर ही रहे क्योंकि अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों कमतर सीटें दी गई थीं। उस दरबार में सैयद अहमद खान को एक पदक दिया जाना था। मेरठ के तत्कालीन कमिश्नर विलियम्स को बाद में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सैयद अहमद खान को पुरस्कार देने के लिए नियुक्त किया गया। विलियम्स ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और इस पर रंज किया कि उन पर दबाव डालकर काम कराया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकारी आदेश पालन करने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है अन्यथा वे सैयद अहमद खान को पदक पेश नहीं करते। सैयद अहमद खान ने यह कहते हुए पदक स्वीकार कर लिया कि वे यह पुरस्कार नहीं लेते पर वे भी सरकारी आदेशों से बंधे थे।”
भारतीय लोकतंत्र उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का परिणाम है, और असहमति इसका मुख्य घटक है: महमूद की असहमति ने उनके समय में राष्ट्रवाद में अपना योगदान दिया था। 2022 में, वी-डेम इंस्टीट्यूट ने भारत को एक चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है, जहां असहमति का अपराधीकरण किया जा रहा है, और न्यायपालिका बहुसंख्यकवादी उत्थान को रोकने में विफल रही है। ऐसे में महमूद का पेशेवर आचरण भारतीय न्यायपालिका में गिरावट के लिए एक उत्साहजनक काउंटरपॉइंट है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में महमूद की सोच
गुएन्थेर के अनुसार, हालांकि महमूद कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन वे कांग्रेस विरोधी प्रचार से "समान रूप से अलग" थे, पर उनके पिता उसमें शामिल थे।"...उन्होंने एक दुर्लभ कैथोलिकता से अधिकांश विवादास्पद प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त किए," वे लिखते हैं। गुएन्थेर आगे कहते हैं,“हिंदुओं [अभिजात्यों] के बीच उनकी स्वीकृति आम तौर पर इस तथ्य से जाहिर हुई थी कि उन्होंने महमूद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजने की कोशिश की, हालांकि उन्हें वह नियुक्ति कभी नहीं मिली।”
फिर भी, अपने पिता की तरह, महमूद ने वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को बरकरार रखा। गुएन्थेर ने 4 सितम्बर 1875 को द पायनियर में महमूद के एक लेख का खुलासा किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार को "मूल निवासी के उच्च वर्ग" के प्रति सहानुभूति के साथ प्रयास करना चाहिए। जब दो सप्ताह बाद एक ही समाचार पत्र में "एक और मूल निवासी" द्वारा अपनी स्थिति का बचाव करते हुए उसे चुनौती दी गई, तो महमूद ने इसका जवाब दिया कि पंजाब और उत्तर-पश्चिमी प्रांत [अब उत्तर प्रदेश] के लोग ऐतिहासिक रूप से निचले बंगाल की तुलना में "बहुत अधिक राजनीतिक महत्त्व" के थे। गुएन्थेर ने अपने लेखन का हवाला देते हुए कहा: "ऐसी कोई भी शैक्षिक प्रणाली जो बंगाली को आकर्षित करने में तो सफल रही और राजपूत, सिख और मुसुलमान के उच्च वर्गों पर कोई भी प्रभाव डालने में असफल रही, उस प्रणाली की विफलता ही मानी जानी चाहिए।”
एएमयू के शीर्ष पदाधिकारियों की सामाजिक-क्षेत्रीय संरचना को ध्यान में रखते हुए, यहां तक कि निष्पक्ष अंदरूनी सूत्र यह भी प्रमाणित करेंगे कि यह अभी भी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को बरकरार रखता है। सर सैयद अकादमी एएमयू के चल रहे शताब्दी समारोह के दौरान कई प्रकाशनों का विमोचन कर रही है। गुएन्थेर के शोध प्रबंध का प्रकाशन इस दिशा में एक उचित श्रद्धांजलि हो सकता है, उन्हें अवश्य ही एमएओ कॉलेज के एक प्रमुख सह-संस्थापक के रूप में माना जाना चाहिए।
(मो. सज्जाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आधुनिक और समकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं। मो. ज़ीशान अहमद दिल्ली के एक वकील हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)
अंग्रेज़ी में मूल रूप से लिखे गए लेख को पढ़ने के लिए नीचे के लिंक पर क्लिक करें
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।























