गुजरात और हिंदुत्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था
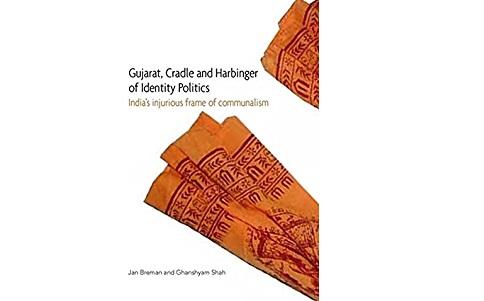
हिंदुत्व के उदय का सबसे हालिया विश्लेषण या तो एक बढ़ती-विकसित ‘हिंदू चेतना' के आसपास उसका विशिष्ट सांस्कृतिक विश्लेषण था या फिर चुनावी अंकगणित के ईर्द-गिर्द एक राजनीतिक विश्लेषण। इन विश्लेषण में से जो गायब था, वह एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था विश्लेषण था कि कैसे विकास मॉडल में किए गए बदलाव ने सांस्कृतिक बहुसंख्यकवाद के उदय में भी अपना शानदार योगदान दिया है। हाल ही में जन ब्रेमन और घनश्याम शाह की एक किताब Gujarat: Cradle and Harbinger of Identity Politics: India's Injurious Frame of Communalism आई है, जो इस खाली स्थान को भरती है।
ब्रमैन एक प्रसिद्ध मानवविज्ञानी हैं और घनश्याम शाह एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। ब्रेमन के निबंध वर्ग गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि शाह बुनियादी रूप से जाति पर अपने को फोकस करते हैं। साथ में, वे अनुभवजन्य और ऐतिहासिक विश्लेषणों का खजाना प्रदान करते हैं। उनके विवरण अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। उनकी पुस्तक,पिछले दो दशकों में दोनों लेखकों द्वारा लिखे गए निबंधों का एक समृद्ध संग्रह है, जिसका बस यही एक शीर्षक हो सकता था-हिंदुत्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। उनका विश्लेषण जाति और वर्ग की बदलते गत्यात्मकता के सुविधाजनक बिंदु से आता है, और किताब में, गुजरात में विभिन्न दंगों के दौरान और उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में काफी जानकारियां जुटाई गई हैं।
वर्ग के संदर्भ में, लेखकद्वय का विश्लेषण मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम और "लुम्पेन सर्वहारा" में संलिप्त लोगों की बढ़ती अनौपचारिकता, हिंसा और आपराधिकता के अंतर्पृष्ठ पर केंद्रित है। ट्रेड यूनियनवाद की गिरावट और कपड़ा मिलों के बंद होने से "समुदाय भावना का सघन जुड़ाव" टूट गया था। "सामाजिक डार्विनवाद की जलवायु ने इसे बदल दिया। इसने यह स्थापित किया कि केवल योग्यतम को ही जीने का हक है, बल्कि इसका आशय था कि समाज के नीचले पायदान पर खड़ा सबसे कमजोर व्यक्ति..खुद ही शिकारी और शिकार के रूप में होड़ लेने के लिए मजबूर है।"
बहुसंख्यकवाद की हिंसक राजनीति विकास मॉडल के सामाजिक डार्विनवाद के तर्क पर आधारित थी। पाठ्यपुस्तक की परिभाषाओं से खींची गई ट्रेड यूनियनवाद की ब्लिंकर्ड समझ ने सामाजिक डार्विनवाद को भी सहायता प्रदान की। यह समझ जमीन पर हुए ठोस विकास से बेखबर थी। जैसा कि ब्रेमन ने सही ही कहा है, "अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को एकजुट न करने के लिए भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन की चली आ रही नीति को एक ऐतिहासिक गलती के रूप में आंका जाना चाहिए।” ये परिवर्तन जातिगत चेतना और वर्गीकृत असमानताओं की मानसिकता के साथ अतिव्यापी थे। किताब के लिए किए गए अनुभवजन्य सर्वेक्षण गुजरात में उनके अथक काम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें ब्रमैन कहते हैं,"मिल श्रमिकों में, यह कानबी पटेल/पाटीदार थे-एक उच्च गतिशील मध्यवर्त्ती जाति के रूप में गिने जाते हैं, वे कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाने के लिए सबसे अधिक तत्पर थे।"
यह किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी (आरएसएस-भाजपा) दोनों की संयुक्त रणनीति में बदलाव को बड़ी मेहनत से पड़ताल करती है। इसकी शुरुआत हिंदू-जातियों को संगठित करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के साथ की गई थी। लेकिन 1985 के बाद, और ओबीसी के बढ़ती दखल के बाद, यह एक अधिक आक्रामक मुस्लिम विरोधी एजेंडा में बदल गया, जिसमें पिछड़े वर्ग धीरे-धीरे सहयोजित कर लिए गए थे। मुस्लिम-विरोधी राजनीति न केवल स्पष्ट और संगठित हिंसा में दिखाई देती थी, बल्कि इसके विरोध में छिपी और अदृश्य आर्थिक अव्यवस्था में भी वह दिखती थी। उदाहरण के लिए, मिलों ने धीरे-धीरे मुस्लिम मजदूरों की जगह पटेलों को दे दी, और इसके बाद, खुले तौर पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार आह्वान किए गए थे।
ये ‘मौन' परिवर्तन आर्थिक सुधार के साथ-साथ चलते गए जिन्होंने श्रमिकों को अधिक से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र में धकेल दिया, जहां उनके पास किसी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उनकी बढ़ती आर्थिक असुरक्षा और एक संगठित क्षेत्र के सम्मानजनक श्रमिकों की सामाजिक हैसियत रूप में गिरावट ने सांप्रदायिक दुष्प्रचार की पृष्ठभूमि बनाई। इसने गुस्से को भड़कने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया, यहां तक कि काफी हिंसा भी बरपाई गई। इस हिंसा ने स्लम लॉर्ड्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा जबरन वसूली के माध्यम से "सार्वजनिक जीवन के अपराधीकरण" और "हिंसा के निजीकरण" का आकार लिया। इन सभी मिल-मिलाकर "बेदखली के जरिए दौलतमंद" होने की रवायत को बढ़ावा दिया। इन बदलावों ने गुजरात के नसीब को सील कर दिया और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ठोस नींव रख दी।
पुस्तक के अन्य विषय जाति, सांप्रदायिकता, दलित, आदिवासी, ओबीसी और हिंदुत्व हैं। कई अध्यायों की श्रृंखला में घनश्याम शाह हिंदुत्व के पुनरुत्थानशील हिंदूकरण के रूप में उभरने का एक जटिल विवरण प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है,'आदिवासियों ने अपने आसपास रहने वाले जातिगत हिंदुओं की कई मान्यताओं और देवताओं को अपना लिया है, जिस तरह हिंदुओं ने आदिवासियों के कई देवताओं को अपनाया है, और कई मामलों में, दोनों एक-दूसरे से अलहदा भी एक जैसे अनुष्ठानों और मान्यताओं का पालन करते हैं। कुछ मामलों में, तो किंवदंतियां हैं कि हिंदू जातियां आदिवासियों द्वारा पूजे गए देवताओं को ब्राह्मणवादी नाम देते हैं।”
इसी तरह, ओबीसी के लिए शाह ने कहा, “बीसवीं सदी की शुरुआत से, कई ओबीसी ने ऊंचे श्रेणी क्रम की तरफ अपनी गतिशीलता के लिए संस्कृतकरण के मार्ग का अनुसरण किया है। मध्य और उत्तरी गुजरात का कोली समुदाय का एक वर्ग खुद के क्षत्रिय का दर्जा पाने का दावा किया है। इस समुदाय के लोगों ने समय के साथ, “उपनयन” का वैदिक अनुष्ठान करते हुए जनेऊ धारण करना शुरू कर दिया है। दलितों के साथ, यह प्रक्रिया, प्रो. आनंद तेलतुंबड़े के कहे मुताबिक "डी-रैडिकलाइजेशन" की तरफ हुई है। गतिशीलता और एक छोटे मध्यम वर्ग के उद्भव ने विशिष्टावादी विमर्श को जन्म दिया है।
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के संदर्भ में, शाह का तर्क है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि दलितों को मुसलमान विरोधी किसने बनाया। वे इसे "केवल" सहयोजन और जोड़-तोड़ की एक कवायद के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है, '2002के दंगों के इस दौर में भाजपा ने दलितों की सहानुभूति में फेरबदल किया और उन्हें राहत प्रदान की। इन दंगों के बाद, अहमदाबाद के दलित भाजपा और (आरएसएस) परिवार के करीब आने लगे।”
शाह और ब्रेमन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक चेतना की शुरुआत और उनकी भौतिक जड़ों को समझने में एक बड़ी स्थायी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आज हिंदुत्व के बारे में कोई समझ बनाने के लिए इसे समझना आवश्यक है, यहां तक कि अपरिहार्य भी है। लेकिन इसके साथ ही, इस समझदारी में एक नया आयाम जोड़ने की भी महत्ती आवश्यकता है कि मौजूदा गतिरोध बनाने के लिए चीजें एकदम से कैसे घूम गईं। ऐतिहासिक हवाले से कहें तो यह पुस्तक बहुसंख्यकवादी मानसिकता की जांच-परख के लिए गांधी-आंबेडकर बहस को प्रभावशाली मानती है।
फिर भी, मुद्दा यह है कि गांधी और आंबेडकर के योगदान को पूरक और परिवर्धक मानने वाले अधिकांश विद्वानों के विपरीत, देश की वर्तमान स्थिति उनकी रणनीतियों और सिद्धांतों के नकारात्मक पक्ष का ही नतीजा है। गांधीवादी तरीकों के परिणामस्वरूप आधे-अधूरे सामाजिक सुधार हुए और वे घने एवं गहन अंतर-सामुदायिक संबंध बनाने में विफल रहे। गांधी पहचान और परिवर्तन के बीच आर्किमिडीयन बिंदु को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा, आत्म-सीमित जरूरतों की उनकी समझ, गैर हस्तक्षेपवादी राजनेता के रूप में उनकी चुप्पी, और स्वयं को अनुशासित करने की उनकी पद्धति उन प्रथाओं में बदल गई है, जो सबाल्टर्न गतिशीलता को रोकती हैं। कम से कम, उन्हें ऐसा माना जाता है, इस तरह वे बर्बर आक्रामकता के दावे को एक वैध रास्ता दे रही हैं। जब विकास के लाभ का इंतजार करते-करते समाज के निचले छोर का धीरज चुकने लगा, तब भाजपा ने इसे पुरुषवादी बाह्यता में बदल दिया। दोनों के बीच सामंजस्य ही हिंदुत्व को उसकी अलंकारिक वैधता प्रदान करता है।
दूसरी ओर, आंबेडकर ने "दमित वर्गों" की सामाजिक हैसियत में बदलाव को जोड़े बिना ही उनको राजनीतिक ताकत हासिल कराने को अपनी प्राथमिकता दी। इसका परिणाम यह हुआ कि बिना किसी सामाजिक एजेंडे के राजनीतिक प्रतिनिधित्व उस व्यापक लामबंदी के लिए आवश्यक संसाधनों के अभाव में महज कोरी बयानबाजी बन कर रह गया। इससे हिंदुत्व को भी मदद मिली, जब इसने दलित-बहुजनों को राजनीतिक रूप से हिंदूकरण के प्रमुख क्षेत्रों में सामाजिक समावेश के साथ समझौते के रूप में समायोजित करना शुरू किया।
आज, औद्योगिक राज्य गुजरात में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समझ की तुलना उत्तर प्रदेश जैसे गैर औद्योगिक राज्य में इसके प्रसार से करने की आवश्यकता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिण और उत्तर - पूर्व के कुछ राज्यों को छोड़कर, भारत की सामाजिक वास्तविकता को व्यापक रूप से कवर करता है। गुजरात में मजदूर औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र में चले गए और इस तरह उन्होंने अपनी सामाजिक सुरक्षा खो दी है, वहीं उत्तर प्रदेश में, ओढ़ी गई अविकसितता एवं बुनियादी संरचनाओं तथा नागरिक सुविधाओं की कमी है। भाजपा ने खुद मुफ्त राशन के वितरण के माध्यम से लेन-देन संबंधी कल्याणवाद को अपना लिया है। इस तरह का कल्याणवाद संघ परिवार की इस तीव्र समझ को दर्शाता है कि उसको रणनीतियों में न केवल लचीला होने बल्कि द्वंद्वात्मक होने की आवश्यकता है, जबकि वाम-प्रगतिशील श्रेणीगत भूल से पीड़ित हैं-प्रतिबद्धता के लिए भ्रमित हठधर्मिता और वैज्ञानिकता के लिए पाठ्यपुस्तकीय समझ से।
धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के साथ दिक्कत है, और यह केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं है कि वे लचीले नहीं हो सकते। लचीला होने का मतलब जोड़-तोड़ करने वाला होना नहीं है, हालांकि यह दूसरी तरफ भी फैलना हो सकता है (अधिकांश दक्षिणपंथी रणनीतियों के साथ)। हम एक जिद्दी धर्मनिरपेक्ष विमर्श और अधिकार के अनैतिक लचीलेपन के बीच फंस गए हैं। अनैतिक लचीलापन छिपे तौर पर समावेशी है, और वाम-धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक और नैतिक रूप से विशिष्टतावादी हैं। इस पुस्तक के दोनों लेखकों की तरह प्रतिष्ठित विद्वानों को भी यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि इस गॉर्डियन गाँठ को कैसे तोड़ा जा सकता है।
(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं)
अंग्रेजी में मूल रूप से लिखे गए लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।














