तेलंगाना कांड : क्या है न्याय का तक़ाज़ा, क्या है लोकतंत्र की कसौटी?
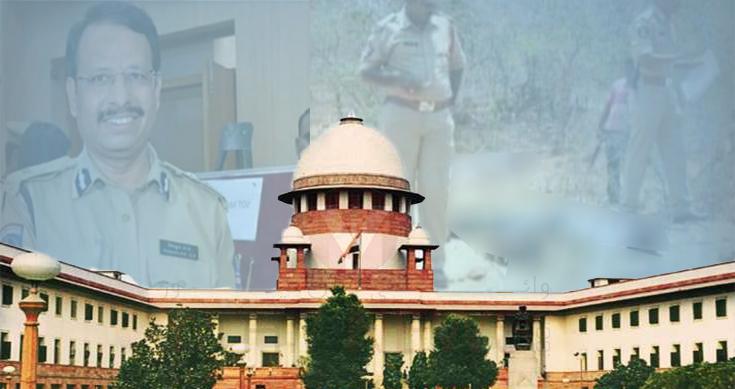
बात 1990 के दशक की है। अविभाजित मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा में मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी उस इलाके के मजदूरों और उनके परिवारजनों के बीच काफी लोकप्रिय थे। इसी वजह से वे वहां के भ्रष्ट उद्योगपतियों, शराब माफिया और उनकी संरक्षक मध्य प्रदेश सरकार (कांग्रेस और भाजपा दोनों ही) की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इसी नाते हमेशा पुलिस के भी निशाने पर रहते थे।
शराब माफिया, नियोगी को इसलिए अपना दुश्मन मानता था कि उन्होंने अपनी यूनियनों से जुड़े 70 हजार से अधिक मजदूरों की शराब छुड़वा दी थी, जिसकी वजह से उनका शराब का कारोबार प्रभावित हो रहा था। एक दिन मजदूरों के एक प्रदर्शन के सिलसिले में जिले की पुलिस 'शांति भंग’ के आरोप में नियोगी को गिरफ्तार कर दल्ली राजहरा से भिलाई ला रही थी। घने जंगलों से गुजरते हुए खुली जीप जब रास्ते में कुछ मिनटों के लिए रुकी तो नियोगी से एक पुलिस वाले ने कहा कि मौका अच्छा है, भाग जाओ, हम कह देंगे कि नियोगी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। नियोगी पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराए और कहा- ''मुझे मालूम है कि मैं जीप से उतर कर कुछ दूरी तक ही जाऊंगा और तुम लोग पीछे से मुझे गोली मार दोगे। बाद में कह दोगे कि नियोगी पुलिस को धोखा देकर भाग रहा था, इसलिए हमने उसे मार दिया। इसलिए मुझे कहीं नहीं भागना है। तुम लोग गाड़ी आगे बढ़ाओ और जिस जेल में बंद करना है, वहां ले चलो।’’
नियोगी उस समय तो नहीं मारे जा सके लेकिन कुछ ही वर्षों बाद सितंबर 1991 में भाड़े के हत्यारों ने नियोगी की उस समय हत्या कर दी जब रात में वे अपने घर में सो रहे थे। उनकी हत्या के पीछे कौन लोग थे और उनको बचाने वाली ताकतें कौन थी, यह एक अलग कहानी है। यहां मूल मुद्दा है नियोगी को एनकाउंटर में मारने की उस कोशिश का, जो कामयाब नहीं हो सकी थी।
यह बात तीन दशक से भी ज्यादा पुरानी हो गई है लेकिन पुलिस का एनकाउंटर का तरीका कमोबेश वही है, जो वह नियोगी के साथ आजमाना चाहती थी। तब से लेकर अब तक देशभर में इस तरह के सैकड़ों 'एनकाउंटर’ हुए हैं और कमोबेश सबकी कहानी एक जैसी है। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस के हाथों बलात्कार के चार आरोपियों के मारे जाने की कहानी भी उन सब कहानियों से जुदा नहीं लगती।
दरअसल, लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव ही नहीं होता। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि उसमें मानवाधिकारों की कितनी हिफ़ाज़त और इज़्ज़त होती है। इस मामले में भारतीय लोकतंत्र का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमारे यहां पुलिस का रवैया लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के तकाजों से कतई मेल नहीं खाता है। आम आदमी पुलिस की मौजूदगी में अपने को सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करने के बजाय उसे देखकर ही खौफ खाता है।
फर्जी मामलों में किसी बेगुनाह को फंसाने और पूछताछ के नाम पर अमानवीय यातना देने की घटनाएं आमतौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा बनी हुई हैं। फर्जी मुठभेडों में होने वाली हत्याओं के साथ ही हिरासत में होने वाली मौतें इस सिलसिले की सबसे क्रूर कडियां हैं। अफसोस की बात यह भी है कि हमारी सरकारें और ज्यादातर राजनीतिक जमातें इस पुलिसिया क्रूरता पर अमूमन चुप्पी साधे रहती हैं। अलबत्ता हमारी न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर समय-समय पर ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त रूख अपनाया है और केंद्र व राज्य सरकारों को कडी फटकार लगाई है।
कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में तो इस तरह की घटना को वर्दी में की गई हत्या करार देकर दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा देने तक की सिफारिश भी थी। 2014 में तो देश की सबसे बडी अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुठभेड की बाबत पुलिस के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे और उनका सख्ती से पालन करने को कहा था।
पुलिस के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में हालांकि इस हकीकत को स्वीकार किया था कि पुलिस को आतंकवादियों, संगठित अपराधिक गिरोहों और जघन्य अपराधियों से मुकाबला करना पड़ता है। इसमें पुलिस को अपने लिए खतरा उठा कर कार्रवाई करनी पडती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बेशक, ऐसा करना पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन इसके बरक्स फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं भी होती रहती हैं। इसके पीछे बडा कारण पुरस्कार या पदोन्नति का लोभ होता है। इसलिए शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि एनकाउंटर वास्तविक था, यह साबित होने के बाद ही एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी को बिना बारी के पदोन्नति का लाभ दिया जाए।
अपने उसी फैसले में अदालत ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था भी दी थी कि पुलिस एनकाउंटर में होने वाली हर मौत पर एफआईआर दर्ज की जाए और सीआरपीसी की धारा 176 के तहत उसकी जांच सीआईडी या किसी अन्य जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या मजिस्टेट से कराई जाए। जांच रिपोर्ट राज्य मानवाधिकार आयोग अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर कोई फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, तो मारे गए व्यक्ति के परिजन मुकदमा दायर कर सकते हैं। आदेश में यह भी कहा गया था कि पुलिसवालों को अपराधियों के बारे में मिली सूचना को रिकॉर्ड कराना होगा और हर एनकाउंटर के बाद अपने हथियार तथा कारतूस जमा कराने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इन दिशा निर्देशों को पांच वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फर्जी एनकाउंटर का सिलसिला देश के विभिन्न राज्यों में आज भी बना हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश भर की पुलिस और राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को नजरअंदाज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उसके दिशा निर्देशों पर अमल क्यों नहीं हो रहा है।और आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर कहना पड़ा है कि तेलंगाना पुलिस एनकाउंटर की की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इसके लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।
इसे पढ़ें : तेलंगाना बलात्कार-हत्या: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे 'एनकांउटर' की जांच
पांच वर्ष पहले अपने विस्तृत आदेश के जरिए ने सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 21 की याद भी दिलाई थी, जिसमें देश के हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। हालांकि इस अनुच्छेद के विरोधाभास भी हमारे कई कानूनों में मौजूद हैं। इसका सबसे बडा उदाहरण सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) है, जिसके तहत सुरक्षा बलों को दंडमुक्ति के आश्वासन के साथ किसी भी हद तक जाने की छूट हासिल है; उनके खिलाफ केंद्र की इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
विवादास्पद कानून से मिली यह निरंकुशता ही जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में फर्जी एनकाउंटर की घटनाओं की जड रही है। मणिपुर हो या जम्मू-कश्मीर, जब भी वहां तैनात सशस्त्र बलों पर फर्जी एनकाउंटर में किसी को मार दिए जाने, लूटपाट करने या महिलाओं से बलात्कार करने के आरोप लगते हैं और उनकी जांच कराने की मांग उठती हैं तो हमारी सरकार का एक ही घिसा-पिटा जवाब होता है कि ऐसा करने से सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा। जनता के मनोबल का क्या होगा, इस बारे में सरकार कभी नहीं सोचती। यह भी कभी नहीं सोचा जाता कि कुछ सुरक्षाकर्मियों के दुष्कृत्य के चलते पूरी सेना की साख पर आंच क्यों आने दी जाए?
दरअसल, अस्सी के दशक में आतंकवाद से प्रभावित पंजाब और अंडरवर्ल्ड गतिविधियों से हलाकान मुंबई से शुरू हुई फर्जी एनकाउंटर की बीमारी देखते-देखते पूरे देश में फैल गई। पुलिस और सुरक्षाबलों ने मुकदमेबाजी के चक्कर से बचने के लिए अपराधियों/आरोपियों को 'टपका देने’ यानी मार गिराने की एक तरह से अघोषित नीति ही बना ली। इस पुलिसिया नीति को राजनीतिक नेतृत्व की भी परोक्ष शह हासिल रही। इसीलिए 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ कहलाने वाले विवादित पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन या वीरता पदक से नवाजने के भी उदाहरण मिलते रहते हैं। पर्दे के पीछे से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की सरकारी नीति का ही नतीजा है कि ऐसी घटनाएं समय के साथ बढ़ती गईं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक 2002 से 2008 के बीच देश भर में कथित फर्जी एनकाउंटर की 440 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि 2009-10 से फरवरी 2013 के बीच संदिग्ध फर्जी एनकाउंटर के 555 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक ही जनवरी 2015 से मार्च 2019 के बीच उसे फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें मिली हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले आंध्र प्रदेश से 57 और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 39 हैं।
यह समस्या कितनी गंभीर हो चली है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगस्त 2011 में तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के हाथों फर्जी एनकाउंटर में हुई एक मौत के मामले की सुनवाई करते हुए ऐसे मामलों में दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने तक सुझाव दे दिया था। मामला यह था कि अक्टूबर, 2006 में राजस्थान पुलिस ने दारा सिंह नामक एक कथित अपराधी को मार डाला था और यह प्रचारित किया था कि वह एनकाउंटर में मारा गया है। इस मामले में पुलिस के कई बडे अधिकारी भी शामिल थे। राज्य के एक पूर्व मंत्री और भाजपा नेता समेत कुल सोलह आरोपियों में से कई तो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के वक्त तक फरार थे। मई 2011 में भी इसी तरह के एक मामले को दुर्लभ में भी दुर्लभतम किस्म का अपराध करार देते हुए तथा आरोपी पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही सुझाव दिया था।
यह सुझाव देते हुए न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद ने सवाल किया था कि पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह लोगों को अपराध और अपराधियों से बचाए लेकिन अगर पुलिस ही अपराध करने लगे या किसी की जान लेने लगे तो कानून के शासन का क्या होगा? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था, इत्तेफाक से उसी दिन जम्मू में मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति को आतंकवादी बताकर मार दिए जाने की खबर आई थी। बाद में हुई जांच से पता चला था कि पुरस्कार और पदोन्नति पाने के चक्कर में एक 'आतंकवादी’ को एनकाउंटर में मार गिराने का यह झूठा किस्सा गढ़ा गया था।
इस सिलसिले में सबसे बेहद सनसनीखेज मामला छत्तीसगढ के सारकेगुडा गांव का है, जहां 28 जून 2012 को 17 आदिवासियों को, जिनमें कुछ बच्चे भी थे, नक्सली बताकर मार डाला था। उस घटना की न्यायिक जांच की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, जिसमें बताया गया है कि वे सभी आदिवासी बेकुसूर थे।
वैसे पुरस्कार और पदोन्नति के लालच के अलावा सबूत मिटाने के मकसद से भी कई बार फर्जी मुठभेड का नाटक रचा जाता है। गुजरात में तो पिछले दशक में ऐसी घटनाओं की बाढ़ ही आ गई थी। वहां सोहराबुद्दीन, उसकी बीवी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति की पुलिस द्वारा हत्याएं इसीलिए की गई थीं। इस मामले में अदालत के सख्त रुख के चलते गुजरात के कई आला पुलिस अधिकारियों को जेल जाना पड़ा। इसी तरह का मामला कुछ साल पहले माओवादी नेता चेरू कुरि राजकुमार उर्फ आजाद और पत्रकार हेमचंद्र पांडेय की आंध्र प्रदेश पुलिस के हाथों हुई मौत का भी है। इस मामले की जांच कराने में आंध्र प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भी आनाकानी करती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन दोनों के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की पुष्टि हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा गणतंत्र इस तरह अपने बच्चों को नहीं मार सकता।
दरअसल, समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक जीवन में पुलिस की मौजूदगी तो एक अनिवार्य तथ्य के रूप में स्वीकृत है ही, साथ ही उसकी क्रूरता और भ्रष्टाचार भी। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक पुलिस की क्रूरता की हजारों कहानियां फैली हुई हैं। देश-विदेश के नागरिक और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों तथा समाचार पत्र-पत्रिकाओं में भी पुलिस की क्रूरता के ब्योरे मिलते हैं। आजादी के बाद भारतीय गणतंत्र में पुलिस की बदली हुई भूमिका अपेक्षित थी लेकिन औपनिवेशिक भूत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा।
लगभग छह दशक पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन जज आनंद नारायण मुल्ला की पुलिस के बारे में की गई टिप्पणी आज भी मौजू है। उन्होंने पुलिस हिरासत में हुई मौत के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था- ''भारतीय पुलिस अपराधियों का सर्वाधिक संगठित गिरोह है।’’ आज भी पुलिस की यही स्थिति बनी हुई है।
हैदराबाद एनकाउंटर को जिस तरह समाज के विभिन्न तबकों का व्यापक समर्थन मिला, वह दरअसल एक तरह से हमारी न्याय व्यवस्था पर कठोर टिप्पणी है, जिसमें वर्षों तक मुकदमों के फैसले नहीं हो पाते हैं या अपराधी किसी तरह बच निकलते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि हैदराबाद की घटना के बाद पुलिस या भीड़ के हाथों बलात्कारियों और दूसरे अपराधियों के 'फैसले’ होने की घटनाओं में इजाफा होने लग जाए।...और जब ऐसा होने लगेगा तो गुनहगारों की आड़ में बेगुनाहों को मारने का सिलसिला और तेज होगा।
हमारी न्याय व्यवस्था पर से जिस तरह समाज का भरोसा उठने लगा है, उसमें ऐसी ही स्थितियां बनती दिख रही हैं। अगर जनभावनाओं के आधार पर ही फैसले होंगे तो फिर पुलिस ही क्यों, अदालतों के जज भी फैसले देने से पहले ट्विटर पर जाकर देखेंगे कि संबंधित मामले में क्या ट्रेंड चल रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचने के जरूरी है कि पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार हो, जो कि कई वर्षों से लंबित हैं।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।





















