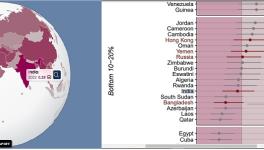पूजा स्थल(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के सही मायने क्या हैं?

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 सभी संप्रदायों की इबादतगाहों/पूजा स्थलों और उनके तबकों की समान रूप से रक्षा करता है। इस प्रकार, उक्त अधिनियम किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के समान अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। एक व्यक्ति का अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अधिकार दूसरे व्यक्ति का उपरोक्त स्वतंत्रता का प्रयोग करने के अधिकार के अधीन है। इस प्रकार, अधिनियम एक संवैधानिक जनादेश को व्यवहार में लाता है, और इसे असंवैधानिक करार देना अकल्पनीय है।
आचार्य महाराजश्री नरेंद्रप्रसादजी आनंदप्रसादजी महाराज बनाम गुजरात राज्य (1974) में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा था:
"एक संगठित समाज में कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता है। किसी के अधिकारों का आनंद दूसरों के अधिकारों के आनंद के अनुरूप होना चाहिए। जहां सामाजिक ताकतों के स्वतंत्र खेल में स्वैच्छिक सद्भाव लाना संभव नहीं है, राज्य को प्रतिस्पर्धी हितों के बीच असंतुलन को ठीक करने के लिए कदम उठाना पड़ता है और वहां राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, हालांकि अदालतों में लागू नहीं होते हैं, वे हैं जो व्यक्तियों के आचरण और उनके मामलों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने में अनुच्छेद 37 के तहत राज्य पर निश्चित और सकारात्मक भूमिका आमद होती है। (उक्त के लेखक ने इस बात को जोर देकर कहा है)
इस प्रकार, अधिनियम संवैधानिकता की एक बुनियादी विशेषता यानि धर्मनिरपेक्षता को लागू करता है और इससे पीछे न हटने को कहता है।
अतीत के कथित गुनाहों/अन्यायों को 'पूर्ववत' करने या उनका बदला लेने का कोई भी प्रयास इतिहास का पिटारा खोल देगा, जो न केवल अव्यवहारिक होगा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप प्राचीन और मध्ययुगीन काल की ज्ञात अराजकता और गहमा-गहमी हो सकती है। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान सहित संविधानवाद और आधुनिक संविधानों का विचार ऐसे बर्बर और सत्तावादी समाजों से विपरीत है।
राजा और देवता की साझा संप्रभुता, या राजा को देवता की नियुक्ति के रूप में मानना प्राचीन और मध्ययुगीन काल की एक सामान्य घटना थी, और किसी भी नए राजा के आगमन के परिणामस्वरूप पिछले शासक वर्ग के देवताओं का विध्वंस होता था। यह घटना न केवल विभिन्न धर्मों के बीच, बल्कि ऐसे धर्मों/विश्वास प्रणालियों के साथ-साथ उनके वर्गों में विभिन्न संप्रदायों के बीच व्याप्त थी। इस संबंध में कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं:
- 587 ईसा पूर्व में नव-बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने यरूशलेम में एक यहूदी टैम्पल का विनाश किया था।
- 70 ईस्वी में टेम्पल माउंट पर दूसरे मंदिर के स्थान पर जुपिटर के टैम्पल की रोमन स्थापना की गई थी।
- हिंदू राजाओं द्वारा मंदिरों को तोड़े जाने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:
पहला, 10 वीं शताब्दी की शुरुआत में, राष्ट्रकूट राजा इंद्र III ने कलाप्रिया के उस मंदिर को नष्ट किया, जिसे उनके कट्टर दुश्मन प्रतिहारस ने संरक्षण दिया था।
दूसरा, जब कश्मीरी शासक ललितादित्य ने गौड़ा (बंगाल) के राजा को धोखे से मार डाला, तो उसके सेवकों ने बदला लेने की कोशिश की। उन्होंने गुप्त रूप से ललितादित्य की राजधानी में प्रवेश किया और कश्मीरी राज्य के प्रमुख देवता विष्णु परिहसकेशव के मंदिर में प्रवेश किया। हालांकि, उन्होंने देवता की चांदी की छवि को परिहसकेशव समझ लिया, और उसे धूल में मिला दिया, जबकि कश्मीरी सैनिकों ने उन पर हमला किया। यद्यपि गौड़ वांछित परिणाम हासिल करने में विफल रहे, उनका प्रतिशोध, शासक द्वारा पूजा की जाने वाली मूर्ति को नष्ट करने में निहित प्रतीकवाद को स्पष्ट करता है।
4॰ हिंदू राजाओं द्वारा देवताओं की मूर्तियों को अपनाना:
पहला, 642 सीई में, पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्यों को हराया, उनकी राजधानी वातापी को तबाह कर दिया, और गणेश की मूर्ति को तमिलनाडु यानि अपने राज्य में ले आए। यहां मूर्ति ने वातापी गणपति की उपाधि हासिल की।
दूसरा, 950 सीई में, चंदेल शासक यशोवर्मन ने विष्णु वैकुंठ की स्थान देने के लिए खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया, जो सोने से बनाया गया था। इस मूर्ति को शुरू में कैलाश पर्वत से "तिब्बत के भगवान" ने हासिल की थी, जिससे उड़ीसा के शाही राजा ने हासिल किया था। प्रतिहार शासक हेरम्बपाल ने सहियों को हराया और देवता की मूर्ति को छीन लिया था। यशोवर्मन ने तब हेरम्बपाल के पुत्र देवपाल को हराया और मूर्ति को खजुराहो ले गए।
इस संदर्भ में, धर्म और एशियाई अध्ययन के अमेरिकी प्रोफेसर रिचर्ड डेविस कहते हैं, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्ययुगीन हिंदू राजाओं ने लगातार अक्सर धार्मिक मूर्तियों/छवियों को नष्ट किया था।"
यह अधिनियम इस अहसास में भी निहित है कि धार्मिक स्थलों की रक्षा करने और इसके चरित्र को बनाए रखने की आवश्यकता धार्मिक झगड़ों से बचने की एक अनिवार्य शर्त है। यह आधुनिक संविधानों की एक अनिवार्य विशेषता है जो धर्मनिरपेक्षता के विकास में योगदान देने वाले कारकों में से एक है।
यह अधिनियम इस अहसास में निहित है कि धार्मिक स्थलों की रक्षा करने और इसके चरित्र को बनाए रखने की आवश्यकता धार्मिक टकराव से बचने की एक अनिवार्य शर्त है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के धार्मिक युद्धों और टकरावों ने बाद की अवधि में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र-राज्यों को विकसित करने के लिए एक प्रोत्साहन दिया गया था। उदाहरण के लिए, मध्य यूरोप में सत्ता के नियंत्रण को लेकर प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिक धर्म के बीच तीस साल तक लड़े गए युद्ध (1618-1648) में लगभग 5 से 8 मिलियन लोगों की जान चली गई थी, और आधुनिक जर्मनी में कुछ क्षेत्रों की आधी से अधिक आबादी का सफाया हो गया था।
अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ में याचिकाकर्ता की याचिका में अधिनियम को अमान्य करार देने और सूट, याचिकाओं या अन्यथा के माध्यम से कुछ पूजा स्थलों के रूपांतरण (या पुन: रूपांतरण) की अनुमति न केवल मौलिक मूल्यों बल्कि व्यक्त प्रावधानों के भी विपरीत है। संविधान, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में मानवता के सभ्यतागत लाभ को एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज की एक अनिवार्य शर्त है।
एक शांतिपूर्ण और स्थिर समाज को बनाए रखने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित शासन की सुविधा के लिए और संविधान के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की शरारत की रोकथाम जरूरी है। अधिनियम या उसमें निहित मानदंडों को उजागर करने का कोई भी प्रयास न केवल संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खतरे में डालेगा, बल्कि मौलिक अधिकारों के पूरे ताने-बाने और वास्तव में हमारे देश में सरकार के संवैधानिक रूप के लिए खतरा होगा। इसलिए, अधिनियम को नष्ट के किसी भी प्रयास को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
यह अधिनियम मानता है कि हमारे देश की स्वतंत्रता धर्म की समानता के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करती है, और अतीत के कथित अन्यायों की पुनरावृत्ति को रोकता है। यह उस स्वतंत्रता के क्षण की पुष्टि करता है जब भारत ने खुद को एक संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध किया था।
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धार्मिक स्थलों का विनाश भविष्य के अधिनायकवादी शासनों के अधिकार को लागू करने के साधनों में से एक रहा है। आधुनिक लोकतंत्रों में, वही खुद को बहुसंख्यकवाद, या एकमुश्त सत्तावाद के रूप में प्रकट कर सकता है। यह परंपरा संवैधानिकता की धारणा के विपरीत है, और संविधान के कामकाज के लिए हानिकारक है।
आधार के रूप में स्वतंत्रता
अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि अधिनियम में, इबादतगाहों/पूजा स्थल के चरित्र में यथास्थिति बनाए रखने की कट-ऑफ तिथि मनमानी है, जो ऐतिहासिक और संवैधानिक वास्तविकता से बढ़कर नहीं हो सकती है, और जोकि जानबूझकर जताया गए भोलेपन का एक प्रयास लगता है।
यह अधिनियम मानता है कि हमारे देश की स्वतंत्रता धर्म की समानता को संवैधानिक आधार प्रदान करती है, और अतीत के कथित अन्यायों की पुनरावृत्ति को रोकता है। यह अधिनियम स्वतंत्रता के उस पल की पुष्टि करता है जब भारत ने खुद को एक संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध किया था। सुप्रीम कोर्ट इस ऐतिहासिक वास्तविकता से गहराई से परिचित है और इससे बचने की जरूरत एम सिद्दीकी (डी) और अन्य बनाम महंत सुरेश दास व अन्य (2019), मामले में संविधान पीठ के फैसले से स्पष्ट है, जिसे 'अयोध्या निर्णय' के नाम से जाना जाता है:
"पूजा स्थल अधिनियम के अधिनियमन के अंतर्निहित एक उद्देश्य है। कानून हमारे इतिहास और राष्ट्र के भविष्य के बारे में बोलता है। जैसा कि हम अपने इतिहास से परिचित हैं और राष्ट्र को इसका सामना करने की जरूरत है, स्वतंत्रता अतीत के घाव को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। लूग्न द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर, ऐतिहासिक गलतियों का समाधान नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करने में, संसद ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के यह अनिवार्य कर दिया है कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य पर अत्याचार करने के उपकरणों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।”
फिर से न्यायालय कहता है:
“यह न्यायालय उन दावों पर विचार नहीं कर सकता है जो आज की अदालत में हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों के कार्यों से उपजे हैं। कोई व्यक्ति, जो कई प्राचीन शासकों के कार्यों के खिलाफ सांत्वना या सहारा चाहता है, कानून उसका जवाब नहीं है। हमारा इतिहास उन कार्यों से भरा हुआ है जिन्हें नैतिक रूप से गलत माना गया है और आज भी मुखर वैचारिक बहस को गति देने के लिए वे उत्तरदायी हैं। हालाँकि, संविधान को अपनाना एक महत्वपूर्ण पल था जहाँ हम, भारत के लोग, अपनी विचारधारा, अपने धर्म, अपनी त्वचा के रंग, या उस सदी के आधार पर अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण से विदा लेते है जिन्हे लेकर हमारे पूर्वज भूमि पर आए थे, और जिन्हे कानून के शासन के रूप में प्रस्तुत किया था। हमारे कानून के शासन के तहत, यह न्यायालय निजी संपत्ति के दावों पर निर्णय ले सकता है जो स्पष्ट रूप से निहित थे या ब्रिटिश संप्रभु द्वारा मान्यता प्राप्त थे और बाद में भारतीय स्वतंत्रता ने जिन पर हस्तक्षेप नहीं किया था।
यह स्पष्ट है कि धर्मांतरण (या पुन: धर्मांतरण) की दलील दूसरों को हुए नुकसान की परवाह किए बिना खुद की मुट्ठी झूलने के समान है, और इस प्रकार यह संविधान के लिए घृणित है।
जैसा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस तर्क दिया था, वह यह था कि अधिनियम स्वतंत्र भारत के आकांक्षात्मक मूल्यों में मजबूती से समाया हुआ है। महात्मा गांधी के एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य के दृष्टिकोण को इतिहासकार बिपन चंद्र ने अपने जर्नल लेख गांधीजी, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता (2004) में प्रकाशित किया है:
"एम के गांधी मूल रूप से गहन धार्मिक होने के बावजूद, पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे, साथ ही यह भी कि वे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहते थे। और उन्होंने 9 अगस्त 1942 को जोर देकर कहा था कि: "स्वतंत्र भारत में कोई हिंदू राज नहीं होगा, यह भारतीय राज होगा जो किसी भी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर नहीं बल्कि धर्म के भेद के बिना देश के सभी लोगों के प्रतिनिधियों पर आधारित होगा।"
धर्मनिरपेक्षता का यह मॉडल, जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और किसी भी राज्य धर्म की अनुपस्थिति पर आधारित है, भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय, सुरक्ष चंद्र चिमन लाल शाह बनाम भारत संघ और अन्य (1975), मामले में यह भी मानता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्रोत स्वतंत्रता आंदोलन है "जिसने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सभी धर्मों के संबंध में राज्य की तटस्थता का आश्वासन दिया था":
"आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के विकास की पृष्ठभूमि बहुत अलग है। सहिष्णुता और उदारवाद की भावना से प्रेरित होकर, जो प्राचीन काल से हिंदू विचारों की विशेषता थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीति में एक गैर-सांप्रदायिक दृष्टिकोण विकसित किया, धर्म को व्यक्ति की अंतरात्मा की बात के रूप में छोड़ दिया था। भारत में धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन के एक हिस्से के रूप में विकसित हुई जिसने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सभी धर्मों के संबंध में राज्य की तटस्थता का आश्वासन दिया था। यह नीति 1931 में कराची में पारित कांग्रेस के प्रस्ताव में सन्निहित थी।
अधिनियम केवल वही व्यक्त करता है जो संविधान में निहित है
अधिनियम के बिना भी, धार्मिक स्थलों के रूपांतरण का कोई भी प्रयास धर्म की स्वतंत्रता के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के विपरीत होगा, जो संविधान की मूल विशेषताएं हैं। अधिनियम स्पष्ट रूप से संविधान में निहित है और स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है; ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति दूर तक भी असंवैधानिक नहीं हो सकती है।
याचिकाकर्ता की दलील मूल रूप से अन्य संप्रदायों या उसके वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में न्यायायिक उपचार मांगने की याचिका है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की इस तरह की याचिका शुरू में पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की दलील, धर्म की स्वतंत्रता के प्रावधानों के विपरीत है, जो अन्य बातों के साथ-साथ नैतिकता को सबसे ऊपर मानता है। 'नैतिकता' शब्द को 'नुकसान के सिद्धांत' के आधार पर समझने की जरूरत है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है "अपनी मुट्ठी घुमाने की आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है"। यह स्पष्ट है कि धर्मांतरण (या पुन: धर्मांतरण) की दलील दूसरों को हुए नुकसान की परवाह किए बिना अपनी मुट्ठी झूलने के समान है, और इस प्रकार यह संविधान के लिए घृणित है।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि संविधान की आंतरिक नैतिकता सभी मनुष्यों की गरिमा और समानता पर आधारित है:
"जैसा कि हमने ऊपर बताया है, हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण और मौलिक स्तंभ के रूप में कानून के शासन के साथ उदार और वास्तविक लोकतंत्र निहित है। सभी मनुष्यों की गरिमा और समानता पर आधारित इसकी अपनी आंतरिक नैतिकता है। कानून का शासन व्यक्तिगत मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग करता है। इस तरह के अधिकारों की गारंटी प्रत्येक इंसान को दी जानी चाहिए। ये टीजी, भले ही संख्या में नगण्य हैं, फिर भी इंसान हैं और इसलिए उन्हें अपने मानवाधिकारों का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। (निर्णय के लेखक ने उक्त पर जोर दिया)
अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका इस तरह की समानता का विरोध करती है, और तर्क देती है कि कुछ संप्रदायों या वर्गों के व्यक्तियों के अधिकारों के मुक़ाबले दूसरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार, यह संवैधानिक नैतिकता के सभी मानदंडों का उल्लंघन करती है।
न्यायिक उपाय
यह अधिनियम किसी गारंटीशुदा अधिकार के लिए न्यायिक इलाज़ में कटौती नहीं करता है। क्योंकि एक पक्ष के दावों को दूसरे पक्ष के गारंटीकृत अधिकारों के अपमान में लागू करने के लिए कोई न्यायिक उपाय नहीं हो सकता है। उपरोक्त न्यायिक इलाज़ के लिए याचिकाकर्ता की दलील मूल रूप से अन्य संप्रदायों या उसके वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए उपाय प्रदान करने की याचिका है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की इस तरह की याचिका शुरू में पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए।
साथ ही, यह तर्क कि अधिनियम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ किसी भी उपाय को रोकता है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। ऐसे किसी भी पूजा स्थल की संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण का उपाय संबंधित कानूनों के तहत उपलब्ध है। वास्तव में, अधिनियम किसी भी धर्म के पूजा स्थलों को उन अतिक्रमणों से बचाता है जो अन्य धार्मिक संप्रदायों के ऐसे पूजा स्थलों या उसी संप्रदाय के अन्य वर्गों के बदलाव की प्रकृति में हैं।
अंत में, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कुछ अवसरों पर, पूजा की जगह के चरित्र का पता लगाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन केवल दुर्लभ मामलों में ही अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें विवाद वास्तविक है और जो विभिन्न विरोधी संप्रदायों या उसके वर्गों से संबंधित लोगों द्वारा स्थान के नियमित उपयोग पर आधारित है। अन्यथा, यह पता लगाना कि संभावना शरारत के साथ गढ़ी गई है, क्योंकि पूजा स्थल को जानबूझकर विवाद में लाया जा सकता है और फिर दावेदार पक्ष इसके चरित्र का पता लगाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित कर सकता है।
ऐसे मामलों में जहां पता लगाने की अनुमति है, उस की संदर्भ तिथि 15 अगस्त, 1947 होनी चाहिए, न कि ऐतिहासिक पुरातनता में एक अलग विरोधी धार्मिक संप्रदाय द्वारा किसी विशेष स्थान का कथित उपयोग होना चाहिए।
वास्तव में, क्रॉस की उपस्थिति मात्र ईसाई धर्म की किसी वस्तु को पारसी विश्वास की किसी वस्तु में नहीं बदल देगी; न ही पारसी धर्म की कोई वस्तु इसे ईसाई धर्म की संरचना बनाता है।
लेकिन अगर कोई संरचना है जहां एक गणेश मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाता है, साथ ही एक संप्रदाय के मंदिर के अन्य सामानों के साथ, केवल उसकी उपस्थिति जगह के चरित्र के बारे में उचित संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसलिए, पता लगाने की कवायद 15 अगस्त, 1947 की तिथि की होनी चहाइए जो विवाद के मजबूत सबूत के साथ उचित आधार पर होनी चाहिए और इसे अत्यंत निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। तभी यह अधिनियम संवैधानिक जनादेश की रक्षा करने में प्रभावी साबित हो सकता है जिसे वह लागू करना चाहता है।
इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें।
The Challenge to Places of Worship Special Provisions Act, 1991 is Misconceived
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।