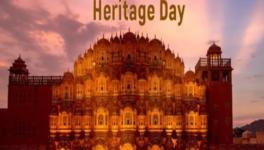आज़ादी@75: आंदोलन के 74 बरस और नई उम्मीद और नया रास्ता दिखाता किसान आंदोलन

आज जब हम अपनी आजादी की 74वीं वर्षगांठ और 75वां दिवस मना रहे हैं, संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉ. आंबेडकर द्वारा दी गयी चेतावनी बेहद प्रासंगिक है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश एक अन्तरविरोधों भरे दौर में प्रवेश कर रहा है, हम एक राजनीतिक लोकतंत्र तो बन गए लेकिन सामाजिक लोकतंत्र कायम न हुआ तो यह राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जायेगा।
इन 74 वर्षों में देश को सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र बनाने की जद्दोजहद लगातार जारी है।
महिला आंदोलन
लैंगिक असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ बराबरी और सम्मान के लिए महिला आंदोलन हमारे समाज की एक विकासमान विशेषता है। वैसे तो यह सतत जारी प्रक्रिया है, पर निर्भया बलात्कार कांड पर देश की राजधानी दिल्ली में हुआ ऐतिहासिक प्रतिरोध महिला आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर है, जब प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राएं-महिलाएं, वामपंथी संगठनों व नागरिक समाज के कार्यकर्ता भारी दमन की परवाह न करते हुए राष्ट्रपति भवन के द्वार तक पहुंच गए थे। अंततः सरकार को यौन हिंसा पर नया कानून बनाना पड़ा था। उस आंदोलन ने महिलाओं की जबरदस्त दावेदारी का ऐसा उद्घोष किया, जिसकी उपेक्षा करना अब किसी के लिए सम्भव नहीं है। आज देश मे चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन में भी वे अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। महिला किसान की एक नई सामाजिक श्रेणी से देश परिचित हुआ है, पिछले दिनों जब किसानों ने जन्तर मंतर पर किसान-संसद लगाई, तो दो दिन महिला किसान-संसद आयोजित हुई।
पितृसत्ता की ताकतें उनकी राजनीतिक दावेदारी से कितनी भयभीत हैं इसका ही प्रमाण है कि विधायिकाओं में 33% महिला आरक्षण का प्रस्ताव 25 वर्ष बाद भी आज तक कानून का रूप नहीं ले सका है। आज तो पितृसत्ता की पोषक सबसे प्रतिक्रियावादी ताकतें सत्ता में हैं, स्वाभाविक रूप से महिला विरोधी हिंसा, कानूनों और पूर्वाग्रहों की बाढ़ आ गयी है। इसके खिलाफ जमीनी स्तर पर तो महिलाएं लड़ ही रही हैं, मोदी राज का महिला-विरोधी तांडव जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश निर्भया आंदोलन पार्ट 2 का साक्षी बनेगा।
कम्युनिस्ट आंदोलन
वर्ग-विषमता के विनाश के लिए, उत्पादन के साधनों पर काबिज प्रभुत्वशाली वर्गों के खिलाफ मेहनतकश वर्गों का राज बनाने की लड़ाइयां कम्युनिस्ट ताकतों के नेतृत्व में तेलंगाना से नक्सलबाड़ी होते हुए अनेक उतार चढ़ावों के साथ लगातार जारी हैं। ग्रामीण इलाकों में सामन्ती जुल्म की रीढ़ तोड़ने, उत्पीड़ित तबकों के मान और उनकी महिलाओं की मर्यादा की रक्षा, वंचित तबकों के पक्ष में जमीनी संघर्षों तथा राजनीतिक- संसदीय दबाव के बल पर अनेक प्रगतिशील कानून बनवाने और एक हद तक उन्हें लागू करवाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही हैं, मसलन जमींदारी उन्मूलन, सीलिंग कानून, बंगाल में बटाईदारी कानून ( ऑपरेशन बर्गा ) खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा...। वे ग्रामीण गरीबों, आदिवासियों के हित में लड़ने वाली सबसे दृढ़प्रतिज्ञ शक्ति हैं। आज फासीवाद की हर अभिव्यक्ति के खिलाफ कैम्पस से लेकर किसान-आंदोलन मेहनतकश-बुद्धिजीवी-नागरिक समाज तक लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली सबसे सुसंगत आवाज हैं वे। यद्यपि, अपनी कतिपय गम्भीर सैद्धांतिक-राजनीतिक कमजोरियों तथा सांगठनिक बिखराव के कारण देश की राजनीति में वे एक बड़ी राजनैतिक ताकत नहीं बन पा रहे हैं और गहरे संकट का सामना कर रहे हैं।
नक्सलवादी धारा
कम्युनिस्टों द्वारा खड़े किए गए संघर्षों में नक्सलवादी धारा का विशिष्ट स्थान है, जिसने किसानों के सशस्त्र संघर्ष को केंद्र कर राजसत्ता दखल का लक्ष्य रखा था और संसदीय संघर्षों का पूरी तरह परित्याग कर दिया। इस आंदोलन की क्रांतिकारी भावना, आदिवासियों, दलितों, उत्पीड़ितों के साथ लड़ते हुए इसके नेताओं-कार्यकर्ताओं के अकूत बलिदान ने 60-70-80 के दशक में समाज में जबरदस्त आलोड़न पैदा किया, तमाम रैडिकल तत्व, छात्र-युवा, बुद्धिजीवी इसकी ओर आकर्षित हुए, साहित्य-संस्कृति पर भी इसका जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा। स्वाभाविक रूप से सत्ता के चरम दमन का इसे शिकार होना पड़ा। भारतीय राजसत्ता व समाज की inadequate समझ पर आधारित रणनीति के एकांगीपन, जनांदोलनों व संसदीय संघर्षों के बहिष्कार जैसे कदमों से इसे मरणांतक धक्का लगा। बाद में भाकपा माले लिबरेशन धारा ने इसे ट्रैक पर लाने की कोशिश की और बिहार में एक राजनीतिक ताकत बन कर उभरी। इसके कुछ अन्य धड़े आज भी पुरानी लाइन पर टिके हुए हैं, राजसत्ता का बर्बर दमन झेलते वे भारी धक्के का सामना कर रहे हैं।
सामाजिक न्याय का आंदोलन
जाति उत्पीड़न और गैरबराबरी के खिलाफ सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन की धारावाहिकता आज़ादी के पूर्व से आज तक अनवरत जारी है, अम्बेडकरवादी और समाजवादी आंदोलन ने इन्हें प्रमुख प्रश्न बनाया, यद्यपि कम्युनिस्ट आंदोलन में भी यह उनके वर्ग-संघर्ष के अभिन्न पहलू के बतौर मौजूद रहा।
डॉ. आंबेडकर की चिंता के केंद्र में हिन्दू समाज के आखिरी पायदान पर खड़े, सामाजिक रूप से बहिष्कृत ( untouchable ) दलित समुदाय की सम्पूर्ण मुक्ति का स्वप्न था। इसके लिए वे जाति का विनाश ( annihilation of caste ) चाहते थे, उन्होंने हिन्दू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उनको शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष किये, उन्हें जमीन दिलाने के लिए भूमि के राष्ट्रीयकरण की State and Minorities में वकालत की, उनके द्वारा बनाये दल RPI ने दलितों को भूमि पर कब्ज़ा दिलाने के लिए अभियान चलाया और आंदोलन किया। अम्बेडकर पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों को निशाने पर रखते थे। वे सामाजिक और आर्थिक दोनों लोकतंत्र की बात करते थे।
एक दौर में अम्बेडकरवाद और नक्सलवाद से प्रभावित दलित पैंथर आंदोलन ने बम्बई और महाराष्ट्र में अपने जुझारू तेवर से जबरदस्त हलचल पैदा की और तमाम रैडिकल ताकतों को आकर्षित किया।
गंभीर संकट में दलित आंदोलन और राजनीति
बाद के दौर में पूरा फ़ोकस दलितों से शिफ्ट होता गया। कांशीराम ने बहुजन की बात की और बाद में वह सर्वजन तक पहुंच गई। पूरा जोर सरकार बनाने पर हो गया, यहां तक कि उसके लिए धुर-पुरातनपंथी, भाजपा तक से हाथ मिलाने से परहेज नहीं किया गया। बसपा गम्भीर वैचारिक-राजनैतिक विचलन का शिकार हो गयी है और अब तो बात ब्राह्मण सम्मेलन और मंदिर बनाने के वायदे तक पहुंच गयी है। सच्चाई यह है कि दलित आंदोलन और राजनीति आज गहरे संकट में है । दलित नेतृत्व का एक हिस्सा सीधे संघ-भाजपा की गोद मे चला गया है । यह अनायास नहीं है कि मोदी-योगी के राज में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की बाढ़ आ गयी है। दलित युवा लड़ाकू नेतृत्व की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
2018 में SC-ST ( Prevention of Atrocities ) Act के dilution को लेकर दलितों का एक जुझारू राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था, 2 अप्रैल को ऐतिहासिक बंद हुआ था, जिसमें एक दर्जन के आसपास दलित नौजवान शहीद हुए थे और सैकड़ों जेल में डाले गए थे। लेकिन मोदी सरकार को अंततः इसके आगे झुकना पड़ा था।
दलित आंदोलन के सामने आज सही राजनीतिक दिशा के साथ आंदोलन को reinvent करने की है।
सामाजिक न्याय के आंदोलनों के फलस्वरूप पुराने सामाजिक ढांचे की वर्चस्वशाली ताकतों का सामाजिक दबदबा टूटा और नई सत्ता संरचना में वंचितों, पिछड़ों, दलितों को शेयर मिलना शुरू हुआ। मंडल आंदोलन इस यात्रा में मील का पत्थर था जब पिछड़ों के लिए नौकरियों में आरक्षण की घोषणा हुई, जाहिर है सवर्ण वर्चस्ववादी ताकतों के भारी विरोध का इसे सामना करना पड़ा, जिसे संघ-भाजपा की शह प्राप्त थी, यहां तक कि आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू कर दी और उसे रोके जाने का बहाना बनाकर वीपी सिंह की सरकार गिरा दी।
लेकिन कालांतर में समाजवादी धारा अस्मिता की राजनीति में reduce हो गयी, सामाजिक न्याय का नारा मंडल आयोग की महज एक सिफारिश -आरक्षण के प्रश्न में सिमट कर रह गया और उसका व्यापक समतामूलक लोकतान्त्रिक परिप्रेक्ष्य गायब हो गया। जल्दी ही अस्मिता की राजनीति की अंतर्निहित कमजोरियों, distortions और अवसरवाद का इस्तेमाल करके हिंदुत्व की पुरातनपंथी ताकतें शक्ति अर्जन करने और दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना तक में सत्ता पर काबिज होने में सफल हो गईं। नतीजतन जनतांत्रिकरण और सामाजिक न्याय की यात्रा पर न सिर्फ ब्रेक लग गया बल्कि हिंदुत्व के आगोश में वंचित तबकों के साम्प्रदायीकरण की उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गयी। इस धारा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे बड़ी पूंजी के नेतृत्व वाले आर्थिक ढांचे को निशाना नहीं बनाते, कारपोरेटपरस्त नवउदारवादी आर्थिक नीतियों का विरोध नहीं करते, यहां तक कि सरकार में रहने पर उन्हीं नीतियों को लागू करते हैं, जबकि इन नीतियों का सबसे बदतरीन शिकार स्वाभाविक रूप से समाज के कमजोर, वंचित तबके ही हैं और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हिंदुत्व की ताकतों का उभार इसी आर्थिक ढांचे की नीतियों के संकट काल की राजनीतिक अभिव्यक्ति है।
सामाजिक न्याय को सुसंगत ढंग से लागू करने की बजाय अपने जातीय आधार और वोटबैंक के अवसरवादी जोड़ गणित के अनुसार लागू करने का परिणाम यह हुआ कि इसका लाभ सभी वंचित समूहों तक नहीं पहुंच पाया और वे हिंदुत्व की ताकतों के आसान शिकार बन गए।
भारतीय समाज मे यह ongoing struggle है। हाल फिलहाल जाति जनगणना को लेकर जद्दोजहद जारी है। जाहिर है जब तक समाज में सत्ता के ढांचे में जाति आधारित विषमता और अन्याय का अंत नहीं हो जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आज जरूरत है कि हिंदुत्व की राजनीति और कारपोरेट अर्थनीति के पूरे पैकेज के खिलाफ सुसंगत सामाजिक न्याय और जाति विनाश की लड़ाई आगे बढ़े।
भाषायी आंदोलन
आज़ादी के बाद भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बड़े आंदोलन हुए। केंद्रीय सत्ता के अतिकेंद्रीकरण और उत्तर भारतीय वर्चस्व के खिलाफ भाषायी, सांस्कृतिक, आंचलिक अस्मिता, क्षेत्रीय स्वायत्तता, राज्यों के अधिक अधिकारों के आंदोलन लगातार चलते रहे हैं, जिन्होंने कई बार हिंसक स्वरूप और अलगाववादी रूप भी ग्रहण किया। मूलतः ये आंचलिक शासक तबकों की सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाइयां थीं पर इनमें भारतीय राज्य के democratisation की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षा की भी अभिव्यक्ति हुई और इन्होंने सत्ता के अतिकेन्द्रीकरण के खिलाफ संघीय ढांचे को मजबूत करने में भूमिका निभाई है तथा समय-समय पर केंद्रीय स्तर पर उभरती केंद्रीकरण और निरंकुशता की प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई।
कई बार फासीवादी प्रवृत्ति के क्षेत्रीय नेताओं ने संकीर्ण आंचलिक/सामुदायिक भावनाओं की दिशा प्रवासी मजदूरों तथा दूसरे समुदायों के खिलाफ मोड़ दी। इसका सबसे वीभत्स रूप 80 के दशक में ethnic व साम्प्रदायिक जनसंहार में असम में तथा गैर-मराठी लोगों के खिलाफ शिवसेना के तांडव में मुंबई में दिखा था।
80 के दशक में गहराते आर्थिक संकट के खिलाफ तमाम तबकों का आक्रोश बड़े आंदोलनों के रूप में फूट पड़ा था।
हरित क्रांति का संकट सामने आने के साथ देश के विभिन्न इलाकों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत, महाराष्ट्र में शरद जोशी, पंजाब में भूपेंद्र सिंह मान, कर्नाटक में प्रो. नानजुंडास्वामी के नेतृत्व में बड़े किसान आंदोलन हुए जिन्होंने राष्ट्रव्यापी असर छोड़ा।
इन आंदोलनों की कमजोरी यह रही कि वे इसकी सुसंगत राजनीति नहीं विकसित कर सके, न समाज के दूसरे तबकों के लोकतांत्रिक आंदोलनों से इसे जोड़ सके। वे अपने जुझारू आंदोलन के बल पर तात्कालिक तौर पर अपनी कुछ मांगे मनवाने में जरूर सफल रहे, पर व्यापक परिप्रेक्ष्य और सही दिशा के अभाव में
किसानों के हित मे बुनियादी नीतिगत बदलाव करवा पाने में असमर्थ रहे और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल होते रहे, यद्यपि वे अपने को "अराजनीतिक" कहते थे। उनमें से कुछ तो बाद में पतित होकर कृषि को बाजार के हवाले करने के कृषि के कारपोरेटीकरण के रास्ते पर चले गए।
उसी दौर में मजदूरों के बड़े आंदोलन भी हुए जिनमें मुंबई के टेक्सटाइल मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल मील का पत्थर थी। एक साल से ऊपर चली उस हड़ताल में तब के बम्बई के 65 कपड़ा मिलों के ढाई लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। लेकिन परिस्थिति के ठोस मूल्यांकन और सही रणनीति के अभाव में आंदोलन न सिर्फ अपनी मांगे मनवाने में विफल रहा बल्कि मिलें बंद हो गईं और बड़े पैमाने पर मजदूर बेरोजगार हो गए।
80-90 दशक में रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, " सबको शिक्षा, सबको काम " जैसे नारों पर और कैम्पस लोकतंत्र के सवाल पर छात्र युवाओं के जुझारू आंदोलन तमाम कैम्पसों और राज्यों में हुए।
उसी दौर में WTO बनने की प्रक्रिया में आये " गुलामी के दस्तावेज " डंकल प्रस्ताव के खिलाफ लाल किले पर वामपन्थी जनसंगठनों की ओर से ऐतिहासिक प्रतिरोध हुआ। जिसमें कई घण्टों तक पुलिस बल के साथ प्रदर्शनकारियों के pitched battle चलता रहा था, अनेक प्रदर्शनकारी घायल हुए थे।
उस दौर में रामजन्मभूमि आंदोलन के नाम पर चलाए जा रहे साम्प्रदायिक फासीवादी अभियान के खिलाफ अमन और भाईचारे के लिए तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार अभियान चलते रहे।
चिपको और नर्मदा बचाओ जैसे चर्चित आंदोलन तो पहले हुए ही थे, हाल के वर्षों में समाज मे पर्यावरण की बढ़ती चेतना के फलस्वरूप जगह -जगह कारपोरेटपरस्त विकास के नाम पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले सरकार के projects, न्यूक्लिअर पावर प्लांट्स आदि के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन खड़े हो रहे हैं।
CAA और NRC के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ शाहीन बाग आंदोलन नागरिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के बाद के दौर का सबसे बड़ा आंदोलन था। मोदी सरकार इसे साम्प्रदयिक रंग देकर और अराजक दिशा में मोड़कर अलग-थलग करने तथा कुचलने में नाकाम रही। आज देश मे राजद्रोह, UAPA, AFSPA जैसे काले कानूनों के खात्मे के सवाल को राजनीतिक एजेंडा बनाने और बड़े जनान्दोलन की जरूरत है।
देश मे 74 सालों में चले आंदोलनों की अपनी उपलब्धियाँ हैं, साथ ही सीमाएं और कमजोरियां रही हैं।
आज देश मे चल रहे किसान-आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता, उसकी ताकत और अपराजेयता का राज यही है कि इसने अतीत के तमाम जनांदोलनों के अनुभवों से सीखा है और सही दिशा और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आज यह मोदी की फासीवादी कारपोरेटपरस्त सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष का सबसे पवित्र अमृत यह किसान आंदोलन ही है जो संघ-भाजपा के विषवमन का सबसे बड़ा एंटीडोट है। देश को सामाजिक लोकतंत्र बनाने की लड़ाई की सबसे बड़ी उम्मीद आज किसान आंदोलन है।
इसे भी पढ़ें : आज़ादी@75: जेपी से लेकर अन्ना तक... भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों की पड़ताल
(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।