कोप-26: मामूली हासिल व भारत का विफल प्रयास
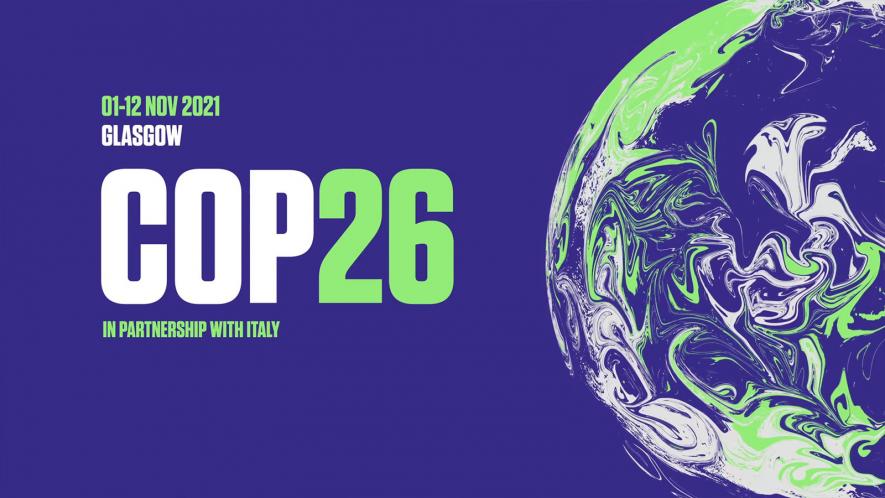
कोप-26 नाम से जलवायु सम्मेलन, मूल कार्यक्रम से करीब 24 घंटा बाद, 13 नवंबर को समाप्त हो गया। सम्मेलन का समापन पूर्णाधिवेशन, कोप बयान के अंतिम मसौदे पर अटक गया था। इस बयान को अब ग्लास्गो पर्यावरण संधि (ग्लास्गो क्लाइमेट पैक्ट) का नाम दे दिया गया है। लाइव प्रसारण के दर्शकों ने देखा था कि किस तरह घंटों तक देश के बाद देश, प्रस्ताव के मसौदे पर अपनी समापन टिप्पणियों में, मसौदे पर गंभीर निराशा जता रहे थे, हालांकि इसके साथ ही वे यह भी कह रहे थे कि सुलह-समझौते की भावना से वे इस वक्तव्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ताकि ग्लास्गो से कम से कम खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़े। खबरों के अनुसार, ऐन आखिरी छोर पर पहुंचकर प्रस्ताव इसलिए अटक गया था कि भारत को, इस प्रस्ताव का एक खास हिस्सा मंजूर नहीं था, जिसमें कोयला-आधारित बिजली उत्पादन को ‘‘फेज आउट’’ करने यानी क्रमश: खत्म करने की बात थी। वास्तव में इस समापन पूर्णाधिवेशन में हुए बहुत से भाषण तो, इस अधिवेशन के हाशियों पर मसौदे पर चल रही बातचीत के लिए समय देने के लिए भी थे, ताकि विवादित सूत्रीकरणों का समाधान निकाला जा सके और किसी समाधान के लिए राजी होने के लिए भारत पर दबाव डालने के लिए भी थे।
भारत का गड़बड़ प्रयास
यह सब डर्बन में 2011 में हुए कोप सम्मेलन की ही याद दिलाता है। हां! उससे इतना अंतर जरूर था कि तब तो तत्कालीन पर्यावरण मंत्री, जयंती नटराजन को पूर्णाधिवेशन के अंदर ही, विकसित तथा विकासशील, दोनों ही तरह के देशों के अनेक प्रतिनिधियों ने घेर लिया था और उन्होंने अंतत: उस संशोधन को स्वीकार कर लिया था, जिसे आगे चलकर खास महत्वपूर्ण माना ही नहीं गया। इस बार ग्लास्गो सम्मेलन में, अग्रणी वार्ताकार, अमरीका, योरपीय यूनियन, चीन और भारत, पूर्णाधिवेशन से अलग एक निजी कक्ष में सिर जोडक़र बैठे थे और अंतत: उन्होंने लौटकर एक सहमत पाठ पेश किया, जो उनके फैसले की प्रतीक्षा कर रहे 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों को पढक़र सुना दिया गया। इस सहमत पाठ की घोषणा का स्वागत, नाराजगी के काफी शोर तथा बड़बड़ाहटों से तथा असहमति की अभिव्यक्तियों से और इस निर्णय पर भी तथा जिस तरह से उक्त निर्णय तक पहुंचा गया था उसकी अपारदर्शिता पर भी, असंतोष जताए जाने के साथ हुआ। फिर भी आखिर में, सम्मेलन ने इसका अनुमोदन कर दिया। कोप-26 के अध्यक्ष, यूके के पर्यावरण मंत्री, आलोक शर्मा ने इस सब पर अपने आंसू पीते हुए, इस पूरे घटनाविकास पर क्षमा याचना की और कहा कि भारत और चीन को, उन देशों को जवाब देना होगा, जिनकी स्थिति पर्यावरण परिवर्तन के खतरे के सामने सबसे नाजुक है। ऐसा समझा जाता है कि चीन ने, और कुछ खबरों के मुताबिक तो दक्षिण अफ्रीका ने भी, इस मामले में भारत के रुख का समर्थन किया था, जबकि जी 77+ चीन के ग्रुप के प्रवक्ता की भूमिका में, गेबोन ने पहले एक समझौते के तौर पर उक्त मसौदे के लिए हामी भर दी थी।
इस तरह अंतिम रूप से स्वीकृत हुए वक्तव्य में मसौदे के ‘‘फेज आउट’’ के सूत्रीकरण को बदलकर, ‘‘फेज डाउन’’ कर दिया गया है यानी जहां पहले वाला सूत्रीकरण कोयला-आधारित बिजली के उत्तरोत्तर खत्म किए जाने का वादा करता था, इसमें उसे उत्तरोत्तर कम करने की ही बात है। दस्तावेज के अंतिम प्रारूप में भारत के गरीब परिवारों को रसोई गैस के लिए सब्सीडियां देने के प्रावधान से संबंधित शब्दावली भी जोड़ दी गयी है। इस सब के बाद, करीब-करीब समूचे पश्चिमी प्रैस ने, कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने तथा अनेक प्रमुख प्रतिनिधियों ने, भारत को इस शिखर सम्मेलन का खलनायक जैसा बनाकर पेश किया है, जबकि वैज्ञानिकों व ऊर्जा विशेषज्ञों ने भारत के प्रति कहीं ज्यादा नरमी दिखाई है। याद रहे कि जैसाकि हाल ही में भारतीय अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि सहमति की उक्त शब्दावली, अमरीका द्वारा ही सुझायी गयी थी।
बहरहाल, यह आंशिक रूप से तो सही है ही कि सभी की निराशाओं तथा असंतोषों के लिए, भारत को ही बलि का बकारा बनाया जा रहा है, जबकि असली दोषी था, कोप-26 शिखर सम्मेलन का अपने सामने खड़े असली मुद्दों का हल निकालने में, पूरी तरह से विफल रहना। ये असली मुद्दे हैं, ताप में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक सीमित रहने के लिए जरूरी समझौते पर पहुंचना और खासतौर पर पर्यावरण परिवर्तन के मामले में सबसे कमजोर तथा सबसे कम विकसित देशों के लिए उल्लेखनीय पैमाने पर फंडिंग मुहैया कराना, ताकि इन देशों को पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए और कार्बन-रहित अर्थव्यवस्था व समाज की ओर आवश्यक संक्रमण के लिए मदद दी जा सके। फिर भी, भारत ने बातचीत के लिए सूत्रबद्घ किए गए अपने रुख के साथ, कोप-26 की अपनी तैयारियों में तथा उसमें अपनी शिरकत में जो गड़बडिय़ां की हैं, उनके लिए भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्मुख, पिछले कुछ महीनों से जिन महत्वपूर्ण संवादकारों से वह संवाद कर रही थी उनके सम्मुख और खुद अपनी जनता के सम्मुख, बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जिन काफी महत्वाकांक्षी तथा साहसिक, संशोधित वचनबद्घताओं का एलान किया था, उनका लाभ उठाने में तथा उनके आधार पर आगे बढ़ने में, भारत पूरी तरह से ही विफल रहा और वास्तव में इस सबसे जो लाभ लिया जा सकता था उसे भी, आगे चलकर अज्ञात कारणों से उक्त वचनबद्घताओं से पीछे हटकर, वास्तव में हाथ से फिसल ही जाने दिया। भारत ने, अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठाओं को और अपने बौद्घिक-नैतिक प्रभाव या सॉफ्ट पॉवर को, गंभीर क्षति पहुंचा ली है। पुन: इसी शिखर सम्मेलन में एक ओर प्रधानमंत्री के और दूसरी ओर उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों तथा आला अफसरों के अलग-अलग रुख अपनाने से इसकी छवि बनी लगती है कि या तो इस शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने ठीक से तैयारी ही नहीं की थी या फिर उसकी नीयत में ही खोट था।
इस सब को और बदतर बना रहा है, इस शिखर सम्मेलन के बाद सरकार के आला अधिकारियों का, सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन में जो कुछ कहा गया था, उससे अलग ही आख्यान को प्रचारित करना जारी रखना। जब इन पंक्तियों को लिखा जा रहा था, तब भी सरकार के अधिकारीगण साक्षात्कारों में यही कह रहे थे कि ग्लास्गो में प्रधानमंत्री तो, भारत के उत्सर्जन में कटौती के भविष्य के मंसूबों के संबंध में सिर्फ सामान्य वक्तव्य दे रहे थे, जिनका लक्ष्य मुख्यत: घरेलू कार्रवाई से संबंधित था, न कि अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं तथा जरूरी एनडीसी के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करना। एनडीसी के संबंध में तो अधिकारियों का कहना था कि उसे तो शायद, भारत की ओर से पेश भी नहीं किया जाए! तो यह सब, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था और उससे संबंधित वार्ताओं के संदर्भ में भारत को कहां पहुंचा देता है? जाहिर है कि आने वाले दिनों में भारत को बहुत तथा कड़ी मेहनत करनी होगी तथा जो नुकसान हो गया है उसे कम करने में जुटना होगा और इसके अलावा अकार्बनकीकरण के रास्ते के संबंध में भारत की नीति को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारी जरूरी तैयारियां करनी होंगी, वह तो अपनी जगह है ही।
विकसित देशों की करनी है ग्लास्गो का मामूली हासिल
बहरहाल, भारत द्वारा और भारत के गिर्द हुआ यह नाटक, हम भारत के लोगों को चाहे जितना ही बड़ा क्यों न लगे, ग्लास्गो शिखर सम्मेलन के वास्तविक नतीजों के लिए तो यह, हाशिए का ही मामला था। इस सम्मेलन के नतीजों पर सरसरी नजर डालने से भी साफ हो जाएगा कि ग्लास्गो शिखर सम्मेलन का हासिल मामूली ही रहना मुख्य रूप से, विकसित देशों की और खनिज ईंधन उद्योग व विशेष रूप से तेल व गैस उद्योगों की ही करनी है।
विकसित देशों ने, ग्लास्गो सम्मेलन से पहले ही उत्सर्जन कटौती की जो वचनबद्घताएं स्वीकार की हुई थीं, उनसे आगे इस मामले में कोई वचनबद्घताएं अंगीकार नहीं कीं। अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा अन्य विकसित देशों ने, सिर्फ 2050 तक नैट जीरो के लक्ष्य की दीर्घावधि वचनबद्घताओं तक ही खुद को सीमित रखा, जबकि सभी विशेषज्ञ इस पर एकमत हैं कि इन वचनबद्घताओं का तब तक कोई खास अर्थ ही नहीं है जब तक कि 2030 तक, अल्पावधि उत्सर्जन कटौतियों में तेज रफ्तार से बढ़ोतरी नहीं की जाती है। अमरीका में बाइडेन प्रशासन ने, पेरिस समझौते के साथ फिर से जुडऩे के समय, 2030 तक उत्सर्जन कटौती की एनडीसी की पहले की 2005 के स्तर से 26-28 फीसद कटौती की वचनबद्घता को, 50 फीसद कटौती तक कर दिया था और 2035 तक बिजली को पूरी तरह से खनिज ईंधन से मुक्त करने तथा 2050 तक नैट जीरो पर पहुंच जाने की वचनबद्घता स्वीकार की थी। इसके बाद भी वह योरपीय यूनियन के उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य से 27 फीसद पीछे है, जिसने 2030 तक 55 फीसद कटौती की वचनबद्घता तो स्वीकार की थी, लेकिन यह कटौती 1990 के स्तर से की जानी है।
कोप-26 सम्मेलन से पहले, 2030 तक विश्व ताप में 2.7 डिग्री की बढ़ोतरी का जो अनु्रमान था, इस सम्मेलन के बाद मामूली कमी के साथ यह अनुमान 2.4 डिग्री पर आ गया है। इससे साफ है कि ग्लास्गो सम्मेलन पर्यावरण परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में किसी उल्लेखनीय प्रगति के बजाए, यथास्थिति बने होने को ही दिखाता है। कम से कम विकसित देशों के लिहाज से तो यही सच है।
ग्लास्गो समझौता अब सभी देशों से इसका तकाजा करता है कि अगले साल तक, उत्सर्जन में कटौती के अपने और संशोधित तथा बढ़े हुए लक्ष्य पेश करें। क्या एक और साल का समय देने से कोई खास फर्क पडऩे जा रहा है? क्या इस तरह की सालाना बढ़ोतरियां, ज्यादा समय तक चलती रह सकती हैं? क्या विकसित देश अपनी उत्सर्जन कटौतियों में और बढ़ोतरी करेंगे और अगर करेंगे भी तो कितनी बढ़ोतरी? एक और आंखों में गढऩे वाली सचाई को किसी न किसी तरह से पहचानना होगा कि चीन का सालाना उत्सर्जन बहुत ज्यादा है और कार्बन बजट में उसका हिस्सा बढ़ ही रहा है। अगर चीन अपनी उत्सर्जन कटौतियों को तेजी से बढ़ाता नहीं है, तो ताप बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमित करने का लक्ष्य हासिल होना बहुत ही मुश्किल होगा।
इस बात का बहुत ढोल पीटा जा रहा है कि ग्लास्गो समझौते में पहली ही बार स्पष्टï रूप से इसका इशारा किया गया है कि कोयला-जनित बिजली का अंत होने जा रहा है। लेकिन, यह ध्यातव्य है कि तेल या प्राकृतिक गैस के मामले में, जोकि ज्यादातर अमरीका तथा योरपीय यूनियन के लिए तेल या कोयले व नवीकरणीय ऊर्जा के बीच, एक संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में उपलब्ध है, इस तरह के ‘‘फेजिंग डॉउन’’ या ‘‘फेजिंग आउट’’, किसी का भी जिक्र ही नहीं किया गया है। समझौते में सिर्फ खनिज ईंधनों के लिए ‘अकुशल सब्सीडियों’ की बात की गयी है, लेकिन यह बताया ही नहीं गया है कि ‘कुशल सब्सीडियां’ कैसी होंगी या इस तरह की सब्सीडियां कोयले के लिए लागू क्यों नहीं होंगी। अनेक प्रेक्षकों ने यह ध्यान दिलाया है कि ग्लास्गो में सबसे भारी उपस्थिति सामूहिक रूप से खनिज ईंधन उद्योगों की ही थी, यानी ब्राजील के विशालकाय, 450 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से भी ज्यादा!
विभिन्न देशों द्वारा किए गए अनेक बहुपक्षीय समझौतों का भी काफी ढोल पीटा गया है, जैसे 2030 तक निर्वनीकरण को रोकने पर समझौता और 2030 तक मीथेन के उत्सर्जनों में कटौती पर समझौता। इसके बावजूद, यह बिल्कुल ही स्पष्टï नहीं है कि क्या ये कदम संबंधित देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए एनडीसी से ऊपर से होंगे या संबंधित देशों के एनडीसी में ही जुड़ जाएंगे? जहां भारत इनमें से किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं है, भारत वित्तीय सहायता से जुड़े कोयला-जनित शक्ति के उपयोग को घटाने के बहुपक्षीय समझौतों का हिस्सा है। ऐसा माना जा सकता है कि यह भी, अपनी ऊर्जा टोकरी में कोयले का हिस्सा घटाने के भारत के समग्र लक्ष्य की ओर बढ़ने का ही, एक और दरवाजा होगा।
विकासशील देशों के लिए नहीं ज़्यादा कुछ
विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता के मामले में भी, विकसित देश एक बार फिर अपने पहले के वादों से फिर गए हैं और अपनी चलाने में कामयाब हो गए हैं। पेरिस समझौते में पहली बार, 100 अरब डालर के आंकड़े को मंजूर किया गया था, जिसे उसके बाद से ही लगातार स्थगित किया जाता रहा है। इसे ग्लास्गो में एक बार फिर, 2023 तक औपचारिक रूप से टाल दिया गया है। अब तक जो एक बड़ी जीत हासिल हुई है, उसमें विकसित देशों द्वारा इसका वादा शामिल है कि एडॉप्टेशन के लिए वित्त को 2019 के 20 अरब डालर के स्तर से दुगना कर के, 40 अरब डालर सालाना कर दिया जाएगा, लेकिन वह भी 2025 तक ही। जाहिर है कि यह भी 100 अरब डालर की उस कुल सहायता के दायरे में ही है, जिसका पहले से वादा किया जा चुका है, लेकिन जिसे अब तक जमीन पर नहीं उतारा जा सका है। द्वीपीय देशों और सबसे कम विकसित देशों द्वारा इसके लिए काफी जोर लगाया गया था कि पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों के चलते, उनका जो नुकसान पहले ही हो चुका है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, क्षति व हानि के लिए वित्त मुहैया कराए जाने के संबंध में, कहीं सख्ती से समझौते के पाठ में व्यवस्था जोड़ी जाए।
क्षति और हानि क्षतिपूर्ति के लक्ष्य के लिए, सम्मेलन में जितने समय तथा ऊर्जा को लगाया गया है, वे शायद उतने फलप्रद साबित नहीं हों, जितना इसके पैरोकार मानते हैं। यह चाहे कितना ही ‘राजनीतिक रूप से गलत’ क्यों न लगे, दो असुविधाजनक किंतु निर्विवाद तथ्यों को यथार्थवादी तरीके से सामना करना होगा। विकसित देशों, खासतौर पर अमरीका को, शायद कभी भी क्षति व हानि का दोष, क्षतिपूर्ति या मुआवजे के रूप में मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वे इसे ऐसी कानूनी देनदारी स्वीकार किए जाने के तौर पर देखते हैं, जिसकी लागत का पूर्वानुमान ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वे क्षति व हानि को एडॉप्टेशन आदि के लिए सहायता की श्रेणी में ही धकेल देना चाहेंगे। पुन: विकसित देशों से मिलने वाली सारी की सारी सहायता, अंतत: तो एक ही खजाने से आ रही होगी और यह सहायता देने से तो वे पहले ही पीछे हट रहे हैं और उसी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ऋणों को, विश्व बैंक आदि के फंडों को इस श्रेणी में जोड़ना शामिल है। दुर्भाग्य से, जैसाकि ग्लास्गो में हुआ, विकसित देश अपने आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल कर के, वित्त मुहैया कराने के मुद्दे का लालच दिखाते रहते हैं, ताकि इसके सहारे उत्सर्जनों में कटौती के लिए अपने ऊपर आने वाले दबाव से निपट सकें।
पर्यावरण के मुद्दे पर अंतर्राष्tट्रीय वार्ताएं, खुद अपनी ही रची त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं तथा दोषपूर्ण उत्सर्जन नियंत्रण ढांचे में फंसी हुई हैं। स्वैच्छिक वचनबद्घताओं की रणनीति, जो पहले कोपेनहेगन सम्मेलन में पेश की गयी थी और पेरिस समझौते में शामिल कर ली गयी थी, अब साफ तौर पर विफल साबित हो चुकी है और शक्ति की बागडोर विकसित देशों के हाथों में पकड़ाना ही साबित हुई है। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए एक ऐसी नयी व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाली, दोनों तरह की रणनीतियों का योग हो।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।























