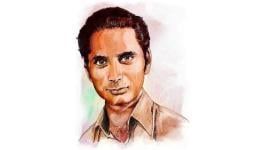जीसस से जयललिता तक : क्या 'बहुमत' ग़लत हो सकता है?

"तीन लोग मिलकर एक शेर बना देते हैं।" यह एक चीनी कहावत है, जो किसी व्यक्ति की उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, जिसके तहत वो अजीबो-गरीब़ जानकारी को भी सच मान लेता है, बशर्ते उस जानकारी को बड़ी संख्या में लोगों ने बोला हो। यह कहावत प्राचीन चीन में वेई नाम के राज्य में एक अधिकारी पांग कॉन्ग द्वारा बोली गई मानी जाती है। पांग कॉन्ग ने वेई के राजा से पूछा कि क्या वे किसी नागरिक की इस बात पर यकीन करेंगे कि बाज़ार में एक शेर घूम रहा है। जिसके जवाब में राजा ने "नहीं" कहा। पांग कॉन्ग ने पूछा कि अगर दो लोग ऐसा कहें तब क्या लगेगा, राजा ने जवाब में कहा कि फिर उन्हें ताज़्जुब होने लगेगा। पांग कॉन्ग ने फिर पूछा कि अगर "तीन लोग यह दावा कर दें कि उन्होंने शेर देखा है?" राजा ने कहा तब वह यकीन कर लेगा। पांग कॉन्ग ने राजा को याद दिलाया कि शेर के बाज़ार में घूमने की बात बेहद बेतुकी है, लेकिन कई लोगों द्वारा जब इस बात को दोहराया गया, तो वह सच्चाई लगने लगती है।
हालांकि आजकल हमें चीन के निर्यात से दिक्कत होने लगी है, लेकिन यह चीनी कहावत भारत के लिए "अच्छी" और "जरूरी" है। यह कहावत अहम सवाल उठाती है, जिससे राजनीतिक दार्शनिक जूझते रहे हैं। हम जानते हैं कि आंकड़े और संख्याएं अच्छी होती हैं, लेकिन वे अपने आप में बेहद अधूरे होते हैं। एक लोकतंत्र जो बड़े स्तर पर आंकड़ों पर निर्भर करता है, सवाल उठता है कि इन आंकड़ों का अगर कोई शिक्षात्मक मूल्य है या फिर यह व्यक्तिगत नज़रिए का बढ़ा-चढ़ा नतीज़ा है।
क्या 'बहुसंख्यकों' द्वारा आदेशित वैश्विक नज़रिया पर्याप्त है या फिर हमारे संवैधानिक ढांचे में कुछ नैतिक निरपेक्षता है, जो खुद को मानने वाले की संख्या से प्रभावित नहीं होती?
इस बिंदु पर 'लोकतंत्र' को 'बहुसंख्यकवाद' से अलग देखना चाहिए।
जब हम यहां एक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको संवैधानिक नैतिकता के साथ बाइबिल का कुछ ज्ञान देता हूं।
एक मध्य-पूर्वी ट्रासेनेरियन इंसान जीसस क्राइस्ट, फटे हुए गंदे कपड़ों में खड़े हुए हैं, उनकी बुरी तरीके से पिटाई की गई है। जीसस, दुनिया के अब तक के सबसे ताकतवर, रोमन साम्राज्य के प्रतिनिधि और जूडा के गवर्नर पोंटिअस पाइलेट के सामने खड़े हैं। यहूदी लोगों की भीड़ आसपास खड़ी है, जो उनके खून की प्यासी है। जबकि जीसस इन्हीं यहूदी लोगों के बीच से आए थे। जीसस के खिलाफ़ ईशनिंदा का आरोप है। पोंटिअस पाइलेट ने भीड़ से पूछा, "आप अपने लिए किसको बाहर निकलवाना चाहते हैं। बारब्बास या फिर जीसस को, जो अपने आप को क्राइस्ट कहता है?" भीड़ की आवाज आई- 'बारब्बास'। बारब्बास पहली सदी में जूडा का ख़तरनाक अपराधी था, जिसे तत्कालीन लोगों ने "आदतन अपराधी" कहा था।
ठीक 2000 साल बाद, भारत में जे जयललिता को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 और IPC, 1860 के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया गया। दोषी ठहराए जाने के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1950 के तहत उन्हें 2001 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। हालांकि उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया और उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन उनकी पार्टी AIADMK जयललिता के करिश्मे और अधिनायकवादी छवि के चलते बड़े बहुमत से जीत गई। जब ताज पहनाने की बारी आई, तो उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इसके लिए संविधान के एक दिलचस्प अनुच्छेद, 'अनुच्छेद 164' का इस्तेमाल किया गया।
अनुच्छेद 164 (4) के ज़रिए किसी व्यक्ति को तब भी मंत्री बनाया जा सकता है, जब वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना हो, बशर्ते उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर विधायिका का हिस्सा बनना होगा।
जैसा पहले बताया गया, लोकतंत्र के क्रियान्वयन का तरीका ही व्यक्तिगत नज़रियों को इकट्ठा कर फैसला लेना है। फिर "लिब्रांडू" हमेशा उन फ़ैसलों का विरोध क्यों करते हैं, जिन्हें बहुमत का समर्थन होता है?
हमारी यादों को ताजा करते हुए बता दूं कि जब किसी राजनीतिक दल का कोई नेता किसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो इस अनुच्छेद का अकसर प्रयोग होता है। हाल में उद्धव ठाकरे के मामले में यही हुआ।
जयललिता की नियुक्ति को एक जनहित याचिका के ज़रिए चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बी आर कपूर बनाम् तमिलनाडु राज्य मामले में अपना फ़ैसला सुनाया। एक व्यक्ति जिसे सदन का सदस्य बनने से अयोग्य ठहराया जा चुका है, वह 164 (4) का उपयोग कर मंत्री बन जाता है। मुख्य चिंता इसी बात को लेकर थी। तकनीकी तर्कों के अलावा, जयललिता के वकील ने तर्क दिया कि भले ही उन्हें अयोग्य ठहराया जा चुका हो, लेकिन "लोगों का मत" साफ तौर पर उनके पक्ष में है, क्योंकि जिस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया था, उसने जीत दर्ज की है। जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरी है, वह उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए।
जीसस से लेकर जयललिता तक, बुनियादी सवाल बना हुआ है कि क्या बहुमत गलत हो सकता है? जैसा पहले ध्यान दिलाया गया, जब लोकतंत्र के क्रियान्वयन का तरीका व्यक्तिगत नज़रिए को इकट्ठा करना होता है, तो क्यों "लिब्रांडु" बहुमत द्वारा समर्थित फ़ैसलों का विरोध करते रहते हैं? क्या यह दोहरा रवैया नहीं है कि लोकतंत्र का समर्थन करते हुए बहुमत के विचारों को कमज़ोर किया जा रहा है? इसका विरोध में यह अवधारणा है कि लोकतंत्र का मतलब सिर और हाथ गिनने से कहीं ज़्यादा है।
हरबर्ट स्पेंसर इस पहले को "राज्य को नजरंदाज करने के अधिकार" के उदाहरण से समझाते हैं। वह कहते हैं: "चलिए मान लेते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जनता में "माल्थुवादी चिंताएं" छा गईं (मालथू एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने आबादी के बारे में अवधारणाएं रखीं), एक विधानसभा जो जनता के मत का प्रतिनिधित्व करती है, उसने एक कानून बनाया कि अगले दस साल में जो भी बच्चे पैदा होंगे, उन्हें डुबोकर मार दिया जाएगा। क्या कोई सोच सकता है कि इस तरह के कानून को अनुमति दी जा सकती है। अगर नहीं, तो साफ है कि बहुमत की शक्ति की अपनी सीमाएं हैं।"
बल्कि कानून ही राजाओं का राजा है और लोकप्रिय मत के ऊपर विजय पाता है।
अनौपचारिक तर्क पाठ में हमें बताया गया है कि "लोकतांत्रिक भुलावा" एक ऐसा त्रुटिपूर्ण तर्क जिस पर लोग निर्भर होते हैं। उदाहरण: हर कोई गतिसीमा के परे जाकर गाड़ी चलाता है, तो इसलिए यह कानून के खिलाफ़ नहीं होना चाहिए। क्या आप यहां समस्या को पहचान पा रहे हैं?
इस बिंदु पर लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद से अलग करने की जरूरत है। लोकतंत्र का एक कम जाना गया पहलू यह है कि लोकतंत्र सिर्फ़ बहुमत का शासन नहीं है। बल्कि इसके भीतर इंसान द्वारा जाने गए सबसे पवित्र विशेषणों में से एक "कानून का शासन" भी निहित है। संख्या + कानून का शासन = लोकतंत्र।
इस समीकरण में अगर कानून का शासन नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ भीड़ का शासन ही बचेगा। इतिहास उन उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनमें बहुसंख्यक बहुत बुरे तरीके से गलत हुए हैं। हिटलर को "चुना" गया था। न्यूरेमबर्ग के नस्लीय कानून विधायिका से पारित हुए थे। सेलेम विच ट्रॉयल पर जनता के मत का गहरा प्रभाव था। अगर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने वक़्त-वक़्त पर नागरिक अधिकारों पर अलग-अलग न्यायिक फ़ैसले और घोषणाएं ना की होतीं, तो आज वहां नस्लीय भेद पर आधारित "जिम क्रो" कानून होते।
डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने एक प्रसिद्ध लेख में इस बिंदु को विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा, "हम कभी यह नहीं भूल सकते कि हिटलर ने जर्मनी में जो भी किया, वह 'कानूनी' था और जो कुछ भी हंगरी के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, वह सब गैरकानूनी था। हिटलर के जर्मनी में एक यहूदी की मदद करना गैरकानूनी था, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं उस वक़्त जर्मनी में रह रहा होता, तो मैं अपने यहूदी भाईयों की मदद की होती, भले ही यह गैरकानूनी होता। अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई करने वाले हम लोग तनाव निर्माता नहीं हैं। हम तो बस उस तनाव को सतह पर लाते हैं, जो पहले से ही मौजूद है।"
बल्कि कानून राजाओं का राजा है और लोकप्रिय मत के ऊपर विजय पाता है। भारत में हमने लिखित संविधान अपनाया है, यह ब्रिटिन की मौखिक परंपरा से अलगाव था। हमने लिखित संविधान इसलिए अपनाया ताकि हम अतार्किक जनमत के दबाव में सत्य के पैमाने को बरकरार रख सकें। ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि वह इतनी ताकतवर है कि वह एक महिला को आदमी और आदमी को महिला भी घोषित कर सकती है। हमने अपनी संसद को इस तरह की शक्तियां नहीं दीं, ताकि ऐसी बुरी स्थिति से बचा जा सके। ताकि इस पूरी प्रक्रिया में सच को किसी तरह का नुकसान ना होने पाए।
मेरी कल्पना में हमारे लोकतंत्र के भविष्य की आशा है। यह वह आशा है, जिसमें हम लोकतंत्र को सिर्फ व्यक्तिगत मतों का गठजोड़ नहीं मानते।
जीसस और जयललिता की एक जैसी कहानी का अंत अलग-अलग है। जीसस को उस वक़्त के लोकप्रिय जनमत के चलते सूली पर लटका दिया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जनभावना के खिलाफ़ रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाया, ऐसा करते हुए कोर्ट ने कुछ पवित्र तारों को छेड़ा, जिनसे एक बेहतरीन संगीत का निर्माण हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "काउंसल द्वारा जो बातें कही गई हैं, उन्हें मान लेना एक आपदा को निमंत्रण है। उदाहरण के लिए, विधानसभा का बहुमत एक विदेशी नागरिक को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। ऐसा विदेशी नागरिक, जो विधायिका का सदस्य नहीं बन सकता और जो अनुच्छेद 173 के तहत सदस्य बनने की अहर्ताएं भी नहीं रखता। लेकिन अनुच्छेद 164 (1) और (4) के तहत विधानसभा राज्यपाल को ऐसा करने के लिए कह सकती है। राज्यपाल यह बात मानने के लिए बाध्य होगा। विधानसभा विदेशी मुख्यमंत्री के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुमतधारी पार्टी इसका विरोध करेगी। इस तरह एक विेदेशी मुख्यमंत्री अगले चुनावों तक पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 164 की इतनी ख़तरनाक व्याख्या को पूरी तरह से नकारना होगा। संविधान, लोगों की उस भावना के ऊपर होता है, जिसका प्रतिनिधित्व बहुमत हासिल करने वाला दल करता है। इस तरह की पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाली भावना तभी लागू हो सकती है, जब यह संविधान सम्मत हो।"
मैं जानता हूं कि आखिरी कुछ पंक्तियां पाठकों के लिए कोई नई बात नहीं हैं। यह बताना लोगों के लिए नया नहीं है कि "लोगों की इच्छा" संविधान के नीचे है, यह उस सच्चाई की चौखट से नीचे है, जिसे हमने 26 जनवरी, 1950 को खुद को सुपुर्द किया था। मेरी कल्पना में हमारे लोकतंत्र के भविष्य की आशा है। यह वह आशा है, जिसमें हम लोकतंत्र को सिर्फ व्यक्तिगत मतों का गठजोड़ नहीं मानते। सामान्य तौर पर लोकतंत्र बहुमत का शासन दिखता है, लेकिन वास्तव मे लोकतंत्र विमर्श और असहमति के ज़रिए चलने वाला कानून है।
केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सुरक्षा को मजबूत करते हुए संविधान को बदलने की संसद की शक्तियों को बेड़ियां लगा दीं। ताकि संविधान के बुनियादी ढांचे को जोड़े रखा जा सके और इस पर तत्कालीन जनभावना का कोई असर न पड़े। मेनका गांधी बनाम् भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे बढ़ा। कोर्ट ने कहा कि किसी कानून की पवित्रता सिर्फ इस बात से नहीं आती कि उसे विधानसभा ने पास किया है। कानून को 'न्यायपूर्ण' भी होना होगा। मेरे हिसाब से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता में जान डाल दी।
असली तनातनी न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित कानून और इसकी गैरमौजूदगी के बीच होती है।
जैसा जॉन एडम्स ने 'अ डिफेंस ऑफ द कांस्टीट्यूशन ऑफ गवर्मेंट ऑफ द यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका' में इंगित किया, लोकतंत्र द्वारा संतुलन बनाने के उपायों को खत्म करने से "बहुसंख्यकों की निरंकुशता" के लिए जगह बन सकती है। एंडमंड बर्क ने 1790 में एक तीखा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत सही तरीके से "बहुसंख्यकों की निरंकुशता, कई गुना बड़ी निरंकुशता है" को परिभाषित किया।
हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि तनातनी बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच नहीं है। क्योंकि इनका ढांचा भविष्य में बदल भी सकता है और एक व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटा अल्पसंख्यक है। असली तनातनी न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित कानून और इसकी गैरमौजूदगी के बीच होती है।
जीसस और पाइलेट के बीच हुई बातचीत में एक दिलचस्प चीज होती है। जीसस के खिलाफ़ जब ईशनिंदा का आरोप लगाया गया, तो पाइलेट ने जीसस से एक सवाल पूछा- "तुम तो राजा हुए तब!"
जीसस ने जवाब में कहा, "तुम कहते हो, मैं राजा हूं। बल्कि मेरा जन्म इसलिए हुआ, ताकि मैं सत्य के लिए गवाही दे सकूं। जो भी सत्य के पक्ष में है, वह मुझे सुनता है।"
घटनाक्रम के आगे बढ़ने के साथ पाइलेट ने एक और सवाल रखा। शायद यह सबसे अहम था। उसने पूछा- सत्य क्या है? लेकिन उसने जवाब का इंतज़ार नहीं किया और चला गया। मैं आशा करता हूं कि जब भी यह सवाल हम पूछें या यह सवाल हमारे सामने आए, तो हम उसका जवाब जानने के लिए इंतज़ार करें।
प्रतीक पटनायक नई दिल्ली आधारित वकील और संविधानिज्ञ हैं। यह उनके निजी विचार हैं।
इस लेख को पहले The Leaflet में प्रकाशित किया गया था।
मूल आलेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।