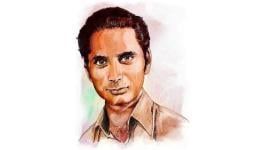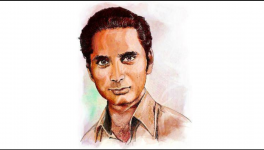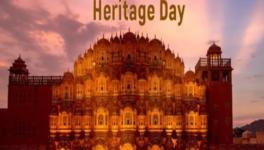कैफ़ी आज़मी: उर्दू शायरी के बाग़ का एक सुर्ख़ फूल

तस्वीर में कैफ़ी आज़मी अपनी जीवनसाथी शौकत कैफ़ी और बेटी शबाना आज़मी के साथ। साभार
कैफ़ी आज़मी एक प्रतिबद्ध वामपंथी थे। अपनी ज़िंदगी के आख़िर तक वे साम्यवादी विचारों में रचे-पगे रहे। इस ख़याल से उनका नाता कभी नहीं छूटा। उनकी एक नहीं, कई ऐसी नज़्में हैं, जिनमें उनके साम्यवादी ख़याल नुमायां हुए हैं। दीगर तरक़्क़ीपसंद शायरों की तरह कैफ़ी आज़मी ने भी अपनी शायरी की इब्तिदा रूमानी ग़ज़लों से की, लेकिन बाद में वे पूरी तरह से नज़्मों की ओर आ गए। मुल्क की आज़ादी की तहरीक में जहां उन्होंने वतनपरस्ती में डूबी इंक़लाबी नज़्में लिखीं, जिसमें उनका समाजवादी फ़लसफ़ा साफ़ नज़र आता है। तो वहीं आज़ादी के बाद मुल्क में बढ़ती फ़िरक़ापरस्ती और साम्प्रदायिक कट्टरता भी उनके निशाने पर रही।
कैफ़ी आज़मी की शायरी के बारे में अफ़साना निगार कृश्न चंदर का ख़याल था, ‘‘वही व्यक्ति ऐसी शायरी कर सकता है, जिसने पत्थरों से सिर टकराया हो और सारे जहान के ग़म अपने सीने में समेट लिए हों।’’ साल 1944 में महज़ 26 साल की छोटी सी उम्र में कैफ़ी आज़मी का पहला ग़ज़ल मजमुआ ‘झनकार’ प्रकाशित हो गया था। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य सज्जाद ज़हीर ने उनके इस मजमुए की शायरी की तारीफ़ में जो बात लिखी, वह उनके तमाम कलाम की जैसे अक्कासी है, ’‘आधुनिक उर्दू शायरी के बाग़ में नया फूल खिला है, एक सुर्ख़ फूल।’’ ‘आख़िर-ए-शब’, ‘इबलीस की मजलिसे शूरा’ और ‘आवारा सज्दे’ कैफ़ी आज़मी के दीगर काव्य संग्रह है।
कैफ़ी आज़मी ने इंक़लाब और आज़ादी के हक़ में खूब लिखा। इसके एवज़ में उन्हें कई पाबंदियां और तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ीं। लेकिन उन्होंने अपने बग़ावती तेवर नहीं बदले। कैफ़ी आज़मी कॉलम निगार भी थे। उनके ये कॉलम उर्दू साप्ताहिक ‘ब्लिट्ज’ में नियमित प्रकाशित होते थे। ‘नई गुलिस्तां’ नाम से छपने वाला यह कॉलम राजनीतिक व्यंग्य होता था। जिसमें सम-सामयिक मसलों पर वे तीख़े व्यंग्य करते थे। उनके ये कॉलम ‘नई गुलिस्तां’ नाम से ही एक किताब में प्रकाशित हुए हैं। तक़रीबन 600 पेज की यह किताब दो खंडों में है। ‘नई गुलिस्तां’ के अनुवादक नरेश ‘नदीम’ जिन्होंने इस किताब का सम्पादन भी किया है, कैफ़ी के नस्र की ख़ासियत को बयां करते हुए लिखते हैं, ‘‘इस पूरे संकलन को नज़्म में लिखी गई नस्र (गद्य) का नाम दें, जो तथाकथित नस्री नज़्म (गद्य काव्य) से कहीं बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है, तो कुछ ग़लत नहीं होगा। इस पूरे संकलन में शायद ही आपको ऐसा कोई वाक्य मिले, जिसमें कैफ़ी ने अपनी शायराना फ़ितरत छोड़ी हो और काफ़िया—पैमाई न की हो। यानी कि कैफ़ी की नस्र भी बड़े ठस्से के साथ यह कहती नज़र आती है कि मैं किसी नस्रनिगार की नहीं, एक शायर की रचना हूं।’’
क़ैफी आज़मी जब मुम्बई आए, तो तरक़्क़ीपसंद तहरीक की दाग बेल सज्जाद ज़हीर डाल चुके थे। कैफ़ी आज़मी ने मुम्बई में प्रगतिशील लेखक संघ, क़ायम करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और यहां बहुत बड़ा संगठन बनाया। आगे चलकर तरक़्क़ीपसंद तहरीक के अहम लीडर के तौर पर उन्होंने देश भर में दौरे किए और लोगों को अपने साथ जोड़ा। कैफ़ी आज़मी बंटवारे और साम्प्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। भारत-पाक विभाजन के समय पार्टी ने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को जहां पाकिस्तान पहुंचा दिया, तो वहीं क़ैफ़ी ने हिंदुस्तान में ही रहकर काम किया। साम्प्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता जैसी अमानवीय प्रवृतियों पर प्रहार करते हुए कैफ़ी ने लिखा,
‘‘टपक रहा है जो ज़ख़्मों से दोनों फ़िरक़ों के
ब ग़ौर देखो ये इस्लाम का लहू तो नहीं
तुम इसका रख लो कोई और नाम मौज़ू सा
किया है ख़ून से जो तुमने वो वजू तो नहीं
समझ के माल मेरा जिसको तुमने लूटा है
पड़ोसियों ! वो तुम्हारी ही आबरू तो नहीं।
(नज़्म—‘लखनऊ तो नहीं’)
कैफ़ी आज़मी मुम्बई में चाल के जिस कमरे में रहते थे, वहीं उनके आस-पास बड़ी तादाद में मज़दूर और कामगार रहते थे। मज़दूरों-कामगारों के बीच रहते हुये उन्होंने उनके दुःख, दर्द को समझा और क़रीब से देखा। मज़दूरों, मज़लूमों का यही संघर्ष उनकी बाद की नज़्मों में साफ़ दिखाई देता है,
आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है
आज की रात न फ़ुट-पाथ पे नींद आएगी
सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो
कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जायेगी।
(नज़्म—‘मकान’)
अली सरदार जाफ़री की तरह कैफ़ी ने भी शायरी को हुस्न, इश्क़ और जिस्म से बाहर निकालकर आम आदमी के दु:ख-दर्द, संघर्ष तक पहुंचाया। अपनी शायरी को ज़िंदगी की सच्चाइयों से जोड़ा। कैफ़ी आजमी अत्याचार, असमानता, अन्याय और शोषण के ख़िलाफ़ ता—उम्र लड़े और अपनी शायरी, नज़्मों से लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। आज़ादी के बाद कैफ़ी ने समाजवादी भारत का तसव्वुर किया था। स्वाधीनता के पूंजीवादी स्वरूप की उन्होंने हमेशा आलोचना की। अपनी नज़्म ‘क़ौमी हुक़्मरां‘ में तत्कालीन भारतीय शासकों की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा,
रहजनों से मुफ़ाहमत करके राहबर काफ़िला लुटाते हैं
लेने उठे थे ख़ून का बदला हाथ जल्लाद का बंटाते हैं।
कैफ़ी के यही आक्रामक तेवर आगे भी बरक़रार रहे। उनकी शायरी में समाजी, सियासी बेदारी साफ़-साफ़ दिखाई देती है। सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सद्भाव को उन्होंने हमेशा अपनी शायरी में बढ़ावा दिया। स्त्री-पुरुष समानता और स्त्री स्वतंत्रता के हिमायती कैफ़ी आज़मी अपनी मशहूर नज़्म ‘औरत‘ में लिखते हैं,
तोड़ कर रस्म का बुत बंदे-क़दामत से निकल
ज़ोफे-इशरत से निकल, वहमे-नज़ाकत से निकल
नफ़्स के खींचे हुये हल्क़ाए-अज़मत से निकल
राह का ख़ार ही क्या, गुल भी कुचलना है तुझे
उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे।
कैफ़ी आज़मी फ़िरक़ापरस्ती और मज़हबी कट्टरता के हमेशा मुखा़लिफ़ रहे। अपनी नज़्मों ‘सोमनाथ’, ‘सांप’, ‘बहुरूपनी’, ‘‘लखनऊ तो नहीं’ और ‘दूसरा बनवास’ में उन्होंने इन इंसानियत विरोधी प्रवृतियों की खुलकर मुख़ालफ़त की। अपनी एक नज़्म में साम्प्रदायिक लीडरों और कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुये वे कहते हैं,
तुम बनाओ तो ख़ुदा जाने बनाओ कैसा
अपने जैसा ही बनाया तो क़यामत होगी।‘‘
(नज़्म—‘सोमनाथ’)
कैफ़ी आज़मी महज एक अदीब ही नहीं थे, बल्कि एक्टिविस्ट भी थे। जब भी ज़रूरत पड़ी, वे बिना किसी ख़ौफ़ के सड़कों पर उतरे। साल 1989 में इप्टा ने उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिकता और पुनरुत्थानवाद विरोधी पांच दिवसीय सद्भावना यात्रा निकाली। यह वह दौर था, जब राम जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद मामला सुर्ख़ियों में था। इस मुद्दे को लेकर पूरे मुल्क में साम्प्रदायिक तनाव चरम पर था। बीमारी के बावजूद कैफ़ी आज़मी इस सद्भावना यात्रा में शामिल हुए। व्हीलचेयर पर बैठकर, उन्होंने यह पूरा सफ़र तय किया। इस यात्रा में उन्होंने जगह—जगह अवाम से सीधा संवाद क़ायम किया। अपनी नज़्मों और ग़ज़लों के मार्फ़त उन्हें समझाने की कोशिश की। एक-दो जगह यात्रा पर हमला भी हुआ, मगर वे हिम्मत नहीं हारे। तमाम प्रगतिशील और जनवादी ताक़तों की कोशिशों के बाद भी साल 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई। इस घटना ने देश में साम्प्रदायिक विभाजन को और बढ़ाया। हिंदू-मुस्लिम के बीच शक की दीवारें खड़ी हुईं। कैफ़ी आज़मी जिन्होंने ख़ुद बंटवारे का दंश भोगा था, वे एक बार फ़िर साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए आगे आए। अपनी चर्चित नज़्म ‘दूसरा बनवास‘ में उन्होंने लिखा,
पांव सरजू में अभी राम ने धोये भी न थे
कि नज़र आये वहां ख़ून के गहरे धब्बे
पांव धोये बिना सरजू के किनारे से उठे
राम ये कहते हुये अपने द्वारे से उठे
राजधानी की फ़िज़ा आई नहीं रास मुझे
छः दिसम्बर को मिला दूसरा बनवास मुझे।
अपनी साम्प्रदायिकता विरोधी नज़्मों की वजह से कैफ़ी आज़मी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मज़हब के कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे। ‘पीर-ए-तस्मा-पा’ नज़्म को पढ़कर, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने तो उन्हें दहरिया (नास्तिक) शायर तक क़रार दे दिया। उन पर ब्लास्फे़मी की तोहमत लगाई। लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। आज जब चारों और फिर वही साम्प्रदायिक सियासत और मज़हबी कट्टरता का दौर—दौरा है, तो हमें कैफ़ी आज़मी और उनकी शायरी शिद्दत से याद आती है।
ये साँप आज जो फन उठाए
मिरे रास्ते में खड़ा है
पड़ा था क़दम चाँद पर मेरा जिस दिन
उसी दिन इसे मार डाला था मैंने
ये हिन्दू नहीं है मुसलमाँ नहीं
ये दोनों का मग़्ज़ और ख़ूँ चाटता है
बने जब ये हिन्दू मुसलमान इंसाँ
उसी दिन ये कम-बख़्त मर जाएगा।
(नज़्म—'साँप')
साल 1974 में आई ‘आवारा सज्दे’ कैफ़ी की आख़िरी किताब है। यह किताब आज़ादी के बाद के पच्चीस सालों का एक तटस्थ लेखा—जोखा है। भारतीय सरकारों से उनकी जो अपेक्षाएं और उम्मीदें थीं, उनके टूटने का इसमें दर्द है। वामपंथी आंदोलन के भटकाव पर भी उनकी नुक़्ता-ए-नज़र है। किताब में शामिल ‘आवारा सज्दे’, ‘दायरा’, ‘दोपहर’, ‘आख़िरी रात’, ‘मेरा माज़ी मेरे कांधे पर’ और ‘इंतशार’ वगैरह नज़्मों में वे बड़ी ही तल्ख़ी से इन सवालों को उठाते हैं।
कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले
उस इंक़िलाब का, जो आज तक उधार-सा है।
(नज़्म-‘इंतशार’)
क़ैफी आज़मी को उर्दू अदब की ख़िदमात के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से नवाज़ा गया। मसलन ‘अफ्रो-एशियन पुरस्कार’, ‘सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार’ आदि। बावजूद इसके वे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लाल कार्ड को समझते थे और उसे हमेशा अपनी जेब में रखते थे। वामपंथी विचारधारा में उनका अक़ीदा आख़िर तक रहा। अपने व्यवहार में वे पूरी तरह से वामपंथी थे। लेखन और उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क़ नहीं था। साल 1973 में कैफ़ी आज़मी को लकवा मार गया। लकवे से उनका आधा जिस्म बेजान हो गया, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। ज़िंदगी के आख़िर तक वे अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहे। उत्तर प्रदेश के मिजवां गांव में जहां कैफ़ी की पैदाइश हुई, उन्होंने अपना आख़िरी वक़्त बिताया। इस दौरान गांव की बुनियादी ज़रूरतों की तरफ उनका ध्यान गया। कैफ़ी आज़मी की ही वजह से इस छोटे से गांव मिजवां को पहचान मिलने के साथ-साथ कई सौगातें भी मिलीं। उन्हीं की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब इस गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा और आवागमन के सभी साधन उपलब्ध हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए उन्होंने वहां काफ़ी काम किया। उनके लिए स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाये। मुल्क में समाजवाद आए, कैफ़ी आज़मी का यह सपना था। वे लोगों से अक्सर यह कहा करते थे, ''मैं ग़ुलाम हिन्दुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद भारत में जिया और समाजवादी भारत में मरूंगा।'' लेकिन अफ़सोस ! कैफ़ी आज़मी की आख़िरी ख़्वाहिश उनके जीते जी पूरी नहीं हो सकी। उनका सपना अधूरा ही रहा। 10 मई, 2002 को यह इंक़लाबी शायर हमसे यह कहकर, हमेशा के लिए जुदा हो गया,
बहार आये तो मेरा सलाम कह देना
मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।