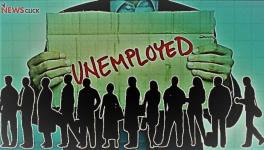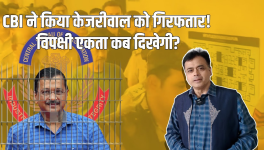मुद्दा: बेरोज़गारी से कैसे निपटें?
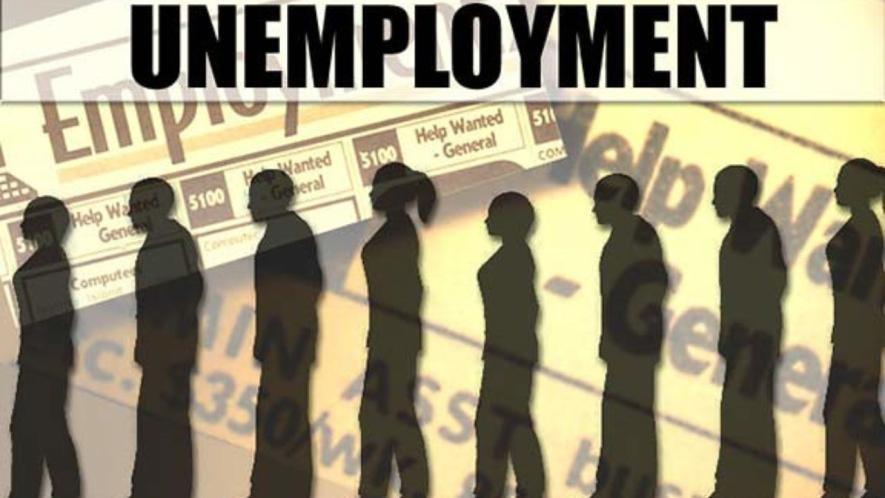
अर्थशास्त्र में मांग-बाधित अर्थव्यवस्थाओं और संसाधन बाधित अर्थव्यवस्थाओं (जिन्हें आसानी के लिए और तुल्यता के लिए हम आपूर्ति बाधित व्यवस्था कहेेंगे) के बीच, अंतर किया जाता है। किसी मांग बाधित अर्थव्यवस्था में, अगर सकल मांग में बढ़ोतरी होती है, तो तंगी से उत्प्रेरित किसी भी मुद्रास्फीति के बिना ही, उत्पाद में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन, आपूर्ति बाधित व्यवस्था में उत्पाद पर या तो इसकी कैद होती है कि उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा हो या फिर किसी अति महत्वपूर्ण लागत सामग्री की या खाद्यान्नों की या श्रम शक्ति की ही तंगी हो, जिसका नतीजा यह होता है कि सकल मांग में बढ़ोतरी, उत्पाद में बढ़ोतरी लाने के बजाए, सिर्फ तंगी से उत्प्रेरित मुद्रास्फीति पैदा करने का काम करती है।
पूंजीवाद सामान्य तौर पर या युद्ध जैसी परिस्थितियों को छोडक़र, एक मांग बाधित व्यवस्था होता है, जबकि समाजवाद, जिस रूप में सोवियत संघ तथा पूर्वी योरप में रहा था, आपूर्ति बाधित व्यवस्था था। एक मांग बाधित व्यवस्था में, अगर सकल मांग में बढ़ोतरी होती है, तो रोजगार भी बढ़ेगा।
चाहिए सकल मांग में बढ़ोतरी के कदम
भारत में इस समय, जबकि बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन चुकी है और जब बेरोजगारी की तीक्ष्णता हाल के चुनाव में भाजपा का मानमर्दन होने के पीछे एक बड़ा कारक साबित हो चुकी है और जब इसका दूर किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता का मुद्दा बन चुका है, इन दो प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच के इस अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।
अब चूंकि सेवाओं के क्षेत्र में, जिसमें सरकारी सेवाएं भी शामिल हैं, उल्लेखनीय रूप से, सोचे-समझे तरीके से रोजगार में कटौती की गयी है, जबकि अचल पूंजी स्टॉक की किसी तंगी की इसमें कोई भूमिका नहीं बनती है, हम बेरोजगारी के वर्तमान ऊंचे स्तर के लिए, उत्पादन क्षमता की किन्हीं सीमाओं को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। इसी प्रकार, बेरोजगारी का वर्तमान ऊंचा स्तर किसी महत्वपूर्ण लागत सामग्री की तंगी की वजह से भी नहीं है। खाद्यान्नों की आपूर्ति के मामले में भी कोई तंगी नहीं है, जो इस तथ्य से खुद ब खुद दिखाई दे जाता है कि मोदी सरकार भी, जो गरीबों के हक में ‘‘हस्तांतरणों’’ का मुफ्त की रेबड़ी कहकर विरोध करती है, खाद्यान्न के वर्तमान भंडारों का ही इस्तेमाल कर, लाभार्थियों की एक विशाल संख्या को प्रतिव्यक्ति 5 किलो अनाज प्रतिमाह देकर, कुछ चुनावी लाभ बटोरने की कोशिश कर रही है।
यह तो सच है कि इस समय भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं खरीदने ही वाला है, ताकि खाद्यान्न के खाली होते भंडारों को भरा जा सके, लेकिन यह कुप्रबंधन के चलते हो रहा है, न कि देश में खाद्यान्न की किसी बुनियादी तंगी के चलते। इसलिए, भारत में इस समय जो तीक्ष्ण बेरोजगारी है, मांग बाधित व्यवस्था को ही दिखाती है। इसलिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तत्काल सरकारी खर्च से संचालित ऐसे कदमों की जरूरत होगी, जिनसे सकल मांग में बढ़ोतरी हो।
वस्तुगत राजकोषीय सीमा का झूठा सिद्धांत
बड़ी तादाद में सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। शिक्षा का क्षेत्र, आश्चर्यजनक हद तक कार्मिकों की कमी का मारा हुआ है और इसकी शिक्षा की गुणवत्ता को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां तक कि सेनाओं तक में सामान्य रूप से जिस पैमाने पर भर्तियां होती थीं, नहीं हुई हैं, जिसके चलते अग्निवीर योजना जैसी भांति-भांति की योजनाएं लायी गयी हैं। संक्षेप में यह कि सरकार, रोजगार देने में अगुआई करने के बजाए, विडंबनापूर्ण तरीके से रोजगार में कटौती करने में ही लगी हुई है। इसका कारण इस तथ्य में छुपा लगता है कि उसे लगता है कि रोजकोषीय स्तर पर उसके हाथ बंधे हुए हैं। आइए, इस पर जरा और नजदीक से नजर डाल लेते हैं।
हमने पीछे जिस बुनियादी भेद का जिक्र किया है, वह मांग बाधित और आपूर्ति बाधित व्यवस्थाओं के बीच का अंतर है। आपूर्ति संबंधी सीमाओं के अलावा, जो हमने जैसा कि देखा बिल्कुल हैं ही नहीं, किसी संप्रभु देश के लिए वस्तुगत राजकोषीय सीमा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसी हरेक राजकोषीय सीमा तो संबंधित राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी द्वारा और उसके स्थानीय समकक्ष, घरेलू कारपोरेट-वित्तीय अल्पतंत्र द्वारा थोपी गयी सीमा होती है। यह सीमा, राज्य की किसी वस्तुगत सीमा को नहीं बल्कि राज्य की स्वायत्तता के हरण को ही प्रतिबिंबित करती है।
इस तथ्य को कि एक मांग बाधित व्यवस्था में, खर्च करने की राज्य की क्षमता की कोई वस्तुगत सीमाएं होती ही नहीं हैं, आर्थिक साहित्य में अब से नब्बे साल से ज्यादा पहले, तभी प्रदर्शित किया जा चुका था, जब कालेकियाई-केन्सियाई सैद्धांतिक क्रांति शुरू हुई थी। इसके बावजूद, इस झूठे सिद्धांत को जिसको नौ दशक से ज्यादा पहले ही ध्वस्त किया जा चुका था, अब भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो वास्तव में राज्य पर बड़ी पूंजी द्वारा थोपी जाने वाली सीमाएं हैं, उन्हें राज्य की वस्तुगत सीमाएं बनाकर पेश किया जा सके। बेरोजगारी का उन्मूलन करने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बड़ी पूंजी से अपनी आक्रांतता से निकल आए। राज्य को जनता की सेवा करने के संकल्प को फिर से हासिल करना होगा और उस पर काम करना होगा।
राजकोषीय घाटे का रास्ता असमानता बढ़ाता है
किसी मांग बाधित व्यवस्था में बढ़ा हुआ सरकारी खर्च, चाहे उसके लिए वित्त व्यवस्था राजकोषीय घाटे के जरिए ही की जाए, बेरोजगारी से उबारने का काम करता है। इसका मुख्य हानिकर प्रभाव किसी तरह से निजी निवेश को ‘‘धकियाकर बाहर किए जाने’’ से या उसके संबंध में किए जाने वाले ऐसे ही अन्य फर्जी दावों की वजह से नहीं होता है। इसका हानिकर प्रभाव इसलिए होता है कि यह बिना कारण के ही संपदा की असमानता बढ़ा देता है। अगर सरकार मिसाल के तौर पर 100 रुपये खर्च करती है और उसके लिए राजकोषीय घाटे से वित्त व्यवस्था करती है, तो इस प्रक्रिया में ऋण लेने के जरिए वह व्यवहार में अपने इस खर्चे के जरिए, यह 100 पूंजीपतियों के हाथों में ही पकड़ा रही होती है (क्योंकि कामगार तो जो कुछ कमाते हैं, वह सब ही करीब-करीब खर्च कर देते हैं) और फिर उनसे ही यह पैसा कर्ज पर ले रही होती है।
इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था को तीन परस्पर अपवर्जी और सर्वसमावेशी हिस्सों में बांट कर देखें--सरकार, मेहनतकश जनता और पूंजीपति। सरलता के लिए हम अर्थव्यवस्था के तमाम बाहरी लेन-देन को अनदेखा कर देंगे और यह मानकर चलेंगे कि हम एक अपनी सीमाओं में ही बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के इन तीनों हिस्सों के घाटे का योग, एक गणितीय सत्ता के रूप में हमेशा शून्य होगा। अब चूंकि मेहनतकश आम तौर पर जितना भी कमाते हैं, उसका उपभोग कर लेते हैं, उनका घाटा या बचत, शून्य ही मानना चाहिए। उस सूरत में अगर सरकार के हिस्से में घाटा आ रहा है, तो इससे खुद ब खुद पूंजीपतियों के हिस्से में उतनी ही बचत पैदा हो रही होगी और यह उनके इसके लिए सचेत रूप से कुछ भी किए बिना ही होगा। अगर सरकार शुरूआत के तौर पर बैंकों से 100 रुपये उधार लेकर खर्च करती है, तो इस अवधि के आखिर तक वह पूंजीपतियों से उन्हें मुफ्त में हुई इस बचत में से 100 रुपये कर्ज ले सकती है और बैंकों का कर्ज चुका सकती है।
पूंजीपतियों पर कराधान से रोज़गार विस्तार
पूंजीपतियों के हाथों में यह अधिशेष इसलिए आ जाता है क्योंकि सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के चलते, उनके मालों की बढ़ी हुई मांग पैदा हो रही होती है। यह उनकी बचतों तथा संपदा में मुफ्त में हो रही बढ़ोतरी होती है और इसलिए इससे संपदा की असमानता बढ़ जाती है। संपदा की असमानता में ऐसी बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार को, कर लगाने के जरिए उनसे इस 100 रुपये की उगाही कर लेनी चाहिए और अपने इस खर्च की वित्त व्यवस्था, पूंजीपतियों पर उतना ही कर लगाने के जरिए करनी चाहिए, जिस कर के लगाए जाने से तो शुरुआत की स्थिति की तुलना में उनकी संपदा तक में कोई कमी नहीं हो रही होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर पूंजीपतियों पर कर लगाने के जरिए वित्त जुटाकर, राज्य द्वारा खर्चे में बढ़ोतरी की जाती है, तो इससे पूंजीपतियों पर कोई बोझ डाले बिना ही, क्योंकि उनकी संपदा शुरू में जितनी थी उतनी ही बनी रहेगी, रोजगार में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसलिए, अगर शासन रोजगार में बढ़ोतरी करना चाहता है तो, उसे अपने खर्च में बढ़ोतरी करने के साहस का प्रदर्शन करना चाहिए और इसके लिए उसके कदमों के रास्ते में घरेलू तथा विदेशी पूंजीपतियों द्वारा जो भी बाधाएं डाली जाएं, मिसाल के तौर पर शुरूआत में पूंजी पलायन का सामना करना पड़ सकता है, उन सभी बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
इसलिए, रोजगार के विस्तार के सबसे पहले तो इसी की जरूरत होगी कि सरकारी तंत्र में जितनी भी रिक्तियां हैं और इसमें स्कूल से यूनिवर्सिटी स्तर तक शिक्षकों की रिक्तियां और स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिंग स्टाफ की रिक्तियां शामिल हैं, उन्हें भरा जाए। दूसरे, यह जरूरी है कि इन क्षेत्रों में पदों की संख्या बढ़ायी जाए। मिसाल के तौर पर हमारे देश में शिक्षा दयनीय स्तर पर पहुंच गयी है और योग्य स्टॉफ के समुचित विस्तार के जरिए, उसमें नये प्राण फूंकने की जरूरत है। तीसरे, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के दायरे का विस्तार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए, इस योजना पर लगायी गयी सारी बंदिशों को हटाया जाना चाहिए और इसे सार्वभौम तथा मांग संचालित योजना बनाया जाना चाहिए। इस योजना का शहरी क्षेत्रों में भी प्रसार किया जाना चाहिए और इसके तहत मजदूरी समुचित स्तर पर तय की जानी चाहिए। यह मजदूरी, इस समय जो बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही है, उससे काफी ज्यादा होनी चाहिए।
यह अपने आप में ही अर्थव्यवस्था में अनेकानेक मालों की मांग पैदा करेगा और इस मांग की पूर्ति आंशिक रूप से तो मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का ही कहीं ज्यादा उपयोग किए जाने के जरिए तथा इस तरह रोजगार बढ़ाए जाने के जरिए होगी। और आंशिक रूप से इस मांग की भरपाई नयी उत्पादन क्षमताओं की स्थापना के जरिए और खासतौर पर लघु-पैमाने के उत्पादन क्षेत्र के विस्तार के जरिए होगी, जिसके लिए ऋण आदि की समुचित व्यवस्था करनी होगी। दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा रोजगार दिया जाना, जिसे ‘बहुगुणक’ कहते हैं उसके जरिए, निजी क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा।
संपदा और विरासत कराधान ज़रूरी
जैसा कि हम पीछे कह आए हैं, सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चों में इस सारी की सारी बढ़ोतरी के लिए वित्त की व्यवस्था, पूंजीपतियों पर तथा आम तौर पर अमीरों पर करों में बढ़ोतरी के जरिए करनी होगी। इस तरह के कर उनकी आय के प्रवाहों पर लगाए जा सकते हैं या फिर उनकी संपदा पर लगाए जा सकते हैं। बहरहाल, इन दोनों में अमीरों की संपदा पर कर लगाना कहीं बेहतर होगा। इसमें उनकी अचल संपत्तियों पर और नकदी बैलेंसों पर कर लगाना भी शामिल है, जिनसे कोई खास प्रत्यक्ष कमाई हो ही नहीं रही होती है। इसके बेहतर होने की वजह यह है कि ऐसे कराधान के मामले में यह तो कोई कह ही नहीं पाएगा कि इसका उत्पादक निवेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो सकता है। बेशक, किसी भी संपदा कराधान के साथ विरसा कराधान भी चलना चाहिए, ताकि संपदा कराधान से बचने की कोशिशों को विफल किया जा सके।
यह हैरान कर देने वाली बात है कि भारत में करीब-करीब कोई भी संपदा या विरसा कराधान है ही नहीं, जबकि नव-उदारवादी दौर में हमारे देश में संपदा असमानता आकाश छू रही है। बहरहाल, इस दयनीय स्थिति का अर्थ यह भी है कि हमारे देश में संपदा तथा विरासत कर लगाने की भरपूर गुंजाइश है।
संपदा तथा विरासत कराधान के जरिए वित्त जुटाकर, सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चों में बढ़ोतरी करना, अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे प्रत्यक्ष रास्ता है। इसके जरिए एक ही तीर से कई-कई निशाने लगाए जा सकते हैं। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी, संपदा असमानता पर अंकुश लगेगा, जो कि जनतंत्र के लिए आवश्यक है और इससे देश में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा सुधरेगी, जो दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी हैं।
(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
मूलतः अंग्रेज़ी में प्रकाशित लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।