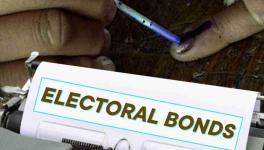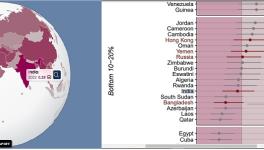सवर्णों के साथ मिलकर मलाई खाने की चाहत बहुजनों की राजनीति को खत्म कर देगी

मई की 2 तारीख को सामाजिक न्याय की दो महत्वपूर्ण पार्टियां उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (सपा) और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने परशुराम जयंती काफी धूमधाम से मनाई। परशुराम की जयंती इतनी धूमधाम से तो उनकी विचारधारा में विश्वास करनेवाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी नहीं मनाई। शायद सपा व राजद नेतृत्व यह मानने लगा है कि परशुराम जयंती मनाने और उनके नाम पर फरसा भांजने व बांटने से सवर्णों खासकर भूमिहारों व ब्राह्मणों का वोट उसे मिलने लगेगा। वोट पाने की लालसा में राजद के घोषित असली वारिस व बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भूमिहारों द्वारा आयोजित परशुराम जयंती पर लालू यादव व राबड़ी देवी के किए ‘कुकृत्यों’ के लिए भूमिहार समाज से माफी भी मांगी। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि ‘हां, हमसे गलती हुई है, लेकिन एक मौका और दीजिए!’
लालू यादव की राजनीति को समझने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनके किए ‘किस अपराध के लिए’ तेजस्वी माफी क्यों मांग रहे हैं? बिहार की राजनीति समझने वाले शायद यह भी जानते हैं कि जिस बात के लिए तेजस्वी सवर्णों, खासकर भूमिहारों से माफी मांग रहे हैं उनकी संख्या बिहार के विभाजन के बाद सवर्णों में सबसे अधिक (लगभग 7 फीसदी) हो गई है। वे शायद यह भी जानते हैं कि इस जाति के पास राज्य के संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा है और भूमिहारों के पक्ष में हो जाने से राजद भले ही ‘ए टू जेड’ की पार्टी न बने लेकिन सत्ता पर काबिज हो सकती है।
अब जातीय गणित को समझने की कोशिश करें। बिहार के विभाजन के बाद वहां यादवों की संख्या 12 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गयी है जबकि मुसलमानों की संख्या 16 फीसदी से अधिक है। मतलब यह कि राजद अभी बिहार में ‘एम वाय’ समीकरण के बहाने तीस फीसदी वोट पर नियंत्रण रखता है। अगर उसमें सात फीसदी वोट और जुड़ जाए तो 37 फीसदी वोट के साथ वह पार्टी अजेय बन जा सकती है! लेकिन सवाल है कि अगर सचमुच भूमिहारों का सात फीसदी वोट राजद के साथ जुड़ जाता है तो बाकी के यादव और मुसलमान वोट उनसे जुड़े रह जाएगा? या फिर वहां कोई अलग समीकरण या हकीकत भी काम कर रही है जो तेजस्वी यादव को इस तरह के गुणा-भाग करने के लिए बाध्य कर रही है?
पिछड़ी जाति की सशक्त राजनीति की शुरुआत 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने के साथ शुरू हुई जिसका परिणाम यह हुआ था कि उस अनुशंसा के लागू होने के पांच महीने के भीतर ही वीपी सिंह को प्रधानमंत्री का पद गंवा देना पड़ा था। उसी मंडल आयोग की रिपोर्ट ने आरएसएस-बीजेपी को लगभग 25 वर्षों तक, जिसमें छह वर्ष तो वाजपेयी सीधे केन्द्रीय सत्ता में थे, अपने एजेंडा को लागू करने से असफल रहा। यह वही दौर था जिसकी वजह से पहली बार ओबीसी के नाम से पिछड़ों की गोलबंदी शुरू हुई, उसी मंडल रिपोर्ट के चलते पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कर दी गयी।
वर्ष 1990 में मंडल लगने से पहले पिछड़ा नेतृत्व का रुतबा बनने लगा था। मंडल लागू होने के बाद सवर्ण सत्ता को पिछड़ों से डर लगने लगा था, लेकिन 32 साल के भीतर पूरा का पूरा पिछड़ा नेतृत्व दीन-हीन अवस्था में पहुंच गया है। सत्ता पर उसकी कोई पकड़ नहीं रह गयी है। भारतीय राजसत्ता ज्यादा सवर्णवादी हो गयी है। सत्तर साल में लड़कर ली गयी हिस्सेदारी धीरे-धीरे छीनी जा रही है लेकिन पिछड़ा नेतृत्व मृतप्राय सा हो गया है। पिछड़े नेतृत्व की एकमात्र कोशिश किसी भी तरह एमपी या एमएलए बन जाने की है न कि अपने समाज के लिए कुछ गुणात्मक कर पाने की है।
दो साल पहले राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों से पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, लेकिन उत्तर भारत के बहुजन नेतृत्व की तरफ से कोई खास पहलकदमी नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए एक चिट्ठी जरूर प्रधानमंत्री को लिखी थी, लेकिन पिछड़ों की पूरी लड़ाई दक्षिण भारत की सामाजिक न्याय की पार्टी डीएमके को लड़नी पड़ी।
उसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कुल 15 फीसदी सवर्णों में से गरीब सवर्णों के लिए केन्द्रीय सेवाओं में 10 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया जिसका समर्थन सपा-बसपा ने जोरदार तरीके से किया। हां, तेजस्वी यादव ने सरकार की इस नीति का जबरदस्त विरोध किया और इस बिल के खिलाफ राज्यसभा में डीएमके के साथ मतदान भी किया। लेकिन जो तेजस्वी यादव सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ अपनी आवाज इतनी जोरदार तरीके से उठा रहे थे, उन्हीं तेजस्वी को एकाएक पितृसत्ता के सबसे बड़े मिथक परशुराम के शरण में क्यों जाना पड़ा?
सवाल है कि जो दलित-बहुजन नेतृत्व लगभग 30-32 वर्षों तक उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करते रहे, एकाएक वह नेतृत्व इतना निष्प्रभावी क्यों हो गया कि अपने समुदाय या सहयोगी के हित की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है? क्या इसके पीछे दलित-बहुजन नेतृत्व का भ्रष्टाचार है या और भी कोई कारण है कि सत्ता से बाहर होने के बाद वह कोई सवाल ही नहीं उठा पाता है? दूसरा सवाल यह है कि वर्तमान राजनीति इतनी सवर्ण केंद्रित हो गयी है कि दलित-पिछड़ा नेतृत्व के लिए सचमुच कोई जगह नहीं रह गयी है कि वे अपने समुदाय के हित की बात कर सकें? मोटे तौर पर इन्हीं दोनों सवालों के बीच दलित-पिछड़ा नेतृत्व की असफलता का जवाब छुपा हुआ है।
जिस मंडल आयोग की रिपोर्ट के बीच पिछड़ा नेतृत्व इतना शक्तिशाली दिखने लगा था, आखिर वह इतनी आसानी से बिखर क्यों गया? इस बिखराव के कारण को समझने के लिए हमें मंडल आयोग की अनुशंसा को देखना पड़ेगा। मंडल आयोग को संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो काम सौंपे गये थे, वे हैं-
1. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की परिभाषा और पहचान के लिए कसौटी तय करना
2. पहचाने गये समूह के विकास के लिए कारगर उपाय सुझाना
3. केंद्र और राज्य की नौकरियों में समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की आवश्यकता की जांच करना और
4. आयोग द्वारा खोजे गये तथ्यों को उचित संस्तुतियों के साथ भारत के राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन सौंपना
बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपी जिसमें उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें की, जैसे-
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं में पिछड़ा वर्ग के 27% सीटें आरक्षित की जाएं
2. जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया जाए
3. सरकार द्वारा अनुबंधित जमीन को न केवल एससी व एसटी को दिया जाए बल्कि उसमें ओबीसी को भी शामिल किया जाए
4. केंद्र और राज्य सरकारों में ओबीसी के हितों की सुरक्षा के लिए अलग मंत्रालय/विभाग बनाये जाएं
5. केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाले वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रोफेशनल तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए, और
6. पिछड़े वर्ग की आबादी वाले क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा केंद्र तथा पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं. पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा भी दी जाए।
बिहार और उत्तर प्रदेश में जब तक लालू, मुलायम, मायावती या अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, नौकरी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। न ही भूमि सुधार की तरफ कदम उठाया गया, न ही दलित-पिछड़े छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल तैयार किया गया, न ही उनके लिए एक भी नया स्कूल-कॉलेज खोला गया। हां, कांशीराम के जिन्दा रहते जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो सांस्कृतिक व सामाजिक रुप से कई बड़े काम हुए। उनके समय में जहां-जहां बसपा की रैलियां होती थीं, वहां ज्योतिबा फुले, पेरियार आदि की किताबें बेची जाने लगी, लोग साबित्री बाई फुले को जानने लगे, साहुजी महाराज के नाम पर विश्वविद्यालय खोले गए। मतलब अगर कुछ काम हुए तो वे सारे काम मायावती के पहले कार्यकाल में ही हुए।
कमोबेश सामाजिक चेतना जगाने के लिए थोड़े बहुत काम लालू यादव के पहले कार्यकाल (1990-95) के बीच हुए। लेकिन उसके बाद नये स्कूल-कॉलेज खोलने की बात तो छोड़िए, जो सरकारी स्कूल-कॉलेज पहले थे भी उसकी सबसे ज्यादा बर्बादी इन्हीं सामाजिक न्यायवादियों के सत्ता में रहने के दौरान हुई। पहले हर जिले में हरिजन छात्रावास हुआ करता था, जिसमें प्रतिभाशाली दलित रहकर अध्ययन करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले ये छात्रावास बहुत आबाद थे लेकिन बिहार में लालू-राबड़ी के शासनकाल में भी उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के समय तो वे छात्रावास पूरी तरह बर्बाद ही हो गये। शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह निजी हाथों में दे दिया गया जबकि दलित-पिछड़ा नेतृत्व को उसे न सिर्फ बचाना चाहिए था बल्कि बेहतरी की दिशा के काम करना था। ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ।
मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू होने के 32 वर्षों के बाद भी सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों ने सत्ता के वैकल्पिक मॉडल की बात ही नहीं सोची। उन्हें आज भी यही लगता है कि सत्ता मिलते ही सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है जबकि हकीकत यह है कि कुर्सी सत्ता तंत्र का एक पुर्जा मात्र है जिसमें अन्य कई पुर्जें लगे होते हैं। अपने सत्ता काल में इन ताकतों ने वैकल्पिक मीडिया बनाने की बात नहीं सोची। लालू, मुलायम, मायावती और हेमन्त सोरेन जैसे नेताओं के पास अपनी पार्टी का एक रेगुलर मुखपत्र तक नहीं है जिसके द्वारा वे अपने समर्थकों से संवाद स्थापित कर सकें।
सामाजिक न्याय चाहने वाली ताकतों की समस्या यह भी है कि वे अपना सारा काम उन्हीं यथास्थितिवादियों के सहारे करना चाहती हैं जो उन्हें नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। यही कारण है कि ब्राह्मणवादी ताकतों को लगभग पच्चीस वर्षों तक सत्ता में रोके रहने के बाद आज वे पूरी तरह दिशाहीन हो गये हैं जबकि जो ताकत हाशिये पर पहुंच गयी थी वह फिर से सबसे ताकतवर दिखायी दे रही है। चूंकि तथाकथित सामाजिक न्याय की ताकतों ने पिछले 32 वर्षों में न जमीन पर कोई आंदोलन खड़ा किया और न ही बहुजन जनता के किसी बड़ी समस्या से जुड़ा, इसलिए उन्हें लगता है कि सवर्णों की गुलामी स्वीकार करके ही फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन पांच-सात फीसदी सवर्णों के लिए अपना सबकुछ दांव पर लगा रहा है, वही नेतृत्व 18-19 फीसदी मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा या गैरबराबरी पर चुप्पी साधे हुए है।
वैसे यह तो तय है कि सवर्ण उसके साथ नहीं ही आएगें, लेकिन मुसलमान उन्हें छोड़कर निकल जाएं तो राजनैतिक रुप से उनकी कितनी हैसियत रह जाएगी? आज भी इन ताकतों के पास यह अवसर है कि अपनी गलती पर विचार करें और एक नयी बौद्धिक चुनौती खड़ी करें!
दलित-बहुजन नेतृत्व को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उसने समाज से जितना लिया उसके बदले में उसने समाज को वापस कितना किया? भाई-भतीजावाद और परिवारवाद तो जो किया उसके लिए तो तब भी उसे माफी दी जा सकती है, लेकिन जिस तरह दलित व बहुजन समाज को सामाजिक रुप से सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले समुदाय के साथ फिर से सिर्फ सत्ता के लिए चरण वंदना कर रहा है उससे बहुजन समाज को और ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि वह समाज बहुजनों का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है बल्कि बहुजनों के हित के खिलाफ हमेशा से खड़ा रहा है।
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।