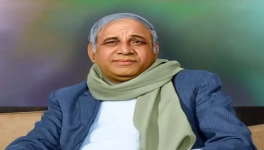बसपा के बहुजन आंदोलन के हाशिये पर पहुंचने के मायने?

कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन राजनीति के लिए जो वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जमीन तैयार की जाती है वह संभावनाओं का खेल नहीं होती बल्कि उसे एक स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य और मजबूत रणनीति के साथ तैयार किया जाता है। और जब यह वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जमीन कमजोर पड़ने लगती है तो उस पर खड़ी राजनीति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बसपा की राजनीति को देखा जा सकता है। कांशीराम के बहुजन आंदोलन ने दलित-बहुजन समाज के लिए 1980 के दशक में उम्मीदों की जो नई खिड़की खोली थी, वह 2022 तक आते-आते बंद-सी होती दिख रही है।
आकांक्षाओं का आसमान और निराशा का घटाटोप
कांशीराम ने हिंदी पट्टी, खासकर उत्तर प्रदेश, में बहुजन आंदोलन के जरिये एक बड़े सामाजिक-राजनीतिक बदलाव की जमीन तैयार की। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदाय को लेकर एक व्यापक गठबंधन की परिकल्पना की और उसे मूर्तरूप देने के लिए 1984 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बनाई। बहुजन समाज के लोगों को जागरुक और शिक्षित करने के लिए आंबेडकर मेलों का आयोजन करना, गीत और नाटकों के मंचन के जरिये जन-चेतना का प्रसार करना, साइकिलों पर सवार जागृति जत्थों की यात्रा निकालना, गांव-गांव में दलित बस्तियों में छोटी-छोटी बैठकें करना – ये सब उस राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का हिस्सा थे जिसे कांशीराम ने शुरू किया था। हालांकि बसपा के निर्माण के पहले से ही कांशीराम डीएस-4 (दलित शोषित समाज संघर्ष समिति) और बामसेफ (ऑल इंडिया बैक्वर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटिज एम्प्लॉइज फेडरेशन) के जरिये बहुजन आंदोलन की एक मजबूत नींव रखने का काम कर रहे थे।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुजन आंदोलन की उस यात्रा में कांशीराम के साथ एक मजबूत राजनीतिक सहयोगी के रूप में मायावती ने कड़ी मेहनत से बसपा के लिए जमीन तैयार की। जब वह साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव घूम रही थीं और कांशीराम के बहुजन आंदोलन का संदेश फैला रही थीं, तो वह बहुजन समाज के भीतर एक नई उम्मीद भी जगा रही थीं। जब वह किसी गांव में पहुंचतीं और पूछती की कि क्या आप इस गांव में या आसपास के गांवों में एक भी दलित परिवार का नाम बता सकते हैं जो बीते चालीस वर्षों में कांग्रेस सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समृद्ध हुआ है, और आमतौर पर इसका उत्तर नहीं में ही होता था। तो वह पूछतीं कि फिर दलितों का 95 प्रतिशत वोट कांग्रेस को क्यों जाता है। (इस वाकये का जिक्र पैट्रिक फ्रेंच ने अपनी किताब ‘इंडिया : अ प्रोट्रेट’ में विस्तार से किया है)। लेकिन अजीब बिडंबना है कि आज आरएसएस के ‘हिंदू राष्ट्र’ और ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ के दो बड़े ध्वजवाहकों नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से वह यह नहीं पूछतीं कि आपके राज में दलितों में जुल्म क्यों बढ़ रहे हैं।
एक दौर में यह मायावती के ही शब्द थे – किसी के सामने एक दलित का सिर झुके, मैं यह नहीं होने दूंगी। सन् 1989 में जब वह पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची, तो उन्होंने संसद में दलितों की आवाज को मुखर किया। उस समय आगरा में दलित महिलाओं के साथ हुई बलात्कार की एक घटना पर उन्होंने लोकसभा में जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन सन 2020 में जब हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ तो वह एक-दो औपचारिक बयान देने के अलावा खामोश ही रहीं और पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गईं। उनकी उस चुप्पी से बसपा की राजनीतिक यात्रा में किस तरह के बदलाव आए हैं और आज वह किस मोड़ पर है, उसे आसानी से समझा जा सकता है। कहा जाता है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता में आई कमी का कारण उन पर लगे भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। क्या सिर्फ यही कारण है या फिर बहुजन आंदोलन के कमजोर पड़ने के और भी कारण हैं?
बसपा के शुरुआती नारों – ‘वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा’; ‘वोट से लेंगे पीएम/सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी/डीएम’; ‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’; ‘ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़, बाकी सब हैं डीएस-4’ ने बहुजनों के बीच बसपा की राजनीति के प्रति नया आकर्षण पैदा किया था। जैसे-जैसे बसपा की राजनीतिक यात्रा बढ़ती गई, तो राजनीतिक समीकरणों के साथ-साथ नारे भी बदलते गए। जैसे- ‘बनिया माफ, ठाकुर हाफ, ब्राह्मिन साफ’। ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा-विष्णु-महेश’ है। फिर, ‘ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा’। लेकिन आज न तो ब्राह्मण बसपा के लिए शंख बजा रहा है और न ही हाथी में दिल्ली तो क्या लखनऊ जाने की ही ताकत दिख रही है। सच तो यह है कि जिस बहुजन आंदोलन और उसकी राजनीति का कांशीराम ने सपना देखा और उसे हकीकत में बदला था, वह आज गहरी निराशा और बिखराव के रास्ते पर है।
कमज़ोर पड़ती राजनीतिक ज़मीन
बसपा का राजनीतिक-सामाजिक आधार सिकुड़ रहा है। बसपा ने उत्तर प्रदेश में 2007 में अपने दम पर सरकार बनाई और मायावती चौथी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनीं। बसपा ने उस चुनाव में 403 में 206 सीटें जीतीं और 30.43 प्रतिशत वोट हासिल किए। 2012 के विधानसभा चुनाव में वह 80 सीटों पर आ गई और उसका वोट प्रतिशत गिरगर 25.91 हो गया। सन् 2017 में उसे मात्र 19 सीटें मिलीं और वोट प्रतिशत गिरकर 22.2 प्रतिशत हो गया।
एक हालिया सर्वे बताता है कि बसपा का वोट प्रतिशत इस समय 15 फीसद के आसपास रह गया है। वर्तमान में बसपा नेतृत्व की स्थिति और उपरोक्त आंकड़े साफ इंगित करते हैं कि बसपा का राजनीतिक-सामाजिक आधार तेजी से खिसक रहा है। उसके बहुजन आधार का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया है। भाजपा की पूरी नजर इस समय दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने पर है। वहीं, समाजवादी पार्टी पिछड़ी जातियों के साथ-साथ अति पिछड़ी जातियों के बीच अपना एक नया राजनीतिक आधार मजबूत करती हुई दिख रही है।
नेतृत्व पर सवाल!
कांशीराम ने दलित जातियों, अति पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों का एक सफल बहुजन गठबंधन बनाया था। उसमें मुस्लिम भी शामिल थे। लेकिन बाद के दौर में अति पिछड़ी जातियों और कुछ पिछड़ी जातियों के ताकतवर नेता जो बहुजन आंदोलन का हिस्सा थे बाद में उसे छोड़ गए।
मायवाती के नेतृत्व में बसपा बहुजन जातियों के बीच संतुलन और उन्हें एक साथ जोड़े रखने में असफल रहीं। बसपा धीरे-धीरे दलितों में एक जाति विशेष यानी जाटवों की पार्टी बनकर रह गई। मायावती ने बसपा में दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं की जमीन तैयार ही नहीं की।
आज कांशीराम का शुरू किया दलित-बहुजन आंदोलन एक व्यक्ति केंद्रित, एक परिवार केंद्रित और दलितों में भी सिर्फ एक जाति विशेष तक केंद्रित होकर रह गया है। मायावती अगर कहती हैं कि उनकी पार्टी पूंजीपतियों और धन्नासेठों की पार्टी नहीं है, तो आज चुनाव जिस हद तक बड़ी पूंजी का खेल हो गया है उसमें उनकी यह बात समझ में आती है, लेकिन बसपा का सामाजिक आधार कभी बड़ी पूंजी और मीडिया के सहारे नहीं बढ़ा है, तो यह बात भी समझनी होगी। बहुजन समाज के सशक्तीकरण के मुद्दे क्या बसपा के राजनीतिक एजेंडे में आज उतनी ही मुखरता और मजबूती से दिखाई देते हैं जिस तरह एक वक्त में हुआ करते थे? दलित बस्तियों में छोटी-छोटी बैठकों का बसपा का जो परंपरागत तरीका था, क्या आज वह उसी मजबूती के साथ दिखाई देता है? क्या पार्टी वंचित समाज तक पहुंच रही है?
सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की कमी
कांशीराम ने आंबेडकर मेलों, जन जागृति जत्थों, गीतों और नाटकों के जरिये बहुजनों के बीच सांस्कृतिक चेतना निर्मित की थी, लेकिन उस तरह की सांस्कृतिक चेतना के निर्माण के कार्यक्रम क्या आज दिखाई देते हैं? क्या बहुजन कर्मचारियों का एक सशक्त संगठन वर्तमान बसपा नेतृत्व की प्राथमिकता में है?
दलित-बहुजन आंदोलन की विरासत को लेकर चलने वाली बसपा ने क्या कभी खेत मजदूरों (जिसमें अधिकांश दलित समुदाय से आते हैं) का कोई सशक्त और व्यापक संगठन खड़ा किया? क्या दलित महिलाओं का संगठन बनाया? क्या दलित बुद्धिजीवियों और लेखकों का उसने कोई सांस्कृतिक और वैचारिक संगठन खड़ा किया है? बहुजन समाज के छात्रों का एक मजबूत संगठन भी बसपा के एजेंडे में दिखाई नहीं देता है।
महत्वपूर्ण यह भी है कि बामसेफ का क्या हुआ? कांशीराम जब तक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे तब तक बामसेफ की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। बामसेफ बहुजनों के पढ़े-लिखे तबकों से न केवल बहुजन राजनीति को जोड़ता था, बल्कि उसकी वैचारिकी का भी एक अहम हिस्सा था। अपनी तरह से वह बहुजन राजनीति के लिए ओपनियन मेकर का काम भी करता था। नैरेटिव बनाने में उसकी भी अपनी एक भूमिका होती थी। लेकिन मायवती के दौर में बामसेफ पूरी तरह से नेपथ्य में चला गया।
कांशीराम ने जब हिंदी पट्टी में बहुजन आंदोलन को साकार किया तो वह कोई सामान्य राजनीतिक परिघटना नहीं थी। हालांकि उत्तर भारत में दलित आंदोलन की जमीन 1920 के दशक में तैयार होने शुरू हो गई थी। उसका श्रेय स्वामी अछूतानंद और उनके आदि हिंदू आंदोलन को जाता है। उस आंदोलन ने शुरुआती तौर पर एक सांस्कृतिक और वैचारिक जमीन तैयार करने का काम किया था। उसके बाद बाबा साहेब डॉ. बी.आर आंबेडकर के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने हिंदी पट्टी में कुछ काम किया, लेकिन उसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। लेकिन कांशीराम का बहुजन आंदोलन, जिसे एक ‘खामोश क्रांति’ कहा गया, उसने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक व्यापक असर पैदा किया। लेकिन आज उस ‘खामोश क्रांति’ का वास्तव में खामोशी में तब्दील होते जाना एक असामान्य परिघटना जरूर लगती है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।