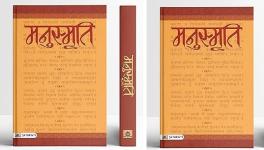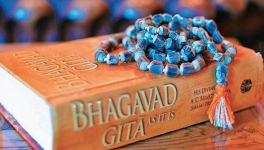इतना अहम क्यों हो गया है भारत में सार्वजनिक शिक्षा के लिए बजट 2021?

भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6% शिक्षा पर खर्च करने की आवश्यकता है, वर्ष 1968 और उसके बाद की हर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह अनुशंसा की गई है, लेकिन वर्ष 2019-20 आर्थिक सर्वेक्षण एक दूसरी कहानी बयां करता है, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के 52 वर्ष बाद भी देश में सार्वजनिक शिक्षा पर महज 3.1% खर्च किया जा रहा है।
दूसरी तरफ, यदि भारत की सार्वजनिक शिक्षा पर प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 6% भी खर्च किया जाता रहता तो इन गए पांच दशकों में स्थिति बेहतर होती और करीब 10 लाख से अधिक उन सरकारी स्कूलों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता, जहां भारत के लगभग 24.8 करोड़ बच्चों में से आधे से कुछ अधिक यानी 52% बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में वित्तीय स्थिति के कारण सीखने के परिणाम कहीं सुखद होते।
सार्वजनिक शिक्षा पर बजट के बारे में बात करने से पहले हमें इसकी एक बुनियादी बात भी रेखांकित करनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों में धन कैसे आवंटित और खर्च किया जाता है। वहीं, इस क्षेत्र में प्रभावी वित्तपोषण के लिए और क्या करने की आवश्यकता है।
दरअसल, शिक्षा बजट को स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच विभाजित किया जाता है, जबकि विशेषज्ञ प्रारंभिक बचपन और स्कूली शिक्षा पर अलग से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताते रहे हैं, क्योंकि बुनियादी शिक्षा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।
केंद्र की होती है बड़ी भूमिका
भारत में जहां तक स्कूली शिक्षा की बात करें तो ज्यादातर धन दस लाख सरकारी स्कूलों पर खर्च होता है, जबकि एक छोटा हिस्सा सरकारी सहायता से संचालित स्कूलों में होता है, जिनकी संख्या 84 हजार से ज्यादा है। भारत में करीब साढ़े तीन लाख निजी स्कूल हैं, जिन्हें सीधे तौर पर सरकारी धन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' लागू होने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों पर पढ़ने वाले कमजोर परिवार के बच्चों के लिए सरकार पैसा देती है।
ये भी पढ़ें: शिक्षा में असमानता को दूर करने का चीनी जतन
केंद्र सरकार शिक्षा में दो तरह से योगदान करती है: एक तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से और दूसरा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से। पहली श्रेणी में समग्र शिक्षा अभियान, स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र सरकार का कार्यक्रम जैसी योजनाएं शामिल होती हैं, जिन्हें ज्यादातर केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% धन केंद्र सरकार से आता है।
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय स्कूल नेटवर्क, और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार पाठ्यपुस्तक और शिक्षक प्रशिक्षण के डिजाइन तथा प्रकाशन के लिए जवाबदेह सरकारी निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को भी धन देती है।
केंद्रीय बजट का विश्लेषण जरूरी
यहां पर केंद्रीय बजट का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है कि केंद्र सरकार पाठ्यपुस्तक और शिक्षक प्रशिक्षण के डिजाइन तथा प्रकाशन से जुड़ी गतिविधियों पर अपने बजट का एक बड़ा भाग खर्च कर देती है, जबकि सुदूर गांवों में संचालित सरकारी स्कूलों के लिए अधिकांश धन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता रहा है। इसके अलावा, केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण और मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों में आंशिक योगदान करता है।
दूसरी तरफ, राज्य सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च करते रहे हैं. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र जैसा राज्य अपनी स्कूली शिक्षा पर राज्य के बजट का 7 से 10% हिस्सा खुद खर्च करता है। दूसरी तरफ, आर्थिक तौर पर पिछड़े राज्यों जैसे बिहार को केंद्र से स्कूली शिक्षा पर वित्तीय सहायता हासिल हो जाती है। वहीं, कई राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अलग अपनी योजनाएं संचालित करते हैं, जो सामान्यत: मिडिल स्कूलों में लड़कियों या आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन पर आधारित होती हैं।
लेकिन, भारत के छह अति महत्त्वपूर्ण राज्यों की ओर नजर दौड़ाएं तो चिंता की बात यह है कि यहां सरकारी स्कूलों पर होने वाले खर्च में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यह राज्य हैं: केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश।
सरकार ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाया
हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि गत पांच-छह वर्षों में सरकार द्वारा शिक्षा पर खर्च बढ़ाया है, वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% हिस्सा शिक्षा पर खर्च हुआ था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3.1% हो गया है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत ने शिक्षा के लिए 6.43 लाख करोड़ रुपए यानी 88 बिलियन डॉलर का सार्वजनिक धन आवंटित किया है। इसमें से केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 56,537 करोड़ रुपए यानी 7.74 अरब डॉलर और उच्च शिक्षा के लिए 38,317 करोड़ रुपए यानी 5.25 अरब डॉलर आवंटित किए।
फिर क्यों महत्त्वपूर्ण इस साल का बजट
बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भारत में 24 मार्च, 2020 से लगभग सभी स्कूल बंद रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा केवल कुछ छात्रों तक ही पहुंच पाई है। सरकार ने इस वर्ष 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को चरणबद्ध रूप से फिर से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन यह भी सच है कि अधिकांश राज्यों ने केवल कक्षा 9 और उच्चतर के लिए कक्षाएं शुरू की हैं।
दूसरी तरफ, यदि लंबे समय बाद प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूल फिर से खुल रहे हैं और सरकार वर्ष 2020 की नई शिक्षा नीति को भी लागू करने की कोशिश करती है तो इन दो स्थितियों के कारण इस वर्ष का बजट अहम हो जाता है। तब सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को देखते हुए इस बार के बजट में शिक्षा पर होने वाले खर्च पर बढ़ोतरी करे। कई विशेषज्ञों की भी यही राय है कि भारत को इस वर्ष शिक्षा पर अधिक खर्च करना होगा और इसी के साथ बदली हुई परिस्थितियों में यह योजना बनाने की भी जरूरत है कि वह शिक्षा पर आवंटित धन को खर्च करती है तो किस प्रकार से।
उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी स्कूलों को डिजिटल लर्निंग को शामिल करना पड़ा है, यह एक नई चुनौती है, क्योंकि 2018-19 में केवल 28% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर थे और केवल 12% के पास इंटरनेट कनेक्शन था।
इसके अलावा, कई कारणों से यह अपेक्षा भी जताई जा रही है कि अपने यहां सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। जाहिर है कि इससे सार्वजनिक शिक्षा पर निवेश बढ़ाना जरूरी हो जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने के लिए
इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों पर जोर देती है। इस बार की शिक्षा नीति प्रारंभिक वर्षों में आधारभूत संख्यात्मकता और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार, रटने से दूर और एक नई मूल्यांकन प्रणाली जो याद रखने के बजाय कौशल और सीखने को मापने पर आधारित है।
जाहिर है कि इसके लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होगी, लेकिन इस बारे में जानकारों का कहना है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि पैसा कहां से आएगा। हालांकि, इस वर्ष जो धन शिक्षा पर खर्च नहीं हो सका है, उसे फिर से आवंटित किया जाना चाहिए और अधिक कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए।
शिक्षा खर्च के अन्य प्रमुख घटकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पात्रताएं शामिल हैं, जैसे यूनीफार्म और पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन, निर्माण और रखरखाव आदि। इसके अलावा, अभी तक राज्यों के पास रिक्त पदों को भरने और स्थायी शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए धन नहीं है। वहीं, शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है, जो कक्षा शिक्षण को बेहतर बनाने और सीखने को प्रभावित करने में मदद कर सकता है, जबकि भारत में लंबे समय से सीखने के परिणामों को सुखद बनाने की मांग की जाती रही है।
(शिरीष खरे पुणे स्थित स्वतंत्र पत्रकार और लेखक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।