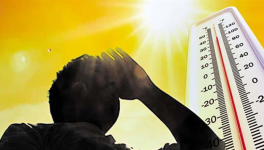अमीर देशों का दोहरा व्यवहार : ग्रीन एनर्जी के स्टोरेज को कर रहे नज़रअंदाज़

असली मुद्दा यह है कि गैर-जीवाष्म ईंधन के रास्ते पर या कम जीवाष्म ईंधन के रास्ते पर भी बढ़ने के लिए ग्रिड स्तर के ऊर्जा संचयन या भंडारण की लागत, फिलहाल जिस स्तर पर है उससे, दसवें हिस्से के स्तर तक कैसे कम हो? अगर ऐसा नहीं होता है, तो ग्रिड से ऊर्जा आपूर्ति अनिश्चित हो जाएगी और इसकी जनता तथा अर्थव्यवस्था को बेहिसाब कीमत चुकानी पड़ेगी।
महत्वपूर्ण हुआ प्राकृतिक ऊर्जा संचयन का मुद्दा
पहले हमें इसकी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी कि हरित ऊर्जा के साथ, उसके संचयन की समस्या लगी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति में होने वाले उतार-चढ़ावों की भरपाई आसानी से, उसी ग्रिड के साथ जुड़े कोयले या गैस से चलने वाले बिजलीघरों के सहारे की जा सकती थी। वास्तव में नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति से जुड़े उतार-चढ़ाव तब तक खास समस्या नहीं करते हैं, जब तक ऊर्जा के यही स्रोत ग्रिड के लिए आपूर्ति का मुख्य स्रोत नहीं बन जाते हैं। लेकिन, जैसे ही अक्षय ऊर्जा स्रोत, ग्रिड के लिए आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं, संंबंधित ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति की सुनिश्चितता ही, ग्रिड स्तर की ऊर्जा संचयन बैटरियों पर निर्भर हो जाती है।
और ये आपूर्तियां कितनी परिवर्तनीय होती हैं। जर्मनी में 2019 में पवन ऊर्जा से जहां एक दिन उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 59 फीसद आ रहा था, तो किसी और दिन बहुत ही कम, 2.6 फीसद हिस्सा ही हासिल हो रहा था। उसी वर्ष में सौर ऊर्जा का अधिकतम योगदान, कुल ऊर्जा आवश्यकता के 35 फीसद के बराबर था और न्यूनतम योगदान, 0.3 फीसद के बराबर। लेकिन, जब सौर तथा पवन ऊर्जा का अदल-बदल कर सहारा लिए जाने की गुंजाइश ही नहीं हो तो तब क्या होगा? ऐसे हालात का सामना करने के लिए, ग्रिड से आपूर्ति को भरोसेमंद बनाए रखने के लिए, आज के हालात में जब हमें जीवाष्म ईंधन का सहारा लेने की सुविधा हासिल, हम जितनी बड़ी ऊर्जा संचय बैटरियों की तैयारियां कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी संचय बैटरियों की जरूरत होगी।
हालांकि, बहुतों को ऐसा लग सकता है कि अक्षय ऊर्जा के दो अलग-अलग स्रोतों का उपयोग कर, दोनों की सापेक्ष अस्थिरता से निपटा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। अगर हवा के शांत रहने का लंबा वक्फा सामने हो, जो आमतौर पर कई-कई दिनों तक चल सकता है, तो रात के समय तो दोनों ही स्रोतों से ऊर्जा अनुपलब्ध होगी। ज्यादा ऊंचाई की जगहों पर यह समस्या और भी ज्यादा होगी क्योंकि वहां दिन अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं।
विकसित ताकतों का दोहरा रवैया
इस सब को देखते हुए, हम या तो अभी से अक्षय ऊर्जा पर आधारित भरोसेमंद ग्रिड निर्मित करने के लिए पैसा खर्च करने का रास्ता अपना सकते हैं या फिर जो भी कमी-बेशी रहे उसकी पूर्ति करने के लिए, जब तक बन पड़े जीवष्म ईंधन का इस्तेमाल करते रह सकते हैं और ऊर्जा संक्रमण को टालते जा सकते हैं। बहरहाल, यह स्वांग कि हम तो सिर्फ कोयले से चलने वालेे बिजलीघरों को ही जीवाष्म ईंधन से चलने वाला मानेंगे और प्राकृतिक गैस को संक्रमणशील ईंधन मानेंगे, ग्रिड स्तर के ऊर्जा संचयन के लिए अमीर देशों द्वारा जो निवेश किए जाने हैं, उन्हें टालने का ही मामला समझा जाना चाहिए।
यह दलील कि बड़े उत्सर्जनकर्ताओं को अपने उत्सर्जनों में कटौती करनी चाहिए, वास्तव में ऊर्जा संक्रमण का बोझ भारत और चीन के सिर पर ही डालने की कोशिश है, जबकि ये दो ऐसे देश हैं, जिनमें सबसे बड़ी आबादियां रहती हैं और जिनके पास प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बहुत ही कम है। इसीलिए, यह स्वांग किया जा रहा है कि सिर्र्फ कोयला ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है और इसे मानने से ही इंकार किया जा रहा है कि प्राकृतिक गैस, जिसका बुनियादी ढांचा ही काफी रिसाव की इजाजत देता है, विश्व ताप बढ़ाने में उतना ही दोषी है, जितना कि कोयला है।
इसी स्तंभ में मैंने पहले भी लिखा था कि प्राकृतिक गैस नाम का यह जो तथाकथित संक्रमणकालीन ईंधन है, उसका वास्तव में विश्व ताप वृद्घि में योगदान, अमीर देश जितने का दावा करते हैं, उससे कहीं बहुत ज्यादा है। न्यू मैक्सिको में, मीथेन गैस के रिसाव के वास्तविक माप पर आधारित ताजा अध्ययन यह दिखाते हैं कि वास्तव में यह रिसाव, जितने का दावा किया जा रहा था, उससे छ: गुना ज्यादा था। यह कोयले को हटाकर, गैस को ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप मेें इस्तेमाल करने के सारे लाभ को ही मिटा देता है। वैसे भी अमरीका तथा योरप में कोयले से हटकर गैस की ओर संक्रमण का ज्यादा संबंध, उनके कोयले से चलने वाले बिजलीघरों के ज्यादा पुराने पड़ जाने से है। कोयला चालित बिजलीघरों का जीवन काल 25 वर्ष माना जाता है, लेकिन अमरीका में ऐसे बिजलीघर औसतन 40 साल से ज्यादा पुराने हैं और योरप में 35 साल। दूसरे शब्दों में वे ऐसे कोयला चालित बिजलीघरों को बंद कर के उसके लिए पीठ ठोके जाने की मांग कर रहे हैं, जो पहले ही इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्हें चालू रख पाना ही मुश्किल है।
इस तरह, ईमानदारी से इस पर विचार करने के बजाए कि कैसे जल्दी से जल्दी कम कार्बन उत्सर्जन के यात्रा पथ पर पहुंचा जा सकता है, धनी देशों की राजनीति यही सुनिश्चित करने की है कि प्राकृतिक गैस के एक ‘संक्रमणशील’ ईंधन होने के नाम पर, हरित ऊर्जा की ओर अपने संक्रमण को ‘हम’ कैसे टाल दें और कैसे ऊर्जा संक्रमण की समस्या को गरीब देशों की सिर पर डाल दें। इसके बाद धनी देश, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उसके संचयन के लिए बैटरियां भी बेचने के जरिए, इस संक्रमण में से भी अपने मुनाफे बटोर सकेंगे। इस मामले में सबसे पाखंडी रुख है, नॉर्डिक देशों का। उनकी दलील है कि वे अफ्रीकी देशों में गैस तथा तेल क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि इससे उत्पादित पूरे के पूरे तेल तथा गैस का वापस उनके लिए ही निर्यात कर दिया जाए। जहां तक अफ्रीकी देशों की अपनी ऊर्जा जरूरतों का सवाल है, उनकी पूर्ति तो सिर्फ और सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में इसकी चर्चा की गयी है, जिसका शीर्षक है-- (यूरोप टु अफ्रीका: गैस फॉर मी बट नॉट फार दी)।
प्राकृतिक ऊर्जा संचयन और जल विद्युत
यह एक जानी-मानी बात है कि नवीकरणीय ऊर्जा के साथ, उसके संचयन या भंडारण की समस्या लगी हुई है। अगर हम कोयले, गैस तथा तेल स्रोतों को कभी खत्म नहीं होने वाला मानें तो, जीवाष्म ईंधन ऊर्जा के भंडार भी होते हैं और स्रोत भी। पर वे असीमित तो हैं नहीं, फिर भी हम यह मानकर चलते आ रहे थे कि उनके सीमित होने की समस्या का सामना तो आने वाली पीढिय़ों को ही करना है, हमें नहीं। लेकिन, जब विश्व ताप वृद्घि की समस्या को भविष्य की समस्या मानकर उससे निपटने के सवालों को टाला जा रहा था, तब तक बढ़ते सूखे, गर्मी और बढ़ते पैमाने पर जलवायु की अति के प्रकरणों ने, हमें अच्छी तरह से बता दिया कि समस्या भविष्य की नहीं है बल्कि सिर पर आकर पड़ गयी है। इसका अर्थ यह है कि हमें ऐसे ग्रिड खड़े करने की तैयारी करनी होगी, जो कहीं ज्यादा मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हों और ऐसे ग्रिडों को जल्द से जल्द स्थापित करना होगा। और इसके लिए हमें ऊर्जा के ग्रिड स्तर के संचयन की समस्या को हल करना होगा।
किसी ग्रिड के लिए ऊर्जा संचयन का सबसे सरल तरीका तो यह है कि वर्तमान जल-विद्युत संयंत्रों को पूरी तरह से वायु तथा सौर ऊर्जा के पूरकों के तौर पर ही चलाए जाने वाले संयंत्रों में बदल दिया जाए। इसके लिए, इन संंयंत्रों को पम्प्ड अप भंडारण के साधनों में तब्दील करना होगा, जिनके जल भंडार में से निकासी सिर्फ तभी की जाए, जब उनमें पानी का भंडारण के उनके वर्तमान स्तर से ऊपर निकलने लगे, जैसाकि अक्सर बारिश के मौसम में होता है। इस तरह के बदलाव की लागत अपेक्षाकृत थोड़ी ही होगी क्योंकि जल टर्बाइनों में तब्दीली की लागत बहुत ज्यादा नहीं होगी। जल विद्युत परियोजनाओं के भंडारण ताल पहले से ही मौजूद हैं और अगर जरूरी हो तो निचले स्तर पर एक छोटा जलाशय और जोड़ा जा सकता है, जिस पर कोई खास लागत नहीं आएगी और भूमि अधिग्रहण के पहलू से जिसका करीब-करीब कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की परियोजनाओं में बड़े जल भंडार ताल पहले ही मौजूद हैं। ऐसे अनेक जल विद्युत संंयंत्र, जिनमें सीधे और उल्टे, दोनों ओर जल सकने वाले जल टर्बाइन होते हैं, यही करते हैं। जल विद्युत के साथ, भूमि के अधिग्रहण तथा लोगों के विस्थापन की जो बड़ी समस्या रहती है, वह तो इस मामले में होगी ही नहीं क्योंकि इसके लिए कोई नयी जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान परिदृश्य में अधिकतम मांग के स्तर पर, आपूर्ति में रह जाने वाली कमी की भरपाई के लिए या पम्प्ड अप भंडारण के साधन के रूप को छोडक़र, और किसी भी रूप में जल विद्युत का प्रयोग करना तो शुद्घ बर्बादी है।
परिवहन के लिए ऊर्जा के उपभोग में बदलाव
दूसरे, इसकी छानबीन करने की जरूरत है कि आज ऊर्जा का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और इस मामले में क्या किया जा सकता है? दुनिया के ऊर्जा कुल उपभोग का 25-30 फीसद हिस्सा परिवहन के क्षेत्र में ही खत रहा है। बिजली से चलने वाले वाहनों की ओर संक्रमण का विचार, इस तथ्य को छुपा लेता है कि बैटरी तो सिर्फ बिजली के भंडारण का काम करती है और उसे ग्रिड की बिजली से ही बार-बार चार्ज करना होता है। चूंकि बिजली की वाहनों की बैटरियां ग्रिड की बिजली से चार्ज की जाती हैं, उनसे ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में कोई कमी नहीं होती है। वे तो सिर्फ उत्सर्जनों की समस्या को, परिवहन से हटाकर ग्रिड पर डालने का ही काम करती हैं। यह हमें फिर ग्रिड के स्तर पर बिजली के संचयन के मुद्दे पर ले आता है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में असली मुद्दा है।
क्या परिवहन क्षेत्र में ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने का भी कोई तरीका है? बेशक है, बशर्ते हम यात्रा के समय के जस का तस बने रहते हुए, प्रतिव्यक्ति किलोमीटर (या माल ढुलाई के मामले में प्रति टन किलोमीटर) परिवहन उत्सर्जन को घटाने का लक्ष्य लेकर चलें। इस मामले में प्रति किलोमीटर उत्सर्जन ही एकमात्र संकेतक है, जिससे फर्क पड़ता है। यह वर्तमान प्रौद्योगिकी से ही किया जा सकता है और परिवहन क्षेत्र की मामूली सी जानकारी रखने वाले भी इस संबंध में बखूबी जानते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, निजी परिवहन साधनों की जगह पर, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाया जाए, जैसाकि चीन कर रहा है। सार्वजनिक परिवहन साधनों--बसों, मैट्रो, रेल आदि--का कार्बन उत्सर्जन प्रभाव, निजी कारों के मुकाबले कहीं कम होता है और इस बदलाव के लिए किसी नयी प्रौद्योगिकी की जरूरत भी नहीं है।
तब इस सामाधान को लागू क्यों नहीं किया जाता है? ऐसा न होने के पीछे आटोमोबाइल उद्योग की राजनीतिक ताकत है, जिसके पीछे जीवाष्म ईंधन लॉबी की ताकत भी जुड़ी हुई है और यही इस समाधान का रास्ता रोकता है। वही ऑटोमोबाइल उद्योग अब हमें निजी पैट्रोल चालित वाहनों की जगह, निजी बिजली चालित वाहन बेचना चाहता है। हमें जरूरत है, प्रति किलोमीटर उत्सर्जन में कमी लाने की न कि सिर्फ निजी वाहनों के टेलपाइप से होने वाले उत्सर्जन में कमी करने की। जाहिर है कि ऑटो तथा ईधन उद्योग के मुनाफे तो इसी से तय होते हैं कि वे आज हमें कितने ज्यादा वाहन तथा कितना ज्यादा ईंधन बेच सकते हैं। रही बात कल की तो कल जाए भाड़ में। पूंजी तो हमेशा ही भविष्य के मुकाबले वर्तमान को तरजीह देती है। उसकी प्रकृति ही ऐसी है।
प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन बनाया जाए पैमाना
कम कार्बन उत्सर्जन के रास्ते पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस गंभीर प्रश्न के उत्तर के लिए हमें सिर्फ भविष्य के समाधानों के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, जो हो सकता है कि आएं या हो सकता है कि नहीं भी आएं। हमें मौजूदा विकल्पों को भी आजमाना होगा। ऊर्जा संक्रमण का बोझ, निर्धनतर देशों पर डालने की कोशिश करने के बजाए, सिर्फ किसी देश के कार्बन उत्सर्जन के पैमाने की चिंता करने की जगह, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन के स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां हम पुराने ऐतिहासिक उत्सर्जन में तो जा ही नहीं रहे हैं, जिसके अधिकांश हिस्से के लिए धनी देश ही जिम्मेदार हैं। हम तो यहां सिर्फ इतना ध्यान दिला रहे हैं कि बिजली का उपभोग आखिरकार इंसानों द्वारा किया जाता है और इसकी कोई तुक ही नहीं बनती है कि चीन के कुल कार्बन उत्सर्जन की तुलना अमरीका से की जाए, जिससे चीन की आबादी पांच गुना ज्यादा है या फिर भारत के उत्सर्जनों की तुलना, उसकी तुलना में आबादी के आकार के हिसाब बहुत छोटे योरपीय देशों से की जाए। इस तरह बहुत ही असमान आबादी वाले देशों को बड़े उत्सर्जनकर्ता करार देकर, तराजू के एक ही पलड़े पर तोलने की कोशिश करना, मुद्दों को गड्डïमड्डï करना ही है। महज रिकार्ड के लिए यह भी दर्ज कर लिया जाए कि भारत की ऊर्जा का सिर्फ 60 फीसद हिस्सा जीवाष्म ईंधनों से आता है, जबकि अमरीका में यही हिस्सा 68.6 फीसद है। और चीन ने पिछलेे तीन वर्षों में अपने ऊर्जा स्रोतों में, नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में हर साल जितना इजाफा किया है, वह अमरीका तथा योरप द्वारा मिलकर ऐसी ऊर्जा में किए गए इजाफे से ज्यादा ही रहा है।
पर्यावरण के संकट से निपटने का तरीका एक ही है: ईमानदारी से सामने खड़ी समस्या को पहचाना जाए और सिर पर मंडराते खतरे को टालने के लिए हरेक देश ज्यादा से ज्यादा जो कर सकता है, उसे करे। मैं तो इसकी बात छेड़ ही नहीं रहा हूं कि अब जो कार्बन उत्सर्जन गुंजाइश दुनिया के लिए बच गयी है, उसका देशों के बीच न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा हो, बस धनी देश बची हुई कार्बन गुंजाइश को भी यूंही नहीं हथिया लें, जैसा करने पर अमरीका-योरप-यूके आमादा नजर आते हैं। इसका मतलब है, जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, इस बात को पहचाना जाए कि धनी देशों को कम उत्सर्जन के रास्ते पर दुनिया के संक्रमण की लागत का कहीं बड़ा हिस्सा अपने कंधों पर लेना होगा और वे इससे संबंधित पेटेंटों/ नो हाऊ के नाम पर, विपन्नतर देशों को लूटें नहीं। और छांटकर सिर्फ कोयले को ही निशाना बनाने और दूसरी ओर प्राकृतिक गैस के संक्रमणकालीन ईंधन होने का स्वांग भरने से बाज आया जाए। पड़ौसी जाए भाड़ में का सिद्घांत तात्कालिक रूप से तो धनी देशों को फायदे का सौदा लग सकता है, लेकिन यह समूची मानवता पर महाआपदा को न्यौतने का ही काम करेगा।
इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Hypocrisy of Rich Countries: Ignoring the Storage Problem in Green Energy
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।