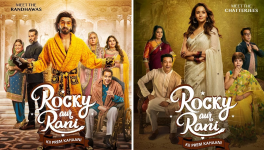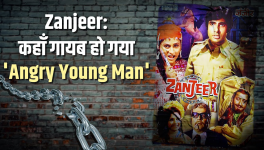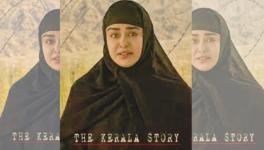‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ सेना में महिलाओं के संघर्ष की कहानी!

“तुम कमज़ोर हो गुंजन और डिफेंस में कमज़ोरी के लिए कोई जगह नहीं है।”
ये डायलॉग शौर्य चक्र विजेता फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट गुंजन सक्सेना पर बनी बॉयोपिक ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ का है। फ़िल्म में डायलॉग भले ही 90 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई गुंजन सक्सेना के लिए लिखा गया हो, लेकिन आज भी पुरुषों का वर्चस्व माने जाने वाले आर्मड फोर्सेस में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर ही दिखाई पड़ती है। इस लिहाज से ये फ़िल्म सिर्फ़ एक रियल हीरो की कहानी ही नहीं बल्कि हमारे समाज में मौजूद कुछ गंभीर समस्याओं की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है।
बात करें फ़िल्म की, तो ये 12 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई और रिलीज़ होते ही विवादों में घिर गई। फ़िल्म के कंटेंट को लेकर भारतीय वायुसेना ने आपत्ति जताई है। भारतीय वायुसेना ने सेंसर बोर्ड को चिट्ठी के जरिए बताया है कि फ़िल्म में उनकी खराब और गलत छवि दिखाई गई है। भारतीय वायुसेना कभी भी लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं करती है।
पितृसत्ता को चुनौती देती लड़कियां
हम फ़िल्म में अगर इंडियन एयरफोर्स के आपत्ति वाले भाग, जोकि ट्रेनिंग अकादमी से लेकर बेस तक अधिकारियों के स्वभाव और भेदभाव की कहानी बयां करता है, इसे छोड़ भी दें तो भी फ़िल्म हमारे पितृसत्तामक समाज और इसकी सोच पर कई सवाल खड़े करती है। इस सच को आज भी कोई नहीं नकार सकता कि जब-जब महिलाएं पितृसत्ता की खिंची लकीर को पार करती हैं तो इसे सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता, आधी आबादी को समाज के साथ-साथ परिवार में भी संघर्ष करना पड़ता है।
कहानी में गुंजन जब अपने भाई से कहती है कि ‘भइया मुझे पायलट बनना है, तो उसका भाई फटाक से कहता है ‘लड़कियां पायलट नहीं बनतीं।’ जब गुंजन का 10वीं का रिजल्ट आता है, तो घर में पार्टी होती है। तभी गुंजन अपने प्लेन उड़ाने के सपने के बारे में सबको बताती है। मां और भाई गुंजन के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन उसके पापा उसका साथ देते हैं। फ़िल्म की कहानी एक आम आर्मी परिवार की कहानी है, जहां घर में बचपन से कभी बेटे और बेटी में भेदभाव तो नहीं हुआ लेकिन जब बात करियर और प्रोफेशन चुनने की आती है तब गुंजन को लड़के और लड़की का अंतर समझाया जाता है। गुंजन अपने भाई से कहती भी है, ‘जब आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं प्लेन क्यों नहीं उड़ा सकती।‘
बेसिक चीज़ों के लिए संघर्ष करती महिलाएं
हालांकि तमाम कठनाईयों को पार करते हुए गुंजन एसएसबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ट्रेंनिंग अकादमी तो पहुंच जाती है, लेकिन यहां भी उसे बार-बार औरत होने का एहसास करवाया जाता है, पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर साबित करने की कोशिश की जाती है। एक अफसर गुंजन से कहता है, ‘हमारी ज़िम्मेदारी देश की रक्षा करना है, तुम्हें बराबरी का अधिकार देना नहीं।’ जब गुंजन लेडीज़ टॉयलेट न होने की बात करती है, तो उससे कहा जाता है कि ‘लेडीज़ टॉयलेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जगह लेडीज़ के लिए है ही नहीं।‘ ये डायलॉग्स भले ही फिल्मी हों, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी कई दफ्तरों, पुलिस चौकियों और कार्यालयों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा नहीं है।
इसके बाद गुंजन का सफ़र उधमपुर बेस पहुंचता है, जहां फिर उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी होती हैं। महिला अधिकारी को सैल्यूट न करना पड़े, इसलिए जवान गुंजन को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। को-पायलट सोर्टिस के लिए उसके साथ उड़ान भरने को तैयार नहीं होते। यहां इंडियन एयरफोर्स की आपत्ति को ध्यान में रखें, तो हो सकता है कि ये दृश्य महज़ फ़िल्म को रोमांचक बनाने के लिए इस्तेमाल किये गए हों, लेकिन सरकार के उस तर्क का क्या जो उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने महिलाओं के सेना में परमानेंट कमीशन की सुनवाई के दौरान दिया था। केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि सैन्य अधिकारी महिलाओं को अपने समकक्ष स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेना में ज़्यादातर पुरुष ग्रामीण इलाकों से आते हैं। सरकार का कहना था कि पुरुष महिलाओं से कमांड लेना पसंद नहीं करेंगे और न ही उन्हें सीरियसली लेंगे।
लड़कियों की उड़ान को चारदीवारी तक सीमित रखने की कोशिश
फ़िल्म में एक जगह गुंजन का अफ़सर उससे कहता है, ‘अगर एयरफोर्स में रहना है तो फ़ौजी बनकर दिखाओ वरना घर जाकर बेलन चलाओ।’ हो सकता है भारतीय वायुसेना इससे इत्तेफाक न रखे, लेकिन हमारी सरकार इससे सहमति रखती जरूर दिखाई देती है। सेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर सरकार की तरफ से वकील आर बालासुब्रह्मण्यम और नीला गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महिला अधिकारियों के लिए कमांड पोस्ट में होना इसलिए भी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें प्रेग्नेंसी के लिए लम्बी छुट्टी लेनी पड़ती है। उन पर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। ये सोच अपने आप में पूर्वाग्रह से ग्रस्त पुरुषवादी मानसिकता दिखाती है, जो महिलाओं की उड़ान को घर के चारदीवारी और रसोई तक ही सीमित रखना चाहते हैं।
‘पुरुष ताकतवर होते हैं और महिलाएं कमज़ोर, ये सोच ग़लत है’
17 फरवरी 2020 को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ करते हुए अपने फैसले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सरकार द्वारा दी गई दलीलें स्टीरियोटाइप हैं। ये गलत अवधारणा है कि पुरुष ताकतवर होते हैं और महिलाएं कमज़ोर। कानूनी रूप से इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन न दिया जाए। महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने से इंकार करना समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ है। अगर महिलाओं की क्षमता और उपलब्धियों पर शक़ किया जाता है ये महिलाओं के साथ-साथ सेना का भी अपमान है।

कोर्ट द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां
* सामाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न मिलना परेशान करने वाला और अस्वीकार्य है।
* महिला सैन्य अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न देना सरकार के पूर्वाग्रह को दिखाता है।
* केंद्र सरकार को महिलाओं के बारे में मानसिकता बदलनी होगी और सेना में समानता लानी होगी।
* महिलाओं को कमांड पोस्ट पर प्रतिबंध अतार्किक है और समानता के ख़िलाफ़ है।
बता दें कि सेना में 1992 से पहले औरतों को सिर्फ मेडिकल रोल में इंट्री मिलती थी। 1992 के बाद शार्ट सर्विज कमिशन यानी एसएससी आया। इसके तहत महिलाओं के लिए सेना के दरवाजे तो खुले, मगर वो सिर्फ 10 साल ही सेवा दे सकती थीं। 2006 में फिर इसे 14 साल तक बढ़ा दिया गया। लेकिन उन्हें पुरुषों के बराबर परमानेंट कमीशन का समान अवसर नहीं दिया गया। जिसके कारण महिला अधिकारी निचली रैंक्स तक ही सीमित रह जाती थीं, उन्हें ऊंची पोस्ट्स, जिन्हें कमांड पोस्ट कहा जाता है वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता था। इसके अलावा 20 साल की सेवा पूरी न होने के कारण वे रिटायरमेंट के बाद पेंशन बेनिफिट से भी वंचित रह जाती थीं। इस भेदभाव को लेकर कई सवाल उठे।
परमानेंट कमीशन को लेकर महिलाओँ का संघर्ष
महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर 2003 और 2006 में पेटिशन फाइल हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 के अपने फैसले में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की बात कही। भारतीय वायुसेना ने इसे मानते हुए अक्तूबर 2015 में फाइटर पाइलेट स्ट्रीम को महिलाओं के लिए खोल दिया। जुलाई 2018 में कमीशन होकर अवनी चतुर्वेदी, भावना और मोहना सिंह ने इतिहास रचते हुए भारत की पहली तीन फीमेल फाइटर पाइलेट बनने का गौरव हासिल किया। अभी तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं भारतीय वायुसेना में ही कार्यरत हैं।
हालांकि इंडियन आर्मी में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हुआ। जिसका सेना द्वारा औपचारिक आदेश 23 जुलाई 2020 को जारी किया गया।
फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट गुंजन सक्सेना थीं ऑपरेशन विजय का हिस्सा
ख़ैर, फिर लौटते हैं फ़िल्म की कहानी के मुख्य हिस्से यानी कारगिल पर। गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल के नाम से इसलिए मशहूर हैं क्योंकि फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट गुंजन सक्सेना की जिंदगी में असली हाई प्वांइट कारगिल ही था। फ़िल्म का फोकस भले ही सिर्फ गुंजन पर हो लेकिन 1999 में जब कारगिल में लड़ाई शुरू हुई तो गुंजन सक्सेना और उनके जैसे आठ पायलट्स को वहां डिप्लॉय किया गया था।
करगिल में जब हालात खराब हो गए तो गुंजन से पूछा गया कि क्या वो डेंजर जोन से बाहर निकलना चाहेंगी, क्योंकि वो एक महिला अधिकारी हैं और शायद वो इसमें हिस्सा न लेना चाहें। लेकिन गुंजन ने पीछे हटने से मना कर दिया और ऑपरेशन विजय का हिस्सा बन गईं।
शुरुआत में उन्हें सर्विलेंस सोर्टिस पर भेजा गया। यानी किसी भी एरिया की निगरानी करते हुए उन्हें एक अकेले मिशन को भी खुद पूरा करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुंजन ने 15,000 से 18,000 फिट की हाइट से अपने सर्विलेंस मिशन किए। बाद में उन्होंने कई और मिशन को भी अंजाम दिया। जैसे खाना और मेडिकल सुविधा पहुंचाना, घायल सैनिकों को रेस्क्यू करना आदि।
इस मिशन में गुंजन के साथ उनकी साथी श्री विद्याराजन भी शामिल थी। जिन्हें फ़िल्म में करीब-करीब इग्नोर कर दिया गया है। दोनों ने मिलकर करगिल के दौरान 80 सोर्टीस मिशन पूरे किए थे। लड़ाई के बाद के चरण में वायुसेना ने छोटे हैलीकॉप्टर की जगह फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया। लेकिन तब तक सोर्टिस मिशन के तहत करीब 900 घायल सैनिकों को बचा लिया गया था और शहीदों को अपने परिवारों तक पहुंचा दिया गया था।
आज गुंजन सक्सेना जैसी महिलाओं के कारण ही आमर्ड फोर्सेस में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हो रही है, उनकी सही जगह तलाशने की कोशिशें जारी हैं। अगर विश्व स्तर पर सेनाओं में महिलाओं की स्थिति देखें तो ये भारत से इतर नहीं है। नेशनल जियोग्रफिक मैगज़ीन के मुताबिक दुनियाभर में 200 से ज्यादा देश हैं लेकिन केवल 16 देश की सेनाओं में ही महिलाएं शामिल हैं।
दुनियाभर की सेनाओँ में महिलाओं की स्थिति
महिलाओं को सेना में जगह देने वाले देशों में सबसे पहले 1980 के दशक में नार्वे, कनाडा और डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं जिन्होंने महिलाओं को कॉमबेट पोजिशन में जगह दी। फिर जापान, चाइना जैसे देशों में भी बदलाव दिखा, वहां भी औरतों को सेना में इस पोजिशन पर एंट्री मिली। हालांकि आर्थिक रूप से संपन्न यूएसए ने 2016 में औरतों के लिए कॉमबेट के दरवाजें खोले। यहां एयरफोर्स और नेवी में उन्हें पहले से ही परमिशन थी।
गौरतलब है कि इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान औरतों ने अहम योगदान दिया था। रूसी सेना में औरतों के खुद की तीन रेजिमेंट थे। बावजूद इसके दुनिया के पटल पर सेना में औरतों की स्थिति चिंताजनक ही है। आज भी सेना में कई पद खाली हैं लेकिन आधी आबादी को इससे दूर रखा जाता है। अगर भारतीय सेनाओं की बात करें तो एक आंकड़ें के मुताबिक अभी भी इसमें 9,427 अधिकारियों और 68,864 जवानों की कमी है। अभी भी कॉमबेट रोल के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी है।
हम कह सकते हैं कि सेना में औरतों को लेकर सोच जरूर बदल रही है लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता की अभी भी बराबरी के हक की लड़ाई में महिलाओं को एक लंबा सफर तय करना बाकी है।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।