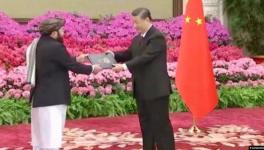क्या चीन एक पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश में तब्दील हो गया है?
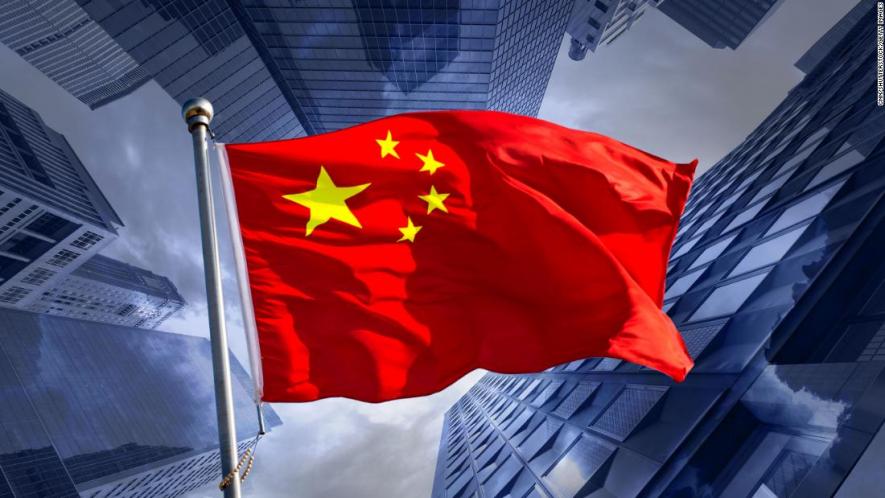
वाम-उदारवादी खेमे के एक हिस्से में चीन-अमेरिका के संबंधों पर जब भी चर्चा होती है तो वे ये कहते पाए जाते हैं कि आखिर चीन के पक्ष में खड़े होने से क्या फायदा? चीन भी तो अंततः नवउदारवादी रास्ते पर चलने वाला पूंजीवादी देश ही है। नवउदारवाद के सभी दुर्गुणों से ग्रस्त है चीन। अब चीन समाजवादी देश नहीं रहा अपितु एक साम्राज्यवादी देश में तब्दील हो चुका है।
एक जमाने में जब अमेरिका व सोवियत संघ के बीच शीतयुद्ध चल रहा था, तब यह खेमा कहता था कि अंततः सोवियत संघ भी तो एक साम्राज्यवादी देश है―सामाजिक साम्राज्यवादी। अफगानिस्तान वगैरह में सोवियत संघ के हस्तक्षेप को साम्राज्यवादी हस्तक्षेप की संज्ञा दी जाती थी। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के ढ़हने पर इन लोगों द्वारा कहा गया कि दो साम्राज्यवादी देशों की लड़ाई में में एक की हार हो गयी।
जिस प्रकार सोवियत संघ को 1991 के पूर्व साम्राज्यवादी बताया जाता था, ठीक उसी प्रकार आज वे चीन को पूंजीवादी व साम्राज्यवादी देश बताने वालों की खासी तादाद है।
चीन के इन आलोचकों को चीजों को बनाम में देखने की आदत है। यदि वो समाजवाद की पूरे रास्ते पर नहीं है तो फिर पूंजीवाद के रास्ते पर हैं। यह एक गैरमार्क्सवादी तरीका है सवाल पूछने का। एक मार्क्सवादी पद्धति में बाईनरी में, काले व सफेद के फ्रेम में देखने के ढ़ंग से सोचने से बचने की सलाह दी जाती है। मार्क्सवाद किसी चीज को ठहरे हुए रूप में नहीं बल्कि एक प्रक्रिया में देखता है। चीन कहां था? आज वो कहां पहुंचा है, अभी उसके भीतर क्या समस्यायें हैं? उसके देश के अपने बद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं? अभी चीन के जो मौजूदा हालात हैं उसे लेकर चीन के बुद्धिजीवियों के मध्य, कम्युनिस्ट पार्टी में किस किस्म की बहसे हैं, कितने ‘स्कूल ऑफ थॉट’ हैं इन तमाम बातों से हममें से अधिकांश लोग नावाकिफ हैं और पश्चिम के उदारवादी किस्म के बुद्धिजीवियों के बनाये फ्रेम के आधार पर एक समझ चस्पां कर देते हैं।
सबसे पहले तो चीन को लेकर सही ढ़ग के प्रश्न उठाए जाने चाहिए। वैसे भी समाजवादी निर्माण एक तकलीफदेह प्रक्रिया होती है। पांरपरिक समाज का पिछड़ापन बाधा के रूप में सामने आता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी देश में क्रांति हुई और समाजवाद का निर्माण होने लगा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चीन एक कम्युनिस्ट समाज में परिवर्तित हो चुका है।
जब रूस में क्रांति हुई तो उनके नेताओं के भाषणों को पढ़ने से पता चलता है कि वे सभी इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि समाजवाद के निर्माण की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए? समाजवाद सिर्फ एक घटना नहीं है, इवेंट नहीं बल्कि एक प्रक्रिया भी है। क्रांति के पश्चात एक समाज की तमाम पुरानी चीजों को भी आप उत्तराधिकार में पाते हैं जिससे छुटकारा पाने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए वियतनाम का नाम लिया जा सकता है। अमेरिका के नापाम बमों ने वियतनाम की खेती को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वहां अभी सैंकड़ों वर्षों तक खेती कर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है। अब कोई कहे कि वियतनाम पूरी तरह समाजवादी देश क्यों नहीं है? आप किसी देश की कृषि को नष्ट कर कहें कि वो क्यों नहीं खेती का सामूहिकीकरण कर रहा है?
कमांडिंग हाइट्स पर अभी भी स्टेट का नियंत्रण
इस बात में कोई शक नहीं कि चीन में आज पूंजीपतियों के ख़ासी तादाद है। चीन आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा केंद्र है। स्टारबक्स और केएफसी के सैंकड़ों शाखाएं आज चीन में मौजूद हैं। निजी पूंजी की चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ी उपस्थिति है।
चीन ने पूंजीवादी तत्वों का सचेत रूप से इस्तेमाल उत्पादक शक्तियों को विकसित करने के लिए किया है। लेकिन निजी पूंजी को तमाम सहूलियतों के बावजूद अर्थव्यस्था में जिसे 'कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकॉनॉमी'- मसलन भारी उद्योग, ऊर्जा, वित्त, संचार और आवागमन- कहा जाता है उस पर शुरू से ही राज्य का ही नियंत्रण रहा है। चीन का बुनियादी एजेंडा अभी भी योजना (प्लान) आधारित होता है। निजी पूंजी को भी पंचवर्षीय योजना के व्यापक फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है। चीन में निजी पूंजी निवेश की प्रकृति दूसरे देशों के मुकाबले भिन्न है। चीन विदेशी निवेश की इजाजत देता है परंतु विदेशी शोषण की नहीं। विदेशी कम्पनियां वहां व्यापार कर सकती हैं, उसके माध्यम से पैसा बना सकती है। लेकिन यह उन्हें चीन के कड़े नियमों के अनुशासित दायरे में काम करना पड़ता है।
सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वित्त या फाइनांस पर किसका कब्जा है। चीन में बैंक व फाइनांस के सभी क्षेत्रों पर राज्य का, सरकारी क्षेत्र का वर्चस्व है। चीन की अर्थव्यस्था में निजी क्षेत्र का अनुपात कभी भी सार्वजनिक क्षेत्र से आगे नहीं जा पाया है।
पूंजीवादी देशों की यह विशेषता होती है कि पूंजी का हित आम जनता के हितों से ऊपर समझा जाता है। पूंजीपतियों का हित ही राष्ट्र का हित समझा जाता है। जैसे भारत में अंबानी-अडानी का हित भारत का हित बताया जाता है। चीन में यह स्थिति नहीं है। चीन सरकार की नीतियों में वहां के बड़े पूंजीपतियों का दखल के उदाहरण नहीं हैं।
चीन में राज्य किस वर्ग के हाथ में है?
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यदि पूंजीवादी देशों ने समाजवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने यहां शिक्षा व स्वास्थ्य को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखा। सामाजिक सुरक्षा पर भी कुछ खर्च किए। लोगों को एक सेफ्टी नेट मुहैया कराया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो देश समाजवादी रास्ते पर आगे बढ़़ गए। क्योंकि देखा ये जाता है कि सत्ता किस वर्ग के हाथ में है। ठीक उसी प्रकार चीन यदि निजी पूंजी को थोड़ी छूट दे रहा है तो इसका ये मतलब थोड़े ही न हुआ कि वहां पूंजीवाद स्थापित हो गया।
1921 में लेनिन ने ‘नई आर्थिक नीति’ (एन.ई.पी) लाकर निजी पूंजी को छूट दी थी तो क्या वो समाजवाद के रास्ते से भटक गए थे? प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ई.एम.एस नंबेदिरीपाद ने चीन में हो रहे परिवर्तनों के बारे में काफी पहले कहा कहा था ‘‘देखना ये चाहिए कि राज्य किस किसके हाथ में है?’’ यदि राज्य कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है तो कभी भी, मान लीजिए कुछ गलत भी हो रहा हो तो उसे दुरूस्त किया जा सकता है। अभी भी चीन में भूमि राष्ट्र की संपत्ति है, राज्य के हाथ में है। किस पूंजीवादी देश में भूमि राज्य के हमें है?
चीन ने विज्ञान व तकनीक के महत्व को बहुत जल्दी समझ लिया था। चीन ने ये समझा कि जब तक उत्पादक शक्तियों का विकास नहीं होगा तब तक समाजवाद का निर्माण संभव नहीं है।आखिर समाजवाद का मतलब गरीबी का सामाजीकरण तो नहीं है। जैसा कि कम्बोडिया ने किया था? चीन इस वक्त उत्पादक शक्तियों के विकास पर बल दे रहा है।
जोसेफ स्तालिन की चर्चित किताब ‘‘सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोलशेविक) का इतिहास’’ में इस बात को रेखांकित किया है कि कैसे हमेशा वहां इस बात पर बहस हुआ करती थी कि उत्पादक शक्तियों के विकास पर बल देना है या फिर उत्पादन संबंधों के बदलने पर जोर देना है? स्तालिन ने अपनी एक अन्य महत्वपूर्ण किताब ‘‘ इकॉनॉमिक प्रॉब्लम्स ने यू.एस.एस.आर।’ में ये सवाल उठाया कि समाजवाद क्यों हारता है? इस किताब में उन्होंने उत्पादक शक्तियों के विकास पर ही समाजवाद की जीत को निर्भर होना बताया है। यदि उत्पादक शक्तियों का विकास नहीं होगा तो समाजवाद कमजोर हो जाएगा और पूंजीवाद हावी हो जाएगा।।’’
चीन में नब्बे प्रतिशत लोगों के पास अपना घर
उत्पादक शक्तियों का विकास करने का सामाजिक-आर्थिक फायदा समाज के निचले तबकों को भी हासिल हो रहा है। आज चीन में लगभग 90 प्रतिशत लोगों के पास अपना घर है। और घर कोई कर्ज लेकर नहीं बनाया गया है। जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में घर अमरीकियों को कर्जदार बनाने का कारण बन चुका है। दुनिया का कोई विकसित देश ये उपलब्धि आज तक नहीं हासिल कर पाया है। चीन में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों ने घरेलू बाजार का विस्तार किया है। पिछले 40 सालों के दौरान चीन ने 85 करोड़ लोगों को गरीबी रेख से ऊपर उठाया है। इस किस्म की उपलब्धि आज तक दुनिया का कोई देश नहीं हासिल कर पाया है जबकि अमेरिका को देखें तो वहां पिछले 35 सालों से मजदूरी में बढ़ोतरी ही नहीं हुई है। तकनीक के मामले में भी देखें चीन अमेरिका से काफी आगे जा चुका है। चीन के पास 165 सुपर कंप्युटर है जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 25।
आज चीन एक अभ्युदयशील देश है तो अमेरिका पतानोन्मुख देश। विकसित देशों के सरगना अमेरिका का ये हाल है कि उसकी आधी आबादी ‘फूड बैंक’ पर निर्भर है। ‘फूड बैंक’ वहां के अमीर व सक्षम लोगों के परोपकारस्वरूप दिए गए धन से चलाए जाते हैं। कोरानावायरस संकट के दौरान अमेरिका का इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य मॉडल ध्वस्त हो चुका लेकिन चीन में स्वास्थ्य सेवाएं चुंकि सार्वजनिक क्षेत्र में है फलतः वो कोराना संकट से बेहतर ढ़ंग से लड़ पाया।
अफ्रीका में पूंजी निवेश का चीनी मॉडल
चीन द्वारा शुरू की गयी महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वन बेल्ट रोड इनीशिएटिव’, सी.पी.ई.सी आदि को मुनाफे की इच्छा से किया गया साम्राज्यवादी कदम बताया जाता है। चीन द्वारा अफ्रीका में किए जा रहे निवेशों के बारे में ऐसा ही कहा जाता है।
साम्राज्यवाद का अर्थ एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें किसी दूसरे देश में गैरआर्थिक शक्तियो यथा ताकत के बल पर अपने देश की निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाता है।
चीन का अफ्रीका में बिल्कुल दूसरा इतिहास रहा है। माओ के जमाने से ही चीन के अफ्रीकी देशों से रिश्ते रहे हैं। माओ के समय ही चीन ने ‘ताजारा’ रेल-रोड का निर्माण किया था। तंजानिया क जूलियस न्येरेरे के साथ भी चीन के पुराने संबंध रहे हैं। ऐसा ही अंगोला आदि कई देशों में रहा है। चीन पहले से अफ्रीकी देशों को तकनीकी सहायता मुहैया कराता रहा है।
चीन के साम्राज्यवादी होने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि चीन अफ्रीका में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर रहा है। यानी पूंजी का निर्यात कर रहा है जोकि साम्राज्यवाद का लक्षण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है।
लेकिन ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि वो निवेश किस प्रकार कर रहा है? अमेरिकन कंपनियों के पूंजीनिवेश के पीछे या कर्ज के पीछे शर्तें बंधी रहती हैं जिसमें उन्हें उनके द्वारा बताए देशों के चिन्हित लोगों या कंपनियों से माल या उपकरण खरीदना होगा। यदि आप हमसे सामान नहीं खरीदेंगे तो हम कूटनीतिक, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर बम बरसा देंगे, आपकी जिंदगी नरक बना देंगे। कभी भूलकर भी उन देशों को अपनी तकनीक स्थानांतरित नहीं की जाती।
चीन इन अफ्रीकी देशों को तकनीक स्थानांतरित करता ही है और कोई शतें भी नहीं थोपता है। दूसरा चीन का प्रयास ये रहता है कि जिन देशों में वो निवेश कर रहे हैं वहां एक उत्पादन का औद्यौगिक आधार तैयार कर सके। यह काम अपने जमाने में सोवियत संघ किया करता था। भारत सहित तीसरी दुनिया के कई देशों में उसने एक औद्योगिक आधार तैयार करने में सोवियत संघ ने सहायता दी थी। निवेश के अमेरिकी व चीनी मॉडल में यह बहुत बड़ा अंतर है।
यानिस वारफाकिस, यूनान और अफ्रीका में चीनी निवेश
इस बात को यूनान के पूर्व वामपंथी वित्त मंत्री यानिस वारफाकिस की बातों से समझा जा सकता है। यानिस वारफाकिस को अपने रैडिकल विचारों के कारण वित्तमंत्री का पद छोड़ना पड़ा क्योंकि पूंजीवादी देश नहीं चाहते थे। अभी हाल में उन्होंने ‘प्रोग्रसिव इंटरनेनल’ की स्थापना भी की है।
यानिस वारफाकिस ने चीन के यूनान में हो रहे निवेश के बारे में बताया ‘‘चीनी लोग इस बात के लिए नहीं आते कि हमारी संपत्ति हड़प लें। बल्कि जिस देश में वे निवेश करते हैं वहां संपत्ति का निर्माण करते हैं। वे सट्टेबाजी के मकसद से नहीं आते बल्कि उनके काम का समय अगले 25-30 सालों का रहता है ’’ यानिस वारवफाकिस ने आगे बताते हैं ‘‘ हमने एक बंदरगाह के लिए उनसे निवेश की बात की थी। हालांकि मेरे छोड़ने के बाद वो योजना फलीभूत नहीं हो सकी। बाद में विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष वाली जो त्रिमूर्ति है उसने चीनी निवेश के मुकाबले बहुत ज्यादा कड़ी शर्तों पर निवेश किया। चीन ने एक साल में जितना निवेश किया था लगभग 180 मिलियन यूरो। वो काफी ज्यादा था। दूसरी बात ये है कि उन लोगों ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी, वे अपना यूनियन बना सकेगे और कलेक्टिव बारगेनिंग (सामूहिक सौदेबाजी) कर सकेंगे। चीनियों ने इसके साथ ये भी कहा कि जो बंदरगाह बनेगा उसमें वहां की म्युनिसैपिलिटी का भी हिस्सा रहेगा। लेकिन जर्मनी ने हस्तक्षेप पर ये डील नहीं होने दिया। चीन अपने इंजीनियर, तकनीक, आदि के साथ आ रहा था। जो काम चीन कर रहा है वो दूसरे पूंजीवादी देश नहीं कर रहे हैं। चीन से पैसा नहीं आ रहा था बल्कि निवेश आ रहा था और दोनों में काफी फर्क होता है। इसलिए इनलोगों को चीन से इतनी दिक्कत भी है। ’’
यानिस वारफाकिस साथ में यह भी जोड़ते हैं "चीनी लोग हस्तक्षेप करने वाले नहीं होते। पश्चिमी मुल्क इस बात को समझ ही नहीं पाते। चीनी लोगों के अंदर कोई सैन्य महत्वाकांक्षा नहीं नजर आती है। ये अफ्रीका में फौजी दस्ते लेकर, पश्चिमी मुल्कों की तरह, लोगों को मारने के लिए नहीं आते। ये एयरपोर्ट, रेलवे, टेलीफोन और आपकी सड़क बनाने आते हैं। इन लोगों ने अपने निवेशों को किसी साम्राज्यवादी लक्ष्यों से कभी भी नहीं जोड़ा है।"
समाजवाद की पहचान है ‘पब्लिक एक्शन'
समाजवाद का मतलब सिर्फ राज्य और उसका चरित्र ही नहीं होता। वहां की जनकार्रवाइयों से भी इसको समझा जा सकता है। चीन में जनकार्रवाई या कहें पब्लिक एक्शन वहां की खास सामाजिक पहचान है। पूंजीवादी मुल्कों में पब्लिक एक्शन का सर्वथा अभाव रहता है। चीन पड़ोस समितियां (नेवरहुड कमिटि) और संगठन हैं, नागरिक समूह हैं जिन्होंने संकट के समय बड़ी-बड़़ी भूमिकाएं अदा की हैं। सिर्फ एक जिले में चार लाख चवालीस हजार लोगों ने स्वंयसेवकों की भूमिका अदा की है। जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोविड महामारी कोराना की अग्रिम पंक्ति में लड़ने के लिए डॉक्टरों का आहवान किया तो वहां लगभग 50 हजार डॉक्टरों ने आवेदन दिया कि वे आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। क्या हम ऐसी स्थिति की कल्पना भारत में कर सकते हैं?
समाजवाद के भौतिक आधार को निर्मित करने में निजी पूंजी को भी साधने की चीनी कोशिश को पश्चिमी देश समझ ही नहीं पाते। चीनी प्रयोग को समझने के लिए खास दृष्टि की आवश्यकता है। पटना में रहने वाले चर्चित हिंदी कवि लगभग डेढ़ दो दशक पूर्व चीन की यात्रा पर गए थे। लौटने पर अरूण कमल ने एक दिलचस्प बात साझा की ‘‘चीन का समझना हो तो वहां खाने के तरीके से समझा जा सकता है। वे लोग खाने के लिए दो कांटों वाले उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। जिसमे एक कांटां स्थिर रहता है जबकि दूसरा चारों ओर हिलता है, मूव करता रहता है। ठीक चीन भी ऐसा ही समाज है जिसमें एक ओर चीनी क्रांति के समाजवादी मूल्य स्थिर हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया के बाजार में चीन ‘मूव’ करने का प्रयास कर रहा है।"
(अनीश अंकुर वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
लेख का पहला भाग पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।