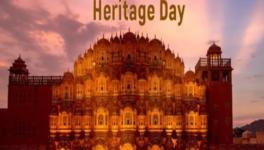इतिहास से उत्पीड़ितों को न्याय की आस: वन अधिकार क़ानून के चौदह बरस

वन अधिकार क़ानून के नाम से प्रचलित ‘अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) क़ानून 2006’ अपने मौजूदा स्वरूप में 14 साल पहले, 15 दिसंबर 2006 को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पारित हुआ था। क़ानून बनवाने के इस अभियान से जुड़े संगठन, कार्यकर्ता और जंगल में निवास करने व जंगलों पर आश्रित समुदाय इस दिन को बड़ी जीत के रूप में देखते हैं। आज कई आदिवासी इलाकों में इस खास दिन के मौके पर जलसे व सभाएं भी होती हैं। हालांकि क़ानून को बने 14 साल बीत जाने और क़ानून को लेकर अपेक्षाओं व उम्मीदों के डूब जाने के बाद अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही लेकिन फिर भी इस दिन के खास मायने तो हैं।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर 2005 को इस क़ानून में एक विभाजक रेखा के तौर पर रखा गया और उन सभी लोगों के व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकार देने की प्रतिबद्धता इस क़ानून के माध्यम से देश की संसद ने दिखलाई थी जो इस नियत तारीख से पहले तक जंगल के संसाधनों पर आश्रित थे और जंगल में या जंगल के आस-पास रह रहे थे।
इस विभाजक रेखा के मायने यह भी हैं कि इसके बाद कोई नयी बसाहट या जंगल का निस्तार करने वालों को इस क़ानून के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। क़ानून के ‘लाभ’ से आशय यह है कि उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाएगी जो इस क़ानून का ‘केंद्रीय या बीज’ शब्द है।
वन अधिकार (मान्यता) क़ानून 2006, इस अर्थ में एक क्रांतिकारी क़ानून माना गया था क्योंकि इसने कई ऐसी अवधारणाओं को पुनर्स्थापित किया था जो औपनिवेशिक काल से ही कलंकित कर दी गईं थीं। इन अवधारणाओं में सबसे बड़ी अवधारणा यह थी कि जंगलों में इन्सानों की मौजूदगी (प्राय: आदिवासी), जंगल की सेहत व सुरक्षा, वन्य जीव और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। आदिवासी या परंपरागत जंगल निवासियों की वजह से इन्हें खतरा पैदा हुआ है। दूसरी अवधारणा काल-बोध के एकदम विपरीत थी और वो ये कि आदिवासियों व अन्य परंपरागत गैर आदिवासी समुदायों ने जंगलों पर अतिक्रमण किया है और इन्हें बलात बाहर निकाला जा सकता है बल्कि निकाल देना चाहिए ताकि जंगल की सेहत, उसकी सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा और अंतत: पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
2003 में इन्हीं मनगढ़ंत मान्यताओं व धारणाओं के आधार पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा ही आदेश जारी भी किया जिसमें आदिवासी व अन्य परंपरगत गैर आदिवासी समुदायों को जंगल से बेदखल करने को कहा गया। कई राज्यों के वन विभाग जैसे इस एक आदेश का इंतज़ार ही कर रहे थे, उन्होंने बेदखली की कार्यवाहियाँ शुरू भी कर दीं। इन कार्यवाहियों के विरोध में देश के लोकतन्त्र में पहली दफा बड़ा ज्वार इन समुदायों की तरफ से उठा। हर स्तर पर बड़े आंदोलन हुए। जंगल और आदिवासियों के मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर आए और सर्वोच्च नयायालय के आदेश के समानान्तर एक विधायिका की प्रक्रिया शुरू हुई जिसकी परिणति इस क़ानून के रूप में सामने आयी। यही वजह है कि इस क़ानून को देश में व्यापक आदिवासी आंदोलन के तौर पर भी देखा जाता है।
इस क़ानून की कई खासियतों में एक बड़ी खासियत यह थी कि इतिहास की एक लंबी अवधि लगभग 250 सालों बाद जंगल और जंगल के संसाधनों के लोकतांत्रिकरण की बात उठी। क़ानून ने ग्राम सभाओं को वन संसाधन सौंपे जाने जैसा क्रांतिकारी कदम उठाया और इसे ऐतिहासिक अन्यायों के बरकस न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बतलाया गया।
देश का लगभग 40 मिलियन क्षेत्रफल जो इस क़ानून के आने से पहले वन विभाग के एकाधिकार में था उसका लोकतांत्रिकरण होना और गाँव के लोगों के अधीन किया जाना वाकई एक ‘क्रांतिकारी विचार’ तो था जो एक परिपक्व होते लोकतन्त्र की बदौलत संभव था। हालांकि विचार जितना क्रांतिकारी था उसे फलीभूत करने की यान्त्रिकी उतनी ही पाषाणहृदय और संवेदनहीन रही जितना वह इस क़ानून के वजूद में आने से पहले थी।
यह यान्त्रिकी जटिल नौकरशाही और जड़ हो चुकी ‘औपनिवेशिक लाटसाहबी’ के मिश्रण से बनी एक ऐसी यान्त्रिकी थी जो कतई यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनका एकाधिकार देश के लगभग 33 प्रतिशत भू-भाग और तमाम प्रकृतिक संसाधनों पर खत्म हो। और यही होता हुआ दिखलाई भी पड़ रहा है।
1 जनवरी 2006 को यह क़ानून राजपत्र में आया और क़ानून के क्रियानवायन के लिए नियम कायदे बने। इस क़ानून को लागू हुए 14 साल चुके हैं। इसका हासिल अभी भी 10 प्रतिशत तक नहीं छू पाया है। हाल ही में एक बैठक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावडेकर व आदिवासी मालों के मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा के बीच हुई जिसका आयोजन वनवासी कल्याण आश्रम के किसी पदाधिकारी ने किया। यह बैठक 10 अगस्त को हुई। इस बैठक के राजनैतिक मायने कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि इस बैठक में दोनों मंत्रालयों ने स्वीकार किया कि अभी तक इस क़ानून का हासिल महज़ 8-9 प्रतिशत ही है।
ऐसा माना गया कि वन विभाग अपना एकाधिकार जंगलों पर छोडना नहीं चाहता और उसकी तरफ से इस क़ानून के क्रियान्वयन में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इसलिए इस मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने मंत्रालय की तरफ से यह लिखित प्रतिबद्धता ज़ाहिर की कि उनका मंत्रालय, इस क़ानून की नोडल एजेंसी होने ने नाते आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो भी नियम-कायदे, नीतियाँ, निर्देश आदि बनाए गए हैं उनका अक्षरश: पालन करते हुए इस क़ानून के क्रियान्वयन में सहयोग करेगा और इसे समुचित ढंग से कार्यान्वित भी करेगा।
यह बैठक और उसमें ज़ाहिर की गयी प्रतिबद्धता बैरंग नहीं लौटी बल्कि 7 सितंबर को प्रकाश जावडेकर के मंत्रालय ने बाकायदा एक अधिसूचना/परिपत्र जारी किया और इस बैठक का हवाला देते हुए वन अधिकार क़ानून के समुचित क्रियान्वयन में सहयोग करने के निर्देश जारी किए।
इस बीच देश के जंगलों को कितनी ही बारिशों के पानी ने सींचा, कितने ही नए पौधे पेड़ बन गए। कितने वन्य जीवों के शावक पैदा हुए, कितनी ही वनस्पति उगी और सूखी। कितने आदिवासी व अन्य समुदाय कितने कितने सपनों के साथ दावे भरते रहे। कितने प्रशिक्षण हुए। कितने फार्मेट बने, कितने आंदोलन हुए। इन सब का हिसाब जंगल के मामले में रखना मुश्किल है लेकिन जब हिसाब लगाया जाये तो इनका भी लगे ताकि यह दर्ज़ हो कि प्राकृतिक संपदा अगर असली दावेदार के पास होती तो उसका कितना हिस्सा अच्छी स्मृतियों में दर्ज़ होता। बहरहाल अब अगर ‘अच्छी मंशा’ से एक राजनैतिक और प्रशासनिक पहल होती दिख रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए।
इस पहल से पहले कुछ ऐसे सवाल ज़रूर दोनों मंत्रालयों को अपने विचार में लाना चाहिए जो इन लगभग डेढ़ दशकों में अनुत्तरित रह गए। और क्योंकि समाधान भी वहीं मौजूद हैं इसलिए इनसे बच कर निकल जाने का सुभीता शायद नहीं है। और इनसे बचकर निकलने का मतलब ‘अच्छी मंशा’ पर भी सवाल होंगे।
देश की सर्वोच्च संस्था संसद ने यह स्वीकार किया था कि जंगल में रहने वाले तमाम समुदायों के साथ ‘ऐतिहासिक रूप से अन्याय’ हुए हैं। यह स्वीकारोक्ति असल में एक परिपक्व, उदार और प्रगतिशील लोकतन्त्र होने की गौरवशाली अभिव्यक्ति थी। यह ‘न्यू इंडिया’ की संसद नहीं थी बल्कि पुराने संसद भवन में ही एक तथाकथित कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौर की संसद थी। इस उदात्त अभिव्यक्ति की जितनी सराहना की जाये कम है लेकिन इस उदारता और विनम्रता के राजनैतिक जेश्चर (भंगिमा) में कुछ ऐसे ऐतिहासिक सवाल अनुत्तरित रह गए जिन्हें कुछ अध्येयता तभी से पूछ रहे हैं।
ऐसे एक अध्येयता और जंगल ज़मीन के मसलों पर तीन दशकों से काम कर रहे एडवोकेट अनिल गर्ग हमेशा पूछते आए हैं कि “जब संसद ने विराट उदारता दिखलाते हुए यह स्वीकार किया कि जंगल में सदियों से बसे आदिवासी व अन्य समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं तो ज़रूर संसद को ये भी बताना चाहिए था कि ये क्या अन्याय थे और किसने किए? आज़ादी से पहले हुए अन्यायों के लिए आप ब्रिटिश राज पर तोहमत दे देते लेकिन आज़ादी के बाद भी जारी इन अन्यायों के लिए जिम्मेदार लोगों, संस्थाओं और विधानों को जिम्मेदार बताने में क्यों संकोच किया गया?”
यह बात वाकई ‘कार्य- कारण’ के सामान्य दार्शनिक सिद्धान्त के लिहाज से पूछे जाने लायक तो है कि जब कोई कार्य हुआ है तो उसका कोई न कोई कर्ता भी ज़रूर होगा? ‘एक्ट ऑफ गॉड’ कह देना न्यू इंडिया में चलन में आया है लेकिन पहले तो ऐसा भी नहीं था।
इस महत्वपूर्ण सवाल से कन्नी काट लेने से जो नुकसान हुआ वो ये कि जिन पर अन्याय होना संसद ने ऐतिहासिक रूप से पाया उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया में उन्हीं से इस बात के प्रमाण मांगे जाने लगे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुए थे? इन अन्यायों के कोई प्रमाण हैं? कभी वन विभाग ने कोई चालान किया हो? वन अपराध दर्ज़ किए हों? गिरफ्तारी हुई हो? कोई मामला अदालत में हो? आदि आदि।
यह उत्पीड़ित को न्याय देने का नया न्यायशास्त्र जैसा बन गया। इसका सबसे बुरा असर ये हुआ कि खुद जंगल में रहने वाले समुदायों के दिमाग में एक ऐसा ‘नेरेटिव’ बन गया कि वो दावा फार्म में यह भरने के लिए अभिशप्त हो गए कि -जी वो जंगल जाते हैं, दिन में दो बार जाते हैं, जंगल से लकड़ी, कांड-मूल-फल लाते हैं, तेंदू पत्ता भी तोड़ते हैं और कई पीढ़ियों से खेती भी करते हैं, प्रमाण के रूप में रूप में जो भी मौजूद दस्तावेज़ थे उन्हें संलग्नक की तरह अपने कहे पर चस्पा करते हैं। यानी एक ऐसे समुदाय के लोगों को, जो हिन्दी के कवि अज्ञेय के अनुसार शहरों में बसना नहीं सीखे थे, जिन्होंने विष नहीं पाया था और जो डसना नहीं सीखे थे लब्बोलुआब यह कि जिसके पास झूठ बोलने की कोई कला और उसका अभ्यास नहीं था वो सच बोलने के लिए प्रमाण तलाशने लगा। सबसे दिलचस्प बात यह कि ऐसे बयान वो वायकती दर्ज़ करवा रहा था जिसके घर तक पहुँचने के लिए कोई सड़क नहीं है और वहाँ केवल पैदल ही जाया जा सकता है और जहां इतना घना जंगल है कि दिन शाम होने से पहले ढल जाता है।
कई बार तो ऐसा लगता है कि उनके सहज, स्वाभाविक जीवन को मान्यता देने के नाम पर उन्हें सबसे कुत्सित ढंग से मुख्यधारा में लाया गया और यह था उनकी मनोदशा को बदलना।
आदिवासियों के जीवन और उनके मुद्दे को दुनिया की नज़र में लाने वाले डॉ. बी. डी. शर्मा अक्सर एक वाकया सुनाते रहे और उनकी लिखी कई किताबों में वो दर्ज़ हैं। यह वाकया एक आदिवासी व्यक्ति का है जो किसी मामले में अदालत लाया गया। अदालत में बैठे न्यायधीश ने उसका बयान लेने से पहले सामान्य अदालती कार्यवाही के अनुसार उसकी कही बात का सबूत मांगा। जिस पर उस व्यक्ति ने कहा- मैं कह तो रहा हूँ। फिर भी जज साहब ने कहा कि -हम इसे क्यों सच माने? तुम जो कह रहे हो, उसके लिए कोई प्रमाण दरकार है। बिना प्रमाण दिये यह बात सच नहीं मानी जाएगी। इसके बाद उसने एक बार और जोर देकर कहा – जज साहब मैं कह रहा हूँ न। अब प्रमाण की क्या ज़रूरत है। फिर भी जब जज साहब नहीं माने तो वो अदालत से बाहर निकल गया।
उस मामले का क्या हुआ? या क्या ही हो सकता था? हम अच्छी तरह समझते हैं लेकिन यहाँ मामला एक आदिवासी व्यक्ति के कुछ कहने का था। जिसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी डिक्शनरी में झूठ नहीं था, उस जीवन में झूठ का अभ्यास नहीं था। आधुनिक और व्यवस्थागत सच्चाई तब तक झूठ माने जाने की है जब तक उस झूठ या सच के पक्ष में कोई प्रमाण न हो।
इस क़ानून के लागू होने के बाद यह शुरूआत में यह जो प्रमाण मांगे जाने की परिपाटी शुरू हुई उसने आदिवासियों को अधिकार सम्पन्न बनाने की बजाय औनिवेशिक चलन की नौकरशाही की गिरफ्त में ला दिया।
(लेखक पिछले 15 सालों से सामाजिक आंदोलनों से जुड़कर काम कर रहे हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।