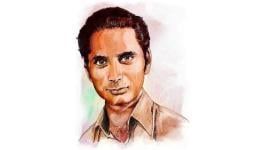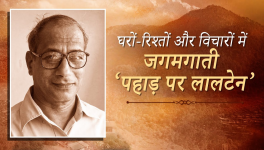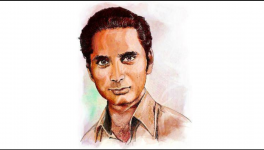बोलने में हिचकाए लेकिन कविता में कभी नहीं सकुचाए मंगलेश डबराल

एक बार ईएमएस नंबूदिरीपाद से किसी पत्रकार ने पूछा कि,`` डू यू आलवेज स्टैमर।’’ इस पर उनका जवाब था, `` नो ओनली व्हेन आई स्पीक।’’ ( `क्या आप हमेशा हकलाते हैं?’ `नहीं जब मैं बोलता हूं।’) मंगलेश जी से मिलते हुए मुझे नंबूदिरीपाद का यह कथन याद आ जाता था। मंगलेश जी जनसरोकारों और मानवीय संवेदना से लबालब भरे हुए कवि थे इसलिए कविता में हकलाने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर चूंकि गद्यः कविनाम निकषः वंदंति यानी गद्य किसी कवि की कसौटी होती है इसलिए वे गद्य कविता जैसा ही सुंदर लिखते थे। उसमें वही प्रवाह और धार होती थी जो कविता में थी। अब यह गद्य की ही सीमा है जो कविता जैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाता तो उसमें मंगलेश जी क्या करते।
मंगलेश जी के हकलाने का जिक्र इसलिए क्योंकि यह स्तंभकार भी बचपन में बहुत हकलाता रहा है। आज भी जब विचारों का प्रवाह तीव्र होता है और अभिव्यक्ति का माध्यम और उपकरण थके होते हैं तो वैसा ही होता है। लेकिन हमारा हकलाना कई बार हमारे संकोच और संयम का भी पर्याय होता है। कई बार वह हमारे शील के कारण भी होता है। हमारी पत्रकारिता आज जिस तरह 24 घंटे बकवास करती हुई जहर फैलाने में लगी है उससे तो यही अच्छा होता कि वह थोड़ा हकलाने लगती। अपनी वाणी और भाषा में थोड़ा संपादन करना और संयम रखना सीख जाती। वही संपादन और संयम जो मंगलेश डबराल जी अपनी पत्रकारिता से हमें दे गए हैं। अब इसके लिए उनका कोई दोष नहीं है कि हमारी पत्रकारिता उसे बचाकर नहीं रख पाई और गाली गलौज पर उतर आई है। मंगलेश जी का हकलाना खटकता नहीं था। लगता था कि सुंदर विचारों और भावों की सरिता पत्थरों से टकराकर कल कल निकल रही है। क्योंकि उनके भीतर न तो कचरा था और न ही जहर। वहां तो एक सुंदर संसार और मानवीय संबधों की कल्पना थी।
नवंबर में जब मेरे पूरे परिवार को कोरोना हुआ तो उनका फोन आया। धीरे धीरे सबका हाल चाल लिया। पूछा कौन सी दवा ले रहे हो। मैंने बताया कि आइवरमेक्टिन नाम की एक दवा, यह वही है जो बच्चों को कीड़ों के लिए दी जाती है। फिर पूछा कि क्या इसमें होम्योपैथिक दवा काम करती है, मैंने बताया कि वह भी सरकारी डाक्टरों ने भिजवाई है, अब देखते हैं क्या असर होता है। लेकिन इस बात का अनुमान नहीं था उनके बीमार होने पर मैं उनसे फोन पर बात करके उनका हालचाल नहीं ले पाऊंगा। सिर्फ मित्रों से उनकी खबर मिल पाएगी और आखिर में जो खबर मिली उसकी आशंका तो थी लेकिन दिल कहता रहता था कि नहीं मंगलेश जी लौट कर आएंगे और एक दिन सोसायटी के बाहर पान की दुकान पर या बिजेंद्र की दुकान पर थोड़ी बातचीत हो जाएगी। वैसा नहीं हुआ और हिंदी समाज के साथ ही गाजियाबाद में बसी जनसत्ता सोसायटी का एक मजबूत स्तंभ ढह गया।
बुद्धिजीवी के इसी चरित्र को परिभाषित करते हुए मंगलेश डबराल ने लिखा था, `` इटली के मार्क्सवादी चिंतक अंतोनियो ग्राम्शी ने `बुद्धि के निराशावाद और हृदय के आशावाद’ को मूलभूत या जैविक ----आर्गेनिक—बुद्धिजीवी की विशेषता के तौर पर चिह्नित किया था। मेरे समय के बहुत से कवियों की कविता इसी नाउम्मीदी और उम्मीद के दोनों सिरों को थामे हुए रही है और उदास नजरिए के बावजूद उसका दिल हमेशा आशावाद से लबरेज है। उसकी निराशा में जितनी अपने समय के यथार्थ की स्याह परछाइयां हैं, उसकी उम्मीद के भीतर उतना ही गहरा आवेग भरा हुआ है और इसी सामर्थ्य से वह एक तरफ मानवीय अस्मिता को उभारने का और बचाने का काम करती है और दूसरी तरफ मनुष्य के विरोध में किए जा रहे षडयंत्रों, उस पर होने वाले अन्यायों-अत्याचारों, भूमंडलीकरण और उसकी पूंजी का बर्बरताओं और सत्ता तंत्र के खिलाफ अपना प्रतिरोध भी जारी रखती है। उसमें बहुत कुछ खोने के एहसास की शिद्दत है तो बहुत कुछ बचाए रखने की चिंता भी।’’
अपनी पीढ़ी के जन सरोकार रखने वाले कवियों की ओर से दिया गया मंगलेश जी का यह बयान इस समय के रचनाशील लोगों का मौलिक कर्तव्य है। मंगलेश जी अपना वह मौलिक कर्तव्य निभा रहे थे लेकिन कितने लोग निभा रहे हैं या निभा पा रहे हैं यह सवाल हमारे समय का बड़ा सवाल है? पूंजी और धर्म के नापाक गठजोड़ से निकली आज की पतनशील और कलही राजनीति और उसे पोषित करने वाले साहित्य और पत्रकारिता ने किस बुद्धिजीवी और रचनाकार को संक्रमित नहीं किया है, यह पता लगाना मुश्किल है। हम दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम पत्रकारों और साहित्यकारों का एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट करा लें, वे सब संक्रमित मिलेंगे। मंगलेश जी कोविड के टेस्ट में जरूर निगेटिव नहीं हो पाए लेकिन सांप्रदायिक राजनीति का संक्रमण उन्हें छू नहीं गया था।
शासक वर्ग की शब्दावली में कहें तो वे `अवार्ड वापसी गैंग’ के सदस्य थे। उन्हें उसका न तो जरा भी खौफ था और न ही रत्ती भर मलाल था। बल्कि फक्र था। 2015 में जब पहली बार उनके घर जाकर इंटरव्यू लिया तो लगा कि वे `फासीवाद’ के बढ़ते खतरे को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। कभी कभी शाम को जब सोसायटी के भीतर टहलते हुए या बाहर खरीदारी करते हुए भेंट हो जाती थी तो मित्रों की बढ़ती सांप्रदायिक फिसलन पर दुखी होते और गुस्सा जताते थे। उनकी कविताएं ` अत्याचारियों की थकान’ `हत्यारा’ और `अत्याचारी के प्रमाण’ इस खौफनाक समय और उसके नायकों(खल) की खूब पहचान कराती हैं।
अत्याचार करने के बाद
अत्याचारी निगाह डालते हैं बच्चों पर
उठा लेते हैं गोद में
अपने जीतने की कथा सुनाते हैं
या फिर `हत्यारा’ कविता में वे कहते हैं---------
सेनाएं कट मरेंगी हत्यारा जीतेगा
हर बार जीतने के बाद
लाशों के बीच अकेला खड़ा
हत्यारा कहेगा
अब मैं जाता हूं बुद्ध की शरण में
इसी तरह `अत्याचारी के प्रमाण’ नामक कविता दमनकारी सत्ता के तर्कों और उसके हाव भाव का सटीक चित्रण करती हैः-
अत्याचारी के निर्दोष होने के कई प्रमाण हैं
उसके नाखून या दांत लंबे नहीं हैं
आंखे लाल नहीं रहतीं
बल्कि वह मुस्कुराता रहता है
अक्सर अपने घर आमंत्रित करता है
और हमारी ओर अपना कोमल हाथ बढ़ाता है
उसे घोर आश्चर्य कि लोग उससे डरते हैं
...
अत्याचारी इन दिनों खूब लोकप्रिय है
कई मरे हुए लोग भी उसके घर आते जाते हैं।
जाड़े की गुनगुनी धूप या रात में महकने वाले बेला की तरह सुगंध देने वाला मंगलेश डबराल का गद्य भी कम लुभावना नहीं है। उनका ढेर सारा पत्रकारीय लेखन और उनका यात्रा वृतांत ` एक बार आयोवा’ इसका प्रमाण है। इसके कुछ अंश आज के पत्रकारों और लेखकों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हिंदी छोटे वाक्यों की भाषा है और अगर आपके भीतर सौंदर्य की अनुभूति है तो आप सुंदर वातावरण को तो पकड़ेंगे ही अपनी भाषा को और भी सुंदर बनाएंगे। आयोवा नदी के किनारे बैठकर वे लिखते हैं, `` मेफ्लावर के सामने आयोवा नदी के किनारे एक पुरानी वीरान बेंच। मैंने इस पर कभी किसी को बैठे नहीं देखा। बारिश, बर्फ और पेड़ों के पत्ते ही इस पर बैठते हैं। धूप है। एक बड़ा सा बादल आसमान में आता है और लगता है जरा सा अटका हुआ है जैसे अभी अभी आसमान से गिर पड़ेगा। चेहरे पर धुंध एक ठंडे रूमाल की तरह चिपक गई है। आयोवा शांत बह रही है। दोपहर के सन्नाटे में जैसे इस शहर की इमारतें, सड़कें, चौराहे और पेड़ चुपचाप इस नदी में उतर गए हों। शांत जल में आराम करते हुए। मैं हालांकि थका हुआ नहीं हूं पर बेंच पर जाकर इस तरह बैठता हूं जैसे बहुत दूर से चलकर आया थकामांदा हूं।’’
अमेरिका में अपने काव्य पाठ के अनुभव पर टिप्पणी करते हुए इसी यात्रा वृतांत में वे कहते हैं, `` जब भी कहीं अपनी कविताएं पढ़ने जाता हूं तो लगता है किसी ऐसे विषय का इम्तेहान देने जा रहा हूं जो मुझे नहीं आता। एक घिग्घी सी बंधने लगती है। शायद हकलाने की अपनी आदत के बारे में भी सतर्क हो जाता हूं या शायद नर्वसनेस ही घुट्टी में मिली है। घबराहट की एक वजह और थी। वह यह कि अमेरिकी लोग हर सभा-गोष्ठी के अंत में बड़े उत्साह से तालियां बजाते हैं। ......अमेरिकी तालियां मुझे प्रायोजित किस्म की लगती हैं। जैसे किसी कंपनी के अध्यक्ष का भाषण देने पर बजती हैं। ....मेरी कविताओं में तो काफी उदासी और निराशा का आलम है। उदासी पर तालियां बजना तो हूट होना हुआ। मैं इसके लिए यहां नहीं आया।’’
अपने समाज और दूर के समाज के बारे में गहरी समझ और संवेदना रखने वाले मंगलेश डबराल से पहली बार 1982 में लखनऊ में भेंट हुई थी। उस समय हम लोग युवा थे और कविता, विचार गोष्ठी, क्रांतिकारी साहित्य पढ़ते हुए क्रांति के सपने देखते थे। लखनऊ की साम्यवादी, समाजवादी, गांधीवादी सर्कल के साथ रचनाकारों के साथ भी उठना बैठना होता था। विश्वविद्यालय से काफी हाउस और फिर कभी इंदिरा नगर तो कभी पेपर मिल कालोनी में अड्डेबाजी होती थी। हम पांच कवि मित्रों पुनीत टंडन, चंद्रपाल सिंह, हरिजिंदर सिंह साहनी, अनूप श्रीवास्तव के साथ हजरतगंज में स्थित तत्कालीन सूचना विभाग के प्रेमचंद कक्ष में काव्यगोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में रणवीर सिंह बिष्ट, कृष्ण नारायण कक्कड़, वीरेंद्र यादव, मुद्रा राक्षस जैसे प्रसिद्ध कवियों और रचनाकारों के अलावा मंगलेश डबराल जी भी आए थे। मेरी कविता से प्रसन्न हुए और बोले कि मुझे अपनी कविताएं देना मैं अमृत प्रभात में प्रकाशित करूंगा। तब वे अमृत प्रभात में रविवारी परिशिष्ट के संपादक थे। यह घटना उनके दिल्ली आने से एक साल पहले की है। उन्होंने मेरी चार कविताएं छापीं।
उसके पांच छह साल बाद जब मैं दिल्ली जनसत्ता से जुड़ा तो उनसे धीरे धीरे पुराने परिचय का नवीकरण किया। लेकिन दिल्ली एक समुद्र की तरह से था और रविवारी जनसत्ता में छपने में समय लगा। पर मंगलेश जी ने मेरी कई कवर स्टोरी छापीं। उनके बेजोड़ संपादन और विषय के चयन ने जनसत्ता को न सिर्फ एक नई पहचान दी बल्कि हिंदी के पाठकों को वही संस्कार दिया जो इससे पहले धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय दे रहे थे। मेरा मानना है कि अगर जनसत्ता में मंगलेश डबराल जैसे भाषा शिल्पी न होते तो उसकी पत्रकारिता एकांगी रहती और प्रभाष जी हिंदी समाज पर वह धाक न जमा पाते जो उन्होंने जमाई।
मंगलेश जी में बहुत सारी कलाएं थीं और विद्वता भी। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी उनकी शालीनता। कभी पायनियर के प्रसिद्ध संपादक एस. एन. घोष ने हम लोगों से कहा था कि पत्रकार की कलम खुली रहनी चाहिए और जुबान बंद रहनी चाहिए। हालांकि 24 घंटे वाले टेलीविजन के आने के बाद पत्रकारों को जिस तरह बोलने का अतिसार हुआ है उसने उस संयम के सुझाव को पलट कर रख दिया है। फिर भी अगर उसका मतलब संयम और सुसंपादित वचन उचारने से है तो वह मंगलेश जी में था। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि वे एक बहुत अच्छे मनुष्य थे जो गेट पर तैनात गार्डों से व सिगरेट वाले और परचून वाले से घंटों बात कर सकते थे। आज वे सब उन्हें बहुत मिस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका नश्वर शरीर गया है लेकिन उनकी कृतियां हमारे बीच हमेशा रहेंगी। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर उनकी सारी कृतियां नष्ट हो जाएं और वही स्वभाव लेकर वे फिर हमारे बीच आ जाएं तो समाज के संवेदनशील और मानवीय होने की संभावना प्रबल हो जाएगी।
(लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
इन्हें भी पढ़ें : स्मृति शेष: वह हारनेवाले कवि नहीं थे
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।