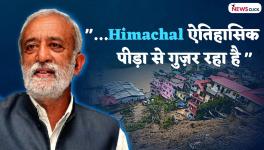जीवन सुगमता सूचकांक का फ़ालतू का मायाजाल
ओ देल्ही माहरा पाहड़ रा शिमला, माहरा देस रा दिल, ओ देल्ही, माहरे देशा रा दिल शिमला (ओ दिल्ली, पहाड़ों का दिल शिमला है, ओ दिल्ली, हमारे देश का दिल भी शिमला है, यह एक लोकप्रिय गीत है)। यह पहाड़ी लोकबोली में गाया जाने वाला एक ऐसा लोकप्रिय गीत है, जिसे लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में गाया जा रहा है।
यह गीत इस बात को दर्शाता है कि शिमला शहर हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों के लिए कितना प्यारा है। देश में दस लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ‘ईज़ ऑफ़ लिविंग इंडेक्स’ (EoLI) के लिहाज़ से सबसे ख़ासियत वाला यह शहर कभी बेहद शानदार हुआ करता था। जो शख़्स कभी वहां रह चुका हो और पांच साल तक डिप्टी मेयर होने के नाते इस शहर की सेवा कर चुका हो, उसका दिल कभी ख़ुशी और गर्व से भर जाता था, लेकिन अब मन ऐसा नहीं मानता, क्योंकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मन के किसी कोने में टीस सी उठती है।
इसकी वजह है और वह यह है कि जिस तरह कोविड-19 महामारी आदि का अनुभव रहा, उससे तो ख़ुद शिमला में रहने वाले यह मानने को तैयार नहीं कि उनके पास देश में रहने का सबसे सहूलियत देने वाली जीवनशैली है या फिर, यह भी हो सकता है कि नयी रैंकिंग से यह पता चलता हो कि हमारे देश के शहरों का किराया कितना ज़्यादा है-अगर शिमला सबसे अच्छा है, तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कि लोग यहां कैसे रहते हैं और बाकी लोगों की आजीविका कैसी है।
इसी शहर से आने वाले स्थानीय मंत्री को भी इस पर यक़ीन नहीं होता और उन्होंने अफ़सरों से विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह दिया है। इसे लेकर कई लेख लिखे गये हैं, जिनमें शहर के मशहूर इतिहासकार और लेखक, राजा भसीन का एक क्षेत्रीय अख़बार में लिखा वह लम्बा लेख भी शामिल है, जिसमें इस पूरे क़वायद पर सवाल उठाया गया है। जब मैंने बेंगलुरु में रहने वाले कुछ लोगों से बात की तब उन्हें भी ‘दस लाख से ज़्यादा आबादी’ वाली श्रेणी वाले देश के शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किये जाने पर अचरज हुआ।
आख़िर ऐसा क्यों है कि शहर को लेकर लोगों की जो समझ है और ईओएलआई के डेटा से जो छवि सामने आती है, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं? वैसे, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम कारणों में से एक कारण तो यही है कि इस क़वायद का हिस्सा बने नागरिकों के सर्वेक्षण ने ईओएलआई के घालमेल को उजागर कर दिया है। जिन शहरों को इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था, वे नागरिकों के सर्वेक्षण में इतने अच्छे स्थान नहीं थे।
इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद जहां तक लोगों के इन शहरों से लौट जाने का सवाल है, तो इस लिहाज़ से ये सबसे जीवंत शहरों / स्मार्ट सिटीज़ (ज़ाहिरा तौर पर शीर्ष 10 में से ज़्यादातर को स्मार्ट शहरों के रूप में नामित किया गया है) के हालात सबसे ख़राब थे। तो ऐसे परिदृश्य को ईओएलआई के लिहाज़ से उच्च सूचकांक कैसे कहा जा सकता है? उदाहरण के लिए, शिमला में एक विधायक को यह सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर बैठना पड़ा था, ताकि ग़रीबों और प्रवासी श्रमिकों को राशन ठीक से वितरित किया जा सके। ऐसे में ईओएलआई की सूची में शीर्ष पर पहुंचना निश्चित रूप से चकित करने वाली बात थी।
इसी तरह, इस पहाड़ी शहर में लोगों के एक बड़े हिस्से की आजीविका का प्रमुख स्रोत पर्यटन है, जहां हर साल तक़रीबन 4. 5 मिलियन पर्यटक आते हैं। हालांकि, महामारी और इसकी वजह से लगने वाले लॉकडाउन ने पर्यटन क्षेत्र को तबाह कर दिया और इससे बड़े पैमाने पर रोज़गार का नुकसान हुआ। आख़िर इसे जीवन जीने में सहूलियत (ईज़ ऑफ़ लीविंग) वाली स्थिति कैसे कहा जा सकता है? इसके अलावे, इस हक़ीक़त के बावजूद कि खाने-पीने के तमाम कारोबार बंद थे, शिमला नगर निगम ने इनसे जुड़े प्रतिष्ठानों की सफ़ाई पर हज़ारों रुपये के बिल बना दिये। ऐसे में स्थानीय आबादी के लिए यह तमाम बातें समझ से परे थी कि आख़िर उन्हें किस तरह की सर्वेश्रेष्ठ 'सहूलियतें' हासिल हैं!
आइये, हम समझें कि यह ईओएलआई आख़िर है क्या। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 4 मार्च, 2021 को भारत में 111 शहरों का ईज़ लिविंग से जुड़ा एक "मज़ेदार" सूचकांक जारी किया था। उस सूची के मुताबिक़, जनवरी 2020 से 20 मार्च 2020 की अवधि में दो तरह की श्रेणियों वाले शहरों को शामिल किया गया था; ये श्रेणियां थीं- एक लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर और दूसरे उससे कम आबादी वाले शहर। ईओएलआई के शब्दजाल के मुताबिक़, शहरों का मूल्यांकन चार आधारों पर किया गया था (i) शहरों में जीवन की गुणवत्ता, (ii) शहरों की आर्थिक क्षमता, (iii) वहनीयता और (iv) नागरिक धारणा सर्वेक्षण।
इसके बाद, आगे मूल्यांकन के लिए 13 श्रेणियां निर्धारित की गयी थीं, जिनमें शामिल थे- शिक्षा; स्वास्थ्य; आवास और आश्रय; WASH (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा) और SWM (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन); सुरक्षा संरक्षण; मनोरंजन; आर्थिक विकास; आर्थिक अवसर; वातावरण; हरित स्थान; ऊर्जा की खपत; और शहर का लचीलापन। ईज़ ऑफ़ लीविंग यानी जीने में सहूलियत का मूल्यांकन करने के लिए 49 और घटकों को शामल किया गया था।
ईज़ ऑफ़ लीविंग है क्या ?
हालांकि, एक शब्दावली के तौर पर 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' शहरी नीति और प्रोग्रामिंग में व्यापक रूप से तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है। किसी के लिए, यह बुनियादी तौर पर पानी की आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्क और हरित स्थान, आदि जैसे भौतिक सुविधाओं से जुड़ा है, तो किसी के लिए यह सांस्कृतिक पेशकश, करियर के अवसरों, आर्थिक गतिशीलता या सुरक्षा से सम्बन्धित है।
यह हमारे शहर की सामूहिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। द आर्ट ऑफ़ सिटी मेकिंग में चार्ल्स लैंड्री एक ऐसे शहर की दिलचस्प परिभाषा देते हैं, जिसमें इस प्रकार के ईज़ ऑफ़ लिविंग शामिल है:
"शहर एक बहुआयामी इकाई होता है"। यहा आर्थिक ढांचा वाली एक अर्थव्यवस्था होती है; यह समुदायों से बना एक समाज होता है; यह मानवीय शिल्प से डिज़ाइन किया गया एक परिवेश होता है; और यह एक पारिस्थितिकी तंत्र वाला एक प्राकृतिक वातावरण होता है।
और यह इन चारों, यानी अर्थव्यवस्था, समाज, शिल्प और पारिस्थितिकी तंत्र नियमों के उस निर्धारित समूह से संचालित होते हैं, जिसे शासन व्यवस्था कहते हैं। हालांकि, इसका आंतरिक इंजन या संचालित करने वाली ताक़त इसकी संस्कृति होती है। संस्कृति, यानी ऐसी चीज़, जिसे हम अहम मानते हैं, मान्यतायें और आदतें शहरों को ख़ासियत देती है और इस ख़ासियत में इसकी ख़ुशबू, स्वर और छाप होती है।”
किसी शहर को परिभाषित करने के कई ऐसे दूसरे तरीक़े होते हैं, जहां लोगों के पास बेहतर जीवन, आजीविका और रचनात्मकता होती है।
शहर की एक अन्य अवधारणा ऐसी है, जिसमें फ़ैसला लेने में उसके नागरिकों की भागीदारी होती है। लेफ़ेब्व्रे द्वारा प्रतिपादित और डेविड हार्वे द्वारा इमज़बूती से की गयी वक़ालत वाले "राईट टू सिटी" के सिद्धांत में उन चीज़ों को लेकर फिर से दावा करना है, जो न सिर्फ़ भौतिक होती हैं, बल्कि शहरों में नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, जो उस विशाल अधिशेष से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, जो शहरों में पूंजी के उत्पादन और पुनरुत्पादन और इसके लोकतंत्रीकरण में सृजित होती है।
शहरों में भागीदारी और ‘संभावनाओं में हिस्सेदारी’ को याद दिलाने के लिहाज़ से 18 मार्च से शुरू होने वाली पेरिस कम्यून की 150 वीं वर्षगांठ मनाने से बेहतर मौक़ा भला और क्या हो सकता है। यहां के श्रमिक इस शहर को उस मुकाम और कल्पनाशील विधि निर्माण तक ले आये थे , जो इस बात की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है कि विश्व नागरिकों की आकांक्षा वाले किसी ‘शहर को कैसा होना चाहिए’, यह स्थिति आज के सिलसिले में भी सच है। यहां शिक्षा मुफ़्त कर दी गयी है, बाल श्रम को ख़त्म कर दिया गया है, प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को लेकर काम किया गया है और संकट के दौरान किराये में छूट दी गयी है।
इस ईज़ ऑफ़ लिविंग के लिहाज़ से कई कारणों में से एक कारण “किराये में छूट” ख़ासकर तब सबसे अहम हो जाता है, जब महामारी की चपेट में लोग आ जाते हैं, महामारी के दौरान अमेरिका ने भी यह छूट अपने नागरिकों को दी थी। भारत में इस तरह की पेशकश का कोई फ़ैसला तक नहीं किया गया था और कोई भी शहर इस तरह के फ़ैसले की कल्पना भी नहीं कर सकता था।
लेकिन, सच है कि इस तरह की चीज़ें शहरों में रह रहे लोगों के जीवन को आसान बना देती हैं। क्या जो तरीक़े अपनाये गये, शहरों की इस कल्पना को धरातल पर उतारने में सक्षम थे ? इसका कोई साकारात्मक जवाब नहीं है। जिन कारणों का हवाला दिया जा सकता है, उनमें से एक कारण यह है कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले यह क़वायद 20 मार्च, 2020 तक ख़त्म हो गयी थी। अगर ईओएलआई आकलन के अहम घटक में यह लचीलापन और स्थिरता नहीं होता है, तो यह पूरा आकलन ही ग़लत होगा और अगर इन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इन शब्दों का कोई मायने नहीं रह जाता है, बल्कि यह शब्दाली महज़ शब्दजाल बनकर रह जाती है।
व्यक्तिनिष्ठता से संचालित होती फ़ैसला करने की प्रक्रिया
आवास और शहरी मामले के मंत्रालय और स्पर्धा संस्थान (IFC) सलाहकार, दोनों सरकारी संस्थाओं की व्यक्तिनिष्ठता ने इस 'ईज़ ऑफ़ लिविंग इंडेक्स' को लेकर लिये जाने वाले फ़ैसले की क़वायद की थी।
सरकार मानती है कि शहर "विकास का इंजन" होता है और शहर की योजना और प्रक्रियाओं को आकार देने के पीछे इस प्रतिस्पर्धा का हाथ होता है। शहरों को उद्यमियों की तरह देखा जाता है और जो-जो शहर ऊपर बताये गये दो मानदंडों पर खड़े उतरते हें, वे मंत्रालय के सबसे ज़्यादा आंखों के तारे होते हैं। स्वतंत्र माने जाने वाले XV FC (15 वें वित्त आयोग) सहित सरकार के विभिन्न दस्तावेजों से होकर गुज़रने वाले ये मानदंड हालांकि उसी सिद्धांत की वकालत करते हैं, जिसमें शहरों को बिना सशक्ति किये उन्हें ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक स्थानों में बदल दिया जाता है, जिसके दो आधार होते हैं-उत्पाद और सेव शुल्क और आर्थिक स्थिरता।
इसी तरह, आईएफ़सी, सलाहकार कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसकी हक़ीक़त ढकी-छुपी हो। इस समूह के संस्थापक और अग्रदूत, माइकल पोर्टर अपने लेखों और वेबसाइट पर अपलोड किये जाने वाले अपने वीडियो में मुखर होकर कहते हैं कि इस संस्थान का मक़सद शहरों में "पूंजीवाद को मज़बूती देना" है। ख़ास तौर पर अमेरिकी लोग शहरी शासन के रूप में जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वह है-मुक्त बाज़ार वाला पूंजीवाद और
चुनाव अभियान में बर्नी सैंडर्स के सुझाये वह विकल्प, जो पोर्टर के लिए बहुत बड़े चिंता का विषय है। इस तरह, इस समूह के पास जो अहम कार्य है, वह है-पूंजीवाद के मूल्यों को मज़बूती देना, यानी उससे सम्बन्धित जानकारी पर सलाह देना। और इस विचार की सीमा इस बात से जानी जा सकती है कि यह विचार कॉरपोरेट के लोक-कल्याण की भावना से लेकर सीएसआर कार्यक्रम तक, बल्कि इसके भी आगे तक जाता है।
इसलिए, ख़ास तौर पर इस सरकार और सलाहकार का ईओएलआई के लिए चुने जाने के पीछे के कारण की हक़ीक़त किसी से छुपी हुई नहीं है। वास्तव में यह उन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के शासनादेश के विरोध में जाता है, जिन्हें ईओएल सूचकांक पर काम करते समय शामिल किया जाना चाहिए।
क्विटो में यूएन हैबिटेट III के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक, जॉन क्लॉस उस बैठक की याद दिलाते रहे, जिसका मैं भी एक हिस्सा था और जिस बैठक में योजना की मूल बातें पर फिर से अमल करने और लाईसेज़-फैयर (मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था) से पीछा छुड़ाने को शहर के विकास का तरीक़ा बताया गया था। यह न सिर्फ़ इस मायने में बेहद ख़ास है कि इसके ज़रिये बड़े-बड़े बहुराष्ट्रीय व्यापारिक समूहों के हितों को सुरक्षित किया जाता है, बल्कि इससे लोगों के बीच की खाई भी चौड़ी होती है और शहर के विस्तार को बेहद अतार्कित बना देता है। हालांकि, लोगों और आम तौर पर उनकी आजीविका का हो रहे भारी नुकसान पर ध्यान दिये बिना हम भारत में शहरों को आर्थिक गतिविधियों और व्यवसाय को प्रेरित करने वाले तत्व के रूप में देखते रहे हैं। कम से कम यह ‘ईज़ ऑफ़ लिविंग’ का सुरक्षित तरीक़ा तो नहीं है।
फिर सवाल उठता है कि ईओएल के इस सूचकांक में जिन शहरों को लक्ष्य बनाया गया है, उनके लिए क्या-क्या हैं। बहुत से लोग, ख़ासकर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA), सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) जैसे शहरी विशेषज्ञ समूह से जुड़े हुए हैं, वे खुलकर तो कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन जब उनसे निजी तौर पर पूछा जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया की साफ़-साफ़ आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि इस पूरी क़वायद का आख़िरी मक़सद इन शहरों में दाखिल हो रहे उन बड़े-बड़े कॉर्पोरेटों को यह सुझाव देना है कि शीर्ष रैंकिंग वाले ये शहर, ख़ासकर सुविधाओं से लैस स्मार्ट सिटी निवेश के लिहाज़ से सबसे अच्छी जगह हैं। चूंकि यह पूरी क़वायद आंकड़ों से संचालित होती है, और ज़्यादातर निवेश, कमांड
सेंटर बनाने और इसी तरह की बाक़ी चीज़ों भी इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे में इस तरह की रैंकिंग इन टेक-कंपनियों को अपने निवेश को लेकर स्पष्ट दृष्टि अपनाने में मदद करती हैं।
लेकिन, इसकी एक विडंबना भी है और वह यह कि नागरिक सर्वेक्षण में नागरिकों की आकांक्षाओं और यहां तक कि उन आकांक्षाओं के संकेतों की अनदेखी करते हुए सरकार शहरों की ऐसी व्यक्तिपरक समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। कोई शक नहीं कि मंत्रालय और इसके
सलाहकार द्वारा इस लिविंग इंडेक्स का ढांचा जिस तरह से तैयार किया गया है, उससे तो यही लगता है कि इसका मक़सद किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है। इससे तो यह संस्था या इसके सलाहकार, दोनों ही
लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पायेंगे। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस बड़े मायाजाल के बजाय, स्थानीय अनुभव के आधार पर आसान तरीक़े भी अपनाये जा सकते थे।
लेकिन, जिस वजह से ये आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं, उस पर विचार किया जाये, तो सवाल उठता है कि क्या ये आंकड़े शहरों में रह रहे लोगों की कल्पनाओं और आकांक्षाओं को पकड़ पाने में सक्षम है या फिर कुछ बड़े कॉर्पोरेटों के लिए काम आने वाले हैं, जो किसी निवेश स्थल के रूप में
शहरों पर नज़र गड़ाये हुए हैं ? इसके बजाय, एक साधारण सी बात, जो मंत्रालय को करनी चाहिए, वह यह कि शहर की सरकारों और वहां रह रहे लोगों को उन तरीक़ों और प्रणालियों को विकसित करने के लिहाज़ से सशक्त बनाया जाये, जहां उन्हें लगे कि शहर का स्वामित्व उनके हाथों में है और उन्हें महसूस हो कि वे अलग-थलग नहीं हैं।
(लेखक शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर हैं। इनके विचार निजी हैं।)
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें
https://www. newsclick. in/The-Unnecessary-Jargon-Ease-of-Living-Index
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।