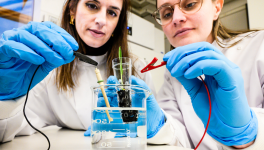कृषि उत्पाद की बिक़्री और एमएसपी की भूमिका

जैसा कि हम सबको पता हैं कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था के सभी मोर्चों पर उठाये गये कई सकारात्मक क़दमों के नतीजे के तौर पर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि से जुड़ी क्रांतियां हुई हैं। इसक नतीजा यह हुआ है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न फ़सलों और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों की उत्पादकता और उत्पादन में अविश्वसनीय बढ़ोत्तरी हुई है। स्वाभाविक रूप से इन उत्पादों का विपणन एक समय में भारतीय कृषि का एक अहम मसला बन गया। उत्पादों की ख़रीद-फ़रोख़्त को सुविधाजनक बनाने में इस विपणन प्रणाली ने अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के कामकाज, आर्थिक विकास, लोगों के हित को बढ़ावा देने आदि जैसे कई मामलों में अहम भूमिका निभायी है।
हालांकि, कृषि उत्पादों के विपणन की प्रणाली में कुछ गंभीर क़िस्म की कमियां थीं, मसलन i) अपर्याप्त भंडारण, ii) परिवहन के अपर्याप्त साधन, iii) अपर्याप्त ऋण सुविधायें, iv) ग्रेडिंग और मानकीकरण की कमी, v) बाज़ार की जानकारी का नहीं होना, vi) एक बड़ी संख्या में बिचौलियों की मौजूदगी के चलते ख़रीद-फ़रोख़्त में कदाचार और vii) संस्थागत विपणन की अपर्याप्तता। इसके नतीजे बहुत कम आय, मामूली प्रोत्साहन, कम विपणन योग्य अधिशेष, खेती में नये प्रयोग में बाधा और योजना बनाने में कठिनाइयां के रूप में सामने आते रहे हैं।
उत्पादकता और उत्पादन में इस तरह की क्रांतिकारी बढ़ोत्तरी को लेकर देश में अच्छे बाज़ार के बुनियादी ढांचे और कृषि उत्पादों की उचित मूल्य नीति की ज़रूरत थी ताकि किसान उचित मूल्य पर अपना उत्पाद बेच सकें। कृषि के नज़रिये से समृद्ध राज्यों में ही नहीं ,बल्कि तक़रीबन सभी राज्यों में उन्नत विपणन सुविधाओं वाले मंडियों और कृषक बाज़ारों की स्थापना के लिए क़दम उठाये गये। जहां-जहां ज़रूरी लगा, राज्यों ने अपनी पहल के साथ क़ानून बनाकर यथासंभव सर्वोत्तम बाज़ार सुविधायें मुहैया करायीं। 1970 के दशक में विभिन्न राज्यों में कृषि बाज़ारों को मार्केट यार्ड और अन्य बुनियादी सुविधाओं वाले विनियमित बाज़ारों के रूप में संचालित किया जा रहा था।
इस सदी की शुरुआत में यूपीए सरकार ने कृषि पैदावार के विपणन में सुधार लाने की ज़रूरत को महसूस किया। भारत सरकार ने राज्य कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2003 नामक एक मॉडल क़ानून तैयार किया और राज्यों से अनुरोध किया कि वे उसके आधार पर क़ानून बनाकर ज़रूरी सुधार करें। ज़्यादतर राज्यों ने उसी मॉडल अधिनियम के आधार पर सुधार किये, और कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMC) को निर्धारित क्षेत्राधिकार के साथ संचालित करने के लिए गठित किया गया। देश के अन्न भंडार के रूप में जाने जाते पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मंडी या कृषक बाज़ार के नाम से एपीएमसी बाज़ार संचालित करते हैं। पंजाब और हरियाणा की मंडियां तो इतनी मशहूर हैं कि पड़ोसी राज्यों-यूपी और राजस्थान के किसान भी इन बाज़ारों में कृषि उत्पादों से भरे ट्रक और ट्रैक्टर के साथ यहां आते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी 307 और तमिलनाडु में 277 एपीएमसी विपणन समितियां हैं, जो लंबे समय से काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने तब से 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के आरकेवीवाई फ़ंड के साथ 186 बाज़ार भवनों, यार्ड और दूसरे बुनियादी ढांचे का निर्माण का काम पूरा कर लिया है। हालांकि, इनमें से कुछ ने ही पूर्ण क्षमता से संचालन का काम शुरू कर पाया है। असल में इन सभी राज्यों ने भारत सरकार के आरकेवीवाई और सहकारी निधि की मदद से अपने-अपने विपणन ढांचे को मज़बूत कर लिया है। ग़ौरतलब है कि देश में इस समय 3,67,70,637 मीट्रिक टन खाद्यान्न की कोल्ड स्टोरेज क्षमता है।
बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यक्रम के साथ-साथ भारत सरकार ने किसानों को सुरक्षा मुहैया कराने और क़ीमतों में आती तेज़ गिरावट का सामना करने से बचाने के लिए एमएसपी तय करके बाज़ार के हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। एमएसपी सरकार की ओर से परिकल्पित मूल्य नीति का प्रमुख घटक बन गया। इस तरह, कृषि मूल्यों को लेकर सरकार की नीति को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित निर्धारित उद्देश्यों के साथ अपनाया गया है:
1.उत्पादक को यह आश्वासन देते हुए उत्पादन को प्रोत्साहित करना कि उत्पाद की क़ीमतें एक निश्चित न्यूनतम मूल्य से नीचे नहीं गिरेंगी।
2.कृषक समुदाय के प्रासंगिक आय स्तरों को सुनिश्चित करना, कृषि और ग़ैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की उचित शर्तों पर ज़ोर देना।
3.क़ीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोककर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
4.कृषि क्षेत्र और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में क़ीमत की स्थिति में निश्चितता लाने के लिए मूल्यों की स्थिरता को सुनिश्चित करना।
इसके लिए इस्तेमल किये जाने वाले उपाय हैं: i) एमएसपी और ख़रीद मूल्य, जो कि उत्पादकों को उत्पादन की अधिकता की स्थिति में न्यूनतम समर्थन की गारंटी देते हैं, ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मूल्य निर्गम, और iii) बफ़र-स्टॉक संचालन के ज़रिये क़ीमतों को बनाये रखना।
इस सरकारी नीति ने 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की स्थापना के साथ ही एक ठोस आकार ले लिया । आयोग के विचारार्थ विषय 'कृषि उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत देने की ज़रूरत के लिहाज़ से कृषि मूल्य नीति और मूल्य संरचना पर निरंतर सलाह' देना था। 'अर्थव्यवस्था की समग्र ज़रूरतों के लिहाज़ से एक संतुलित और एकीकृत संरचना विकसित करने' पर ज़ोर था। जहां ज़रूरी था,वहां आयात से पूरक उपर्युक्त उपायों को लागू करने के ज़रिये लागू की गयी इस मूल्य नीति ने एक अच्छी तरह से निर्धारित स्वरूप के रूप में काम किया है, जहां एमएसपी ने अहम भूमिका निभायी है।।
नीति का मूल्यांकन:
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ख़रीद मूल्य और निर्गम मूल्य के मूल्य घटक, उत्पादन, अधिशेष (ख़रीद मूल्य) हासिल करने और वितरण या उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने (निर्गम मूल्य) पर वहन किया गया है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसी ख़रीद एजेंसियों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों ने इस मूल्य नीति के कार्यान्वयन में सहायता पहुंचायी है। इसके असर में से एक असर यह रहा है कि कृषि उत्पादों की क़ीमतें ग़ैर-कृषि उत्पादों की क़ीमतों के मुक़ाबले तेजी से बढ़ी हैं। 1965-66 (पूर्व-सीएसीपी) और 1974-75 (सीएसीपी के बाद की अवधि) के बीच कृषि उत्पादों की अनुमानित क़ीमत वृद्धि 9.54%,ग़ैर-कृषि उत्पादों के मुक़ाबले 7.84% तेज़ थी।
इसके अलावा, कृषि उत्पादों की क़ीमतों में वृद्धि की दर में अंतर आयोग के बाद की अवधि में 5.56% ज़्यादा रहा है, जो 1955-56 से 1964-65 तक की आयोग पूर्व अवधि में 4.13% था। औद्योगिक मूल्यों के मुक़ाबले कृषि मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि की यह प्रवृत्ति 1980 और 1990 के दशक में प्रचलित थी। विनिर्माण मूल्य सूचकांक के प्रतिशत के रूप में कृषि मूल्य सूचकांक 1982-83 में 103.7 से बढ़कर 1990-91 में 108.5 और 2000-01 में 115.5 और 2003-04 में 116.8 हो गया।
हालांकि, व्यापार के लिहाज़ से यह प्रभाव मिश्रित रहा है। यह साठ के दशक के मध्य में कृषि के अनुकूल था। लेकिन, सत्तर के दशक के मध्य से विनिर्मित उत्पादों के 150 के स्थान पर कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक 100 बढ़ गया। कृषि और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य सूचकांक का अनुपात 1977-78 में 97.5, 1978-79 में 95.8 और 1979-80 में 87.6 था। हालांकि, इस प्रवृत्ति को 1980 के दशक में कुछ उतार-चढ़ाव के साथ 104-114 की सीमा में उलट गया था। यह अनुकूल कृषि प्रवृत्ति 1990 के दशक में स्थिर हो गयी, जो 2000-01 में बढ़कर 116 हो गयी।
जहां तक क़ीमतों में स्थिरता का सवाल है, तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के चलते अल्पावधि क़ीमतों में उतार-चढ़ाव आया है। आम तौर पर चावल, ज्वार, बाजरा और मूंगफली की कटाई के समय क़ीमतें सबसे कम रही हैं, जिसका एक हिस्सा नक़दी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संकटपूर्ण बिक्री के अधीन है और उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (55% से 74%) पर्याप्त ऋण और भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता के चलते फ़सल के छह महीने के भीतर ही बेच दिया जाता है। मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव गेहूं जैसे उत्पादों के मामले में किसी स्तर तक इसलिए सीमित थे,क्योंकि उत्पादक धनी थे और उनके पास उत्पाद को सुरक्षित रखने और बेहतर वित्तीय/भंडारण की अच्छी ख़ासी क्षमता थी। पर्याप्त मूल्य समर्थन नहीं मिलने से दलहन और तिलहन जैसी फ़सलों को नुकसान हुआ है। मध्यम अवधि की क़ीमतें कई सालों से कई उच्च उत्पादकता वाली क़िस्मों की फ़सलों में निवेश/तकनीकी सुधार में सहायक रही हैं। गेहूं की ऊंची क़ीमतों के चलते भूमि पर दूसरे फ़सलों के मुक़ाबले गेहूं की फ़सल पैदा करने की प्रवृत्ति ज़ोर पकड़ने लगी है।
ऐसा देखा गया है कि ग़ैर-मूल्य और मूल्य से जुड़े कारकों की वजह से फ़सलों के उत्पादन में होने वाली बढ़ोत्तरी ने सरकारी खाते में ख़रीदे गये विपणन योग्य अधिशेष में योगदान दिया है। 1965 में ख़रीद शुद्ध उत्पादन का महज़ 5% था, जो उत्पादन में वृद्धि और आकर्षक ख़रीद क़ीमतों के चलते बढ़कर 16% हो गया। मूल्य नीति ने उत्पादन बढ़ाने, फ़ायदेमेंद फ़सलों के पक्ष में फ़सल के स्वरूप को बदलने और ऊंची क़ीमतों से किसानों की आय को बढ़ाने में मदद की है। उपभोक्ताओं को भी उस निर्गम मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों के ज़रिये पीडीएस के संचालन से लाभ हुआ है, जो बाज़ार मूल्य से कम है।
सतत आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी, बढ़ते शहरीकरण आदि जैसे कारक गेहूं और मोटे अनाज और चावल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों से फल, सब्ज़ियां, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली उत्पादों, मांस जैसे ऊंची क़ीमत वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के पक्ष में खपत के स्वरूप में बदलाव का कारण बना। यह इस सदी की शुरुआत थी। उपर्युक्त कारकों के साथ-साथ ढांचागत विकास, हरित क्रांति के घटते प्रभाव और उदारीकरण ने कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को रफ़्तार दे दी। ऊंचे मूल्य वाले कृषि उत्पादों के बढ़ते निर्यात (1980 में अमेरिकी डॉलर में 430 मिलियन रुपये की जगह 2000 में 1415 मिलियन रुपये) ने भी इस विविधीकरण प्रक्रिया का इस्तमाल किया।
बदलते कृषि परिदृश्य ने कृषक समुदाय और नीति निर्माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद और उत्पादन के व्यवहारिक स्वरूप की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह के अहसास के साथ नीति निर्माताओं ने विविधीकरण पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया और उच्च मूल्य वाले उत्पादों को एमएसपी कवरेज के तहत लाया गया। शोधकर्ताओं के विभिन्न वस्तुओं के हिस्से के रूप में कृषि विकास के स्रोतों के विश्लेषण से साफ़ है कि इस मूल्य नीति ने कृषि क्षेत्र की मदद की है।
पीके जोशी के किये गये ऐसे ही अध्ययनों में से एक (संदर्भ 'क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन इन इंडिया: नेचर, पैटर्न एंड ड्राइवर्स', एग्रीकल्चर,फ़ूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट,वॉल्यूम 3, एशियन डेवलपमेंट बैंक) कारकों के उस सापेक्ष महत्व को समझने में मदद कर सकता है, जिसने कृषि विकास में योगदान दिया। यह अध्ययन 20 सालों तक चला और इसकी अध्ययन अवधि मुख्य रूप से दो कारणों से दो दशकों,यानी 1980-81 से 1989-90 और 1990-91 से 1999-2000 में विभाजित था।ये दो कारण थे - i) हरित क्रांति का प्रभाव 1980 के दशक के अंत से फीका पड़ने लगा था और ii ) दूसरी पीढ़ी का वह कृषि सुधार 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जो कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के नियमों की स्थापना के साथ मेल खाता था। भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर इस अध्ययन ने अध्ययन अवधि के दौरान कृषि विकास पर क्षेत्र, उपज, मूल्य और विविधीकरण के प्रभावों का पता लगाया। यह पता चला कि 1990 के दशक में सभी अनाज (चावल और गेहूं का एमएसपी और फलों और सब्ज़ियों के मामले में बढ़ती मांग) की वास्तविक क़ीमतों का हिस्सा सकारात्मक निकला, जिसने कृषि विकास में अहम योगदान दिया। इस सुधार अवधि के दौरान उत्पादन क़ीमतों और फॉसल विविधीकरण का योगदान कृषि के विकास में बढ़ा। यह स्थिति इस समय भी वैसी है बनी हुई है। इसके बजाय, समय के साथ विविधीकरण और क़ीमतों की अहमियत बढ़ गयी है।
ऊपर के विचार-विमर्श से हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भारत में सभी कृषि क्षेत्र के हितधारकों की तरफ़ से एमएसपी के लिए इतनी मांग क्यों है। हालांकि, इस व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है।
सरकार ने 22 अनिवार्य फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफ़आरपी) की घोषणा की। अनिवार्य फ़सलों में ख़रीफ़ मौसम की 14 फसलें, छह रबी फ़सलें और दो अन्य व्यावसायिक फसलें हैं। इसके अलावा, तोरिया और छिलके वाले नारियल के एमएसपी क्रमशः दलहन/सरसों और कोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किए जाते हैं। फ़सलों की यह सूची इस तरह है:
अनाज (7) - धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
दालें (5) - चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
तिलहन (8) - मूंगफली, रेपसीड/सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजर बीज,
और, कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, भूसी वाला नारियल, गन्ना (उचित और लाभकारी मूल्य), और वर्जीनिया फ्लू कर्ड (VFC) तंबाकू
सुधार की कमियां और सुझाव:
i) कृषि क़ीमतों को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की ज़रूरत है। यह अनुभव किया गया है कि कुछ राज्यों ने केंद्र की ओर से तय की गयी क़ीमतों से भी ज़्यादा क़ीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे विभिन्न फसलों और विभिन्न क्षेत्रों की क़ीमतों में गड़बड़ियां हो रही हैं। ऐसे में राज्यों की ओर से अपनायी जाने वाली नीतियों को राष्ट्रीय नीति के साथ अच्छी तरह से समन्वयित किया जाना चाहिए।
ii) उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने को लेकर प्रोत्साहन क़ीमतों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि बचत के रूप में संसाधन आगे के विकास के लिए उभी पलब्ध हों। सामाजिक वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों ने इस सिलसिले में अक्सर कृषि आय पर कराधान के मुद्दे का ज़िक़्र किया है। इसकी उचित महत्व के साथ जांच-पड़ताल किये जाने की इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि इस मूल्य नीति का लाभ मुख्य रूप से उन बड़े किसानों को मिला है, जो बड़े ऋण और निवेश को हासिल कर सकते हैं।
iii) मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता के विचारों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना है। छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास छोटी जोत और निवेश की छोटी हैसियत है, वे इस मूल्य प्रोत्साहन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ग़रीब किसानों के लिये गये कर्ज़ बड़े पैमाने पर नहीं चुकाये जा सके हैं, और खेती उनके लिए व्यावहारिक नहीं रह गया है। हाल के दिनों में किसानों की आत्महत्या के मामलों की बढ़ती संख्या इस लिहाज़ से एक संकेत देने वाला कारक है। ऐसे किसानों को वित्तीय और ढांचागत प्रोत्साहन के रूप में ग़ैर-मूल्य प्रोत्साहन के ज़रिये उचित सहायता मिलनी चाहिए।
iv) मांग और लागत दोनों ही पक्षों के कारकों पर विचार करते हुए मूल्य निर्धारण को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक होना चाहिए। बीज, उर्वरक, बिजली, पानी, प्रसंस्करण, बाज़ार शुल्क आदि जैसे विभिन्न निवेशों की लागत और उपलब्धता का ठीक से अनुमान लगाया जाना चाहिए। पारिवारिक श्रम की लागत, स्वामित्व वाली अचल पूंजी पर ब्याज़ और स्वामित्व वाली भूमि के किराये के मूल्य की गणना में सावधानी बरती जानी चाहिए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर और दूसरे ग़ैर-मूल्य उपायों के सिलसिले में सिफ़ारिशों को तैयार करने में आयोग, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के अलावा, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना और विशेष वस्तु या वस्तुओं के समूह और ख़ासकर उत्पादन की लागत, इनपुट कीमतों में परिवर्तन, इनपुट-आउटपुट मूल्य समता, बाजार की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर-फसल मूल्य समता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, जीवन की लागत पर प्रभाव, प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, भुगतान की गयी क़ीमतों और किसानों को मिली क़ीमतों के बीच समानता जैसे व्यापक नज़रिये को ध्यान में रखता है।
निर्गम मूल्यों पर प्रभाव और सब्सिडी के निहितार्थों को समझने के लिए आयोग ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म-स्तरीय डेटा और समुच्चय दोनों का इस्तेमाल करता है। आयोग की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली सूचना/डेटा में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होते हैं:
- प्रति हेक्टेयर खेती की लागत और देश के विभिन्न क्षेत्रों में ख़र्च की संरचना और उसमें हो रहे बदलाव;
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति क्विंटल उत्पादन लागत और उसमें हो रहे बदलाव;
- विभिन्न निवेशों की क़ीमतें और उनमें हो रहे बदलाव;
- उत्पादों के बाजार मूल्य और उनमें परिवर्तन;
- किसानों द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की कीमतें और उनमें परिवर्तन;
- आपूर्ति संबंधी जानकारी - क्षेत्र, उपज और उत्पादन, आयात, निर्यात और घरेलू उपलब्धता और सरकार/सार्वजनिक एजेंसियों या उद्योग के पास स्टॉक;
- प्रसंस्करण उद्योग की कुल और प्रति व्यक्ति खपत, रुझान और क्षमता जैसी मांग सम्बन्धित जानकारियां;
- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क़ीमतें और उसमें हो रहे बदलाव, विश्व बाज़ार में मांग और आपूर्ति की स्थिति;
- चीनी, गुड़, जूट के सामान, खाद्य/अखाद्य तेल और सूती धागे जैसे कृषि उत्पादों के डेरिवेटिव की क़ीमतें और उनमें हो रहे बदलाव;
- कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की लागत और उसमें हो रहे बदलाव;
- विपणन- भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, विपणन सेवायें, कर/शुल्क और बाज़ार पदाधिकारियों की ओर से बनाये रखे गये मार्जिन की लागत; और
- क़ीमतों का सामान्य स्तर जैसे मैक्रो-इकोनॉमिक वैरिएबल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को दर्शाते हैं और वे कारक, जो मौद्रिक और राजकोषीय कारकों को दर्शाते हैं।
गन्ने के लिए मूल्य निर्धारण नीति:
गन्ने का मूल्य निर्धारण असल में अक्टूबर 2009 में संशोधित गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों से नियंत्रित होता है। एसएमपी की अवधारणा को गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) से बदल दिया गया था। उसके आधार पर सीएसीपी को नियंत्रण आदेश में सूचीबद्ध सांविधिक कारकों के सिलसिले में नीचे दिये गये कारकों को ध्यान में रखते हुए भुगतान करना ज़रूरी है:
गन्ने के उत्पादन की लागत; वैकल्पिक फ़सलों से उत्पादक को होने वाला फ़ायदा और कृषि वस्तुओं की क़ीमतों की सामान्य प्रवृत्ति; उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता; चीनी की क़ीमत; गन्ने से चीनी बनने की दर; शीरा, खोई और पेड़ाई के बाद गन्ने का बचा हुआ अवशेष या उनका आरोपित मूल्य (दिसंबर 2008 में डाला गया) जैसे उप-उत्पादों की बिक्री से होने वाली प्राप्ति और जोखिम और मुनाफे के चलते गन्ने के उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन (अक्टूबर 2009 में डाला गया)।
आयोग का यह काम प्राथमिक महत्व वाला है। जहां आयोग की पहुंच गुणवत्तापूर्ण आंक़ड़ों तक होना ज़रूरी है, वहीं प्रभावित होने वाले किसानों, ख़ास तौर पर किसान संगठनों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श से सम्बन्धित इसके नज़रिये का उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है।
लेखक पश्चिम बंगाल सरकार में पूर्व प्रधान सचिव (कृषि) रहे हैं। इनके व्यक्त विचार निजी हैं।
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।