क्या सूचना का अधिकार क़ानून सूचना को गुमराह करने का क़ानून बन जाएगा?
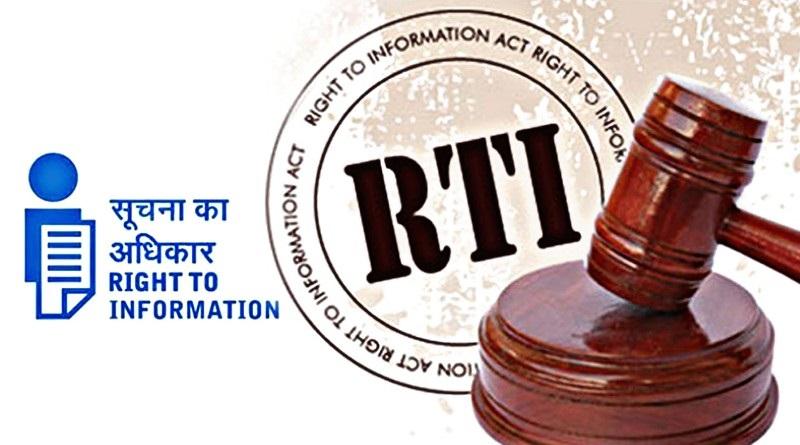
संसद द्वारा पारित और प्रख्यापित सबसे बेहतरीन पारदर्शी क़ानूनों में से एक को अब न्यायिक निर्णयों और व्याख्याओं के घेरे से खतरा पैदा हो है जो व्याख्याएँ क़ानून के अनुरूप नहीं हैं और इसे कमजोर कर देंगी। शैलेश गांधी लिखते हैं, यदि क़ानून के दायरे को व्यापक बनाने और छूट देने को अधिक महत्व दिया जाता है, तो लोकतंत्र के लिए इसके दुखद परिणाम होंगे।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1975 से 2005 तक लगातार इस बात को माना है कि सूचना का अधिकार (RTI) नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। 2005 में, संसद ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पारदर्शिता वाले क़ानूनों में से एक को लागू किया था। हालांकि, पिछले दशक में अदालतों द्वारा दिए गए कुछ फैसलों और इसकी व्याखाओं से इस शक्तिशाली मौलिक अधिकार के कमजोर होने के आसार नज़र आते हैं। इन पर आरटीआई का इस्तेमाल करने वालों और क़ानूनी बिरादरी को चर्चा करनी चाहिए।
सूचना आयोग के निर्णयों को चुनौती देना
क़ानून के मुताबिक आयोग के निर्णयों के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता है। हालांकि, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार करने के मामले में कई सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालयों में इन फैसलों को चुनौती दी जा रही है। इनमें से अधिकांश मामलों में, एक्स-पार्टी स्टे मिल जाता है।
कई बार आयोग के सामने आए मामलों की जांच करने उसे रोक दिया जाता है। अधिकतर ऐसे मामले अपनी मौत मर जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर आवेदक संसाधनों की कमी चलते अदालतों में प्रभावी तरीके से इनकी वकालत नहीं कर पाते हैं।
न्यायालय को इस बात की प्रथम दृष्टया जांच करनी चाहिए कि क्या मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और अगर स्टे नहीं दिया गया तो क्या सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई अपरिवर्तनीय हानि हो सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि किसी भी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक आदेश के मामले के पीछे के जरूरी कारण बताए जाने चाहिए।
सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना देने पर रोक लगाने वाले आदेश देते वक़्त उच्च न्यायालय को स्टे देने के पीछे के जरूरी कारणों को भी बताना चाहिए और यह भी कि याचिका न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कैसे आती है।
लोकतंत्र में, नागरिक सरकार के शासक होते हैं और इस प्रकार, सभी जानकारी के सार्वजनिक रिकॉर्ड के मालिक भी होते हैं। क़ानून में बिना किसी रोक-टोक के अधिकांश सूचनाओं को मुहैया कराने के मजबूत प्रावधान हैं और आरटीआई अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि इसके प्रावधान पहले के अन्य क़ानूनों से ऊपर हैं। यह निर्धारित करता है कि सूचना न देना केवल धारा 8 या 9 के प्रावधानों पर आधारित हो सकता है। इसके अलावा, किसी भी अपील की कार्यवाही में सूचना को अस्वीकार करने का औचित्य या अधिकार केवल लोक सूचना अधिकारी पर है। जानकारी से इनकार करने का मामला दुर्लभ होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले
आरटीआई अधिनियम के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे बहुत कम निर्णय हैं जिनमें सूचना देने के आदेश दिए गए है। जबकि बहुमत निर्णय जानकारी देने से इनकार करने के लिए दिए गए हैं और वे निर्णय छूट के दायरे का विस्तार भी करते हैं। इस उदाहरण के लिए हम शीर्ष अदालत के तीन फैसले लेते हैं:
लोकतंत्र में, नागरिक सरकार के शासक होते हैं और इस प्रकार, सभी जानकारी के सार्वजनिक रिकॉर्ड के मालिक भी होते हैं। क़ानून में बिना किसी रोक-टोक के अधिकांश सूचनाओं को मुहैया कराने के मजबूत प्रावधान हैं और आरटीआई अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि इसके प्रावधान पहले के अन्य क़ानूनों से ऊपर हैं।
*2011 की अपील नंबर 6454 में, न्यायालय ने कहा था कि: "कुछ उच्च न्यायालयों ने माना है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 धारा 3 के अपवाद के रूप में है जो नागरिकों को सूचना के अधिकार के साथ सशक्त बनाता है, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लिया गया है; और इसलिए धारा 8 को कड़ाई से, शाब्दिक और संकीर्ण रूप से माना जाना चाहिए। यह सही तरीका नहीं हो सकता है।” मुझे लगता है कि पहले के दृष्टिकोण में, छूट की व्याख्या संकीर्ण तरीके से की गई थी क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की काट-छाँट करते हैं।
निर्णय में एक अन्य मजबूत बयान इस प्रकार है:
“सभी और विविध जानकारी की मांग के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अंधाधुंध और अव्यवहारिक मांग या निर्देश (सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए असंबंधित और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अंधाधुंध और अव्यवहारिक मांग या दिशा-निर्देश) इस अधिकार के मक़सद के विरुद्ध होंगे क्योंकि यह प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और परिणामस्वरूप कार्यपालिका सूचना एकत्र करने और प्रस्तुत करने के गैर-उत्पादक कार्यों में लगी रहेगी। अधिनियम का दुरुपयोग या गलत उपयोग नहीं होने दिया जाना चाहिए, और न ही उसे राष्ट्रीय विकास और एकीकरण में बाधा डालने, या नागरिकों के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट करने का उपकरण बनने देना चाहिए। न ही इसे अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास करने वाले ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न या धमकी के उपकरण में बदलने देना चाहिए। राष्ट्र ऐसा परिदृश्य नहीं चाहता है जहां 75 प्रतिशत सार्वजनिक प्राधिकरणों के कर्मचारी अपने नियमित कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय आवेदकों के लिए जानकारी एकत्र करने और उन्हे प्रस्तुत करने में अपना 75 प्रतिशत समय लगाएँ।”
मौलिक अधिकार का प्रयोग करने वाले नागरिकों के खिलाफ इस तरह के आरोप को किसी भी केस के संबंध के बिना और बिना किसी सबूत के लगाया गया था। इसे आतंकवादियों पर निर्देशित किया जाता तो समझ में आता।
एक एनजीओ, आरएएजी फाउंडेशन के एक अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 50 प्रतिशत ही आरटीआई आवेदन किए जाते हैं क्योंकि विभाग आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, जो क़ानून के अनुसार अधिकांश सूचना देने की अनुमति देता है। अन्य 25 प्रतिशत आरटीआई में राशन कार्ड जारी जारने में देरी, विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए किए गए आवेदन में हुई प्रगति या अवैध गतिविधियों की शिकायत के बारे में जानकारी मांगते हैं, जिनके लिए सरकारी विभागों को जवाब देना होता है। उन अधिकारियों की कोई निंदा नहीं की गई है जो बिना घूस के अपना काम नहीं करते हैं। यह बिना किसी सबूत या आधार के नागरिक के ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण लांछन था।
*गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य (2013) के मामले में, न्यायालय ने कहा कि एक लोकसेवक को मिले मिमोज/ज्ञापनों, कारण बताओ नोटिस और सस्पेंशन/सजा, के आदेश, संपत्तियां, आय विवरणी, प्राप्त उपहारों के विवरण की प्रतियां इत्यादि व्यक्तिगत जानकारी हैं, जिनकी जानकारी न देने की छूट धारा 8 (1) (जे) आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दी गई है।
निर्णय आगे कहता है कि ये कर्मचारी और नियोक्ता के बीच के मामले हैं, बिना यह महसूस किए कि नियोक्ता एक नागरिक है, वह लोकतंत्र का मालिक है जो सरकार को वैधता प्रदान करता है। इस फैसले में कोई क़ानूनी तर्क या सिद्धांत नहीं है और यह केवल सूचना आयोग द्वारा सूचना न देने पर आधारित है।
आरटीआई अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे बहुत कम निर्णय हैं जिनमें सूचना देने के आदेश दिए है। जबकि अधिकांश निर्णय जानकारी देने से इनकार करते हैं और छूट के दायरे का विस्तार करते हैं।
1994 में सुप्रीम कोर्ट के आर.राजगोपाल द्वारा दिए गए फैसले से स्पष्ट है कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रिकॉर्ड पर व्यक्तिगत जानकारी के मामले में गोपनीयता का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि न्यायालय ने इस निर्णय पर विचार नहीं किया है।
धारा 8 (1) (जे) में एक प्रावधान है कि "जिसके मुताबिक ऐसी कोई भी सूचना जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है" उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। फैसले में इस प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कोई भी ऐसा शब्द जिससे न्यायालय संतुष्ट हो कि इस जानकारी को संसद या राज्य विधायिका को प्रदान नहीं की जाएगा।
*सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च, 2020 को एक सिविल अपील संख्या 1.1666667/2020 में एक निर्णय दिया था, जो आरटीआई अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रावधान की उपेक्षा करता है। जिसके मुताबिक वह यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र के शासकों यानि जनता को जानकारी देने से इनकार करने के मामले में अन्य क़ानूनों और बाधाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, संसद ने धारा 22 में एक गैर-अवरोधक खंड प्रदान किया है जिसमें कहा गया है: "इस अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद ओफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 में निहित कुछ असंगत प्रभाव के बावजूद यह प्रभावी रहेगा और इस क़ानून की तुलना में कोई भी अन्य क़ानून जो लागू है या किसी उपकरण पर इसका असर है वह प्रभावी नहीं होगा।"
आरटीआई अधिनियम से हुए गुमराह
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अदालत के नियम जो आरटीआई अधिनियम से काफी हद तक विचलित हैं, उन्हें क़ानून के साथ असंगत नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उनके पास जानकारी देने का प्रावधान न हो! इसने इस तथ्य पर विचार करने से इनकार कर दिया कि ऐसा आरटीआई अधिनियम द्वारा स्वीकृत शर्तों को लागू करने के परिणामस्वरूप होगा। यह वास्तव में धारा 22 को समाप्त करने के प्रभाव में कहा गया है।
2011 की अपील संख्या 6454 में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि: "अधिनियम का दुरुपयोग या दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए, न ही राष्ट्रीय विकास और एकीकरण में बाधा डालने, या उसके नागरिकों के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट करने का उपकरण बनने देना चाहिए। न ही इसे अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास करने वाले ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न या धमकी के उपकरण में बदलने देना चाहिए।”
न्यायालयों को आरटीआई की पहुंच और दायरे का विस्तार करने में सक्रिय भाग लेना चाहिए। उन्हें इस तथ्य के बारे में सचेत होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रकाशन की जानकारी सभी अनुच्छेद 19 (1) (ए) से उत्पन्न होती हैं और उन्हें बराबर माना जाना चाहिए। पहले दो का विस्तार अदालतों द्वारा किया गया है, जबकि पिछले 15 वर्षों में सूचना के अधिकार को न्यायिक निर्णयों ने सीमित कर दिया गया है।
पारदर्शिता पर सबसे बेहतरीन क़ानूनों में से एक जिसे संसद ने पारित किया और लागू किया था, वह अब न्यायिक व्याख्याओं के खतरे से घिर गया जो इस क़ानून के मक़सद के अनुरूप नहीं हैं। यदि वे आरटीआई अधिनियम की व्याख्या छूट और इसके दायरे को बढ़ाने के महत्व को अधिक देकर करते है तो यह महान क़ानून जिसे "सूचना का अधिकार कहा जाता है वह सूचना न देने का क़ानून" बन सकता है। यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद परिणाम होगा।
नागरिक समाज और क़ानूनी पेशे से जुड़े वर्ग भी इस तथ्य के प्रति अभी सचेत नहीं है कि अगर सूचना के अधिकार को बाधित किया जाता है, तो अभिव्यक्ति और प्रकाशन की स्वतंत्रता को भी ऐसी ही बाधाओं को झेलना होगा।
यह लेख The Leaflet. में प्रकाशित हो चुका है।
(शैलेश गांधी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं और एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें
Will the Right to Information Act Become the Right to Denial of Information Act?
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।






















