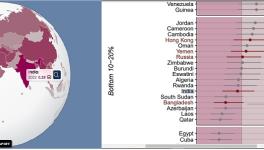ब्राह्मणों को रिझाना यानी आदित्यनाथ के जाल में फंसना

राज्य में नई विधानसभा के चुनाव होने से ठीक छह महीने पहले, उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख विपक्षी दल - बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी- कोविड-19 द्वारा बरपाई गई भयावह बरबादी की पृष्ठभूमि में, ब्राह्मणों को लुभाना अतीयथार्थवादी या अजीब सा लगता है, एक ऐसा तबका जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे दृढ़ समर्थक हैं।
शायद लगता है कि राजनीतिक वर्ग को इस बात का एहसास है कि लोग जल्द ही कोविड-19 की त्रासदी को भूल जाएंगे और इस बात को भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वायरस का मुकाबला करने और उन्हें सहायता देने में विफल रहे हैं। अगर ऐसा है तो अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश जाति के बारे में सोचेगा और फिर से जाति के आधार पर मतदान करेगा।
इस संबंध में, ब्राह्मण अन्य जातियों से कुछ भिन्न नहीं हैं। आदित्यनाथ से ब्राह्मण जाति का अलगाव महसूस करने का बड़ा कारण यह बताया जाता है कि उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखा गया है। आदित्यनाथ जोकि एक राजपूत जाति से है, उन पर अपनी जाति के सदस्यों को ब्राह्मणों के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करते हुए सत्ता में तैनात करने का भी आरोप लगा है। इस मामले में गैंगस्टर विकास दुबे और एप्पल के अफसर विवेक तिवारी की हत्या को सबूत के तौर पर माना जा रहा है।
बसपा नेता मायावती राज्य भर में ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन करके इस अलगाव का फायदा उठाने की उम्मीद कर रही हैं, जिनमें से पहला सम्मेलन पिछले हफ्ते अयोध्या में किया गया था। उन्होने उनसे "निष्पक्ष सौदे" का वादा किया है, जिसके तहत राम मंदिर के निर्माण में तेजी लाई जाएगी और भगवान परशुराम की एक मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, जिन्हे ब्रहमाण विष्णु के छठे अवतार के रूप में मानते हैं, जो समाजवादी पार्टी के वादे से 108 फुट अधिक लंबा होगा। इसका अनुसरण करते हुए, सपा नेता अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को समुदाय को सपा के समर्थन में रैली/सम्मेलन आयोजित करने का फरमान जारी किया है।
मायावती और यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग, जिनमें ब्राह्मण भी शामिल हैं, उन अन्यायों को याद करने के मामले में अधिक इच्छुक हैं, जिन्हें माना जाता है कि जाति के नाम पर किया गया है न कि सार्वभौमिकों मुद्दों – जो हर सामाजिक समुदाय का मुद्दा हो सकता है और उन्हे प्रभावित करता है - जैसे कि आदित्यनाथ की कोविड-19 का मुकाबला करने में विफलता – जो विफलता गंगा के तट पर सामूहिक कब्रों से पता चलती है।
ऐसा भी लगता है कि वे लोगों को यह बताना जरूरी नहीं समझते कि आदित्यनाथ सरकार नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, 2011 और 2017 के बीच, 6.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा था। मार्च 2019 में आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद, 2017 और 2020 के बीच औसत विकास दर घटकर 5.6 प्रतिशत रह गई है।
सामाजिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का खर्च 14.3 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा था, जो 2011 और 2017 के बीच किए गए खर्च की तुलना में 2.6 प्रतिशत कम है। उनके लिए इस बहस का कोई महत्व नहीं है कि सामाजिक खर्च में कमी इस बात का कारण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 हमले के खिलाफ घुटने टेक दिए थे। न ही उनकी नज़रों में इस बात का महत्व है या कोई राजनीतिक मूल्य है कि 7 फरवरी 2020 तक, 33.94 लाख लोग बेरोजगार के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 30 जून 2018 तक पंजीकृत 21.39 लाख बेरोजगारों की तुलना में 58.43 प्रतिशत की अविश्वसनीय छलांग है।
मायावती की बयानबाजी से ऐसा लगता है कि ऊपर सूचीबद्ध निराशाजनक सांख्यिकीय विवरणों की तुलना में जाति का सही अंकगणित भाजपा सरकार को सत्ता बाहर करने में अधिक निर्णायक भूमिका निभा पाएगा। उन्होंने बार-बार इस बात की चर्चा की है कि कैसे दलित और ब्राह्मण संयोजन ने 2007 में बसपा को सत्ता में लाकर खड़ा कर दिया था।
मायावती पार्टी की 2007 की जीत का विश्लेषण संभवतः ग़लत है।
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के चुनाव सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 2007 में केवल 16 प्रतिशत ब्राह्मणों ने बसपा को वोट दिया था। इसके विपरीत, 86 प्रतिशत जाटव, 71 प्रतिशत वाल्मीकि, 53 प्रतिशत पासी, 58 प्रतिशत अन्य अनुसूचित जातियों और 30 प्रतिशत अन्य ओबीसी (यादवों और कुर्मी/कोरी को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग) जातियों ने बसपा को वोट दिया था। यह उनकी वजह से है, न कि ब्राह्मण समुदाय की वजह से, बसपा ने 403 सीटों वाली विधानसभा में 206 सीटें जीतीं थी।
यह धारणा कि बसपा की जीत में ब्राह्मणों ने निर्णायक भूमिका निभाई, वह इस धारणा से उत्पन्न हुई क्योंकि बसपा के 51 में से 20 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। यद्द्पि उनकी जीत ब्राह्मणों की तुलना में सबाल्टर्न सामाजिक या वंचित तबकों के वोटों से तय हुई थी।
2012 में, बसपा सत्ता से बाहर हो गई थी, भले ही पार्टी को 19 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले थे, जो 2007 के मिले वोट से 3 प्रतिशत अधिक थे। बल्कि हक़ीक़त यह है कि 2012 में दलित मतदाताओं के वोट न देने के कारण बसपा हार गई थी - उदाहरण के लिए, केवल 62 प्रतिशत जाटव और 42 प्रतिशत वाल्मीकियों ने पार्टी को वोट दिया था।
ओलिवर हीथ और संजय कुमार ने अपने 2012 के पेपर जिसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित किया था और जिसका शीर्षक, दलितों ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ा? था, जीमें वे कहते हैं, दलित मायावती की प्रतिकों की राजनीति (उदाहरण के लिए दलित विचारकों के बुत लगाना) से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे सत्ता में 'अपनी' पार्टी के होने से अधिक ठोस लाभ की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि युवा, सुशिक्षित, धनी दलितों का बसपा की प्रतीकात्मकता और राजनीतिक मान्यताओं की राजनीति से प्रभावित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में कम है जो कम शिक्षित और गरीब हैं।
सीएसडीएस ने 2017 के विधानसभा चुनावों में जाति आधार पर वोटिंग पैटर्न को प्रकाशित नहीं किया है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदाताओं का वोट करने का पैटर्न अलग-अलग है, इसलिए बसपा को चिंता इस बात पर करने की जरूरत है कि 2014 के राष्ट्रीय चुनावों में पार्टी के मुख्य आधार जाटवों में से केवल 68 प्रतिशत और अन्य अनुसूचित जातियों में से केवल 29 प्रतिशत ने वोट दिया था। 2019 में, 75 प्रतिशत जाटवों ने महागठबंधन, या सपा-बसपा गठबंधन को मतदान किया था, लेकिन अन्य अनुसूचित जातियों में से केवल 42 प्रतिशत ने ऐसा किया था। जाटव वोटों में वृद्धि काफी हद तक इन उम्मीदों के कारण हुई कि अगर त्रिशंकु लोकसभा बनती है तो मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उनकी इस उम्मीद और उत्साह को अन्य दलित उपसमूहों ने साझा नहीं किया।
ब्राह्मणों के बीच बसपा का समर्थन लगातार गिर रहा है - उनमें से केवल 5 प्रतिशत ने 2014 में बसपा को वोट दिया था, और उनमें से ही करीब 6 प्रतिशत ने 2019 में एसपी-बीएसपी गठबंधन को मतदान किया था। जबकि इसके विपरीत भाजपा ब्रहामण वोट का प्रमुख भंडार रही बनी रही। भाजपा को 2007 में 44 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले, 2014 के लोकसभा चुनाव में 72 प्रतिशत और 2019 में 82 प्रतिशत वोट मिले थे।
इसकी संभावना नहीं है कि बसपा का हाई-वोल्टेज ब्राह्मण सम्मेलन पार्टी को इस प्रभावशाली जाति के वोटों का बड़ा हिस्सा हथियाने में मदद करेगा। जैसा कि हीथ और कुमार एक अन्य संदर्भ में कहते हैं, "पक्षपातपूर्ण समर्थन के समाजीकरण के सिद्धांत इस बात की तसदीक करते हैं कि किसी राजनीतिक दल के प्रति वफादारी समय के साथ मतदान की निरंतर पुनरावृत्ति के माध्यम से मजबूत होती है"।
दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणों की बड़ी संख्या के भाजपा को छोड़ने की संभावना नहीं है। 2007 में भी, जब बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन किया था तो तब भी 44 प्रतिशत ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था, जबकि उससे सत्ता पर कब्जा करने की उम्मीद भी नहीं थी।
चुनावी राजनीति में जाति की अहम भूमिका होती है। लेकिन यह मतदाता के निर्णय लेने का कोई एकमात्र आधार नहीं है। 2012 में, सपा को यादव वोटों का सिर्फ 66 प्रतिशत हिस्सा मिला था, जो पार्टी का मुख्य आधार था, जो 2007 में मिले 72 प्रतिशत से काफी से कम था। बावजूद इसके, उसने 2012 में 224 सीटें इसलिए नहीं जीतीं थी, कि यादवों के बीच उन्होने बेहतर प्रदर्शन किया था, बल्कि इसलिए, जैसा कि हीथ और कुमार बताते हैं, पार्टी "विभिन्न अन्य समुदायों के मतदाताओं को आकर्षित करने" में कामयाब रही थी।
2012 में सपा की जीत से इस बात का पता चलता है कि राजनीतिक दलों के लिए विभिन्न जाति/वर्ग की लामबंदी का विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त जगह है। जातीय गौरव और आघात के मुद्दे के इर्द-गिर्द ब्राह्मण वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने से बेहतर, सपा आज भी अन्य जातियों को लामबंद करने के मामले में एक चुंबक बनने की बेहतर स्थिति में है। उदाहरण के लिए, सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चल रहे किसान आंदोलन का लाभ उठाने की उम्मीद कर सकती है, कम से कम राष्ट्रीय लोक दल के साथ अपने संभावित गठबंधन के कारण, जो किसान/जाट हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
दरअसल, विपक्ष के लिए ब्राह्मणों को लुभाना वैसा ही है जितना कि आदित्यनाथ के जाल में फंसना। पहचान की राजनीति पर जितना अधिक फोकस होगा, उतना ही आदित्यनाथ के कुशासन के रिकॉर्ड के जनता की जांच से बचने की संभावना अधिक होगी। इस तरह का फोकस आदित्यनाथ और भाजपा के 2022 के विधानसभा चुनाव को हिंदु और मुसलमान के बीच की लड़ाई में बदलने में मदद करेगा।
पत्रकार डीके सिंह ने प्रिंट वेबसाइट में लिखे गए एक लेख में बताते हैं कि आदित्यनाथ अपने सार्वजनिक भाषणों में मायावती या यादव की तुलना ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी से क्यों करते हैं। उदाहरण के लिए, जब ओवैसी ने घोषणा की कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की: “ओवैसी जी एक बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। वह चुनाव प्रचार के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं और लोगों के बीच उनकी अपनी साख है। अगर वे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती को स्वीकार करते है।'
जब शासन-प्रशासन एक चुनावी मुद्दा बन जाता है तो ऐसे बयानों की गूंज होने की संभावना नहीं होती है- और इसलिए विभिन्न जातियों/वर्ग को अपील करना और उनकी लामबंदी का मुख्य तरीका बन जाता है। आदित्यनाथ की इस तरह की बयानबाजी इसलिए है कि कहीं विधानसभा चुनाव उनके शासन पर जनमत संग्रह न बन जाए, इसलिए यह किसी चाल से अधिक कुछ नहीं लगती है।
लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।