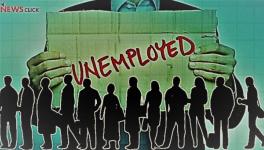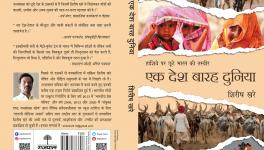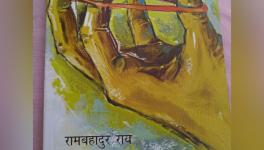उदारवाद का संकट
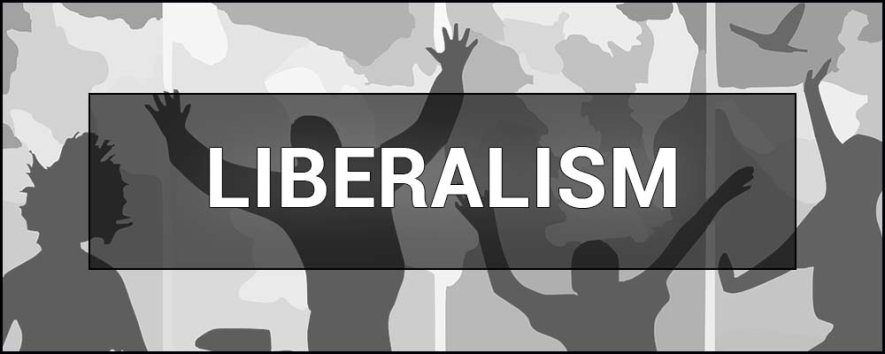
राजनीतिक अमल की हरेक धारा के पीछे एक राजनीतिक दर्शन होता है, जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया और खासतौर पर आधुनिक समय में, उसकी आर्थिक चारित्रिक विशेषताओं का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर संबंधित राजनीतिक दर्शन वे लक्ष्य तय करता है, जिनके लिए संघर्ष करना हो और उस राजनीतिक दर्शन पर आधारित राजनीतिक अमल, इस संघर्ष का संचालन करता है। लक्ष्य हासिल करने में कठिन हो सकता है, कुछ संदर्भों में यह लक्ष्य दूसरे संदर्भों के मुकाबले और ज्यादा कठिन भी हो सकता है और यह कठिनाई, राजनीतिक अमल के लिए बाधा बनकर भी सामने आ सकती है, लेकिन इसे संबंधित राजनीतिक दर्शन के लिए संकट नहीं कहा जाएगा। कोई लक्ष्य हासिल करने में कठिनाई आने को ही, उसके लिए संकट नहीं माना जा सकता है। किसी राजनीतिक दर्शन में संकट तब आता है, जब उसमें कोई आंतरिक अंतर्विरोध होता है; जब इस राजनीतिक दर्शन द्वारा पेश किया जाने वाला लक्ष्य, वह दर्शन जिन चीजों में विश्वास करता है, उनमें से किसी से तार्किक रूप से टकरा रहा होता है।
नव-उदारवाद का आधार क्या है?
बहुत से लोग यह दलील देंगे कि मार्क्सवादी राजनीतिक दर्शन, समाजवाद के जिस लक्ष्य को पेश करता है, वह लक्ष्य आज के संदर्भ में हासिल करने में किसी हद तक कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। लेकिन, इससे वामपंथ के इस समय कमजोर हो जाने को तो समझा जा सकता है, लेकिन इसे किसी तरह से मार्क्सवाद का संकट नहीं माना जा सकता है। बहरहाल, उदारवाद नाम का राजनीतिक दर्शन इस अर्थ में संकट का सामना कर रहा है कि वह जिसे मानव स्वतंत्रता समझता है, उसे हासिल करने के लिए वह जो लक्ष्य पेश करता है, उसे उस दुनिया में हासिल ही नहीं किया जा सकता है, जो खुद उदारवाद को इतनी प्यारी है। दूसरे शब्दों में खुद इस राजनीतिक दर्शन में एक तार्किक अंतर्विरोध है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में निकल कर आया है और जिसका इस राजनीतिक दर्शन के पास कोई जवाब नहीं है। उदारवाद जिस संकट का सामना कर रहा है, इसी प्रकृति का है।
आधुनिक उदारवाद, दो विश्व युद्धों के बीच के पूंजीवादी संकट के दौरान, बोल्शेविक क्रांति के जवाब में, इस पूंजीवादी संकट और भविष्य में पैदा हो सकने वाले ऐसे ही अन्य संकटों के ऐसे समाधान के रूप में विकसित हुआ था, जिसमें पूंजीवाद को लांघा नहीं जाना था। उदारवादी राजनीतिक दर्शन का यह मानना था कि पश्चिमी शैली के उदार जनतंत्र और पूंजीवाद का योग, जो राज्य के हस्तक्षेप से अनुशासित हो, मानव स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बेहतरीन ढांचा है। वह यह मानता था कि पश्चिमी शैली के उदार जनतंत्र की संस्थाओं के अंतर्गत, राज्य एक वर्गीय राज्य न रहने की जगह, सामाजिक विवेक को अभिव्यक्त करता है और वह इसे, दूसरे किसी भी संस्थागत ढांचे के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करेगा। इस तरह, एक उदार जनतांत्रिक राज्य, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर, पूंजीवाद के स्वत:स्फूर्त तरीके से काम करने के चलते, पैदा होने वाली गड़बडिय़ों को दुरुस्त करा सकता है और जहां गड़बड़ी का मामला नहीं हो वहां पूंजीवाद के इस स्वत:स्फूर्त तरीके से काम करने को, सामाजिक विवेक के तकाजों के अनुरूप बनाने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है। उदारवाद का यह रूप, जिसकी स्थापना में अंग्रेज अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड केन्स ने एक प्रमुख भूमिका अदा की थी और जिसे केन्स ने नव-उदारवाद का नाम दिया था, उदारवाद के इससे पहले के रूपों से इस माने में भिन्न था कि वे इसके पक्ष में थे कि राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम पर रखा जाए। उनका यह विश्वास इससे पहले तक हावी रही इस भ्रांतिपूर्ण धारणा पर आधारित था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा ही, पूर्ण रोजगार के आधार पर संचालित होती है।
पूंजी का वैश्वीकरण और नव-उदारवाद का संकट
उदारवाद का यह नया रूप, यहां हम खुद उसके द्वारा ही संकल्पित संस्थागत ढांचे के अंदर उसकी वैधता में नहीं जा रहे हैं (बेशक इस लिहाज से वह पूरी तरह से अवैध था और अन्य चीजों के अलावा साम्राज्यवाद की उस परिघटना के चलते बिल्कुल अवैध था, जिस परिघटना को तो यह पहचानता तक नहीं था), अब तो निश्चित रूप से अपनी वैधता खो चुका है, जब पूंजी का, जिसमें वित्त भी शामिल है, वैश्वीकरण हो गया है। इसकी वजह यह है कि अब यह स्थिति नहीं रह गयी थी कि कोई राष्ट्र-राज्य पूंजी के सिर पर बैठा हो, जो पूंजी खुद बुनियादी तौर पर राष्ट्रीय होती थी। अब तो एक राष्ट्र-राज्य के वैश्वीकृत पूंजी के आमने-सामने होने की स्थिति है। और इस तरह की किसी भी मुठभेड़ में राष्ट्र राज्य को वैश्वीकृत पूंजी की मांगों को स्वीकार करना ही होता है, अन्यथा पूंजी का पलायन हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पक्के से पक्के नव-उदारवादी भी यह स्वीकार करेंगे कि राज्य अब सामाजिक विवेक की मूर्ति के रूप में काम कर ही नहीं सकता है।
इसे जरा भिन्न तरीके से कहें तो, ‘नव-उदारवाद’ के पीछे पूर्वधारणा यह थी कि वह क्षेत्र, जिस पर राज्य का हुक्म चलता है और वह क्षेत्र जिसमें संबंधित देश से निकली पूंजी काम करती है, कमोबेश एक ही हैं। वास्तव में, जब केन्स लिख रहे थे तब और काफी बाद तक भी, यही स्थिति थी। लेकिन, पूंजी का वैश्वीकरण बढ़ने के साथ, इस पूर्वधारणा ने अपनी वैधता खो दी है। और जब ऐसा होता है, उस सूरत में यह दिखावा तक करना गैर-यथार्थवादी हो जाता है कि देश की कार्यपालिका को जनमत के जरिए कोंच-कोंच कर इसके लिए आगे बढ़ाया जा सकता है कि ऐसे तरीके से काम करे, जो उसके विचार से सामाजिक रूप से विवेकपूर्ण हो, फिर भले ही वैश्वीकृत पूंजी, उसके कदम से सहमत हो या नहीं हो।
इसलिए, उदारवाद के संकट की जड़ें वैश्वीकरण की परिघटना में हैं। लेकिन, यह संकट साफ तौर पर नव उदारवाद के संकट के दौर में खुद को अभिव्यक्त कर रहा है, जब बड़े पैमाने पर जन बेरोजगारी निकल कर सामने आ गयी है। इसी को तो केन्स पूंजीवाद की दुखती रग समझते थे और यह मानते थे कि अगर राज्य के हस्तक्षेप के जरिए बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था ही बोल्शेविक किस्म की क्रांति के लिए वेध्य हो जाएगी।
केन्सवादी किस्म के मांग प्रबंधन की नहीं रही गुुंजाइश
पूंजीवाद अधिउत्पादन के जिस संकट से ग्रस्त होता है, उस पर काबू जिस केन्सवादी ‘मांग प्रबंधन’ से पाया जा सकता है, उसका यह तकाजा होता है कि राज्य द्वारा बढ़े हुए खर्चे के लिए संसाधन या तो अमीरों पर ज्यादा कर लगाकर जुटाए जाएं या फिर कोई अतिरिक्त कर लगाए बिना ही यानी बढ़े हुए राजकोषीय घाटे का सहारा लेकर जुटाए जाएं। राज्य द्वारा बढ़े हुए खर्चे के लिए संसाधन अगर मेहनतकश जनता पर बोझ डालकर जुटाए जाएंगे, जो वैसे भी अपनी आय का अधिकांश हिस्सा उपभोग पर खर्च करती है, इस तरह के राज्य के बढ़े हुए खर्चे से सकल मांग में बढ़ोतरी नहीं होगी और इसलिए संकट से उबरने में भी मदद नहीं मिलेगी। लेकिन, राज्य द्वारा अतिरिक्त खर्च किए जाने के लिए संसाधन जुटाने के पीछे बताए गए दोनों तरीकों यानी अमीरों पर कर बढ़ाना और राजकोषीय घाटा बढ़ाना दोनों का, वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी विरोध करती है और इस तरह, इस संकट के खिलाफ राज्य द्वारा राजकोषीय हस्तक्षेप किए जाने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। बेशक, राज्य इसके बाद भी मौद्रिक औजारों से हस्तक्षेप कर तो सकता है, लेकिन जैसाकि सभी जानते हैं, ये औजार बहुत ही भोंथरे साबित होते हैं और अक्सर मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, और यह बढ़े हुए निजी निवेश को उत्प्रेरित करने के बजाए, संकट को बढ़ाने का ही काम करता है। इसलिए, नव-उदारवाद के दायरे में इस संकट पर काबू पाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यहां केन्स का नव-उदारवाद फेल हो जाता है। इसलिए, नव-उदारवादी आर्थिक निजाम का बंद गली में पहुंच जाना, उदारवाद के राजनीतिक दर्शन का ही संकट बन जाता है।
नव-उदारवादी निजाम के बंद गली में पहुंच जाने को, यूरोप के उदाहरण से समझा जा सकता है। सत्तर के दशक के मध्य तक, यूरोपियन यूनियन के देशों में (जिनकी संख्या तब 15 थी) बेरोजगारी की दर लंबे समय से 3 फीसद से भी नीचे चली आ रही थी। सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध में तथा अस्सी के दशक में वैश्वीकरण के आगे बढ़ने के साथ, वहां बेरोजगारी की दर ऊपर चढऩी शुरू हो गयी और उसके बाद से मोटे तौर पर 7 फीसद से ऊपर बनी रही है, हालांकि विभिन्न देशों के बीच इस मामले में भिन्नताएं भी बनी रही हैं। और राज्य का हस्तक्षेप, बेरोजगारी की इस बढ़ी हुई दर को नीचे लाने में असमर्थ रहा है।
राष्ट्र-राज्य के हाथ बंधे हुए हैं
जब सामना वैश्वीकृत पूंजी से है, कोई राष्ट्र-राज्य अकेले-अकेले सकल मांग को बढ़ाने और बेरोजगारी घटाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में यही रास्ता रह जाता है कि या तो संबंधित देश वैश्वीकृत वित्त के संजाल से बाहर ही निकल जाने के लिए पूंजी नियंत्रण लगा दे या फिर अन्य देशों के साथ मिलकर तालमेलबद्ध तरीके से राजकोषीय उत्प्रेरण लाए, जिससे मांग का विस्तार करने वाले किसी भी देश से, उड़न छू हो जाने की पूंजी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। अगर सभी देश राज्य के खर्चे को बढ़ाने की एक समान नीति का पालन कर रहे होंगे, तो पूंजी उडऩ छू होकर कहां जाएगी! इनमें से पहले रास्ते का मतलब है, नव-उदारवादी निजाम के दायरे से बाहर जाना। पूंजी नियंत्रणों के साथ देर-सबेर व्यापार नियंत्रण भी आवश्यक हो जाएंगे और इसका अर्थ यह है कि नव-उदारवादी निजाम के बुनियादी चरित्र पर ही यानी पूंजी तथा मालों व सेवाओं के अपेक्षाकृत बेरोक-टोक प्रवाहों की उसकी मूल विशेषता पर ही जंजीरें पड़ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी इसका हर चंद विरोध करेगी। इसलिए, ऐसा रास्ता अपनाने के लिए तो वैकल्पिक वर्गीय गोलबंदी की जरूरत होगी और ऐसी गोलबंदी खुद को इजारेदार पूंजीवाद की हिफाजत करने के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रख सकती है।
जहां तक इनमें से दूसरे रास्ते का सवाल है, अगर इसे तमाम देशों के बीच सच्चे तालमेल पर आधारित राजकोषीय उत्प्रेरण बनना है, तो इसके लिए जिस दर्जे के अंतर्राष्ट्रवाद की जरूरत होगी, वह पूंजीवाद तो प्रदर्शित कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें तो आर्थिक हाशिए पर हावी होने की प्रवृत्ति तो हमेशा समायी ही रहती है। इसलिए, पूंजीवाद से ज्यादा से ज्यादा इसी की उम्मीद की जा सकती है कि विकसित देशों में तालमेल के साथ राजकोषीय उत्प्रेरण लाए, जबकि आर्थिक हाशिए या विकासशील दुनिया पर राजकोषीय कमखर्ची थोपता रहे। और इसका मतलब होगा, साम्राज्यवाद का शिकंजा कसना। पूंजीवाद इसकी कोशिश कर तो सकता है, लेकिन साम्राज्यवाद के शिकंजे के इस तरह कसने को उदारवाद अपनी कामयाबी की निशानी तो नहीं बना सकता है। उल्टे इसका अर्थ तो उदारवाद खुद को जिस रूप में पेश करता है, उसकी शिकस्त ही है। आखिर, वह तो खुद को मानव स्वतंत्रता का वैकल्पिक गैर-समाजवादी रास्ता बनाकर ही पेश करता है।
उदारवाद का आंतरिक संकट
उदारवाद की यह दुर्दशा ही उसका संकट है। जब तक बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बनी हुई है, जो मजदूरी को भी नीचे दबाए रखती है, आम गतिरोध पैदा करती है या मजदूरों की दशा बदतर करती है। उदारवाद इस भौतिक यथार्थ से, नव-उदारवादी पूंजीवाद को लांघे बिना उबर नहीं सकता है और इसके लिए एक ऐसे वर्गीय गठबंधन की जरूरत होगी, जो अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद के दायरे से ही बाहर ले जाएगा। नव-उदारवाद पूर्व के पूंजीवाद पर लौटने की बातें ऐसी ही हैं, जैसे इजारेदार पूंजीवाद की बुराइयों से उबरने के लिए चिर-मिथकीय ‘मुक्त प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद’ पर लौटने की बातें, जिनकी लेनिन ने अपनी पुस्तक, इंपिरियलिज्म में अच्छी तरह खबर ली है। बेरोजगारी कम करने के लिए, महानगरीय देशों के बीच ही किसी ऐसे तालमेल युक्त राजकोषीय उत्प्रेरण के लिए कोई भी रजामंदी, जो हाशिए वाले देशों को बाहर ही रखकर चलता हो, उदारवाद जिन मूल्यों की पक्षधरता का दावा करता है, उनके साथ ही विश्वासघात करना होगा।
शास्त्रीय उदारवाद, तीस के दशक की महामंदी के दौरान विफल हो गया था। केन्सवाद या नव-उदारवाद, नव-उदारवाद के संकट के दौर में विफल हो गया है। और उदारवाद के कोई दूसरे प्रारूप न तो उपलब्ध हैं और न ही संभव हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं को उनके पूंजीवादी खोल में बनाए रखते हुए भी, उन्हें अपने वर्तमान गतिरोध से निकाल भी सकते हों।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।